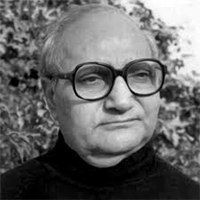श्रीलाल शुक्ल के उद्धरण

योग्य आदमियों की कमी है। इसलिए योग्य आदमी को किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वह एक ओर छूटता है तो दूसरी ओर से पकड़ा जाता है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

किसान को—जैसा कि ‘गोदान’ पढ़नेवाले और दो बीघा ज़मीन' जैसी फ़िल्में देखनेवाले पहले से ही जानते हैं—ज़मीन ज़्यादा प्यारी होती है। यही नहीं, उसे अपनी ज़मीन के मुक़ाबले दूसरे की ज़मीन बहुत प्यारी होती है और वह मौक़ा मिलते ही अपने पड़ोसी के खेत के प्रति लालायित हो उठता है। निश्चय ही इसके पीछे साम्राज्यवादी विस्तार की नहीं, सहज प्रेम की भावना है जिसके सहारे वह बैठता अपने खेत की मेड़ पर है, पर जानवर अपने पड़ोसी के खेत में चराता है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

हमारे अधिकांश उपन्यास अति सामान्य प्रश्नों (ट्रीविएलिटीज) से जूझते रहते हैं और उनसे हमारा अनुभूति-संसार किसी भी तरह समृद्ध नहीं होता।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

दिन-रात गर्द के बवंडर उड़ाती हुई जीपों की मार्फ़त इतना तो तय हो चुका है कि हिंदुस्तान, जो अब शहरों ही में बसा था, गाँवों में भी फैलने लगा है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

हमारे न्याय-शास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ-जहाँ धुआँ होता है, वहाँ-वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ बस का अड्डा होता है, वहाँ गंदगी होती है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

तुम मँझौली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फँस गये हो। तुम्हारे चारो ओर कीचड़-ही-कीचड़ है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

तर्क और आस्था की लड़ाई हो रही थी और कहने की ज़रूरत नहीं कि आस्था तर्क को दबाए दे रही थी।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया


हमारे साहित्य में एक बहुचर्चित स्थापना यह है कि भारतीय उपन्यास मूलतः किसान चेतना की महागाथा है—वैसे ही जैसे उन्नसवीं सदी के योरोपीय उपन्यास को मध्यम वर्ग का महाकाव्य कहा गया था।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

भारत जैसे विराट मानवीय क्षेत्र के अनुभवों, गहरी भावनाओं, आशाओं, आकांक्षाओं और यातनाओं आदि को हमारा उपन्यास अभी अंशतः ही समेट पाया है—और जितना तथा जिस प्रकार उसे समेटा गया है उसमें प्रतिभा एवं कौशल के कुछ दुर्लभ उदाहरणों को छोड़कर, अब भी बहुत अधकचरापन है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

विरोधी से भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। देखो न, प्रत्येक बड़े नेता का एक-एक विरोधी है। सभी ने स्वेच्छा से अपना-अपना विरोधी पकड़ रखा है। यह जनतंत्र का सिद्धांत है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया


कीचड़ की चापलूसी मत करो। इस मुग़ालते में न रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता है। कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है। यह जगह छोड़ो। यहाँ से पलायन करो।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया



‘झूठा सच’ उन दुर्लभ कृतियों में से है जो ठोस, यथार्थवादी स्तर पर, भावुकता के सैलाब में बहे बिना इस भयानक मानवीय त्रासदी को अत्यंत सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया


वर्तमान शिक्षा-पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है, जिसे कोई भी लात मार सकता है।
-
संबंधित विषय : सिस्टम
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया




‘मैला आँचल’ के साथ ही हिंदी में उपन्यासों में एक नई कोटि का प्रचलन होता है, जिसे ‘आंचलिक’ कहते हैं।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

संस्कृत के पुराने कवि, टकसाली बातें कहने के शौक़ीन हुआ करते थे। उन बातों को आज कहावत कहा जाएगा, तब सुभाषित कहा जाता था। उनमें से एक प्रसिद्ध सुभाषित है, ‘उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मी’। यानी, लक्ष्मी उद्योगी पुरुषसिंह के ही पास जाति है।
-
संबंधित विषय : व्यंग्य
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

जो दिन भर एक ऐसी भाषा और शब्दावली का प्रयोग करता है जिसके शब्द बरसों के इस्तेमाल से अपनी सारी नई संभावनाएँ खो चुके हैं, जिसका सारा चिंतन और आचरण निर्दिष्ट पद्धति और पूर्वदृष्टांत का पिछलगुआ हो, जिसकी धारणाएँ और विवेक पूर्वानुभव से या किसी ऊपरी सत्ता से अनुशाषित हों, वह धीरे-धीरे अपने व्यक्तित्व में उन तत्त्वों को आत्मसात् करेगा ही जो बुनियादी तौर पर अच्छे सर्जनात्मक लेखन के ख़िलाफ़ हैं।
-
संबंधित विषय : भाषा
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया


जब कभी क्लर्क वैद्यजी को 'चाचा' कहता था, प्रिंसिपल साहब को अफ़सोस होता था कि वे उन्हें अपना बाप नहीं कह पाते।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

हिंदी ही नहीं, कोई भी भाषा जब दफ़्तरों में घुसती है तो उसका एक बँधा-बँधाया शब्द-जाल विकसित होता है—वह टकलाली स्वरूप ग्रहण कर लेती है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

लखनऊ विचारकों का नहीं—स्वप्न-द्रष्टाओं का नगर है।

‘कुल्ली भाट’ जैसे छोटे उपन्यास में निराला ने यथार्थ को एक साथ इतने धरातलों पर खोजा है और इतने जटिल शिल्प के साथ कि उसका निर्वाह—असाधारण प्रतिभा ही कर सकती थी, जो कि स्वयं वे थे।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

साहित्यकार के प्रति स्वाभाविक सहानुभूति होने के बावजूद, मुझे उसकी ग़रीबी का अनावश्यक गरिमा-मंडन अप्रिय लगता रहा है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

कुछ दिन पहले इस देश में यह शोर मचा था कि अपढ़ आदमी बिना सींग-पूँछ का जानवर होता है। उस हल्ले में अपढ़ आदमियों के बहुत-से लड़कों ने देहात में हल और कुदालें छोड़ दीं और स्कूलों पर हमला बोल दिया।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

'कुकरहाव' गँजही बोली का शब्द है। कुत्ते आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे को बढ़ावा देने के लिए शोर मचाते हैं। उसी को कुकरहाव कहते हैं।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया


आज के भावुकतापूर्ण कथाकारों ने न जाने किससे सीखकर बार-बार कहा है कि दुःख मनुष्य को माँजता है! बात कुल इतनी नहीं है, सच तो यह है कि दुःख मनुष्य को पहले फींचता है, फिर फींचकर निचोड़ता है, फिर निचोड़कर उसके चेहरे को घुग्घू-जैसा बनाकर, उस पर दो-चार काली-सफ़ेद लकीरें खींच देता है। फिर उसे सड़क पर लंबे-लंबे डगों से टहलने ले लिए छोड़ देता है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

कृषिप्रधान संस्कृति में महत्त्वाकांक्षा के पनपने की ज़्यादा जगह नहीं है।

अभावग्रस्त बचपन, मेहनत और चिंताओं से भरा विद्यार्थी-जीवन, बाद में मँझोली हैसियत की एक सरकारी नौकरी—अपने इन अनुभवों की कहानी सुनाना बेकार है क्योंकि इस तरह की कहानियाँ बहुत बासी हैं और बहुत दोहराई जा चुकी हैं।

हमारे इतिहास में—चाहे युद्धकाल रहा हो, या शांतिकाल—राजमहलों से लेकर खलिहानों तक गुटबंदी द्वारा ‘मैं’ को 'तू' और ‘तू' को 'मैं' बनाने की शानदार परंपरा रही है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति-प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फ़रेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

भारतीय भाषाओं में जब साहित्यकार के संघर्षशील क्षणों या उसकी गर्दिश के दिनों का प्रसंग उठता है, तो वह प्रायः उसकी ग़रीबी या अभाओं का प्रसंग होता है—अपने परिवेश से टकराने या रचना-प्रक्रिया के तनावों को झेलने का नहीं।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

यह सही है कि ‘सत्य’ ‘अस्तित्व’ आदि शब्दों के आते ही हमारा कथाकार चिल्ला उठता है, 'सुनो भाइयो! यह क़िस्सा-कहानी रोककर मैं थोड़ी देर के लिए तुमको फ़िलासफ़ी पढ़ाता हूँ, ताकि तुम्हें यक़ीन हो जाए कि वास्तव में मैं फ़िलासफ़र था पर बचपन के कुसंग कारण यह उपन्यास (या कविता) लिख रहा हूँ। इसलिए हे भाइयो! लो, यह सोलहपेजी फ़िलासफ़ी का लटका; और अगर मेरी किताब पढ़ते-पढ़ते तुम्हें भ्रम हो गया हो कि मुझे औरों-जैसी फ़िलासफ़ी नहीं आती, तो उस भ्रम को इस भ्रम से काट दो।'
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

किसी भी सामान्य शहराती की तरह उसकी भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

जो जितना ही सफल और प्रतिष्ठित है, वह मेरे लिए उतनी ही बड़ी अपौरुषेय हस्ती बन जाता है जिसके मंदिर का गर्भ-गृह तो दूर की बात है, उसकी चहारदीवारी के दर्शन से भी मुझे विरक्ति होती है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

जैसे कला, साहित्य, प्रशासन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में, वैसे ही डकैती के क्षेत्र में भी मध्यकालीन पद्धतियों को आधुनिक युग में लागू करने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

हमारी योजनाओं में जैसे काग़ज़, वैसे ही हमारी गंदगी का महत्त्वपूर्ण तत्त्व थूक है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

हमारे देश में साहित्यकार फ़र्शी क़ालीन की तरह या तो ग़ैरज़रूरी शोभा की सामग्री है, या शौकिया रौंदने की चीज़, यहाँ तो उसके बारे में कुछ जानना किसी कामकाज़ी नागरिक के लिए भी अनावश्यक है। तभी रंजीता और विजयेता पंडित के बारे में कहानी-लेखिका मृदुला गर्ग को सबकुछ मालूम होगा, पर रंजीता और विजयेता को शायद पता भी न होगा कि मृदुला गर्ग और मेहरुन्निसा परवेज़ क्या हैं और कहाँ हैं।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया


उर्दू कवियों की सबसे बड़ी विशेषता उनका मातृभूमि-प्रेम है। इसलिए बंबई और कलकत्ता में भी वे अपने गाँव या क़स्बे का नाम अपने नाम के पीछे बाँधे रहते हैं और उसे खटखटा नहीं समझते। अपने को गोंडवी, सलोनवी और अमरोहवी कहकर वे कलकत्ता-बंबई के कूप-मंडूक लोगों को इशारे से समझाते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे शहर ही में सीमित नहीं है। जहाँ बंबई है, वहाँ गोंडा भी है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

तुम्हारे विचार बहुत ऊँचें हैं पर कुल मिलाकर उससे यही साबित होता है कि तुम गधे हो।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

चाहिए यह कि लीडर तो जनता की नस-नस की बात जानता हो, पर लीडर के बारे में कुछ भी न जानता हो।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया

अँग्रेज़ी शब्द-समूह का हूबहू हिंदी अनुवाद निरर्थक ही नहीं—विपरीत अर्थ सृजित करनेवाला भी हो सकता है। वास्तव में भाषा का विकास ऐसे कृतिम उपायों से नहीं, संस्कृति और चिंतन के विकास के अनुरूप ही होता है।
-
शेयर
- सुझाव
- प्रतिक्रिया