मैं पृथ्वी से बिछुड़ गया था : कविता की हवा को ताज़गी से भरता संग्रह
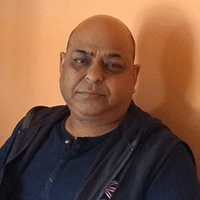 प्रेम शशांक
21 नवम्बर 2024
प्रेम शशांक
21 नवम्बर 2024
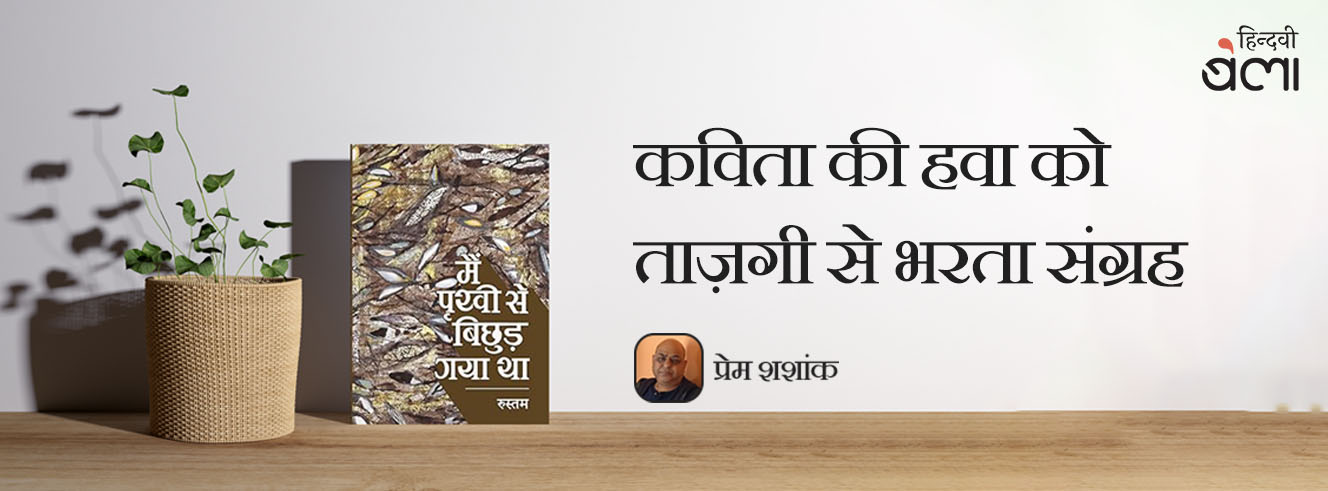
इधर रुस्तम का नया कविता-संग्रह ‘मैं पृथ्वी से बिछुड़ गया था’ (संभावना प्रकाशन) सामने आया है। रुस्तम के काव्य-संसार में प्रवेश से पहले रिलेक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि वह जीवन की आपाधापी के कवि नहीं हैं। वह कविता में दृश्य रचते हैं—जैसे पानी पर तैरते अक्स के कुछ विजुअल कौंध जाते हैं और स्मृति में ठहर जाते हैं। एक रूह की तरह उतरकर, वह ठीक बग़ल में दृश्य के गवाह बन जाते हैं। सृजन का अहंकार उनके यहाँ दूर-दूर तक नहीं है। कविता से उनका वही रिश्ता नज़र आता है, जैसा किसी चित्रकार और चित्र के बीच में होता है।
पाठक की कठिनाई को भी वह अच्छी तरह समझते हैं। उसकी यह उपस्थिति कितनी ज़रूरी है लेकिन उतनी ही मुश्किल भी। पाठक की ज़रूरत और कठिनाई के इसी संकट को व्यक्त करती हुई कविता।
यह गहरी, सूनी राह
सूनी ही रहेगी।
यहाँ कोई नहीं आएगा।
इस पर कोई नहीं चलेगा।
मैं चाहूँ भी तो
यह दृश्य बदलेगा नहीं,
यूँ ही बना रहेगा।
[पृष्ठ 68]
इस कविता के पाठ के साथ बनते हुए दृश्य को देखा जा सकता है, जिससे कवि के संस्कारों और सरोकारों को समझना सरल हो जाता है। जैसे कि इसे पढ़कर किसी गाँव की निर्जन पगडंडी का दृश्य उभरता है। यहाँ दृश्य का महत्त्व है, जहाँ एक कवि और चित्रकार के अनूठे और विरल साम्य को महसूस किया जा सकता है। यहाँ दृश्य एक रचना है, जैसे कैनवस पर कोई चित्रकार अपनी कलाकृति को निहार रहा हो। उसी तरह एक कवि को इन पंक्तियों से सृजित दृश्य को एक गवाह के रूप में निहारते और सृजन का सुख लेते हुए देखा जा सकता है, जहाँ कोई दूसरा और तीसरा मौजूद नहीं है और भविष्य में किसी के उपस्थित होने की कोई संभावना भी नहीं है।
कवि इस दृश्य से उत्सर्जित आनंद में पूरी तरह डूबा हुआ है। उसे किसी अन्य की मौजूदगी का ज़रा-सा भी ख़लल पसंद नहीं है, चाहे वह पाठक हो या आलोचक। कवि अपनी रचना के सृजन-सुख से सराबोर है। इसके अतिरिक्त उसके भीतर और कोई आकांक्षा भी नहीं है। एक साधारण-सी कविता—संवेदना और व्यंजना की दृष्टि से कैसे असाधारण हो जाती है, हम इन पंक्तियों में अनायास ही इस रूपांतरण को देखने के साक्षी हो जाते हैं।
इस संग्रह में प्रेम-कविताएँ काफ़ी हैं और बहुत अच्छी हैं। इन कविताओं की ख़ूबसूरती इस बात में है कि इन कविताओं को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि जिस कवि को हम पढ़ रहे हैं, यह उसकी ही प्रेम-कविताएँ हैं। प्रायः प्रेम-कविताएँ पढ़ते हुए कवि का चेहरा एक चित्र की मानिंद हमारे ज़ेहन में उभरने लगता है लेकिन इन कविताओं को पढ़ते हुए कवि का नहीं बल्कि किरदारों के रूप में किसी दृश्य-चित्र की भांति एक प्रेमी जोड़े का अक्स उभरता है। क्योंकि कवि—इन कविताओं में दो किरदारों की प्रेमानुभूति के अनुभवीय बिंब जिस कुशलता से हम तक पहुँचाने का काम करता है, उससे पाठक कवि-स्मृति में नहीं बल्कि दृश्य-बिंब में उलझता है और कवि का सरोकार भी यही है।
संवेदनात्मक अभिव्यक्ति के ये बिंबित अक्स पाठक को बहुत अनूठे ढंग से रससिक्त करते हैं। रुस्तम जिन किरदारों के राज़ खोलते हैं, ज़्यादातर अनुभव बिछोह से संबंधित हैं। उनका कच्चा-पक्का रचनात्मक विन्यास धधकते अलाव से निकलकर जिस तरह से प्रकृति में अपना रूपाकार ले लेता है तो वह प्रकृति के चित्र से बाहर और अलग नहीं दिखता।
पतझड़ के मौसम में
सबसे ज़्यादा
याद करूँगा तुम्हें।
तुम एक पत्ते की तरह गिरीं,
भूरी पड़ीं
और सूख गई।
और हवा तुम्हें उड़ा ले गई।
[पृष्ठ 21]
अंतिम बार दूर उस उजाड़ में हम बिछुड़े।
मैं तुम्हें वहाँ अकेले ही छोड़ आया,
धरा के नीचे।
फिर मुझे सूझा तुम्हारा मन नहीं लगेगा
वहाँ अकेले में
मैंने तुम्हारे साथ एक और क़ब्र खोदी और उसमें अपने हृदय को रख दिया।
यूँ ख़ाली हृदय मैं वहाँ से चला आया।
मेरा हृदय अब वहीं तुम्हारे पास था।
मात्र देह लेकर मैंने पृथ्वी पर अपना बचा हुआ समय बिताया।
[पृष्ठ 15]
पत्थरों के बीच
दो गड्ढों में
पानी चमक रहा है—
वह श्वेत है।
पत्थर भूरे हैं
और दाहिनी ओर उठते हुए पहाड़ बन गए हैं।
जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ थोड़ी-सी हरी घास है और उसमें एक साँप है—
मेरे पैरों के पास, वह उनसे जुड़ा हुआ बैठा है।
वह भी मेरे साथ इस दृश्य को देख रहा है।
[पृष्ठ 57]
रुस्तम की इन प्रेम-कविताओं से गुज़रना जैसे जेठ की तपती दुपहरी में किसी गाँव के सिवान पर ठहरे हुए धूप-छाहीं जंगल में थोड़ी देर सुस्ता लेने जैसा है। बदन पर पड़ते चकत्ते, ऊँचे-ऊँचे पेड़ों के बीच माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखने को विवश कर देते हैं। कुछ इसी तरह इन कविताओं से औचक सामना होता है, ये पहली नज़र में प्रेम-कविताएँ ज़रूर हैं और इनके कवि भी रुस्तम ही हैं; लेकिन वह इन कविताओं के साथ एक स्रष्टा की तरह इंवॉल्व नहीं हैं।
कविताओं में व्यंजित संवेदना और बिंब से जो दृश्य उपस्थित होता है, उसे वह पाठक के साथ सहअस्तित्व में देख रहे हैं। इस तरह दो दृष्टा एक साथ दृश्य में उतरते हैं। यह एक अद्भुत पाठीय अनुभव है। एक साथ दो लोगों का पाठ में उतरना जैसे—उदास नदी में चुपके से दो लोग पानी की थाह नापने के लिए यह सोचकर उतर जाएँ कि नदी को ख़बर नहीं हो। स्रष्टा और दृष्टा का यह विरल संयोजन अर्थात् पाठ के साथ दोनों का एक स्तरीय धंसाव हिंदी-कविता में हवा के एक ताज़े झोखे की तरह है।
इन कविताओं में यूँ तो बिछोह की स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बिछोह तो एक छोर है दूसरा छोर तो मिलन होना ही ठहरा। मिलन की कविताओं में देह की स्मृतियाँ बहुत मुखर हैं, जिसे हिंदी-कविता में बहुत पसंद नहीं किया जाता। मेरा मानना है कि यह एक ग़लत प्रवृति है। यह पांडित्य के वाहियात प्रदर्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पांडित्य से आशय वर्ण-व्यवस्था में हस्तक्षेप से नहीं बल्कि वैचारिक पांडित्य से है।
जब हम विदेशी कवियों की अनूदित प्रेम कविताएँ पढ़ते हुए नहीं शर्माते और उनकी तारीफ़ करने में कोई कसर बाक़ी नहीं रखते अर्थात् बहुत चाव से पढ़ते हैं, तो हिंदी-कवियों को पढ़ते हुए क्यों नाक-भौं सिकोड़ते हैं। देह और गेह का कवि कहकर एक हिंदी-कवि के तिरस्कार का उदाहरण हिंदी-आलोचना को कमतर करता है। रुस्तम की एक दो कविताओं का ज़िक्र ग़ैर-मौज़ूँ नहीं होगा।
तुम मुझे विचलित करती हो।
सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में।
ओ साध्वी
कैसे तुम्हारी देह
इच्छा से भरी है—
इच्छा ने उसे
भारी कर दिया है।
उठ नहीं पा रहे तुम्हारे पाँव।
तुम धीरे-धीरे चल रही हो।
एक तीव्र गंध
तुममें से फूट रही है
और तुम्हारे चहुँ ओर फैल रही है।
[पृष्ठ 75]
केवल पाँव तुम्हारे देखूँगा
और फिर सोचूँगा
तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा वक्ष, तुम्हारी नाभि, तुम्हारी जाँघें।
और
अँधेरा वह स्थल
जहाँ वे मिलती हैं,
कल्पना में ही
उसे सूँघूँगा।
केवल पाँव तुम्हारे छूऊँगा
और उन्हीं में छू लूँगा तुम्हारी देह का हर एक अंग।
[पृष्ठ 77]
इन कविताओं में देह अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित है, लेकिन देह की उपस्थिति जड़न ही है। यहाँ दृष्टि एक तरल पदार्थ की तरह देह के विभिन्न अवयवों के प्रति दुरनिवार आकर्षण से गतिशील है जैसे—चेहरा, आँखें, होंठ, वक्ष, नाभि, जाँघें और जाँघों से होती हुई उस अँधेरे स्थल तक पहुँचती है जहाँ ये दोनों मिलती हैं। कवि के लिए देह और उसके प्रति उसके आकर्षण में कोई ऑब्सेशन नहीं है। एक सम्मान और आस्था का भाव इन कविताओं को एक अलग ऊँचाई देता है। इसलिए इन दोनों कविताओं में देह अपने पूरे वजूद में होने के बावजूद अनुभूति का स्तर ठोस दैहिक नहीं है।
भारतीय वांग्मय और सांस्कृतिक परंपरा में देह को भोग की वस्तु से अलग जो सम्मान-जनक स्थान प्राप्त है, उसकी एक हल्की-सी झलक इन कविताओं में देखी जा सकती है। इसे आप भौतिकवादी दृष्टि से कल्पना और यथार्थ की लुकाछिपी का खेल भी कह सकते हैं। लेकिन अपने-अपने राम के भाववादी नज़रिए के बावजूद नि:संदेह संवेदना का महत्त्व सर्वोपरि है।
इन कविताओं में दो प्रेमिल किरदारों का दैहिक खेल जिन संवेगों से होते हुए अध्यात्म की शरण-स्थली में अपनी जिस पूर्णता को प्राप्त करता है, उसके साथ हिंदी-कविता में कुछ नया जुड़ता भी देखा जा सकता है। इन किरदारों की यात्रा केवल देह से देह तक सीमित नहीं है। यह यात्रा जिस तरह स्थूल जगत से अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करती है, भारतीय चिंतन परंपरा को बहुत बल मिलता है। वैश्विक ख्यात दार्शनिक ओशो ‘संभोग से समाधि’ रचना में तन और मन के एक लय में हो जाने की जो परिकल्पना करते हैं, उसकी कुछ अर्थ छावियाँ इन कविताओं में पाई जा सकती हैं।
इन प्रेम-कविताओं के लिए रुस्तम शब्दों के चयन को लेकर ज़रा भी परेशान नज़र नहीं आते। अनुभूतियों के संवेग के साथ शब्द जैसे ख़ुद ही इकट्ठे हो गए हों। बहुत मामूली शब्द संयोजना से ही अनुभूति-परक संवेगों का भाव पक्ष बहुत मज़बूत है। कहना न होगा कि रुस्तम चमकदार शब्दों से कोई थ्रिल पैदा करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि साधारण शब्दों से संवेगों को एक नई ऊँचाई देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। वह साधारण कवियों के बीच असाधारण कवि हैं।
मृत्यु भी रुस्तम के लिए एक अलग महत्त्व रखती है। उनकी कई कविताओं में मृत्यु का स्मरण देखा जा सकता है। जिस तरह निर्मल वर्मा के गद्य में मृत्यु का ज़िक्र बार-बार आता है, उन्हें मृत्यु से ज़रा भी घबराहट नहीं लगती बल्कि उसे अलग-अलग ढंग से याद करने और समझने के प्रयास दिखाई देते हैं, वैसे ही रुस्तम की कविताओं में मृत्यु की रचनात्मक समझ साफ़ नज़र आती है। मृत्यु को लेकर उनके मन में भी कोई भय नहीं है।
एक खिड़की खुली थी।
हम उड़ते हुए
उसमें से भीतर चले गए।
हम एक छोटे से कमरे में थे।
सूरज की रोशनी
बिस्तर पर पड़ रही थी।
एक मृत व्यक्ति वहाँ पड़ा था।
[पृष्ठ 35]
स्वप्न में भी
हम वहाँ पहुँच नहीं पाए
नीले पर्वतों से घिरी
नीली एक नदी
जहाँ
झील में मिल रही थी।
काले वस्त्रों में
चार छायाएँ वहाँ खड़ी थीं।
एक खंडहर
जो कभी क़िला रहा होगा।
एक मल्लाह नाव पर झुका हुआ था—
यह
प्राचीन कोई सदी थी।
हम
हम नहीं थे, कोई और ही थे।
[पृष्ठ 38]
अंतिम बार
उस घर के आगे से मैं गुज़रा।
उस घर का दरवाज़ा बंद था,
खिड़कियाँ भी।
एक झिर्री से मैं अंदर चला गया।
सब कुछ वैसे ही पड़ा था जैसे पिछली बार।
[पृष्ठ 38]
रुस्तम जटिल कवि नहीं हैं। वह बहुत सहजता से समझ में आते हैं। यह उनकी ताक़त है। जबकि हिंदी में चलन इसके बिल्कुल उलट है, समझ में आ जाने वाले कवि को अच्छा नहीं माना जाता। इसके बावजूद वह अपने इस गुण-धर्म का त्याग नहीं करते। वह सिर्फ़ कवियों के लिए नहीं लिखते। कविता के जो पाठक अच्छी कविता के लिए बेताब रहते हैं, उन्हें रुस्तम बहुत अच्छे लगने वाले हैं।
मृत्यु से घबराने वाले तो बहुत हैं। ऐसे लोग जो मृत्यु की आँख में देखने का साहस रखते हैं, रुस्तम जैसे ही हो सकते हैं। वह अपनी कविताओं में एक तरह से मृत्यु के साथ आँख मिचौली खेलते हुए नज़र आते हैं। मृत्यु को वही व्यक्ति इतनी सहजता से ले सकता है जो उसे जीवन जितना महत्त्व देता हो। उनकी मृत्यु-संबंधी कविताओं में जीवन की धड़कनों को साफ़ सुना जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। वह जीवन और मृत्यु के सौंदर्य में कोई फ़र्क़ नहीं करते। इसलिए उनकी कविताओं में मूल्यों के स्तर पर ज़बरदस्त सौंदर्य-बोध का एहसास होता है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
