रविवासरीय : 3.0 : ‘इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊँचा है सादगी का...’
 अविनाश मिश्र
09 फरवरी 2025
अविनाश मिश्र
09 फरवरी 2025
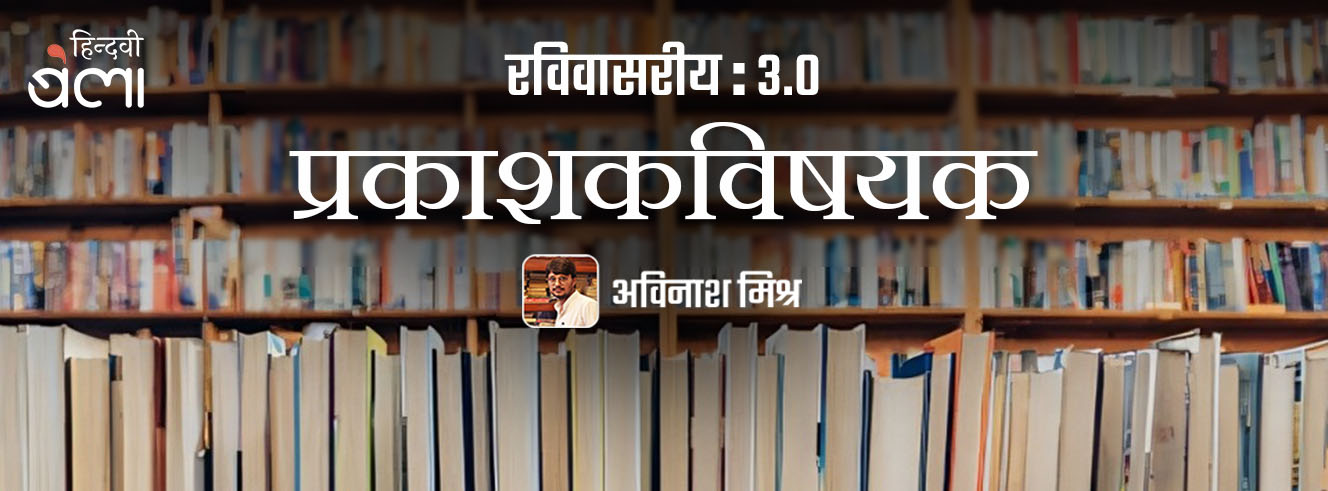
• एक प्रकाशक को देखकर मेरे मन में सबसे पहला ख़याल यही आता है कि उससे किताब ले लूँ। यहाँ ‘किताब ले लेने’ का अर्थ एकायामी नहीं है।
• हिंदी के साहित्यिक प्रकाशकों के विषय में जो बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वह है—उनका बहुत कम पढ़ा-लिखा होना। लेकिन यह सोचकर ख़ुशी भी होती है कि उन्होंने अपने हिस्से का पढ़ने के लिए आदमी रखे होते हैं, अपने हिस्से का लिखने के लिए तो रखे ही होते हैं। उन्हें कहीं दो-चार मिनट भी बोलना हो, तो उनके वक्तव्य पर उनका समस्त संपादकीय विभाग सारा दिन काम करता है। अगर कभी किसी परिस्थिति या विवाद या मुद्दे पर; समाज या राजनीति या पत्रकारिता को उनका पक्ष जानना हो, तो वे उसे अपने शब्दों में लिखकर नहीं बता सकते।
• प्रकाशकों के पास अपने शब्द नहीं होते।
वे प्रकटतः कभी असहमत या नाराज़ नहीं होते।
वे एक चुनी हुई दृष्टिविहीनता से काम लेते हैं।
वे बेहतर से ज़्यादा बुरे पर ध्यान इसलिए देते हैं, क्योंकि बुरा पीछे पड़ जाता है।
वे मानते हैं कि लेखक के सौ साल मनाए जाने की शुरुआत सौ साल पहले हुई थी।
• ‘वर्षावास’ शीर्षक उपन्यास में इन पंक्तियों के लेखक ने हिंदी प्रकाशकों की कुछ ‘विशेषताएँ’ संगृहीत की हैं। इस संग्रह के अनुसार :
संसार के प्रतिष्ठित प्रकाशकों के सूचीपत्र काफ़ी काम की चीज़ हैं। उन्हें पढ़कर—केवल उन्हें पढ़कर भी—दूसरों को बताया जा सकता है कि वे क्या पढ़ें!
हमारे घर में भले ही बहुत सारी किताबें हों, लेकिन हमें सूचीपत्र से बाहर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है; क्योंकि पढ़ना फिर हमारे लेखन में ही नहीं, चाल-चलन में भी नज़र आने लगेगा।
दरअस्ल, पढ़ना भी वैसे ही झलकता है, जैसे न पढ़ना।
हमारा लेखन और चाल-चलन—तमाम अंतरराष्ट्रीय स्तर की नेम-ड्रॉपिंग के बावजूद—यह बताता है कि हमारा घर किताबों की अच्छी दुकान है और हमने अब तक सूचीपत्रों के सिवाय किसी भी टेक्स्ट को ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर हमने अपना अध्यवसाय सचमुच किया होता, तब हम इतने कम मनुष्य नहीं होते और हमारा जीवन और हमारा एक-एक वाक्य इस तथ्य को प्रकाशित न कर रहा होता।
हमारा काम कम नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ने से भी—बेहतर ढंग से जारी रह सकता है। हमारे अपने निरक्षर हमें अब ज़्यादा समझदार नज़र आते हैं, बनिस्बत उनके जिन्हें अक्षर-ज्ञान है। निरक्षरों के साथ हमारे रिश्ते कभी ख़राब नहीं हुए, जबकि हम विद्वानों को खोते चले गए।
संसार में एक प्रतिशत से भी कम लोग हैं, जो पढ़ने लायक़ चीज़ें पढ़ते हैं। इस एक प्रतिशत में भी एक प्रतिशत से कम हैं, जिन्हें कविता में दिलचस्पी है। कुछ प्रकाशकों के सूचीपत्र देखते हुए यह पाया गया कि वे कविता के चक्कर में पड़ते ही नहीं हैं।
शब्दकोश, दिवंगत और कॉपीराइटमुक्त प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएँ एवं रचनावलियाँ, रामकथाएँ; राजनेताओं, अभिनेताओं की आत्मकथाएँ, जीवनियाँ और कुंडलियाँ; एन्साइक्लोपीडिया, अकादमिक महत्त्व की छात्रोपयोगी विमर्शात्मक किताबें, पर्यावरण-मैनेजमेंट-पत्रकारिता-सिनेमा-संगीत-नाटक-कला से जुड़ी किताबें, व्याकरण-विज्ञान शिक्षण-भाषाविज्ञान से संबंधित प्रयोजनमूलक किताबें, अत्यंत लोकप्रिय और जासूसी साहित्य, धर्म-राजनीति-दर्शन-समाजशास्त्र-मनोविज्ञान-इतिहास-अर्थशास्त्र-गणित-ज्योतिष-क़ानून-स्वास्थ्य-चिकित्सा-सशक्तीकरण-कम्प्यूटरविज्ञान-व्यंग्य और अंत में विविध... ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है जो सूचीपत्र से बाहर है। यहाँ तक कि कभी-कभी पढ़े जाने लायक़ गंभीर कविता भी गंभीर स्थान घेरे रहती है—सूचीपत्र में। पर पता नहीं वह सूचीपत्रों से पुस्तकाकार निकलकर जाती कहाँ है!—पुस्तकालयों में? हाँ, वह सबसे ज़्यादा पुस्तकालयों में पाई जाती है। वहाँ भी उसे वर्षों से किसी ने नहीं छुआ है, लेकिन वह वर्षों से आ रही है—नई-नई जिल्दों में।
कविता की किताब लेकर चलते हुए व्यक्ति आज तक समाज में कहीं नहीं देखे गए, नमूने ज़रूर देखे गए हैं; जिनका कविता से कोई रिश्ता नहीं, कविता की किताबों और सूचीपत्रों से ज़रूर है।
• हिंदी के साहित्यिक प्रकाशकों के विषय में एक और बात जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वह है—उनका लेखकों के साथ मंच शेअर करना। यह मरज़ इधर दस-ग्यारह वर्षों में बहुत बढ़ा है। इस दरमियान यों पाया गया है कि लेखक मंच पर चुपचाप बैठा रहता है और उसका प्रकाशक उसके सामने माइक पर अल्ल-बल्ल बकता रहता है। इस विषय में एक-डेढ़ दहाई पहले तक हमारे प्रकाशकों में एक संकोच और शर्म का भाव था और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वे लेखक के सामने वक्तव्य [?] दे सकें। आख़िर एक लेखक का सब कुछ ले लेने के बाद, वे उसके सामने वक्तव्य दे भी कैसे सकते हैं!
• अकार-58 [सितंबर 2021] में प्रकाशित संपादकीय ‘लेखक-प्रकाशक : संबध, अनुबंध के नए आयाम की संभावनाएँ’ में प्रियंवद कहते हैं :
‘संगमन’-5 धनबाद में 3-5 सितंबर 1999 को हुआ था। जब इसके विषय चुने गए तो यह तय हुआ कि नए लेखकों की पुस्तकों के प्रकाशन की समस्याओं पर भी एक सत्र केंद्रित किया जाए। ज़ाहिर है कि हिंदी के प्रकाशक और प्रकाशन जगत इस विषय की परिधि में था। नए लेखकों के साथ प्रकाशकों का व्यवहार, उनके संबंध, कॉपीराइट, रॉयल्टी, नए संस्करण की समस्याएँ भी विषय का हिस्सा थे। यह भी कि क्या ऐसा कोई रास्ता मुमकिन है कि दोनों के बीच किसी तरह के आपसी विश्वास और सहूलत का वातावरण बन सके। नए लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन अधिक आसानी और अधिक पारदर्शिता के साथ हो सके।
इस आयोजन में राजेंद्र यादव और दूधनाथ सिंह भी थे। दोनों ही इस विषय पर बोले थे। ये दोनों ही हिंदी के बड़े लेखकों में शामिल किए जाते थे। प्रकाशकों से इनके पुराने और गहरे संबंध थे। पर ये दोनों जो बोले, वह बहुतों को, ख़ासतौर से नए लेखकों को हैरान और हतप्रभ करने वाला था। उनका पूरा वक्तव्य प्रकाशकों के पक्ष में था। उनका स्वर कुछ इस तरह का था कि प्रकाशक जब किसी नए लेखक को छापता है, तो उस पर एहसान-सा करता है। पुस्तक के प्रकाशन तक लेखक को कोई नहीं जानता, उसकी कोई पहचान नहीं होती। प्रकाशक इसे बनाता है। नए लेखक को उसका यह एहसान समझना और स्वीकार करना चाहिए। यह भी कि प्रकाशक नए लेखक की किताब पर पूँजी लगाने का जोखम उठाता है, उसकी किताब को प्रचारित-प्रसारित करने पर जो ख़र्च करता है, लेखक को स्वीकृति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। दोनों वरिष्ठ लेखक लगभग एक ही स्वर में बोल रहे थे।
...वास्तव में हिंदी साहित्य का यह एक दिलचस्प पहलू है कि स्थापित और वरिष्ठ लेखक कभी प्रकाशकों के ख़िलाफ़ नहीं बोलते। इसका कारण सीधा और साफ़ है : अपनी पुस्तक छपवाने में उन्हें प्रकाशकों से कोई दिक़्क़त नहीं होती। प्रकाशक भी उनकी आव-भगत करता है। उन्हें रॉयल्टी के अलावा दूसरे रूपों में भी धन देता है। राजेंद्र यादव के फ़्लैट में कौन-सा सामान किस प्रकाशक ने दिया या नामवर सिंह के फ़्लैट की आंतिरक सज्जा किस प्रकाशक ने कराई, ये सब बातें चर्चा का विषय रह चुकी हैं। प्रकाशक वरिष्ठ लेखकों की पुस्तकों के लिए ख़ुशामद करता है, इसलिए कि अधिकांश अपनी या उसकी दूसरी पुस्तकें बिकवाने में वे समर्थ होते हैं। वे प्रकाशक की पुस्तकें कोर्स में लगवा सकते हैं। सरकारी ख़रीद में उनका हस्तक्षेप होता है। शोध, विभिन्न जगहों के पुरस्कार, विभिन्न संस्थाओं में ख़रीद, पुस्तकों के छात्र संस्करण आदि का उनका मज़बूत नेटवर्क होता है। वे पढ़े भी जाते हैं और उन पर चर्चाएँ, सेमिनार, शोध आदि होने से वे निरंतर चर्चा में रहते हैं। संभव है कि मेरी इन बातों से बहुत से लोग सहमत न हों। अपनी बात के समर्थन में दशकों तक हिंदी के साहित्यिक जगत के सबसे बड़े नाम, नामवर सिंह के साथ हुई बातचीत का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है। नामवर सिंह का यह साक्षात्कार मैंने, देवेंद्र और हरिनारायण ने लिया था। साक्षात्कार की शर्त यही थी कि नामवर सिंह लगभग ‘कन्फ़ेशन’ की हद तक सच बोलेंगे। नामवर सिंह तैयार हो गए थे। वह बोले भी। 27 जनवरी 2006 को शाम सात बजे दरियागंज के एक होटल में हमारी यह बातचीत रिकॉर्ड हुई। कई मुद्दों पर बातें हुई थीं। उस समय नामवर सिंह ‘राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी’ की ख़रीद के मामले में उलझे हुए थे...
इस पूरी बातचीत में नामवर सिंह कहीं भी लेखकों के पक्ष में नहीं बोलते हैं। अलबत्ता दबे स्वर में निर्मल वर्मा और अमरकांत के बारे में संकेत देते हैं कि पार्टी के कारण वे छपे, वरना कोई छापने वाला नहीं था। अपने गुरु हजारीप्रसाद द्विवेदी से उन्होंने क्या सीखा, बड़ी सरलता से और निश्छलता से बताते हैं। वह लेखक-प्रकाशक के बीच आपसी विश्वास और मधुर संबंधों की बात करते हैं। अपने और दूसरों के उदाहरण से बताते हैं कि प्रकाशक ने जब जो दिया, रख लिया। कभी पूछा नहीं। रमाप्रसाद घिल्डियाल ‘पहाड़ी’ की बात भी करते हैं; जो प्रगतिशील लेखक संघ [प्रलेस] के सम्मेलनों में कॉपीराइट और रॉयल्टी, अनुबंध आदि समस्याओं पर बातें करते थे... पर प्रलेस ने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। दो अन्य लेखक संगठनों में से भी किसी ने इस मुद्दे पर किसी प्रकाशक पर उँगली नहीं उठाई, कोई बहस नहीं छेड़ी, इस पर कोई सेमिनार केंद्रित नहीं किया। कारण वही, इनके पदाधिकारियों की गोटे प्रकाशकों से सेट होती थीं। वे क्यों बोलें?
नामवर सिंह की बातों से लगता है कि पहले प्रकाशक-लेखक संबंध आत्मीय और मधुर होते थे। पर ऐसा नहीं था। दूधनाथ सिंह ने हमें इसका संकेत दिया है। ममता कालिया ने ‘तद्भव’-42 में प्रकाशित अपने संस्मरण में एक क़िस्सा लिखा है। उसे भी पढ़िए :
‘‘इलाहाबाद में ‘लोकभारती’ सबसे बड़ा और समर्थ प्रकाशन था। वहाँ लेखकों का जमघट लगता और अहर्निश पुस्तक प्रकाशन भी होता रहता। बहुत पहले की बात है। अमरकांत जी की बेटी संध्या का विवाह होना था। उन्हें ‘मित्र प्रकाशन’ से बहुत सीमित वेतन मिलता था। उनके दोनों बेटों में एक भी अभी रोज़गार से नहीं लगा था। दहेज का आडंबर न भी हो, न्यूनतम तैयारी होनी आवश्यक थी।
अमरकांत जी ने ‘लोकभारती’ से उपन्यास की एवज़ में चार हज़ार रुपए अग्रिम धनराशि ली। वह उन दिनों अपना वृहद उपन्यास ‘इन्हीं हथियारों से’ लिख रहे थे। पत्नी की बीमारी और परिवार की परेशानियाँ उन्हें बहुत कम अवकाश देतीं।
अगले दो-तीन महीनों में ‘उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान’ [लखनऊ] से पुरस्कारों की घोषणा हुई। यह घोषणा इलाहाबाद में हमेशा सावन के पहले दौंगरे की तरह ली जाती थी। बहुतों के चेहरे खिल जाते, बहुतों के चेहरे बुझ जाते। कई लोग ढाई हज़ार के इनाम से गद्गद हो जाते, कुछ को पच्चीस हज़ार भी कम लगते। उन दिनों पुरस्कार-राशि कम थी, मगर उसका ओहदा बड़ा था।
‘लोकभारती’ में रमेश जी और राधे बाबू अपने मनोभावों का पता न चलने देते, लेकिन दिनेश जी में वह धैर्य नहीं था। उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकें जब पुरस्कृत होतीं; वह तिलमिलाते, ‘सरकार को यह नहीं पता कि फलाने जी की किताब तीन साल से गोदाम में सड़ रही है। गोदाम के दीमक-चूहों से तो मैं बचाता हूँ।’
रवि [रवींद्र कालिया] मज़ाक़ करते, ‘एक सुझाव दिया जाए कि लेखक के पुरस्कार में प्रकाशक का भी हिस्सा हो।’
दिनेश जी बिना शर्मिंदा हुए कहते, ‘बिल्कुल होना चाहिए। आप तो सरकार के मुँह लगे हैं, उनसे कहिएगा।’
रवि कहते, ‘फिर तो मुद्रक का हिस्सा भी बनेगा।’
उस साल अमरकांत जी का एक कहानी-संग्रह पुरस्कार पा गया। धनराशि चार हज़ार थी। तब नियम यह था कि सात हज़ार से नीची धनराशि वालों के पुरस्कार डाक से भेज दिए जाते थे। ऊँचे पुरस्कार विजेताओं को 14 सितंबर को आमंत्रित कर एक उत्सव में सम्मानित किया जाता। पता नहीं, कैसे अमरकांत जी के पुरस्कार का चेक ‘लोकभारती’ के पते पर भेजा गया। वह ही इस कहानी-संग्रह के प्रकाशक थे।
दिनेश जी लिफ़ाफ़े से मज़मून पहचानने वाले इंसान थे। उन्होंने शाम को अमरकांत जी को कॉफ़ी हाउस में बैठे देखा तो अपने कार्यालय में बुलाया। उन्हें बधाई दी। अमरकांत को ख़बर थी। वह अख़बार में घोषणा देख चुके थे। अमरकांत जी के आगे लिफ़ाफ़ा रखते हुए दिनेश जी ने कहा, ‘आपने अपना उपन्यास पूरा कर लिया?’
‘अभी तो आधा भी नहीं हुआ है।’ अमरकांत बोले।
‘आपने उस पर अग्रिम ले रखा है, याद है।’ दिनेश जी ने कहा।
अमरकांत जी का चेहरा पसीने-पसीने हो गया। स्वास्थ्य और अर्थ के संघर्षों ने उनकी ऊपरी झिल्ली एकदम छील डाली थी। उन्होंने कहा, ‘दिनेश जी, मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। क़लम दीजिए इधर। मैं यह चेक आपके नाम इंडोर्स करता हूँ।’
बिना ज़रा भी लज्जित हुए दिनेश जी ने क़लम उनके हाथ में पकड़ाई और अमरकांत जी ने चेक के पीछे अपने हस्ताक्षर कर दिए।
कई बार ऐसा हुआ कि शहर के लेखक को संस्थान से सिर्फ़ ढाई हज़ार का पुरस्कार मिला तो उससे अपना उधार वापस लेने वाले कई ढाई हज़ारिए पहुँच गए।
इसी सबसे आजिज़ आकर इलाहाबाद में आए दिन कोई न कोई लेखक अपना प्रकाशन खोलने का फ़ैसला करता। सबने खोले भी। भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय, अमरकांत, शैलेश मटियानी, रवींद्र कालिया और सतीश जमाली। लेकिन वितरण और विक्रय के बैताल से ये सब हार गए। प्रायः शत-प्रतिशत घाटा उठाकर ये सब प्रकाशन बंद हुए।’’ [‘तद्भव’-42 : पृष्ठ 189-190]
...ममता कालिया ने बात जहाँ छोड़ी है, वहाँ अभी उसे छोड़ा नहीं जा सकता। हमने देखा कि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, जवाहर चौधरी सभी ने प्रकाशन खोला। लेखकों को प्रकाशक क्यों बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, यह सवाल भी हमारी इस पूरी बात का हिस्सा है। इस बात को तर्क और विस्तार से समझने के लिए अब पढ़िए 1 अप्रैल 1972 के लिखे एक विस्फोटक पत्र का लंबा अंश। वैसे तो यह पत्र 99 फ़ुल स्केप पृष्ठों का है। टाइप मशीन पर टाइप किया हुआ है। लेखक हैं—उपेंद्रनाथ अश्क और उन्होंने पत्र लिखा है—‘लोकभारती’ के राधे बाबू को, जिनका ज़िक्र ममता जी ने भी किया है। यह पत्र गिरिराज किशोर के पत्रों में मिला है। उनके पत्रों के दूसरे खंड में यह पूरा पत्र प्रकाशित होगा। फ़िलहाल पढ़िए ममता कालिया की बात को आगे बढ़ाने वाला यह पत्रांश। इसे ज़रूर ध्यान रखें कि अश्क का ख़ुद ‘नीलाभ प्रकाशन’ था और अश्क लेखक भी थे। लोकभारती के बिल्कुल पास उनका दफ़्तर था। दोनों प्रकाशकों में व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता भी थी, और यह भी ध्यान रखें कि अश्क को लोगों से उलझने और उन्हें उलझाने में बहुत रस मिलता था। पढ़िए, यह लंबा ज़रूरी अंश :
‘‘मैं आज से लगभग तीस वर्ष नहीं, चालीस वर्ष पहले हिंदी में लिखने लगा था और केशव जी [केशवचंद्र वर्मा] ने माना है कि तब ये तनाव और झगड़े नहीं थे; न वैसी बिक्री थी, न लालच। इस पर भी कवियों में श्री मैथिलीशरण गुप्त, उपन्यासकारों में प्रेमचंद और वृंदावनलाल वर्मा और बाद में श्री यशपाल ने लेखक-प्रकाशक बनना स्वीकार किया और आज यदि श्री रमेश ग्रोवर ‘लोकभारती’ के हिस्सेदार; हितचिंतावश लेखकों को इस ज़हमत से बचाना चाहते हैं, तो उस वक़्त भी लेखकों के ऐसे ‘हितचिंतक’ प्रकाशकों की कमी नहीं थी।
इस पर भी हिंदी के उन मूर्द्धन्य साहित्यकारों ने यह ‘ज़हमत’ मोल लेना श्रेयस्कर समझा और लगभग उन्हीं कारणों से मैंने, दिनकर, बेनीपुरी और जैनेंद्र ने आज से बीस-बाईस वर्ष पहले यह ज़हमत उठाना स्वीकार किया। कौशिक [विश्वम्भरनाथ शर्मा], भगवतीचरण वर्मा, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय, भैरव प्रसाद गुप्त, श्रीनरेश मेहता, ओंकार शरद और बहुत से अन्य लेखकों ने भी। यह और बात है कि ये सफल नहीं हुए। [राजेंद्र] यादव ने अब दूसरी कोशिश की है और सफल भी हुए हैं। जहाँ तक बिक्री के नए-नए साधनों की बात है, तब वे नहीं थे। रही पाठ्य पुस्तकें, तो प्रेमचंद की ज़िंदगी में उनकी पुस्तक पाठ्यक्रम में नहीं आई [जबकि प्रकाशक के हाथों में होने से जयशंकर प्रसाद तभी कोर्स में आ गए]। [इस पर ध्यान दें— प्रियंवद]
प्रेमचंद की पुस्तकें उनके सुपुत्र श्रीपत राय के अथक प्रयासों से पाठ्यक्रम में आईं और उन्होंने इसके लिए कितना संघर्ष किया, मैं उसका साक्षी हूँ। मैथिलीशरण गुप्त प्रकाशन शुरू करने के वर्षों बाद राज्यसभा में आने के उपरांत ही ज़ोरों से पाठ्यक्रमों में आए। [इस पर ध्यान दें— प्रियंवद]
यशपाल की पुस्तक स्वतंत्रता मिलने के बीस वर्ष बाद तक कोर्स में नहीं आई। पहले ‘राधाकृष्ण प्रकाशन’ और अब ‘लोकभारती प्रकाशन’ के कारण उनकी पुस्तकें पाठ्यक्रमों में आई हैं [और उनके दो उपन्यासों के संक्षिप्त संस्करण लेखक ने स्वयं नहीं, इन्हीं दो प्रकाशकों ने किए हैं]।
जैनेंद्र के बारे में मैं नहीं जानता कि उनकी कितनी पुस्तकें कोर्स में हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, हिंदी में मेरी पहली पुस्तक ‘जय पराजय’ और दूसरी ‘स्वर्ग की झलक’ आज से पैंतीस वर्ष पहले कोर्स में आ गई थीं और पंजाब से बिहार तक स्वीकृत हो गई थीं। मेरे स्वयं प्रकाशन करने का यह फल हुआ है कि पूरे हिंदी प्रदेश में [जहाँ पहले मेरे नाटक लगे हुए थे] इन बीस वर्षों में, बिहार को छोड़कर उन तमाम जगहों से धीरे-धीरे निकल गए। मेरे एकांकी-नाटक और कहानियाँ ही पढ़ाई जाती हैं; क्योंकि उनकी रॉयल्टी, प्रकाशक, संपादक अथवा बोर्ड के किसी मेंबर की जेब में जाती है और लेखक को पत्रं-पुष्पं देकर टाल दिया जाता है।’’
• वे अब इतनी चमकती हुई किताबें छाप रहे हैं कि उन्हें पढ़ने-समझने की चाह नहीं होती, चूमने की ज़रूर होती है।
• हिंदी साहित्य के प्रसंग में इस प्रकाशक-प्रकाशन-स्थिति में ‘रुख़’ शीर्षक प्रकाशन गए कुछ वक़्त में एक उम्मीद की भाँति उभरा है। ‘रुख़’ के संस्थापक-संचालक-संपादक अनुराग वत्स वे सारी शिकायतें दूर करते नज़र आते हैं, जो यहाँ ऊपर दर्ज की गई हैं। यह अलग बात है कि वह नई शिकायतें उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बावजूद ‘रुख़’-मॉडल अत्यंत प्रभावी है। चयन, सुरुचि, संपादन, प्रस्तुति, स्टैंड, पारदर्शिता के प्रसंग में ‘रुख़’ का रुख़ क़ाबिल-ए-ज़िक्र है।
• मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी किताबें हों कि घर में घुसूँ तो पैर के नीचे कोई किताब आ जाए। मैं चाहता हूँ कि सुबह घर से किताबें पैक करके निकलूँ, शाम को झोले में किताबें लिए हुए लौटूँ। घर में किताबें ही किताबें महकें। रात में करवट लूँ तो किताबों के गले पड़ जाऊँ। मैं सब वक़्त बस उन्हें पढ़ता-समझता ही रहूँ। लेकिन फिर सोचता हूँ कि खाऊँगा क्या! नौकरी छोड़ दूँगा तो भीख माँगनी पड़ेगी। आप सबसे कहना पड़ेगा—मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं दानपात्र या गुल्लक हो जाऊँगा। आपको मुझमें कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। मैं फूट जाऊँगा—अपने आधी कौड़ी के वस्तुसत्य [Content] के साथ।
यह सब पढ़कर मुझे दयनीय न समझें, मुझमें कोई कमी न समझें; क्योंकि मेरे पास शहर में मकान और गाँव में खेत भले ही न हों, व्यक्तित्व में कमीनापन बहुत है और यही वह गुण है जो मुझे कमीनों के बीच सक्रिय और जीवित बनाए रखता है।
• कुछ किताबें, किताबें नहीं; काग़ज़ के फूल हैं।
• ये सब चालू और घिसे हुए मुहावरे हैं कि रचयिता अपने रक्त से रचता है, वह अपनी रचना को अपनी संतान की तरह आकार देता है; लेकिन क्या किया जाए अगर चमक ने कुछ ख़ास नहीं दिया और चालू और घिसे हुए मुहावरे ही सचाई सँभाले हुए हैं। ...तब इसी मुहावरे में अपने रक्त से रची संतति को लेकर एक रचयिता प्रकाशक के पास जाता है कि वह इसे प्रकाशित करे। प्रकाशक इस संतति में निवेश करता है, पास खड़ी प्रकाशक की संतानें शोषण की अनंत संभावनाओं से समृद्ध इस निवेश के दीर्घकालिक लाभ को पहचानती हैं और क़सम खाती हैं—दूसरे धंधे में न जाने की।
•••
अन्य रविवासरीय : 3.0 यहाँ पढ़िए — गद्यरक्षाविषयक | पुष्पाविषयक | वसंतविषयक | पुस्तकविषयक
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
