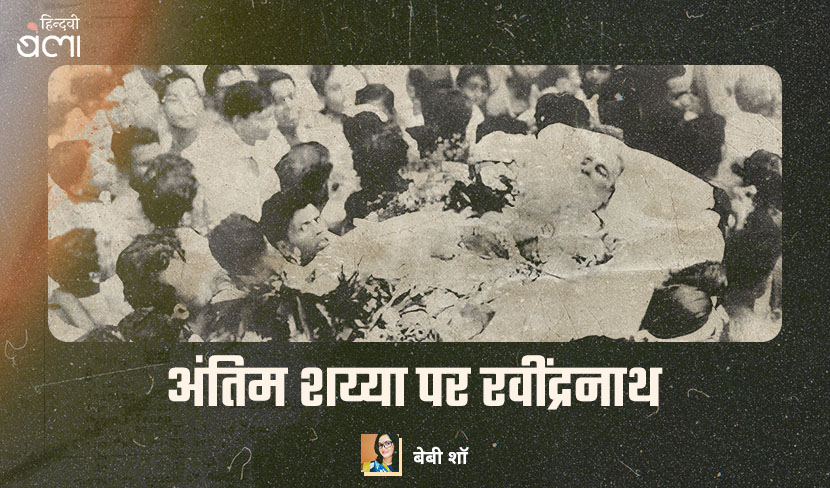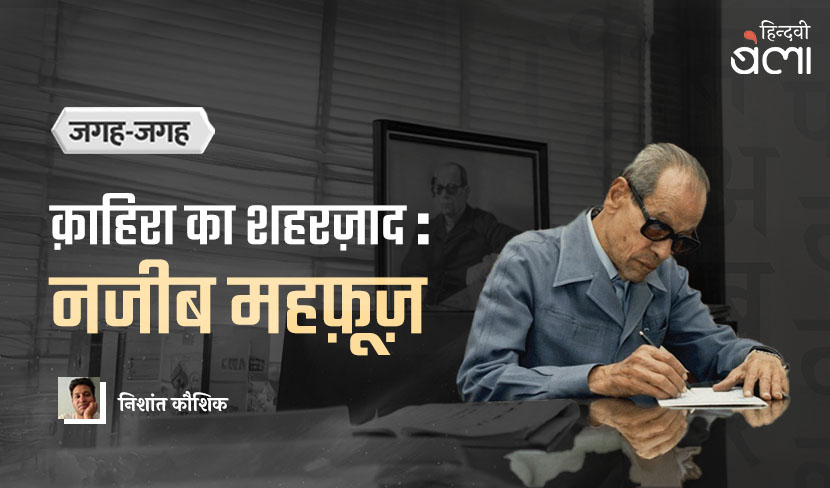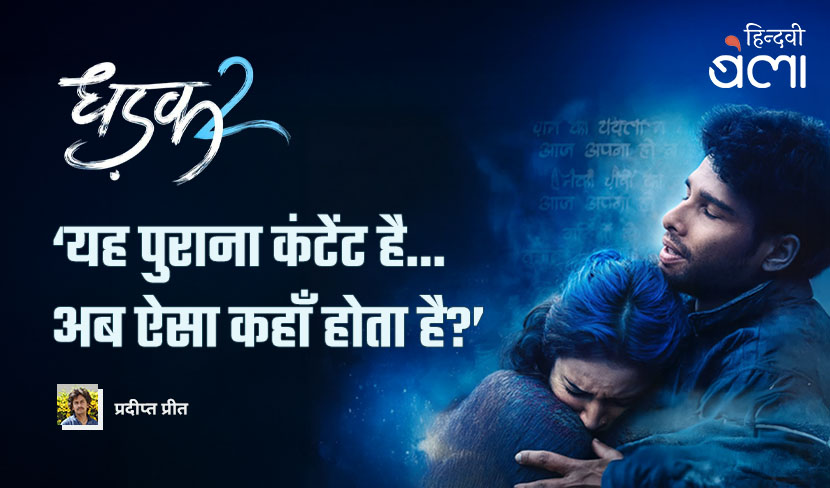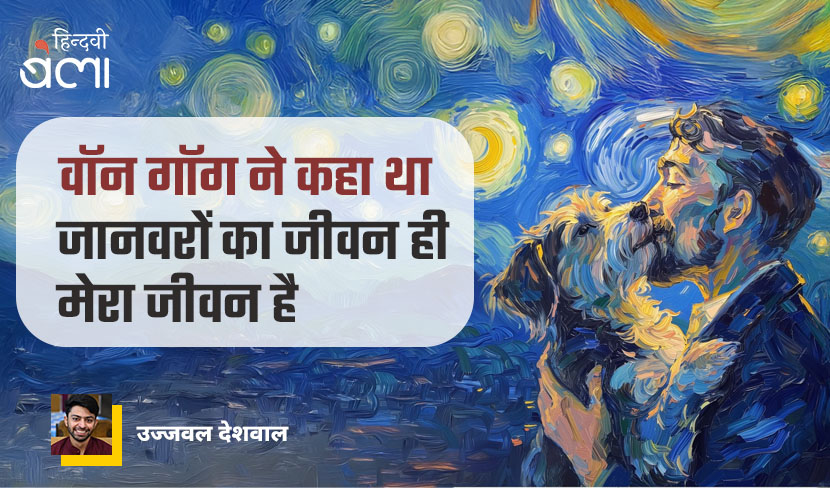माइथोलॉजी : देवदत्त पटनायक और उनका रचना संसार
 ध्रुव हर्ष
21 सितम्बर 2025
ध्रुव हर्ष
21 सितम्बर 2025

पटनायक ग्रीक मिथकों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखना जानते हैं, और उनकी सबसे बड़ी ख़ूबसूरती यह है कि वह बहुत सरल ढंग से कहते हैं। तब यह बात और दिलचस्प हो जाती है, जब ये सब कहते हुए वह अपना भारतीय होना नहीं भूलते।
—नील गैमन
निसंदेह देवदत्त पटनायक ने माइथोलॉजी के प्रति लोगों में एक उत्कंठा पैदा की है। उनका ‘स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस’ भारत की संस्कृति, लोक के चरित्र और मनोविज्ञान को बख़ूबी समझता है। उन्होंने वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत को न केवल पढ़ा है, बल्कि उसको आत्मसात भी किया है। वह देवी-देवताओं, पर्वों, त्योहारों, बिंबों, चित्रों, मंदिरों, मूर्तियों के आकार, धर्म, नीति, न्याय, मानवीय संबंधों, विवाह, प्रेम, आलिंगन, कामुकता, संभोग, लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर अंतरसंबंधों को किसी वैज्ञानिक की तरह मिथकों का सहारा लेकर डिकोड करते हैं। वह किसी धर्मगुरु या गॉडमैन की तरह बात नहीं करते। न ही, वह कहीं कुछ बोलते हुए अतिवादी दिखते हैं। वह आस्तिकता-नास्तिकता के बीच की कड़ी हैं। पॉलिटिकली वह किसी खेमेबाज़ी में नहीं पड़ते। जिसे धर्म में आस्था है, वह भी पटनायक को पढ़ता है; जिसकी आस्था नहीं है और मिथकों को एक कल्चरल टेक्स्ट/सिग्निफ़िकेंस की तरह देखता है, वह भी। वह राइट, लेफ़्ट, लिबरल सबके चहेते हैं। धर्म को देखने का उनका अपना नज़रिया है। वह मिथक को ‘कल्चरल और सब्जेक्टिव ट्रुथ’ मानते हैं। उनका कहना है कि जो घटा नहीं, वह क़िस्सों और कहानियों में नहीं आ सकता है।
रामायण-महाभारत जैसी कहानी आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन वे हमारी चेतना में इस तरह शामिल है कि हमें अपने लोककथा और पुरखों की महागाथा लगती है, जो वर्तमान को हर क़दम पर आगाह करती रहती है। महाभारत में आदर्शवादी राजा भरत समय-समय पर अपने वंशजों के सपनों में आकर उन्हें मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई दृष्टांत हैं, जब उन्होंने अधर्म के रास्ते पर चल रहे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र को बेचैन किया था। ऐसे ही हिंदू धर्म में पितरों का भी बहुत महत्त्व है। ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज भी हमें समय-समय पर रास्ता दिखाते हैं। इसी तरह हमारी माइथोलॉजी भी हमें गाइड करती रहती है। हमें अच्छाई, बुराई, धर्म, अधर्म और उसकी परिणति का पता चलता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर हम कहाँ पहुँच सकते हैं और अति महत्त्वाकांक्षा, लालच, असत्य और व्यभिचार हमें कहाँ ढकेल सकता है। मिथक कोई कल्पना नहीं, बल्कि मानवों के स्वभाव और जिजीविषा का एक अनूठा दस्तावेज़ है, जिससे हम अपने भूत, वर्तमान और भविष्य को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं या कहें तो भूत को समझते हुए वर्तमान को गढ़ सकते हैं, ताकि भविष्य को एक नई दिशा दी जा सके। गौर करें तो—समय, काल, परिस्थिति के अनुसार आज का यथार्थ भी आने वाले हज़ारों साल बाद मिथक में परिवर्तित हो सकता है। वह सब कुछ मिथक मान लिया जाता है, जो हम इंसानों के पहुँच से बहुत दूर है या होना असंभव जैसा जान पड़ता है। जैसे आप महात्मा गांधी का ही उदाहरण ले लें। उनके मरणोपरांत आइंस्टाइन ने कहा “आने वाली नस्लों को मुश्किल से यकीन होगा कि इस धरती पर कोई ऐसा हांड-मांस का पुतला कभी पैदा हुआ था।”
यह मानने की ही बात है कि बुद्ध और महावीर को भी हिंदू भगवान ही मानते हैं। जो नहीं मानते, उनके लिए हीनयान, महायान, जातक या त्रिपिटक भी मिथक हैं और बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी। भारत के महाकाव्यों—वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाभारत और रामायण पर बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ लिखी गई हैं। पटनायक ने उन टिप्पणियों को आज के समय के हिसाब से, बड़े, बूढ़ों, युवाओं, बच्चों के लिए एक नई भाषा विकसित करके उन्हें पेश किया है। उनकी लेखनी आज के बच्चों के लिए, जो जे के राउलिंग, नील गैमन, जे आर आर टॉलकिन को पढ़ते हैं, उन्हें भी पसंद आती है। देवदत्त पटनायक अपनी किताब ‘मिथक = मिथ्या’ में लिखते हैं :
अनंत मिथकों में ही एक शाश्वत सच छुपा है,
ये कौन देख पाता है?
वरुण के पास हज़ार आँखें हैं,
इंद्र के पास सौ,
तुम्हारे और मेरे पास तो केवल दो।
तमाम विद्वानों और किताबों ने माइथोलॉजी को ‘स्टोरी ऑफ़ द पीपल’ और उनकी अभिव्यक्ति कहकर परिभाषित किया है। मिथक को परिभाषित करना उतना ही मुश्किल है जितना धर्म को। आप बस उसकी विशेषता समझ सकते हैं, अर्थात् मूल तत्व को जो किसी महाकाव्य को मिथक के परिधि में रखते हैं। ऐसे तो माइथोलॉजी पारंपरिक कहानियों का संग्रह है, जिसमें तमाम अलौकिक प्रक्रियाएँ, सांस्कृतिक मूल्य, वस्तुओं की उत्पत्ति, सृष्टि का निर्माण, प्राकृतिक घटनाएँ, सामाजिक संरचना और दैवीय हस्तक्षेप या आदेश को किसी धर्म और आस्था के साथ जोड़कर देखा जाना माइथोलॉजी है। दैवीय हस्तक्षेप की बात करें तो महाभारत में कृष्ण उस समय दख़ल देते हैं, जब चारों तरफ़ असंतुलन व्याप्त है; मतलब धर्म की स्थापना का अर्थ संतुलन लाना है। कृष्ण उस स्थिति में पांडवों के साथ खड़े होकर धर्म की रक्षा करते हैं। वह अपने लक्ष्य से भटके अर्जुन को गीता का उपदेश देकर सही मार्ग पर लाते हैं। इन कहानियों को पुश्त-दर-पुश्त जनश्रुतियों में ज़िंदा रखा गया है, जिसे आज हम मिथक कहते हैं। गीता आज भी अपनी वैज्ञानिकता की वजह से दुनिया के चर्चित ग्रंथों में है। हिंदू उसे अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानते हैं। यहाँ तक कि जर्मन विद्वानों (ओरिएंटल फिलोसफर) ने उसे सबसे प्रासंगिक माना है। विद्वान मारिया लीच और जेरोम फ़्राइड ने मिथ के विषय में कहा है : “मिथ वैज्ञानिक भाषा में तत्वों की व्याख्या विज्ञान युग से पहले करता है।” कार्ल युंग कहता है : “मिथ इंसानों के दिमाग़ का एक आवश्यक पहलू है, जो इस दुनिया में अर्थ और संतुलन लाता है; मतलब एक ऑर्डर जिससे प्रकृति अपने मूल स्वरूप में लौट जाती है।”
देवदत्त पटनायक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट धर्मों और मिथकों के साथ-साथ नॉर्स (नॉर्वेजियन), ग्रीक, चाइनीज़, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन मिथकों पर भी लिखते रहते हैं। मिटती सभ्यताओं के साथ इंसानों ने अपने पुराने देवी, देवताओं, प्रतीकों को भी दफ़्न कर दिया। कई देवता और मिथक बदलते वक़्त के साथ इर्रेलेवेंट हो गए। जैसे अब ओडिन, विदार, लोकी, फ्रेया, थॉर और उनके साथ कई पेगन देवताओं को लोग भूल चुके हैं। ऐसे ही ग्रीक देवता ऑपोलो, जियस, प्रोमिथियस की अब पूजा नहीं होती। होमर के महाकाव्य ‘इलियड’ और ‘ओडिसी’ में जिन देवताओं और महामानवों की बात की गई है, उन सबको बस मिथकों तक ही सीमित रखा गया। बाद के धर्मों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। बस अब तक दुनिया में अगर सबसे जीवंत कोई माइथोलॉजी है, तो वो भारतीय माइथोलॉजी और उसके देवता हैं, जिनकी आज भी पूजा होती है। शुरुआती मिथकों और सभ्यताओं की तरफ़ अगर ध्यान दें, तो बहुत समानता है, भले ही वे भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग हों। उनके परिधान और भाषा अलग हों। जैसे ग्रीक, चाइनीज़ और हिंदू मिथकों में कई देवता एक जैसे हैं। जियस को हिंदू मिथकों में इंद्र और चाइनीज में नुवा की तरह देखा जाता है। प्रोमिथियस को हिंदू माइथोलॉजी में अग्नि देवता और चाइनीज़ माइथोलॉजी में फू सी (फुक्सी) कहा जाता है। नॉर्स माइथोलॉजी में आसमान में बिजली चमकती है, तो मान्यता है कि थॉर का रथ आसमान में दौड़ रहा है। भारतीय माइथोलॉजी में लोग कहते हैं—इंद्र का वज्र है जो आसमान में चमक रहा है। मिथकों में ऐसी समानताएँ आपको अक्सर मिल जाएँगी। होमर की ‘इलियड’ और ‘ओडीसी’ की तुलना भारतीय महाकाव्य ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ से की जाती है। मेसोपोटामिया का मशहूर मिथक ‘मिथ ऑफ़ गिलगमेश’ में ऐसे कई दृष्टांत हैं जो रामायण और महाभारत के चरित्रों से मेल खाते हैं। दुनिया की पुरानी संस्कृति और सभ्यताएँ, चाहे वो भारत की हों, चाहे ग्रीस या नॉर्वे की, आपस में इतनी मिलती जुलती हैं कि उन्हें पढ़ने पर लगता है कि सारी मानव सभ्यता का केंद्र बिंदु एक रहा है, उनकी कहानियाँ और मानवीय संवेदनाएँ एक रही हैं। उनके संस्कृतियों और सभ्यताओं का आदान प्रदान होता रहा है।
मिथकों के घटनाक्रम और उसकी समय के साथ अनुबंध को मानवीय प्रयासों से टाला नहीं जा सकता है। कार्ल युंग और कैंपबेल ने ‘ईडिपस’ को अध्ययन करते हुए ये पाया कि जो चीज़ें घटित होने वाली हैं या मनुष्य के भाग्य में हैं, उसे कितना भी चाहकर इंसान बदल नहीं सकता। ईडिपस भाग्य से पीछा छुड़ाने के लिए इधर-उधर भागता फिरता है, लेकिन अनजाने में वह जिस व्यक्ति को मारता है—वह उसका पिता लियस, थेब्स का राजा है, और जिस महिला से वह शादी करता है, वो उसकी माँ जोकास्टा है। आख़िरी में जब उसे यह सब पता चलता है, तो वह ख़ुद को अंधा करके आत्महत्या कर लेता है। मिथक भी किसी ऐसे रहस्य का पैंडोरा बॉक्स है जो समय के साथ इंसान के जीवन में तमाम किस्म की दर्द, पीड़ा, ख़ुशी और अवसाद लेकर आता है। कभी राजा को रंक, कभी रंक को राजा बना देता है; कभी किसी मृत व्यक्ति को जीवन मिल जाता है, तो कभी किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। कभी एक धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कठोर-से-कठोर परीक्षाओं से गुज़रना पड़ता है, तो कभी एक कपटी और भ्रष्ट व्यक्ति को ऐश्वर्य और सत्ता मिल जाती है। लेकिन समय सबका हिसाब रखता है। कभी-कभी दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी बहुत आसानी से मार दिया जाता है, और कभी डेविड जैसा एक चरवाहा दैत्याकार भीमकाय गोलियथ को एक पत्थर के टुकड़े से मार देता है। भाग्य और समय के सामने न तो कोई मानव टिकता है और न ही महामानव। वह सबको एक कसौटी पर रखकर तौलता है। होमर के महाकाव्य ‘इलियड’ में, राजकुमारी ब्रिसियस से प्रेम में पड़कर अकिलीस जैसा महान् योद्धा भी ट्रॉय के राजकुमार पैरिस के हाथों मारा जाता है। वेदव्यास रचित भारत के महान् ग्रंथ ‘महाभारत’ में कृष्ण, जो स्वयं सर्वविदित और धर्म के रक्षक हैं, उनके कुरुभूमि में उपस्थित होते हुए उनका ख़ुद का भांजा अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त होता है, और वह हस्तक्षेप नहीं करते। इन सारी संभावनाओं, होनी और अनहोनी को मिथकों का महाकाव्य कहते हैं, जिसको पटनायक बहुत करीने से देखते हैं और उसको अपने तर्क से सिद्ध करते हैं या आपको उसके मूल में लेकर जाते हैं।
देवदत्त पटनायक का नाम पहली बार 2009 में सुना था। पता लगा था उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अँग्रेज़ी विभाग के एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में आना था, जहाँ वह किसी कारणवश नहीं आ पाए थे। उनके नाम से परिचित होने के बाद थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्फिंग से पता चला कि वे पेशे से डॉक्टर हैं और लगभग डेढ़ दशकों तक अपोलो व अन्य फार्मेसी कंपनियों के लिए बतौर मेडिकल प्रोफ़ेशनल काम किया है, हालाँकि उनकी दिलचस्पी मिथकों में है और वह बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर हैं। अभी उनके रचनाधर्मिता के विषय में मोटा-मोटी इतनी ही जानकारी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अँग्रेज़ी में एम. ए. ख़त्म करने के बाद वहीं पी. एच. डी. में दाख़िला मिला और जब विषय चुनने की बात आई, तो मेरी सुपरवाईजर प्रो. वंदना शर्मा ने चित्रा बनर्जी दिवाकरूनी का द्रौपदी पर आधारित उपन्यास ‘द पैलेस ऑफ़ इल्यूशंस’, शशि थरूर का ‘द ग्रेट इंडियन नॉवेल’, विक्रम चंद्रा का ‘रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन’ और देवदत्त पटनायक का ‘द प्रेग्नेंट किंग’ सुझाया। इन चारों उपन्यासों की पृष्ठभूमि महाभारत थी या इनके कथानक कहीं-न-कहीं महाभारत से प्रभावित थे।
महाभारत पर कुछ लिखना जितना आसान लगता है, उतना ही जटिल है। किरदारों और उनके चरित्र में बहुत पेचीदगी है। चूंकि नैरेटिव पहले से लोक का हिस्सा है, ओरल ट्रेडिशन में सदियों से ये कथा सुनी-सुनाई जाती रही है, इसलिए कुछ भी इधर-उधर होने से आम जनमानस की स्वीकृति आसानी से नहीं मिलती। मसलन, जब तक लेखक की कोई अलग दृष्टि न हो, कोई भी उपन्यास, कहानी या नाटक अपनी पहचान नहीं बना पाता। चित्रा बनर्जी दिवाकरूनी का उपन्यास ‘द पैलेस ऑफ़ इल्यूशन’ ने द्रौपदी के किरदार को एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। दिवाकरूनी ने द्रौपदी को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा है। एक महिला जो शताब्दियों से न्याय को लेकर वंचित रही। भरी सभा में जिसका अपने पतियों, कुल खानदान, बड़े-बुज़ुर्गों, पिताओं और पितामहों के सामने अपमान हुआ, उसे क्या चाहिए था? इतने शूरवीर और धर्मशास्त्र के ज्ञाताओं के होते हुए द्रौपदी अपने सखा कृष्ण की तरफ़ क्यों देखती हैं? महारथी कर्ण से उनके कैसे रिश्ते थे? यदि द्रौपदी को कर्ण के उत्पत्ति के विषय में पता होता, तो क्या द्रौपदी उनको सूत-पुत्र कहकर उनका इस तरीक़े से उपहास उड़ाती? या कि यदि वे पांडवों के साथ होते, तो क्या वे भी सभी भाइयों की तरह द्रौपदी को प्रेम और भोग करते? दिवाकरूनी एक ऐसी व्याख्या गढ़ती हैं। वह द्रौपदी और कर्ण को लेकर उनके सीक्रेट क्रश की बात करती हैं। महाभारत तमाम संभावनाओं, घटित होने और न होने की भी कथा है। मनः स्थिति और द्वंद्व की कथा है। मानवीय और अमानवीय किरदारों की कथा है। मनुष्यों में जितनी अच्छाई और विसंगतियाँ हो सकती हैं, उसकी कथा है।
अपने शोध के दौरान मैंने इन लेखकों को एक-एक करके पढ़ना शुरू किया। मुझे सभी बहुत दिलचस्प लगे। जब बारी पटनायक की आई और मैंने उनका उपन्यास ‘द प्रेग्नेंट किंग’ पढ़ना शुरू किया, तो बिना रुके पढ़ता गया। भाषा बहुत सरल थी और कथानक बहुत दिलचस्प लगा। ऐसे देखा जाए तो उपन्यास महाभारत पर प्रत्यक्ष रूप से आधारित नहीं है, बल्कि उसके आस-पास की कहानी है। कई जगह महाभारत के प्रसंग आते हैं। कहानी एक राजा की है, जो निसंतान है; यज्ञ, पूजा अर्चना के बाद एक ऋषि राजा को कोई द्रव्य देते हैं और कहते हैं कि अपनी पत्नियों को पिला दें, लेकिन ग़लती से उस द्रव्य को राजा स्वयं ग्रहण कर लेता है। फलस्वरूप वह गर्भ धारण कर लेता है। पटनायक ने इस उपन्यास में ऐसे कई ‘क्वीयर’ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाया गया है। उन्होंने अपने मिथकों से ऐसे कई दृष्टांत लिए हैं, जहाँ पुरुषों ने स्त्री रूप धरा है और स्त्रियों ने पुरुषों का। जैसे अर्जुन ने बृहनला का, कृष्ण ने मोहिनी का। यहाँ तक कि कृष्ण ने मोहिनी बनकर अर्जुन और उलूपी के पुत्र इरावन से विवाह किया था, ऐसा भी एक दृष्टांत पटनायक अपने उपन्यास में प्रस्तुत करते हैं। एफेमिनेट होना हमारे समाज में ग़लत समझा जाता है, जबकि हमें कृष्ण के शृंगार से कोई आपत्ति नहीं होती। पटनायक ने अपने उपन्यास में दिखाया है कि एक पुरुष के अंदर भी ममता होती है। वह भी एक स्त्री की तरह व्यवहार करना चाहता है। वह दिखाते हैं कि कृष्ण भी अपने स्त्री रूप पर मोहित हो जाते हैं। जब वह दैहिक आनंद की बात करते हैं, तो कहते हैं कि स्त्री की काया ज़्यादा आकर्षक होती है। पटनायक अस्तित्व के मूल में जाते हैं। वह तन और मन दोनों की बात करते हैं। उनका क्वीयर होना किसी दर्द और विषाद की महागाथा न होकर उसके एक्सेप्टेंस में है। किसी रचनाकार के रचनाधर्मिता को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ज़रूरी है। पटनायक मूलतः उड़िया हैं, पैदाइश मुंबई की है। वह गे हैं और इसे बहुत सहजता से स्वीकार करते हैं। पटनायक माइथोलॉजी को बहुत ही प्रैक्टिकल होकर समझाते हैं। वह पॉप कल्चर को बख़ूबी समझते हैं। उन्होंने मिथ को मैनेजमेंट के साथ जोड़ा है। उनका मानना है कि व्यक्ति की रुचि और उपभोग करने की इच्छा कहीं-न-कहीं रिचुअल और उसकी आस्था से प्रभावित है। अध्यात्म इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उनकी दृष्टि व्यक्ति के मूल बनावट में है; वह कैसे क़िस्से-कहानियों से बना है। मिथकों ने उसे कैसे प्रभावित किया है। आस्था, अपराधबोध, प्रायश्चित उसके मनोविज्ञान को किस तरह प्रभावित करते हैं। इन सारे विषयों पर वह खुलकर बात करते हैं। उनका रचना संसार बड़ा है। अब तक लगभग उन्होंने पचास के क़रीब अलग-अलग कई विषयों पर काम किया है और सैकड़ो लेख लिखे हैं, जो अपने अलग कथ्य और रोचकता के लिए पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे हैं।
उन्होंने महाभारत, रामायण, गीता, पुराण, शिवपुराण, विष्णु पुराण और ग्रीक माइथोलॉजी जैसे और तमाम विषयों पर गहन चिंतन कर उसे नए ढंग से प्रस्तुत किया है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
07 अगस्त 2025
अंतिम शय्या पर रवींद्रनाथ
श्रावण-मास! बारिश की झरझर में मानो मन का रुदन मिला हो। शाल-पत्तों के बीच से टपक रही हैं—आकाश-अश्रुओं की बूँदें। उनका मन उदास है। शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। शांतिनिकेतन का शांत वातावरण अशांत
10 अगस्त 2025
क़ाहिरा का शहरज़ाद : नजीब महफ़ूज़
Husayn remarked ironically, “A nation whose most notable manifestations are tombs and corpses!” Pointing to one of the pyramids, he continued: “Look at all that wasted effort.” Kamal replied enthusi
08 अगस्त 2025
धड़क 2 : ‘यह पुराना कंटेंट है... अब ऐसा कहाँ होता है?’
यह वाक्य महज़ धड़क 2 के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यह ज्योतिबा फुले, भीमराव आम्बेडकर, प्रेमचंद और ज़िंदगी के बारे में भी कहा जा रहा है। कितनी ही बार स्कूलों में, युवाओं के बीच में या फिर कह लें कि तथा
17 अगस्त 2025
बिंदुघाटी : ‘सून मंदिर मोर...’ यह टीस अर्थ-बाधा से ही निकलती है
• विद्यापति तमाम अलंकरणों से विभूषित होने के साथ ही, तमाम विवादों का विषय भी रहे हैं। उनका प्रभाव और प्रसार है ही इतना बड़ा कि अपने समय से लेकर आज तक वे कई कला-विधाओं के माध्यम से जनमानस के बीच रहे है
22 अगस्त 2025
वॉन गॉग ने कहा था : जानवरों का जीवन ही मेरा जीवन है
प्रिय भाई, मुझे एहसास है कि माता-पिता स्वाभाविक रूप से (सोच-समझकर न सही) मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वे मुझे घर में रखने से भी झिझकते हैं, जैसे कि मैं कोई बेढब कुत्ता हूँ; जो उनके घर में गंदे पं