सौंदर्य की नदी नर्मदा : नर्मदा के वनवास से अज्ञातवास की पूरी कहानी
 यतीश कुमार
07 दिसम्बर 2024
यतीश कुमार
07 दिसम्बर 2024
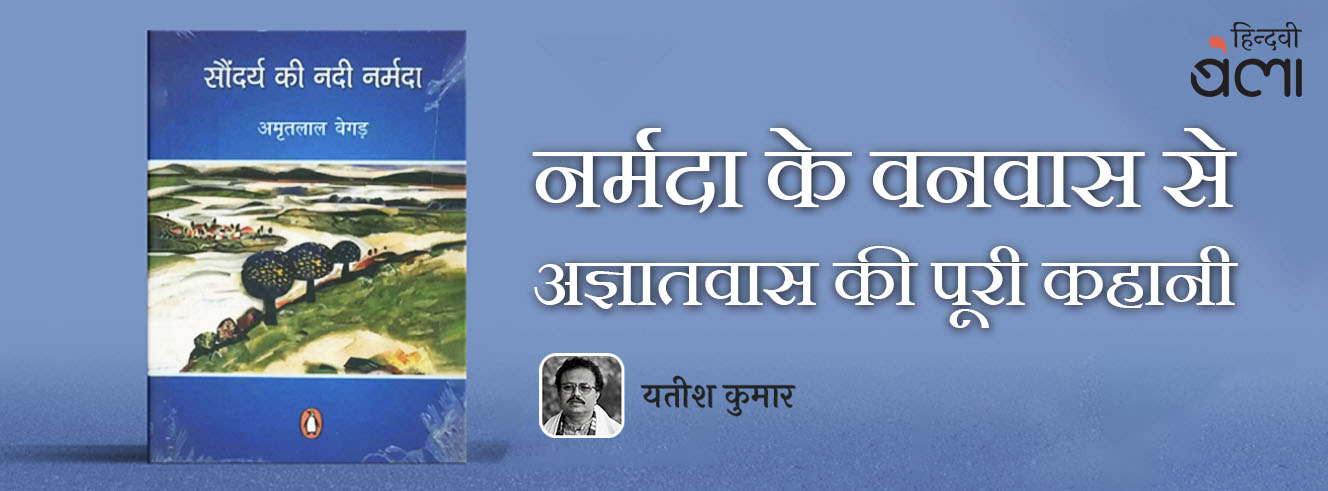
“सौंदर्य उसका, भूल-चूक मेरी!” शुरुआती पन्नों में ही यह पंक्ति लिखकर लेखक अपनी मंशा बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। सारे ग्रह से लेकर परमाणु तक सब अपनी-अपनी कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं और इसी तरह प्रत्येक पदार्थ के भीतर उसकी अपनी परिक्रमा जारी है। इसलिए कई बार मुझे लगता है कि इन सब से परे अपनी एक सजग परिक्रमा करने निकले हैं—अमृतलाल वेगड़। शिल्प से भाषा तक की ऐसा सूक्ष्म फेरबदल कोई साधक या योगी ही कर सकता है।
सभी सामाजिक लगावों से विरत होकर नर्मदा के हर पल बदलते रूप का दर्शन करने अमृतलाल वेगड़ बार-बार पहुँचते हैं और फिर अपने अनुभव की बाँच रचते हैं। सहज भाषा की सिद्धि विरल होती है। अपने संपूर्ण समर्पण के तदुपरांत जो अनुराग साहित्य संग गुना जाता है, उसी से ऐसी भाषा-सरिता निकलती है और इसलिए इस पुस्तक में उक्ति की सूक्ति पनकौवे की तरह रह-रह कर उभरती है।
यह यात्रा वृत्तांत सिर्फ़ पथ-प्रांतर और वन-वनांतर की नहीं है बल्कि यात्रा के क्रम में अपने भीतर होते हुए शुद्धिकरण की भी है जो कि अंदर घटते विघटन का प्रतिफल भी समझा जाती है। “यह एक द्रष्टा जिसके भीतर तादाम्य से अलगाव तक की भावना एक साथ निहित हो, जो करुणा के साथ हास्योद्रेक परिस्थिति को भी एक साथ साधता हो, जो प्रकृति और जीवन के इस अखूट सौंदर्य को साथ-साथ उकेरने की क्षमता रखता हो और जो नर्मदा से बालहठ लिए रूठता हो, जिसे चिंता है कि भीतर का दीया क्यों नहीं जलता और इसी हठ में वो तट पर दिया नहीं जलाता और फिर एक बच्चे के माफ़िक़ दादू के समझाते ही निर्मल भाव में डूबकर दिया बालता हो, स्वान्तः सुखाय को बहुजन सुखाय की कथा में बदलने वाले प्यारे अमृतलाल वेगड़ के समयांतराल में घूमी और लिखी गाथा है।”
पढ़ते हुए मालूम पड़ता है जैसे कोई बालक सृष्टि रचना को अचंभित दृष्टि से देख रहा हो। सोंचता हूँ उगते हुए बड़े नारंगी सूरज की तुलना जब लेखक ने नवजात बच्चे की त्वचा की कोमलता से की होगी तो उस पल उनका मन कितना पवित्र रहा होगा। इस यात्रा के दौरान ऐसी मीठी पंक्तियाँ ओस-सी यों टपकती हैं कि आँख और मन दोनों तृप्त हो उठे।
यह यात्रा वृत्तांत उसी दृष्टि से वलयाकार, वक्रीम भाप की उठान और वक्र गतिप्रियता से उभरते चलचित्र को निहारते और सिरजते हुए अपने प्राकृतिक विस्तार से गढ़ी गई है। इस वृत्तांत में नर्मदा कभी क्रोधित उफान लिए तो कभी मौन की दीक्षा देती जलधारा तो कभी बनबाला से शैलबाला बनती दिखाई देती है।
लेखक चाँद को एक कैनवास की तरह देखते हैं इसलिए नर्मदा में उभरते रंग का वर्णन करने के क्रम में उसके भीतर से वही चित्र उभारते हैं—“कहीं नीला, कहीं बैंगनी, तो कहीं हरा है। दूर भूरा है।” यह दूर भूरा है—लिखना लेखक के दर्शन भाव से ओत-प्रोत दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। कभी लेखक सूरज और चाँद के आपस में बदलते कपड़े की बात करते हैं, तो कभी ललछौहां सूरज से नर्मदा को सुनहरे किरणों में नहाने की।
जब वेगड़ लिखते हैं—“सूरज की रोशनी जब-जब चंद्र ताल में नहाती है तो चाँदनी बन जाती है।” तब लगता है हम कहाँ शहर में कीड़े-मकोड़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसे ज़िंदगी नाम देना उसकी तौहीन ही है।
हर आगे बढ़ते पन्ने के साथ मन भी उस ओर भागने की तीव्रता पकड़ता जाता है, जहाँ अमरकंटक में किसी का डेरा है—जहाँ सोनभद्र, नर्मदा और जुहिला की कहानी अब भी कई परतें खोलने को बेचैन है। घरोबा होना तो कोई इस प्रकृति प्रेमी से सीखे जहाँ गया वहीं का हो गया। जिसने पनाह दिया उसी के घर का हो गया। पानी, चट्टान, प्रपात, शोर और मोड़ से बनी खेतों और आत्मा दोनों को एक साथ तृप्त करने वाली नदी को लेखक ने एक मूर्तिकार की दृष्टि से देखा है, जो कई बरस से सख़्त पत्थरों पर अपने निशान छोड़ अपनी चित्रकारी कर रही हो।
पश्चिम वाहिनी नर्मदा को कपिलधारा से निकलते देख मुझे ख़ुद भी विश्वास नहीं हुआ था कि नर्मदा का स्रोत यहीं-कहीं है, लेकिन आज जब इस किताब को पढ़ रहा हूँ तो नर्मदा यानी रेवा, मेकलसुता के सारे रूप जैसे सामने चलचित्र भाँति निकलते जा रहे हैं। एक नाले-सा उद्गम, कब हुंकार भरती नदी, कब चीत्कार करता जल प्रपात में बदल जाता है, पता नहीं चलता। उद्गम से संगम की यह यात्रा शिशु को प्रौढ़ और फिर अनुभवी बुज़ुर्ग बनते देखने जैसी है।
यात्रा वृत्तांत न सिर्फ़ नदी निहारने का अलौकिक वर्णन है, अपितु उसके किनारे बदलते संस्कार और संस्कृति का रोचक चित्रण भी है। अमरकंटक की मेकल पहाड़ी से उतरते हुए किरंगी गाँव की एक लोक-परंपरा का ज़िक्र अमृतलाल वेगड़ ने किया है—“वहाँ आम का विवाह विधिवत कराए बिना रिवाज है कि आम नहीं तोड़ा जा सकता।”
लेखक का मानना है कि गाँव के कठोर जीवन में ऐसे अनुष्ठान और ऐसी परंपराएँ उनके जीवन में रस घोलने का काम करती हैं।
खरमेर और देवनाला जैसी अद्भुत जगहों के बारे में पढ़ने के बाद मन बेचैन हो उठता है, मानो किताब कह रही हो कि अभी उठो और उन गुफ़ाओं के साथ उसके ऊपर से बहते झरने को देख आओ। पुस्तक की एक और ख़ास बात है कि हर मोड़ पर मददगारों और पनाहगारों का ज़िक्र है। इसकी निश्छलता ही पूरी यात्रा का यूएसपी है। यह कहीं से घी, आटा, चावल, तो कहीं रहने की जगह और इस सबसे ज़्यादा स्नेह और प्रेम भाव थोक में मिलने की यात्रा है।
कनई संगम पर गोसाईं जी के भाई का रात में यूँ नर्मदा पार कर के मिलने आना मानुस के निश्छल प्रेम का असाधारण उदाहरण है। नर्मदा तीर पर बनी हुई कुटिया मानो लेखक और उनके साथी मित्र के ठहरने के लिए ही बनी हों। इनके विविध आतिथ्य का भावपूर्ण वर्णन किताब के समानांतर चलता रहता है और यह आपके भीतर सकारात्मकता का दिया बालेगा।
सभी छोटी-बड़ी बातों का सुगठित पंक्तियों में इतना सुंदर विवरण है कि मुझे यही लग रहा है यहाँ किसका ज़िक्र करूँ और किसको छोड़ दूँ। लगता है जैसे किसी अदृश्य डोर में सबकुछ बँधा है कि बीहड़ में भी व्यवस्था अपनी जगह संतुलन बनाए मिलती है। लोगों के बीच कीर्तन, भजन और राग मिलकर किस तरह जीवन राग का निर्माण एक झलक है। मंदिर निर्माण के पीछे शरण्य का ध्येय यहाँ आपको आकर्षित करेगा। यात्रा क्रम में लेखक कई बार मंदिर में शरणार्थी होते हैं जो इस बात का प्रमाण है कि मंदिर सिर्फ़ मूर्ति पूजा के लिए नहीं बल्कि मानुष पूजा के लिए भी है। पुजारियों का जो मनोभाव यहाँ बारम्बार प्रस्तुत होता है, वह आपको मंदिर के स्थापना के एक और उद्देश्य से परिचय कराता है।
जगहों के साथ वहाँ की कला-साहित्य-संस्कृति पर लेखक की दृष्टि हमेशा रही है, तभी तो वह सैला और रीना नृत्य शैली की बात करते हैं। नृत्य के साथ पूरे रास्ते चाँद के विविध रूपों की झलक सूरज से ज़्यादा मिलेगी। रास्ते में एक पचहत्तर साल के बुज़ुर्ग परकम्मावासी का यह बताना कि वह समुद्र को नहीं लांघते इसलिए जिलहरी परिक्रमा कर रहे हैं। यह आपको एक और आश्चर्य में डाल देगा।
इस उम्र में अकेले किस आस्था और विश्वास के बल पर वह यात्रा में थे—यह समझना हम जैसे पाठकों के लिए आसान नहीं है। एक तरफ़ जिलहरी परिक्रमा तो दूसरी तरफ़ अखंड और फिर खंड परिक्रमा, जैसी शक्ति वैसी भक्ति वाली बात यहाँ सटीक लगती है। मुझे लगता है कि अलौकिकता एक ऐसी सुरंग है इसके भीतर जाने से डर लगता है।
पढ़ते हुए आप कई बार जीवन-दर्शन से भरी पंक्तियों पर ठहर जाएँगे। एक जगह लिखा है—“तारों की शोभा हम तभी देख सकते हैं जब चाँद न हो!” चीटियों के ग़ुब्बारे वाले घर का ब्योरा जितना रोचक है, पोली चोर रेत वाली घटना उतनी मार्मिक। रेत का रूप भयावह और ख़तरनाक रूप आपको भीतर तक हिला देगा।
आश्चर्य होता है कि सारे रास्ते लेखक को कहीं भी दूध की कमी नहीं हुई। हर जगह लगभग दूध पीने को मिला। जबकि शूलपनेश्वर से कबीरबड़ जाते हुए लगभग अकाल की स्थिति थी। पीने को पानी नहीं था, लेकिन दूध उपलब्ध था। सुखद यह भी है कि पूरे रास्ते उन्होंने छायाचित्र बनाना नहीं छोड़ा। प्रकृति और आकृति दोनों को अपने भीतर और काग़ज़ पर एक साथ उतारा। क्या ही अच्छा हो कि उन चित्रों की भी एक किताब प्रकाशित हो।
लेखक नर्मदा की सहेलियों का ज़िक्र किए बिना कहीं आगे नहीं बढ़ते। कभी दूधी, जामदी, कभी अंजनी तो कभी कुब्जा या चांदला, फिर कभी तवा, केवलारी या कावेरी। ये छोटे-छोटे प्रयाग उत्तराखंड के देव, रुद्र और कर्ण प्रयाग की याद दिला रहे हैं लेकिन एक असमानता जो मेरी समझ में आ रही है, वह है ‘अंत्येष्टि स्थल’—जो उत्तराखंड के लगभग हर प्रयाग के बग़ल में है। वह इस पुस्तक में कहीं पढ़ने को नहीं मिली। शिव का प्रयाग पर बिराजना शायद इस अंतर का भेद है।
लेखक चूँकि समयांतराल के साथ यात्रा करते हैं, तो बदलते सांस्कृतिक, राजनीतिक हस्तक्षेप पर भी अपने हस्ताक्षर करते चलते हैं। नर्मदा का बीच-बीच में टूटना, रुकना और फिर चलना निहारते हैं। चिंता व्यक्त करते हैं। बरगी, इंदिरा सागर या सरदार सरोवर जैसे बनते बाँध को कोसते हैं। यह पुस्तक नर्मदा के वनवास से अज्ञातवास की पूरी कहानी है। पच्चीस वर्ष बाद पायली दुबारा जाने पर लेखक सिर पीट लेता है कि कहाँ गए पेड़ और लताएँ जिन्हें देख उसे प्रकृति की सुंदरता पर घमंड हुआ करता था। “कुल्हाड़ियों ने क्या कर डाला भला!”
पत्नी की अँगूठी बेचकर की गई यात्रा—चीते, भैंसे और मगर की बातें, सदाव्रत जैसी सीखों से भरी, भील का पसरा आतंक समेटे, मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की हवा पानी को समेटने की बेहद सरल शब्दों में सफल कोशिश, सूक्तियों से भरी किताब अमरकंटक से विमलेश्वर तक स्रोत से गंतव्य तक फैला यह रेवा सागर संगम गाथा तट सौंदर्य के साथ तट जन जीवन गाथा भी है।
यह किताब नर्मदा को प्रकट होते, पुष्ट होते, लुप्त होते देखने का सुख है। नदी की तरह यह वृत्तांत भी सचल है। अमृतलाल वेगड़ ने जो लिख छोड़ा है, वह अनंत काल तक लोगों को नर्मदा परिक्रमा के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा। बेहतर मनुष्य, बेहतर प्रकृति प्रेमी और यहाँ तक कि बेहतर साधु बनने को भी प्रेरित करता रहेगा।
मैं मानता हूँ कि वेगड़ ने अपने गुरु आचार्य नन्दलाल बसु की बात को पूरी तरह निभाया है, जिसका सार है—“सफल नहीं सार्थक बने जीवन!”
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
