अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव
 वागीश शुक्ल
06 अक्तूबर 2025
वागीश शुक्ल
06 अक्तूबर 2025
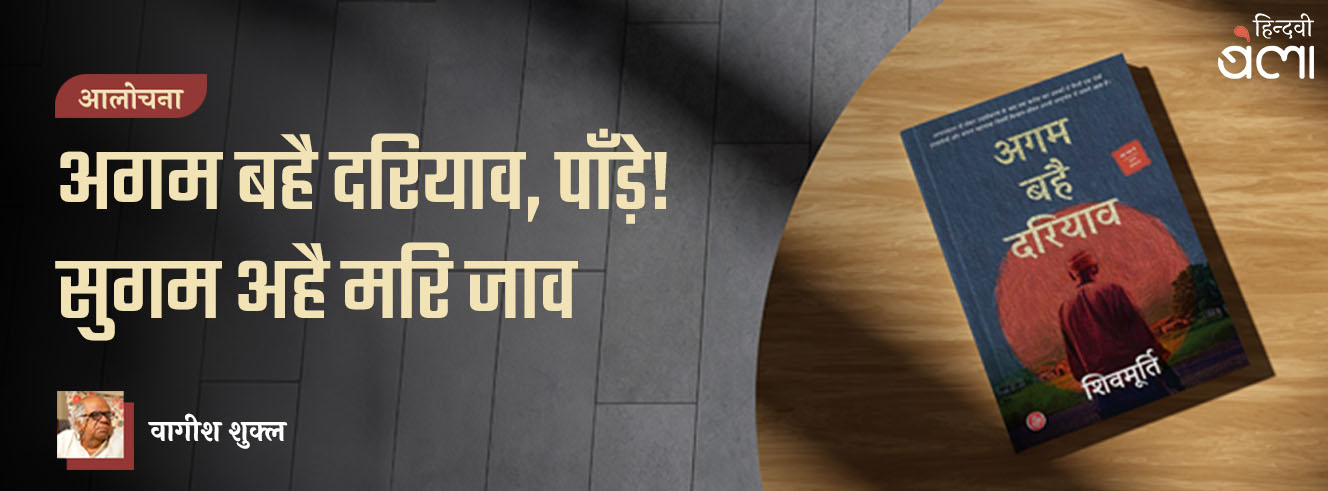
एक
पहलवान कुछ न समझते हुए भी पाँड़े बाबा का मुँह ताकने लगे तो उन्होंने समझाया :
अपने धर्म की व्यवस्था के अनुसार मरने के तेरह दिन बाद तक, जब तक तेरही नहीं हो जाती, जीव मुक्त रहता है। फिर कहीं न कहीं जन्म लेता है। मान लीजिए, फिर किसी किसान परिवार में पैदा हो गए। यानी जो कुछ झेलते-झेलते बूढ़े होकर मरे थे, उसी कुर्की-नीलामी-हवालात के नरक-कुंड में पहुँच गए तो? मरकर भी चैन नहीं मिलता। इस मामले में मुसलमानों के धर्म की व्यवस्था बढ़िया है। ज़िंदगी जैसे भी लंगे-नंगे कटे, लेकिन जब एक बार मर गए तो फिर पैदा होने के झमेले से जान छूटी। जब तक क़ियामत का दिन नहीं आ जाता, निश्चिंत हो कर अपनी कब्र में आराम फ़रमाते रहिए। क़ियामत कब आएगी, किसी को पता नहीं, अभी तक तो आई नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में अगर ऐसे चैन चाहिए तो अकाल मौत मरना पड़ेगा। रेल से कटकर, पानी में डूबकर, ज़हर खाकर या फाँसी लगाकर; क्योंकि अकाल मौत मरने पर आदमी न स्वर्ग में जाता है, न नरक में; न फिर पैदा होता है। प्रेत-योनि में भटकता रहता है। हम इसे भटकना क्यों कहें? स्वच्छंद विचरण करता रहता है। सूक्ष्म शरीर से वायुमंडल में जहाँ मर्ज़ी पहुँच जाइए। दुनिया की नज़र से दूर रहकर दुनिया का नज़ारा लीजिए। प्रेत-योनि माने आदर्श योनि। न कोई चिंता, न कोई शोक। परम स्वतंत्र, परम सुखी।
— अगम बहै दरियाव (शिवमूर्ति, राजकमल प्रकाशन, द्वितीय संस्करण : 2024, पृष्ठ 560-561)
दो
‘अगम बहै दरियाव’ का प्रकाशन होने के छह माह बीतते-बीतते ही उसका दूसरा संस्करण आना भी यह बताता है कि जब कोई अच्छी किताब आती है तो लोग उसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर यह बिकाऊ किताब न होती तो भी यह एक अच्छी किताब है। किताब थोड़ी देर से मेरे हाथ लगी और इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में यह जानने की उत्सुकता जगी कि इसे अन्य पाठकों द्वारा कैसे पढ़ा गया है। जब मुझे एक लंबी और प्रशंसा से लबालब समीक्षा दिखाई दी, जिसमें छत्रधारी सिंह का नाम निरंतर ‘क्षत्रधारी सिंह’ लिखा हुआ था और ‘किलो’ समय-रेखा पर पिछड़कर ‘सेर’ की शक्ल में विराजमान था तो मैंने ख़ुद कुछ लिखने की सोची।
तीन
यह उपन्यास जिन जगहों पर थोड़ा ध्यान देने से; मेरे ख़याल में थोड़ा और अच्छा हो जाता, उनमें से कुछ गिनाता हूँ :
1. पृष्ठ 567 पर तूफ़ानी का नाम तूफ़ानी सरोज लिखा हुआ है। यह उपन्यास जिस क्षेत्र में मौजूद है; उसमें ‘सरोज’ पासी जाति के लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं, किंतु तूफ़ानी पासी जाति के नहीं हैं।
2. इस उपन्यास के प्रारंभ में पृष्ठ 24 पर छत्रधारी सिंह के भाई का नाम ‘तिलकधारी सिंह उर्फ़ करिया सिंह’ बताया गया है। आगे चलकर तिलकधारी सिंह प्रधानी के चुनाव में छत्रधारी का साथ देते हुए छलपूर्वक विद्रोही जी को हरवाकर छत्रधारी सिंह को जितवाते हैं, किंतु कुछ और आगे करिया सिंह ठाकुर टोले के भीतर एक ऐसे अपवाद के रूप में हैं; जिनके दरवाज़े पर फगुआ गाने के लिए सारा गाँव सहर्ष आमंत्रित है, यहाँ तक कि दलित टोले के लोग भी आए हुए हैं। यह न खटकता, अगर ये दोनों भिन्न पात्र होते।
3. पृष्ठ 138 पर सुनरा अइया द्वारा गाया जाने वाला एक गीत दिया हुआ है :
आज तुमड़ी में भाँग घोटाउ रसिया
मातल मदन रैन अँधियारी
रैन अँधियारी, रैन अँधियारी
टोउ न टाउ सोझै डाउ रसिया
आज तुमड़ी में भाँग घोटाउ रसिया॥
जिसकी चौथी पंक्ति मेरी समझ में सोझै डायु, न टोउ, न टाउ रसिया होनी चाहिए।
4. पृष्ठ 49 पर है :
खेतिहर मज़दूरों का दर्द उनके गीतों में मुखर होता रहा है—
बाबू के बखार भरीं कइकै हलवाहीं
बिटिया बहिन मिलि करें लगवाहीं
कइसे गुजारा होये दुइ अँजुरी मा?
दलित सतावा जाँय यह नगरी मा॥
जिस गीत में ‘दलित’ शब्द आया हुआ है; उसके पहले ‘नया’ विशेषण जुड़ना चाहिए, इसलिए भी कि ‘हरवाहीं’ को ‘हलवाहीं’ लिखा गया है। यह गीत हो सकता है कि खेतिहर मज़दूर गाते हों, किंतु लिखा किसी शहर के पार्टी कार्यालय में गया—जैसे सज्जाद ज़हीर ने किसानों मज़दूरों के गाने के लिए अवधी में गीत लिखकर उन्हें थमाए थे।
5. पृष्ठ 105 की सूचना के अनुसार छत्रधारी सिंह की माँ का नाम मनराज कुँवरि है। पृष्ठ 15 पर संतोखी के खेत का झूठा बयनामा ‘मनराज कुँवरि जौजे छत्रधारी सिंह’ के नाम है। सास और पतोहू का एक ही नाम असंभव तो नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों नाम अलग होते तो अच्छा था।
इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उपन्यास में ‘कमी’ बताती हो—ये सब एक संपादकीय पुनरीक्षण से दुरुस्त की जा सकती थीं। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल ज़रूर उठाना चाहता हूँ। खेलावन के बेटे की शादी में जब बराती भोजन कर रहे हैं, उस समय कन्या-पक्ष की औरतें गाली दे रही हैं और (पृष्ठ 465 पर) माठा बाबा के लिए वे अश्लीलतम गालियाँ देती हैं। ये गालियाँ ‘अश्लीलतम’ क्यों हैं?
यह सच है कि गाँव की बोलचाल को जितनी खुली शब्दावली में इस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, उतनी खुली शब्दावली मेरे देखने में तो किसी उपन्यास में नहीं आई। किंतु ये गालियाँ जिस समय गाई जा रही थीं, उस समय गानेवालियों और सुननेवालों में से किसी को अश्लील नहीं लगी थीं। सच पूछिए तो इनके बिना ज्यौनार अधूरी थी—ये अनिवार्य थीं। फिर लेखक ‘अश्लीलतम’ का विशेषण क्यों जोड़ रहा है?
‘अ-श्लील’ और ‘श्लील’ का निर्धारण इस पर निर्भर है कि अवसर क्या है, कहने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है। यदि ये गालियाँ ‘अ-श्लील’ थीं; तो इन्हें उपन्यास में कोई जगह मिलनी ही नहीं चाहिए थी, किंतु ये हैं और बिल्कुल मौज़ूँ हैं। इनका होना ही साबित करता है कि ये अश्लील नहीं हैं, अगर ये अश्लील हैं तो गाँवों में बसा हमारा भारत भी अश्लील है।
चार
इस उपन्यास में समेटा गया कालखंड लगभग पचास वर्षों का है, जिसे पहचानने के लिए कुछ सूत्रों का सहारा लेना पड़ता है।
पारस सिंह की हत्या झूरी के जिन बेटों ने की है; वे नसबंदी के डर से गाँव छोड़कर भाग गए थे, फिर लौटे हैं। तो यह समय 1977 के इर्द-गिर्द का होगा। भगवत पाँड़े और अनारा की सुल्ताना डाकू वाली नौटंकी इसके बाद आयोजित होती है—शायद 1980 आ गया हो—इस वक़्त अनारा और भगवत पाँड़े दोनों जवान हैं और अनारा पाँड़े पर आशिक़ है। यह नौटंकी कंपनी भगवत पाँड़े ने पृष्ठ 351 की सूचना के अनुसार 1970 में खोली है।
पृष्ठ 105 की सूचना के अनुसार इस अनारा की एक मौसी अनारा की नानी कलाधरी द्वारा गजराज सिंह की पतोहू मनराज कुँवरि की इज़्ज़त बचाने के लिए अपने कैशोर में ‘अँग्रेज़ पुलिस कप्तान’ की सेवा में पहुँचाई गई है—इसी पतोहू ने इस घटना के चार साल बाद छत्रधारी सिंह को जन्म दिया। छत्रधारी सिंह का जन्म मान लीजिए 1947 के आस-पास हुआ। इस हिसाब से उनकी उम्र भगवत पाँड़े के आस-पास ही ठहरती है। पृष्ठ 155-156 की सूचना के अनुसार ये छत्रधारी सिंह सोलह-सत्रह बरस की उम्र में कलाधरी की बेटी चम्पा की ‘बड़ी बेटी’ कामिनी के साथ सोना शुरू करते हैं और यह सिलसिला यहाँ डेढ़ पौने दो बरस बताया गया है, किंतु अन्यत्र सूचित है कि कोई सोलह बरस और चलता है—मान लीजिए 1977 आ गया—इस समय तक पाँड़े की नौटंकी कंपनी को खुले हुए सात साल बीत चुके हैं। फिर छत्रधारी सिंह अनारा की नानी को ठगकर एक भट्ठा खोलते हैं। अनारा की उम्र कामिनी की उम्र से कितनी कम है?
पृष्ठ 205 की सूचना के अनुसार विद्रोही जी की नेतागीरी का आग़ाज़ महेंद्र सिंह टिकैत के दिल्ली वाले प्रदर्शन के बाद हुआ है, जो 1988 में हुआ था। इसके बाद विद्रोही जी को भाषण-कला में प्रशिक्षित करने वाले ‘बाउर पंडित’ हैं। ये बाउर पाँड़े पृष्ठ 532 पर भगवत पाँड़े के पिता बताए गए हैं और ब्राह्मणों में इनका इतना प्रभाव था कि जिस पंचायत में कनक तिवारी को बिरादरी से बाहर किया गया, उसके मुखिया ये ही थे—यह कोई पचास साल पहले की बात थी, जिसका बदला इन्हीं कनक तिवारी के बेटे रघुनंदन तिवारी ने पाँड़े की खेती नीलामी में ख़रीदकर लिया है। यह नीलामी राजरानी के हाथी को गणेश में बदलने वाले मुख्यमंत्रित्व के दौरान हुई है—मान लीजिए 2010 के आस-पास। भगवत पाँड़े ने ट्रैक्टर भी 1996 में ही ख़रीदा है; क्योंकि उनके पिता ये बाउर पाँड़े अर्धकुंभ में लापता हुए, जो 1995 में पड़ा था और ट्रैक्टर का लोन भी 1996 का होने के नाते माफ़ नहीं हुआ है।
यह जानना अच्छा होगा कि क्या 1960 के इर्द-गिर्द ब्राह्मणों की ‘पंचायत’ इतनी दमदार थी कि किसी को जात-बाहर कर सके?
‘कहाँ से छेड़ूँ फ़साना, कहाँ तमाम करूँ...’ यह तय करना अफ़सानानिगार का काम है और इसमें मशवरा किसी को नहीं देना चाहिए—किंतु चूँकि उपन्यास 2023 में प्रकाशित हुआ, इसलिए मेरे ख़याल में अच्छा होता यदि ‘राजरानी’ के राज के बाद विद्रोही जी की पार्टी द्वारा मुख्यमंत्रित्व प्राप्त करने की भी कथा इसमें आती। इसकी कोई सूचना उपन्यास में है नहीं और हम यह जानने से महरूम हैं कि विद्रोही जी की पार्टी के किसान-हितैषी मुख्यमंत्री या उनके बाद आने वाले रामवादी मुख्यमंत्री के समय में बनकटा ख़ुर्द का क्या हुआ। जिन बाहुबलियों ने ‘राजरानी’ के समय में तूफ़ानी सिंह अम्बेडकर को पार्टी से निकलवाया और जंगू जनसेवक को ज़िंदा नहीं मुर्दा हाज़िर करने का हुक्म जारी करवाया उनका आगे क्या हुआ?
पाँच
इस उपन्यास का शीर्षक (पृष्ठ 145 पर दिए गए) एक गीत के टुकड़े से लिया गया है :
सरजू नदिया कहर घाघरा
अगम बहै दरियाव रे भाई
अगम बहै दरियाव॥
यह गीत ‘गंगाजमुनी’ है; अर्थात् ‘ग़ाज़ी मियाँ’ को मनाने के लिए सुनाया जा रहा है, जो भाका की मिलावट के चलते अपने सारे नुक़्ते गँवाकर ‘ग़ाज़ी = काफ़िरों पर जीत हासिल करने वाले मुसलमान योद्धा’ न रहकर ‘गाजी’ हो गए हैं, किंतु जिसमें सरजू अभी भी ‘सरजू मैया’ न होकर ‘सरजू नदिया’ ही है।
मेरे बचपन तक फगुआ जैसे वे सार्वजनीन गीत मौजूद थे, जो इस उपन्यास में हैं और वे सारे जाति-परिभाषित नाच भी मौजूद थे, जो इस उपन्यास में नहीं हैं—अहीरों की फरुआही, कुम्हारों का ‘हुड़का’ और जिस टोले का नेता तूफ़ानी है, उसमें बसने वालों का नाच ‘कठघोड़वा’ जिसमें एक ‘मिरजा जी’ नाचनेवालों को जूते से पीटते दिखाए जाते थे। ‘मिरजा जी’ का जूता सिर्फ़ उस टोले के लोगों के सिर पर तो न पड़ता होगा, किंतु इस उपन्यास में वे सारी स्मृतियाँ लुप्त हैं और किसान को ठगने-लूटने-पीटने के लिए स्वातंत्र्योत्तर भारत की सरकारें और आंदोलन मौजूद हैं—‘रामवादी पार्टी’ और ‘राजरानी’ की पार्टी जो अब ‘मान्यवर’ की पार्टी न रही और इस नाते जिसमें अब ‘कड़ाह का दूध बिगाड़ने के लिए नींबू की अकेली बूँद की तरह ब्राह्मण आ घुसा है’ जिसके पास ‘धन भी है’ (पृष्ठ 553) जो शायद उसने रूस से आयातित तेल निर्यात करके कमाया होगा। मिरजा जी अब मियाँ टोले में बस रहे हैं और जंगू-असलम मैत्री थाने में मार खाती हुई ‘जय भीम, जय मीम’ बुदबुदाती लगती है। और हाँ, विद्रोही जी की ‘किसान यूनियन’ भी है। वे सारी राजनीतिक ध्वनियाँ-प्रतिध्वनियाँ इसमें मिल जाएँगी, जो 2012 तक उत्तर प्रदेश के वायुमंडल में तैर रही थीं।
लेकिन इस उपन्यास के डाल-पत्ते चाहे जितना फैलना चाहें, उसकी जड़ सुल्तानपुर-प्रतापगढ़ ज़िलों में है; इसलिए विद्रोही जी के पास नारे भले ही प्रदेश-स्तरीय यूनियन के हैं, वे भीमकाय बख़्तरबंद ट्रैक्टर नहीं हैं—जो किसान को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली की सड़कें घेर सकें। सो वे तहसील और ज़िला कार्यालय तक ही पहुँच पाते हैं। लेकिन इस उपन्यास में एक ट्रैक्टर है, जैसे ‘गोदान’ में होरी की गाय—ट्रैक्टर चार एकड़ की जोत वाले किसानों के लिए है ही नहीं (पृष्ठ 433)
गाय की जगह ट्रैक्टर, भोला जादो की जगह वह अदृश्य सरकार है जिसको पहलवान लाठी लेकर खोज रहे हैं; लेकिन उसके दृश्य ‘नयबवा’ को ही एक काल्पनिक कुश्ती में पछाड़कर रह जाने पर मजबूर हैं। और दातादीन, नोखेराम, पटेसरी जैसे लोग अब गाँव में नहीं बचे जो भोला जादो को कह सकें कि यह धर्म नहीं है; क्योंकि धर्मनिरपेक्ष सरकार उन काग़ज़ात और उन क़ानूनों से चलती है, जिन्हें समझने-समझाने के लिए आवश्यक भाषा भी गाँव में किसी के पास नहीं है।
और जिस गाय का नाम ‘लछमिनिया’ रखा गया है; उसे बेचना पड़ता है और जब वह ‘दो बैलों की कथा’ सुनकर अपने पुराने थान पर लौट आती है, तो उससे पूछा जाना है कि वह कंगाली में आटा गीला करने क्यों वापस आ गई—उसका बछड़ा बकरीदी को बेचने के बाद पगहा थामे पहलवान को ख़ुद कुछ दूर जाना पड़ता है, ताकि वह चितकबरा बिना कोई ऊधम मचाए चारख़ाने की लुंगी लपेटे बकरीदी के साथ चला जाए। अहे निष्ठुर परिवर्तन! से गुज़रता गाँव यही है—पैंतालीस सौ रुपये नक़द पाकर भी जिन किसानों का मन रात को चूल्हा जलाने का न कर रहा हो, उनका गाँव।
कुछ सूत्र बिना छोर के हैं—अगर पुलिस-भर्ती रद्द होने के बाद भगवत पाँड़े का बेटा दिवाकर बेकार हो गया है, तो उसी पुलिस-भर्ती में चुना गया खेलावन का बेटा क्या कर रहा है?
छह
इस उपन्यास का गाँव बनकटा खुर्द ‘ख़ुर्द = छोटा’ होते हुए भी बहुत कुछ समेटता है—इसमें कामिनी मौजूद है, जिसकी नथ उतारने के लिए बनवारी सेठ पचीस हज़ार रुपये नक़द के साथ पाँच थान सोना देते हैं और अनारा है जिसके घर में इतनी दौलत गड़ी है कि अगर भगवत पाँड़े उसका कहा मानकर उसमें से कुछ खोद लें तो अपना तीन लाख से ऊपर का लोन तुरंत चुका सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों वह ऐसा नहीं करते—क्या इसलिए कि वह अब नौटंकी छोड़ने के बाद से नेमटेम से रहने लगे हैं?
जो भी हो, घाव कई तरह के हैं। पाँड़े हवालात में इसलिए बंद होते हैं कि बकाया में बंद होने वाले ज्यादातर जनेवधारी ही आते हैं (पृष्ठ 507), लेकिन ‘मेहनतकश जाति’ से आने वाले पहलवान के बेटे जोगी इंजीनियर बनने के बाद अपने खेतिहर बाप की कुछ मदद करने की जगह ‘अपने हिस्से का खेत’ बेचकर मुम्बई में फ़्लैट ख़रीदना चाहते हैं (पृष्ठ 581)।
और जिन दिवाकर को पुलिस में भर्ती कराने के लिए मोटी रक़म घूस में देने के नाते उनके बाप भगवत पाँड़े के ट्रैक्टर लोन की क़िस्त पिछड़ गई है, वह माँ से अचार और देसी घी के साथ अपनी शादी में मिले दहेज़ का बर्तन-भाँड़ा समेटते हुए नई नौकरी की कमाई से ‘मेहरी का गहना गढ़ाने’ सपत्नीक अपनी पोस्टिंग पर जा रहे हैं तो :
रिक्शा सड़क पर पहुँचने वाला था कि एक मोटरसाइकिल आकर बग़ल में रुकी। आने वाले ने दिवाकर के हाथ में एक काग़ज़ पकड़ाया। दिवाकर ने रिक्शे पर बैठे-बैठे ही पढ़ा। बैंक की नोटिस थी। उसे वापस लौटाते हुए पुलिसिया रोब से बोले, ‘‘भगवत पाँड़े के नाम से है तो भगवत पाँड़े को खोज कर दो।
चलो जी रिक्शा।’’ (पृष्ठ 473)
चोट ऊपर से ही नहीं, भीतर से भी लगती है। जात से नाई होते हुए भी बाबू जीयैं बरिस हज़ार, हर गंगा का आशीर्वाद-गान गाते हुए सीधा बटोरने वाले ब्राह्मणों की तर्ज़ पर ‘हर गंगा’ गुहारते हुए संतोखी, भगवत पाँड़े की आत्महत्या और पहलवान की विक्षिप्तता ही इस उपन्यास का समापन है। किंतु उपन्यास इस पर समाप्त नहीं किया गया।
इस उपन्यास में एक दरियाव है—दरियाव पाँड़े जो ज़मींदार ज्वाला सिंह के क़त्ल में उम्र-क़ैद काटते हुए इस उम्मीद में मर जाते हैं कि जेल से छूटकर लौटेंगे तो उन खेतों को फिर देखेंगे जिन पर से बेदख़्ली का ख़तरा ज़मींदारी-उन्मूलन के बाद हट गया है। इसी जुर्म को सात आदमियों ने अलग-अलग अकेले ही करना क़ुबूल किया था और उनमें से छाँगुर पासी को फाँसी हुई थी। इन दरियाव पाँड़े के पौत्र भगवत पाँड़े के समधी ने अपनी बेटी उनके घर में ‘दरियाव पाँड़े का ख़ानदान’ समझकर दी है—दरियाव पाँड़े एक हत्यारे नहीं, ज़ालिम-वध करने वाले जवार भर के आदर्श-पुरुष हैं, ब्राह्मणों की नाक।
क्या ग़ाज़ी मियाँ को रिझाने वाले गीत को इस तरह लिख सकते हैं?—
सरजू मैया कहर घाघरा
अगम बहै, दरियाव पाँड़े!
सुगम अहै मरि जाव॥
सात
इस उपन्यास को पढ़ते हुए जिन उपन्यासों की तरफ़ ध्यान जाता है, वे हैं ‘राग दरबारी’, ‘मैला आँचल’ और ‘परती : परिकथा’। इन उपन्यासों जैसा ही यह उपन्यास भी ‘आंचलिक’ है—हिंदी की ‘गोबरपट्टी’ के एक भूखंड के लोगों में समकालीन भारत को समेटता हुआ। महानगर में बैठकर गाँव में जलाई जा रही पराली से घबराती पाठकीय नाक इसके कई आँकड़े नहीं पहचान सकती, मसलन यह कि खलनायक छत्रधारी सिंह—जिनके ‘पेशाब से इलाक़े में चिराग़ जलता है’ (पृष्ठ 13)—की बंदूक़ और उनके सारे जाल-बट्टे के पीछे केवल पंद्रह एकड़ जोत की ताक़त है—सरकारी सुधारों द्वारा निर्धारित अधिकतम जोत अठारह एकड़ जोत से कम, और अपने पुश्तैनी हज्जाम संतोखी की जिस ज़मीन को हथियाने के लिए उनकी काग़ज़-निर्मित और लौह-निर्मित गोलियाँ चल रही हैं; उसका रक़बा सत्रह बिस्वा तीन धुर है—एक बीघे से भी कम। ‘चार हरों का बड़ा किसाना’ इस इलाक़े में नहीं है। वे तालुकेदार नहीं हैं जो ‘भूले-बिसरे चित्र’ बनाते थे, फणीश्वरनाथ रेणु के वे किसान नहीं हैं जो दो हवाई जहाज़ रखते हैं और ‘राग दरबारी’ के वे चतुर सुजान भी नहीं हैं जो हर सरकारी ग्रांट और क़र्ज़े की स्कीम से उगाही करने में माहिर हैं। इसलिए जाति-प्रथा के सारे परिचित शब्दजाल के नीचे से झाँकता यह सवाल भी पहाड़ की तरह आँख-ओझल रहने को विवश है कि लोहा तिवारी वस्तुतः उपाध्याय होते हुए भी अपने को क्यों ‘तिवारी’ कहते हैं!
भारतीय वर्णव्यवस्था एक जटिल व्यवस्था है—जिसकी जानकारी ‘सवर्ण’, ‘पिछड़ा’ और ‘दलित’ जैसे कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए लोगों को इतना मालूम है कि ‘ऊँची जात’ के लोग ‘नीची जात’ का छुआ नहीं खाते। फलतः रेणु जैसे सूक्ष्मदर्शी लेखक के ‘मैला आँचल’ में हमें मिलता है कि महंत सेवादास जब भंडारा करते हैं, तो बाभन और सिपहिया टोले के लोग आकर इनकार करते हैं—ग्वाला लोगों के साथ एक पंगत में बैठकर नहीं खाएँगे। क्या महंत सेवादास को भंडारा करने के पहले से यह नहीं मालूम है कि जब वह सबको न्यौत रहे हैं तो सब बिरादरी के लोग कैसे खाएँगे? उनको मालूम है, किंतु उपन्यास के बाभनों और सिपहिया टोले के लोगों को नहीं मालूम है।
भंडारा जब होता है तो पंगत एक ही होती है, रसोई और परोसना उच्च-वर्णी ब्राह्मण के हवाले होता है जिसका बनाया हुआ सब लोग खा सकते हैं और वर्ण-व्यवस्था के ऊँच-नीच के क्रम में सारी बिरादरियाँ बैठती हैं—जो परोसता है वह या उसके हाथ की परात किसी खाने वाले को नहीं छूती है, जिसके चलते उसकी गति रसोई तक निर्बाध रहती है और भोजन करनेवाले भी एक-दूसरे को नहीं छूते, क्योंकि भोजन करते समय किसी भोजन कर रहे का स्पर्श होने का अर्थ है कि आपने उस व्यक्ति का जूठा खाया। लेकिन पंगत एक ही होती है।
‘अगम बहै दरियाव’ में भी एक पंगत है—खेलावन के बेटे की शादी की। पूरी बरात जीम चुकी है; लेकिन जब तक माठा बाबा खा रहे हैं, कोई कैसे उठ जाए? (पृष्ठ 465)। अगर यह बता दिया गया होता कि इस पंगत में करिया सिंह कहाँ बैठे हैं, खेलावन कहाँ बैठे हैं, पकवान किसने बनाए और परोस कौन रहा था; तो अच्छा था—यह पता लगता कि कौन किसका छुआ नहीं खा सकता।
और हाँ, यद्यपि इस उपन्यास में तूफ़ानी को लगता है कि उनके बरात में शामिल होने से असहज स्थिति उत्पन्न होगी, दलित भी बरात में जाते हैं—चाहे वह सवर्णों की ही क्यों न हो। ‘कफ़न’ कहानी के घीसू—जो एक ठाकुर की बरात में इतना खा गए थे कि खाने के बाद पेश किया गया पान लेने की भी हिम्मत न रही थी—क्या एकदम से अदृश्य हो गए? मेरे गाँव में तो अभी भी दृश्य हैं।
और यद्यपि इस उपन्यास में खेलावन मियाँ टोले से किसी को अपने बेटे की बरात में चलने के लिए नहीं कहते; गाँव के मुसलमान भी गाँव के हिंदू की बरात में जाते हैं, भले ही गंगाजमुनी क़लम उनका शामिल होना न लिख पाए।
आठ
समकालीन आलोचना की सतह पर जलकुंभी की तरह उतराते मुहावरों में से एक—स्त्री-सशक्तीकरण—भी इस उपन्यास पर आज़माया गया है। लेकिन इस ‘शक्ति’ की भी जड़ें इसी क्षेत्रीयता में हैं। विद्रोही जी की पत्नी इस अर्थ में सशक्त हैं कि वह अपने साथ फेरे लेने वाले पति को दरकिनार करते हुए गौना होने के पहले ही विद्रोही जी के साथ भाग आई थीं और अपनी नाक की कील बेचकर उन्हें दूध के बाज़ार में उतार दिया है जिसका खूँटा सह जाने के नाते वह आज कमा-खा रहे हैं और एक सरकारी कर्मचारी का पोता उमेठकर नसबंदी-अभियान के विरुद्ध एक सफल योद्धा भी हैं। किंतु यह सारा तेज़ तभी तक है; जब तक उनकी बिरादरी ‘उन्नत’ नहीं है, क्योंकि जहाँ उनके भाई अपनी नाक कट जाने के बावुजूद सिर्फ़ उनसे नाता तोड़कर रह गए—जो उन्होंने एक अरसे बाद फिर क्राइम भी कर लिया—वहीं उनकी बिरादरी का फ़ौजी सिर्फ़ इस संदेह पर उनके बेटे की हत्या कर देता है कि उसकी बीवी सोना का इस लड़के के साथ प्रेम-संबंध रहा है। नौकरी पाते ही यौन-शुचिता के मानदंड भी बदल जाते हैं—जिसके पास वह रोजगार है जो सवर्ण भी अपनाते हैं, उसे सवर्णों की ही तरह अक्षत योनि पर्दा-नशीन स्त्री भी चाहिए।
जिन विद्रोही बहू ने महुआ खाकर खरमिटाव किया है; उनकी शक्ति कहाँ चली जाती है, जब उनका पौत्र जोगी इंजीनियर होते ही अपने हिस्से का खेत बेचकर मुम्बई में फ़्लैट ख़रीदने के लिए दस लाख रुपये की माँग करते हुए नौकरी पाने के बाद ‘पहली बार’ एक चिट्ठी भेजता है?
संतोखी की ज़मीन का झूठा बयनामा छत्रधारी सिंह की पत्नी मनराज कुँवरि के नाम है—उनके भी नक़ली हस्ताक्षर उस पर होंगे। यह कुछ आश्चर्यजनक है कि इतने लंबे चले मुक़दमे में कहीं उनके बयान की ज़रूरत का ज़िक्र नहीं आया, लेकिन अगर आता तो वह क्या कहतीं? उस बयान से सामने आता कि वह कितनी ‘सशक्त’ हैं।
नौ
उस रात घने जंगल में छोटी पहाड़ी के ढाल पर बने छपरे में बैठी शकुंतला रोटी की थाली परे ठेलती हुई कहती है—“मुझे रोटी नहीं, गोली खानी है। तुम गोली मारो।”
“खा लो. बहुत दूर से चल कर आई हो।”
‘‘नहीं, जंगू भइया को बुलाओ।”
आख़िर जंगू सामने आता है।
‘‘मुझे क्यों उठाकर लाए जंगू भइया? बेइज़्ज़ती करोगे? कब की दुश्मनी निकाल रहे हो?’’
‘‘दुश्मनी तुमसे नहीं, तुम्हारे बाबा छत्रधारी से है। अब उन्हें पता चल रहा होगा कि बेइज़्ज़ती झेलना, ज़ुल्म सहना कितना खलता है।”
‘‘तो क्या छत्रधारी मर गए कि गाँव छोड़कर भाग गए कि मेरी दुनिया नरक करने की सोच लिए?’’ जंगू की पकड़ में किसी औरत के रात गुज़ारने का मतलब जानते हो? मेरी दुनिया नैहर, ससुराल दोनों जगह अँधेरी हो जाएगी।...
...
‘‘सुना था कि किसी लड़की की बेइज़्ज़ती करने पर तुमने अपराधी की नाक काट ली थी। अब ख़ुद उसी राह पर उतर आए?’’
...
‘‘पास के गाँव में तुम्हारी केवला बुआ ब्याही हैं। चलो, तुम्हें उनके घर पहुँचा देते हैं।”
बेइज़्ज़त नहीं करना था तो क्या डाकू उसे पूड़ी छनवाने के लिए ले गए थे?
— पृष्ठ 401-402 (ज़ोर मेरा है)
संतोखी के ऊपर हो रहे ज़ुल्म के प्रतीकार के रूप में उठा ली गई शकुंतला कितनी सशक्त है?
इस उपन्यास में (पृष्ठ 511-513 पर) एक लंबी चिट्ठी दी हुई है, जिसमें जंगू जनसेवक पुलिस कप्तान को सरेंडर करने से इनकार करते हुए जनसेवा करते रहने के दृढ संकल्प पर अडिग रहता है और लिखता है :
मेरा नारा है—
दबना नहीं
दबाना नहीं
रोना नहीं
रुलाना नहीं
झुकना नहीं
झुकाना नहीं॥
त्याग और शौर्य से लबालब इस बलिदानी चिट्ठी में ऊपर दिए गए उद्धरण में मौजूद किसी प्रश्न का ज़िक्र नहीं है, न इसका कि क्या छत्रधारी सिंह मर गए, न इसका कि शकुंतला ने कितनी पूड़ियाँ उस रात छानकर जंगू जनसेवक को खिलाईं। और यह न पूछा गया प्रश्न भी अनुत्तरित है कि जंगू भइया द्वारा शकुंतला दीदी का अपहरण कर लेने से संतोखी की ज़मीन कैसे वापस मिल जाएगी—जंगू के उस वादे का क्या हुआ कि ‘‘आप को बाँसकोट से क़ब्ज़ा दिलाएँगे’’ (पृष्ठ 390)—बाँसकोट, जो हाई कोर्ट से ऊपर होता है।
किंतु इस चिट्ठी में यह बताया गया है कि ‘बाहुबली’ कौन हो सकता है :
मुझे पता है कि इस समाज में बाहुबली बनने के लिए सवर्ण या कम से कम मुसलमान होना ज़रूरी है और मुसलमान अगर बाहुबली बन भी गया तो बहुत जल्दी या तो अंदर जाएगा या ऊपर...
आपकी पुलिस जाति-धर्म और अमीर-ग़रीब देखकर अपना पक्ष चुनती है...
यद्यपि यह पत्र 2012 के पहले का लिखा हुआ है, जंगू जनसेवक पुलिस कप्तान को यह चुनौती नहीं देते कि वह पुलिस रिकार्ड्स देखकर ख़ुद तसदीक़ कर सकते हैं कि कितने ‘मुसलमान बाहुबली’ अंदर गए या ऊपर गए।
‘आतंकवादी’ का कोई धर्म नहीं होता, किंतु ‘बाहुबली’ का होता है!
शक्ति को हथियाकर अपना बल बढ़ाने वाले ‘स-शक्त’ कहलाते हैं, किंतु उन्हें बाहुबली ही कहना चाहिए। शकुंतला जैसी वे तमाम स्त्रियाँ, जिनकी दुनिया नैहर और ससुराल से परिभाषित है, कभी सशक्त नहीं हो सकतीं। वे शक्तिस्वरुपा हैं, क्योंकि जिस नैहर और ससुराल से समाज बनता है, उन दोनों को वे ही अस्तित्ववान् और वर्तमान करती हैं—वे निर्मात्री भी हैं, केवल भोक्त्री नहीं। इसलिए शक्ति उनके लिए कोई बाहरी तत्त्व नहीं, जिसको अपने में लाकर वे ‘स-शक्त’ हो सकें। फ़िलहाल तो सशक्त होने के लिए सरकार के क़ानून या साहूकार के ओ.टी.टी. की ज़रूरत है और जेन-ज़ी की फ़्रेंनज़ी की फ़्रेंचाइज़ी अमरीका-नियंत्रित सोशल मीडिया के हवाले है।
दस
लेखक ने उपन्यास को इस तरह ख़त्म करना ठीक समझा है :
इधर उन्हें जंगू पर लिखी एक नौटंकी की हस्तलिखित पुस्तिका मिल गई है। उसी को खेलने की तैयारी है—
जंगू कहैं कि गाँव-देस से
अत्याचार मिटावा हो
गारी देइ मजूरी मारै
टाँग तोरि बैठावा हो
जंगू कहैं कि बाघ और बकरी
एक घाट पानी पियावा हो
बहिनी बिटिया की इज्जत लूटैं
नाक काटि लै आवा हो॥
सड़क से गुज़रता तूफ़ानी बैताली को भीटे पर बैठा हुआ देखकर रुक जाता है। मोटरसाइकिल का इंजन बंद करके सुनता है, फिर मोटरसाइकिल पटरी पर खड़ी करके पास जाता है।
जंगू कहैं कि...
‘‘जय भीम काका! क्या गा रहे हैं बा-आवाज़े-बुलंद?’’
‘‘अरे तूफ़ानी बच्चा’’, बैताली पुस्तिका बंद करते हुए कहते हैं, ‘‘एक खेला मिला है, जंगू का। वही याद कर रहे हैं। समय काटने के लिए।”
‘‘काका, अब समय काटने वाला नहीं, समय बदलने वाला खेला खेलने की ज़रूरत है।”
‘‘क्या मतलब?’’ बैताली अपनी खिचड़ी दाढ़ी की खूँटियों पर हाथ फेरने लगते हैं।
‘‘अब जंगू की बहादुरी से काम नहीं चलने वाला। दुनिया बहुत ख़राब हो चुकी है। जंगू के हाथ इतने बड़े नहीं हैं कि दुनिया को ख़राब करने वाले शैतानों तक पहुँच सकें। ख़ुद हमारे रहनुमा शैतानों से हाथ मिला चुके हैं। अब ज़रूरत है कि दुनिया को आमूलचूल बदल दिया जाए।”
बैताली थोड़ी देर तूफ़ानी का मुँह ताक़ते रह जाते हैं; फिर कहते हैं, “इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बच्चा! इतनी ख़राब तो दुनिया कभी नहीं रही। दुनिया बदलने वाला खेला दीजिए तो वही खेला जाए।”
‘‘ढूँढ़कर देता हूँ। बहुत पहले कहीं देखा था। उसका एक चौबोला सुनिए—
रात नफ़रत की काली ख़तम जल्द हो
एक ऐसी सुबह की यहाँ पौ फटे
जिसमें इंसाँ बराबर हाँ दुनिया के सब
जाति-धर्मों की नामोनिशानी मिटे॥’’
सुनकर बैताली के कानों में नगाड़ा, नगड़ची, हरमुनिया, टुनटुनिया, सब साज़ एक साथ बज उठे।
‘‘अब तक कहाँ छिपाकर रखा था इसे?’’ कहने के साथ बैताली तनकर खड़े होते हैं और बुलंद आवाज़ में आलाप लेते हैं—राऽऽत न-फ़-र-त की...
जिस रात की सुबह ज्वाला सिंह की हत्या से नहीं हुई, जिस रात की सुबह 15 अगस्त 1947 को नहीं हुई, जिस रात की सुबह ज़मींदारी-उन्मूलन से नहीं हुई, उस रात की सुबह के लिए चले चलो कि ‘वो मंज़िल अभी नहीं आई...’ गुँजाता हुआ यह चौबोला जिस किताब में लिखा हुआ है, उसकी खोज में तूफ़ानी को बहुत भटकना न पड़ेगा—यह चौबोला जिस ‘समय बदलने वाले खेला’ से उठाया गया है, उसकी शुरुआती इबारत अँग्रेज़ी में यों है :
The Philosophers have only interpreted the world, in various ways. The point, however, is to change it.
यह इबारत कार्ल मार्क्स की क़ब्र पर ख़ुदी हुई है—सिर्फ़ लंदन तक एक ज़ियारत करने की ज़रूरत है।
इस आह्वान के कुछ पहले ये पंक्तियाँ हैं, जो इसी हस्तलिखित पुस्तिका से हैं :
डाकू एक रहा सुलताना
जेका जानै सकल जहाना
दूजा अब जंगू उधियाना
जेसे हारि गए दारोग़ा थानेदाऽऽऽऽऽर॥
मैं नहीं समझता कि लेखक को ‘उधियाना’ क्रिया का प्रयोग नहीं मालूम है—यह ओसौनी का शब्द है, जब धान से भूसी और गेहूँ से भूसा उड़ाया जाता है। पहले दो लोग मिलकर एक चादर फटकारते हुए तेज़ हवा बनाते थे, अब मशीन में लगे हाथ-पंखे का हैंडिल घुमाकर यह हवा पैदा की जाती है—भूसी इसी हवा की ताक़त से उड़ती है, उसके पास कोई अपना डैना नहीं होता। इस कारण से ही जब कोई आदमी किसी दूसरे की ताक़त से—मसलन नया धनी होने के बल पर—अंट-संट बकता है, तो कहा जाता है कि वह ‘उधिया’ रहा है।
जंगू जनसेवक किसके बल पर ‘उधियाना’ है?
धूमिल ने हिंदी लेखकों को सही सलाह दी थी—काँख भी ढकी रहे और मुट्ठी भी तनी रहे।
ग्यारह
‘सबल’ जातियाँ कौन-सी हैं? इस उपन्यास का यह ‘सूक्ष्म और सटीक’ विश्लेषण बहुत सराहा गया है—कई समीक्षक इस पर लहालोट हैं :
अपवाद छोड़ दें तो यहाँ सबल मानी जाने वाली जातियों के नाम में ‘राम’ आगे-आगे चलते हैं यथा रामप्रताप, रामकुमार आदि और दलित समुदाय के नाम में राम पीछे से सहारा देते हैं—यथा तुलसीराम, सीताराम आदि। (पृष्ठ 25)
इस उद्धरण का आनंद मैं इसके बावुजूद ले सकता था कि मेरे अपने गाँव में सारे दलितों के नाम में ‘राम’ पहले आया है; लेकिन जब ऐसे उद्धरणों को ‘अनुभवात्मक यथार्थवाद’ कहकर समीक्षक प्रस्तुत करते हैं, तब देखना पड़ता है कि उपन्यास में वस्तुतः है क्या! इस हिसाब से विद्रोही जी सबल जाति के हैं; क्योंकि उनका नाम ‘रामबोध’ है और रामनाथ कोइरी भी सबल जाति के हुए, किंतु हम देखते हैं कि रामनाथ की सबल जाति के सारे खेत चकबंदी में छत्रधारी सिंह ने हथिया लिए और विद्रोही जी भी जब अपनी पूरी सबलता के साथ ग्राम प्रधान हो जाने के बावुजूद जेल जाते हैं तो ‘बोधा भाई’ ही उनकी आत्मीय पहचान है।
यह ‘अनुभवात्मक यथार्थवाद’ ही है, जिसके चलते ‘पिछड़ों’ द्वारा ‘दलितों’ से की जाने वाली मारपीट भी अख़बार में ‘सवर्णों द्वारा दलितों पर हमला’ की सुर्ख़ी के रूप में ही स्थान पाती है और मुसलमानों-दलितों के बीच का झगड़ा ‘दो धार्मिक समुदायों के बीच का झगड़ा’ बताया जाता है। बहरहाल, इस उपन्यास में सारे मुसलमान पात्र निश्छल हैं तथा विद्रोही जी की पार्टी, तूफ़ानी सिंह अम्बेडकर की पार्टी और मियाँ टोले के बीच की प्रगाढ मैत्री जिन सबल सवर्णों के विरुद्ध एकजुट है—वे ठाकुर हैं, जिनके भट्ठे की ईंटों पर उस समय तो ‘महाराणा प्रताप’ छपता था, जब वह कलाधरी के शिवाले के लिए ईंटें पका रहा था, किंतु ‘रामवादी पार्टी’ के आंदोलन के समय रामनाम छपने लगा है। इस चतुराई के बावुजूद पुलिस-भर्ती की घूस तो छत्रधारी सिंह के बेटे को भी देनी पड़ी है और भगवत पाँड़े के बेटे दिवाकर पाँड़े को भी, फिर कैसे सरकारी तंत्र छत्रधारी सिंह के पक्ष में और भगवत पाँड़े के विपक्ष में खड़ा है?
बारह
मैं प्रेमचंद के लेखन का प्रशंसक नहीं हूँ, क्योंकि उनके गाँव पर अल्लामा इक़बाल के शे’र चढ़े रहते थे, लेकिन कभी-कभार ‘कफ़न’ जैसी कहानियाँ गाँव में झाँक लेती हैं। हिंदी-साहित्य में गाँव पहली बार ‘मैला आँचल’ में आया, फिर ‘परती : परिकथा’ और ‘राग दरबारी’ के माध्यम से—बीच में छपे ‘लोक-परलोक’ को किसी ने गिना नहीं। और फिर गाँव इस उपन्यास (‘अगम बहै दरियाव’) में दिखा। ‘राग दरबारी’ को छोड़कर इन सबमें किसी न किसी शक्ल में नया सबेरा झाँक रहा है—इस उपन्यास में उसकी किरनें कुछ ज़ियादा सुर्ख़ हैं और शबनम के लिए कोई जगह नहीं है।
लेकिन इस उपन्यास की ख़ूबी इसके आँकड़ों में है, उनके इस्तेमाल में नहीं। समकालीन हिंदी-लेखन एक ज़माने से लंदन में लिखी गई एक हस्तलिखित पुस्तिका में दिए गए कुछ पूर्व-निर्दिष्ट मुहावरों, तर्कों और फ़ैसलों में आबद्ध रहने के लिए आदिष्ट है; जिसके नाते हमारी सचाइयाँ भी वैसे ही ‘पितरा’ जाती हैं, जैसे पीतल के बर्तन में अच्छा-ख़ासा दही।
लहराते परचम के पीछे बरबत पर कौन गा रहा है, यह भी सामने आना चाहिए।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
