ज्ञानरंजन और उनकी ‘संगत’ के बहाने
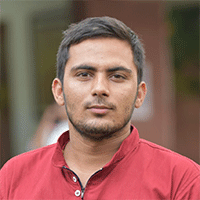 शुभम सिंह
13 अगस्त 2025
शुभम सिंह
13 अगस्त 2025

मैं ‘हिन्दवी’ का पुराना पाठक-दर्शक हूँ। ‘संगत’ का जब पहला एपिसोड आया, तब मैं बहुत ख़ुश हुआ था। ‘संगत’ के उस एपिसोड के माध्यम से, कवि आलोकधन्वा को मैं पहली बार सुन रहा था। उनका कविता-संग्रह ‘दुनिया रोज़ बनती है’ पढ़ा था, पर वे कविताएँ आलोकधन्वा को सुनने के बाद मुझे और ज़्यादा समझ आईं। मैंने अपने दोस्तों को भी यह शृंखला देखने की सलाह दी। साहित्य की दुनिया में हम ‘संगत’ के साथ आहिस्ता-आहिस्ता दाख़िल हुए। जैसे-जैसे एपिसोड आते गए, साहित्य की दुनिया से हमारा परिचय विस्तृत होता गया। ‘संगत’ में जिस भी साहित्यकार का इंटरव्यू होता, हम उसकी किताबों को खोज-खोजकर पढ़ते। हम कई बार सोचते कि ‘हिन्दवी’ की ‘संगत’-शृंखला में अगर गजानन माधव मुक्तिबोध का इंटरव्यू संभव होता तो क्या उनसे पूछा जाता, “पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है?” या मुक्तिबोध यह कविता पढ़ते—“बहुत शर्म आती है मैंने ख़ून बहाया नहीं तुम्हारे साथ...”
बहरहाल, गए दिनों ‘संगत’ में मैंने व्योमेश शुक्ल को सुना, उन्हें मैं बहुत पहले से जानता हूँ। तब से जब वह मोर्चे पर अकेले थे। उनका किरदार बेहद मज़बूत है। इसके बाद आया ‘संगत’-शतक यानी सौवाँ एपिसोड ज्ञानरंजन की संगत। सच बताऊँ तो इससे पहले मैंने ज्ञानरंजन का बस नाम सुना था और मेरे सीनियर ने उनकी एक कहानी मुझे पढ़ने को दी थी—‘पिता’। यह एक कमाल की कहानी है। मेरा सुझाव है कि इसे प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैंने ज्ञानरंजन का लिखा कुछ भी नहीं पढ़ा था। हाँ, कभी-कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरह ज़रूर याद किया कि ‘पहल’ पत्रिका के संपादक कौन थे?
ज्ञानरंजन
मैंने जब ‘संगत’ में उन्हें सुना, नए सिरे से उन्हें पढ़ने लगा। मैंने उनकी छह कहानियाँ पढ़ीं—‘घंटा’, ‘पिता’, ‘संस्मरण’, ‘अनुभव’, ‘बहिर्गमन’ और ‘छलांग’। मैं यहाँ इन कहानियों की समीक्षा नहीं करूँगा। मैं उसके क़ाबिल भी नहीं हूँ; लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ‘कहानी’ क्या होती है, इन्हें पढ़ते हुए आप इस प्रश्न-बात का जवाब पा जाएँगे।
इन कहानियों से गुज़रते हुए बार-बार महसूस हुआ कि रोज़मर्रा का जीवन ऐसे ही होता है। रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी ही भाषा का उपयोग होता है। गद्य को कब और किस दिशा में मोड़ना है, यह हम-आप उनकी कहानियों से सीख सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि ज्ञानरंजन संसार के सबसे बड़े कहानीकार है, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि वह हिंदी के अत्यंत महत्त्वपूर्ण कहानीकारों में से एक हैं।
अब ‘पहल’ की बात करते हैं। जब मैं साहित्य पढ़ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुँचा तो ‘पहल’ का 125वाँ अंक आ चुका था। मैंने पिछले दिनों इंटरनेट पर मौजूद ‘पहल’ का 20वाँ अंक पढ़ा। सितंबर 1982 में छपा यह अंक बेर्टोल्ट ब्रेष्ट की अनूदित कविता से शुरू होता है। कविता कुछ यूँ है :
अख़बार का हॉकर
सड़क पर
चिल्ला रहा था
कि जनता ने
सरकार का विश्वास
खो दिया है
और अब ये विश्वास
दिन-दूनी और
रात-चौगुनी मेहनत
करने पर
ही जीता जा सकता है
(परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं)
मेरी राय है
कि सरकार
इस जनता को भंग कर दे और
अपने लिए दूसरी जनता चुन ले।
दूसरे पन्ने में लिखा है, “इस महादेश के वैज्ञानिक विकास के लिए प्रस्तुत प्रगतिशील रचनाओं की अनिवार्य पुस्तक” और बग़ल में गोरख पांडे की कविता है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ हैं :
कविता युग की नब्ज़ धरो
अफ़्रीका, लातिन अमेरिका
उत्पीड़ित हर अंग एशिया
आदमख़ोरों की निगाह में
ख़ंजर-सी उभरो
~
उल्टे अर्थ-विधान तोड़ दो
शब्दों से बारूद जोड़ दो
अक्षर-अक्षर पंक्ति-पंक्ति को
छापामार करो
ऐसी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए सीने में कितने बूते की आवश्यकता होगी, आप इन कविता-पंक्तियों को पढ़कर समझ गए होंगे। इसके साथ ही पत्रिका के भीतर प्रगतिशीलता की जिस तरह से पैरोकारी है, वह मानीख़ेज़ है। साहित्यिक जमात तो ‘पहल’ के बारे में और ज़्यादा जानती होगी, लेकिन नई पीढ़ी को जानना होगा कि ‘संगतकार’, ‘कपड़े के जूते’ और ‘सीलमपुर की लड़कियाँ’ सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुई थीं? जवाब—‘पहल’।
मैं आख़िर में कुछ अनुभव भी साझा करना चाहता हूँ : मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य को विभाग के चंद लोग अपनी बपौती मानते हैं। क्या हिंदी की विशाल परंपरा प्रोफ़ेसरों के चाटुकार शोधार्थियों और गुटों तक सीमित है? जवाब है नहीं। बक़ौल धूमिल—साहित्य संसद से सड़क तक हर जगह मौजूद है।
मैंने एक दफ़ा किसी लेखक की पुस्तक-समीक्षा करते हुए फ़ेसबुक पर कुछ लिखा, हमारे एक प्रोफ़ेसर (जिनकी हर हफ़्ते एक किताब प्रकाशित होती है) ने अपने एक शोधार्थी से फ़ोन करवाकर लगभग धमकी दिलवाई और मुझे वह पोस्ट हटानी पड़ी।
दूसरी घटना कि एक बार विनोद कुमार शुक्ल का नाम आते ही हमारे विभाग के एक प्रोफ़ेसर (जो ख़ुद को ग़ज़लगो मानते हैं) ने कहा, “हालाँकि कुछ लेखक न पढ़ने लायक़ होते हैं, न मैं उन्हें पढ़ता हूँ।”
इन अनुभवों में मुझे जो समझ आया कि हिंदी-साहित्य को अपनी जागीर समझने वाले और लेखकों को ख़ारिज करने वाले लोग सब जगह हैं और रहेंगे—जिस तरह ज्ञानरंजन के साथ ‘संगत’ आने पर कुछ लोगों ने अपने भीतर छुपी-छपी-दबी कुंठाओं को ज़ाहिर किया, वह इसका प्रमाण है। मुझे उनके प्रति सहानुभूति है।
अंत में ‘पहल’ के अंतिम अंक में ज्ञानरंजन की कही बात ही उद्धृत करना चाहूँगा :
“अंत श्मशान में नहीं, इतिहास में दर्ज होगा।”
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
