समीक्षा : त'आरुफ़-ए-मंटो
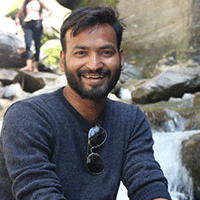 सुयश मौर्य
01 सितम्बर 2025
सुयश मौर्य
01 सितम्बर 2025

पिछले हफ़्ते विभाजन पर आधारित एक नाटक देखने गया था। नाटक दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में था। विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप और उसके लोगों पर घटी एक त्रासदी है—उसे याद किया जा सकता है, उससे सीखा जा सकता है; लेकिन नाटक देख के लगा कि विभाजन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। नाटक मूल रूप से एक उपन्यास पर आधारित था। लगे हाथ निर्देशक ने उपन्यास कि मूल भावना पर भी उन्माद का गोबर लीपने कि कोशिश की। इस पर बात कभी और। विभाजन पर कई प्रस्तुतियाँ देखीं, कई नाटक पढे, ज़्यादातर लेखक/निर्देशक अपनी कथावस्तु को लेकर बहुत संवेदनशील रहे हैं। उस त्रासद समय की कहानियों के मंचन के ज़रिये कई प्रस्तुतियों ने आज के वक़्त के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश की। कल और आज के बीच पुल बने कि उनके दर्शक उस पार की विषाद, वेदना, और विस्थापन को इस पार तक महसूस लें। उन्होंने दर्शकों को उस भयानक बियाबान में ले जाकर छोड़ दिया, जहाँ नई-नई खिच रही सरहदों ने सच-झूठ, सही-ग़लत, अच्छाई-बुराई की हदों को धुँधला कर दिया था। मगर ताम-झाम वाले इस नाटक को रिपोर्ट लगानी थी। निर्देशक को किसी सुपर बॉस को दिखाना था कि उसके रथ को धक्का देने वालों में वह भी है।
ख़ैर, इस वाले नाटक को देखने के बाद मई के महीने में हुई—एक नए-नए निर्देशक की पुरानी प्रस्तुति याद आ गई। नाटक का नाम था ‘त’आरुफ़-ए-मंटो’। निर्देशक साहिल आहूजा और मुखावरण थिएटर ग्रुप के उनके साथियों कि यह प्रस्तुति स्टुडियो सफ़दर, शादीपुर, नई दिल्ली में हुई। इस प्रस्तुति की अँग्रेज़ी में लिखी समीक्षा का अनुवाद यहाँ पेश कर रहा हूँ।
कल्पना कीजिए कि आप नाटक देखने एक इंटीमेट थिएटर में जा रहे हैं। इंटीमेट थिएटर : आमतौर पर एक वर्गाकार कमरे में दर्शकों के बैठने के लिए दीवारों से सटी दो या तीन पंक्तियाँ होती हैं। इनका आयाम लगभग उतना ही होता है, जितने बड़े हमारे घरों के हॉल हुआ करते हैं, इसीलिए इसमें दर्शकों की संख्या सीमित होती है। मंच प्रायः हॉल के बीच-ओ-बीच होता है। प्रोसीनियम थिएटर की तुलना में दर्शक और प्रस्तुति के बीच का फ़र्क़ बहुत ही कम होता है। इसी कारण ये प्रस्तुतियाँ और ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। हॉल में घुस रहे दर्शकों की कतार में आप भी लगे हैं। तीसरी घंटी (नाटक का मंचन शुरू होने से पहले तीन घंटियाँ बजती हैं। नाटक तीसरी घंटी पर शुरू होता है।) अभी बजी नहीं है। नाटक अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आप अंदर जाते हैं। आप सामने की ओर सीट ढूँढ़ने के लिए बढ़ते हैं कि आप को एक तांत्रिक जैसा कोई दिखाई देता है। ‘नाटक नहीं शुरू हुआ है और यह तांत्रिक झाड़-फूँक कर रहा है’। आप अपने स्वागत की उम्मीद करते हैं और वह भूत भगा रहा होता है। दिमाग़ पे बहुत ज़ोर डालने पर भी वो मंटो के किसी पात्र की तरह नहीं लगता है। मंटो की कहानियों पर आधारित किसी नाटक की शुरुआत भला क्यों ही किसी तांत्रिक से होगी? क्या यह अति-आत्मविश्वास में निर्देशक से हुई कोई भूल है, या इस प्रयोग का कोई बड़ा महत्त्व है? दर्शक अगली पंक्ति में बैठते हैं। एक वॉयस-ओवर गंभीर आवाज़ में नाटक की घोषणा करता है।
यह नाटक के प्रदर्शन का चौथा और आख़िरी शो था। 10 और 11 मई, 2025 को मुखावरण की ओर से इस नाटक की कुल चार प्रस्तुतियाँ हुईं। इंटीमेट थिएटर के क्षमता को ध्यान में रखते हुए, साहिल आमतौर पर दिन में दो या तीन बार अपना शो दोहराते हैं। उन्होंने अपनी पिछली प्रस्तुतियों जैसे इल्हाम, ख़ामोश अदालत जारी है, लाहौर तों अंबरसर, एंड देन देयर वेयर नन इत्यादि के प्रदर्शन भी इसी प्रारूप में किए थे। 120 मिनट लंबे ‘त’आरुफ़-ए-मंटो’ में, मुखवारण थिएटर समूह के निर्देशक मंटो की सूरत उनकी कहानियों, रेखाचित्रों, भाषणों और बयानों के जरिये गढ़ने की कोशिश करते हैं। साहिल दिल्ली के विभिन्न रंगमंचों में प्रतिवर्ष इस नाटक का प्रदर्शन करते रहे हैं।
नाटक शुरू होता है। मंटो की शख़्सियत और उनके अफ़सानों की परतें खुलने लगती हैं। धीरे-धीरे नाटक की अबसर्ड शुरुआत, तांत्रिक और उसका डरावना अंदाज़ एक रूपक में तब्दील हो जाते हैं। उस भयावह वास्तविकता का रूपक जो विभाजन के विकृत रूप में उस वक़्त सामने आई, जब लोग औपनिवेशिक काल के अंत के बाद एक बेहतर भविष्य बाट-जोह रहे थे। आज़ादी की दहलीज़ पर उन्हें कुछ मिला तो विभाजन जिसने उनसे सब कुछ लूट लिया। तांत्रिक-सा दिखने वाला यह पात्र मंटो की कहानी ‘काली सलवार’ का ‘पीर बाबा’ होता है, जो कहानी में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद भी नहीं होता है, लेकिन कहानी के मुख्य पात्रों, सुल्ताना और ख़ुदाबख़्श की बरबादी का ज़िम्मेदार होता है।
‘त’आरुफ़-ए-मंटो’ समाज की कड़वी सच्चाई को उतनी ही बेबाकी से पेश करता है, जितनी बेबाकी से मंटो ने इसे लिखा है। ठीक वैसी, जैसी उस वक़्त मौजूद थी। हत्या, लूट, बलात्कार, वैश्यालय, आदि, मंटो के साहित्यिक आख्यानों में प्रमुखता से उजागर होते हैं। इनका मंचन करते हुए निर्देशक और अभिनेताओं ने पूरी संवेदनशीलता दिखाई है ताकि उनकी चुभन तो बनी रहे, लेकिन कहीं से वह फूहड़ या फहश न लगे। यही कारण है नाटक हमें कई जगह असहज भी करता है। नाटक के एक दृश्य में वेश्यालय में वेश्याओं से घिरा एक आदमी का उनमें से एक के कंधे पर अपना पैर रखना जहाँ मर्दों के अपनी ताकत और हनक को साबित करने की कोशिश को दिखाता है, वहीं सुगंधी का किरदार ख़ुद को शरीर की सीमाओं के पार एक इंसान के तौर पे पेश करता है। ऐसा करने के लिए मंच पर पड़ी मेज को सुगंधी जिस तरीक़े से अपने अभिनय और संवाद का हिस्सा बनाती है, उसका ज़िक्र ज़रूरी हो जाता है। शुरू में वह मेज़ के चारों पैरों के बीच बैठी रहती है और इसे अपने कमरे की तरह इस्तेमाल करती है। ज़ाहिर है यह उसकी कैद को दर्शाता है। इसके बाहर निकल कर जब वह उसके पास खड़ी होकर उसे अपनी बालकनी की तरह इस्तेमाल करती है। इसे देख कर लगता है की उसकी इच्छाएँ फिर से खिल उठी हैं। जब वह मेज़ को उलट कर उसके बीच में अपने प्रेमी के साथ बैठती है तो ऐसा लगता है—उसकी दुनिया बहुत बड़ी और सुंदर है। अंत में, वह मेज के ऊपर चढ़ जाती है और अपनी दोनों तांगे फैला कर अपनी देह तक सीमित अपनी पहचान का अतिक्रमण करती है और अपने आशिक़ और उसके जैसे मर्दों पर अपना ग़ुस्सा निकालती है। यहाँ, उसका हाव-भाव मेज़ तक सीमित उसकी पहचान पर उसके ख़ुद को नियंत्रण को दर्शाता है।
रेलवे तथा सड़क दोनों ही रस्तों से सरहद पार कर रहे शरणार्थियों के साथ लूट-पाट और कत्ल-ए-आम हुआ। साहिल ने इसकी विभीषिका का मंचन प्रकाश और ध्वनि के माध्यम से दिल-दहलाने की हद तक किया और विभाजन के दौरान अपनों को कंधे पे उठाए, पोटली दबाये लोगों के जत्थे को रीक्रिएट किया जिसका मुद्रण यशपाल के ‘झूठा सच’ के आवरण चित्र के रूप में हुआ है। ट्रेनों में हुई हिंसा और अन्य कहानियों को क़लमबंद करते हुए मंटो कभी-कभी असहाय गवाह नज़र आते हैं और कभी-कभी उन्हीं कहानियों का हिस्सा होते हैं। नाटक के मंचन में कई अलग-अलग नाट्य विधाओं का सहज सम्मिश्रण दिखाई देता है। निर्देशक ने फ़िज़िकल थिएटर और एक्सपेरिमेंटल थिएटर, दोनों को ही इस नाटक का हिस्सा बनाया है। शारदा और मुख़्तार की प्रेम कहानी के मंचन में अभिनेता पेड़, पत्थर, मेज़ आदि वस्तुओं को दर्शाने के लिए अपने शरीर की भिन्न-भिन्न मुद्राओं का उपयोग करते हैं। कुछ अन्य कहानियों के मंचन में अभिनेता दर्शकों से सीधे संवाद करने के लिए बार-बार चौथी दीवार ( चौथी दीवार या फ़ोर्थ वॉल एक काल्पनिक दीवार होती है, जो मंचन और दर्शकों को एक-दूसरे से अलग करती है। इस काल्पनिक दीवार को तोड़कर दर्शकों को सीधे संबोधित करने की तकनीक ब्रेख्त के नाटकों में देखने को मिलती है।) को तोड़ते रहते हैं। दो अलग-अलग प्रकार के रंगमंचों के अलावा, प्रदर्शन के दौरान पंजाबी और बंगाली गाने भी बजाए जाते हैं। मंचन के एक्सपेरिमेंटल नेचर और दर्शकों को समाज के जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर ‘फ़ूड फ़ॉर थॉट’ प्रोवाइड करके, यह नाटक एक एपिक थिएटर की तरह बन जाता है।
यहाँ कुछ भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, लेकिन अभिनेताओं ने पात्रों को उतनी ही निर्भीकता से निभाया भी है, जितनी बेबाकी से निर्देशक ने उनके चरित्रों को गढ़ा है, जैसा कि मूल रूप से मंटो ने लिखा था। अभिनेता, चाहे वे हत्यारे, छेड़छाड़ करने वाले, चोर, दलाल या वेश्याओं की भूमिका निभा रहे हों, सभी ने अपने ज़्यादातर ग्रे शेड किरदारों की भूमिका निभाते समय पूरी ईमानदारी दिखाई। मंटो, सुगंधी, सुल्ताना, शारदा, मुख़्तार, मकसूद, रणधीर, शंकर, सलमा आदि के किरदारों को निभाने वाले कलाकारों ने उनके अंतर्मन की उथल-पुथल, दुविधा, पीड़ा, इच्छाओं, महत्त्वाकांक्षाओं, अच्छाई-बुराई इत्यादि को सामने लाया। हर किरदार विभाजन के पीड़ितों और गवाहों के एक पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। यही बात इस प्रदर्शन को मंटो के समकालीन समाज के माइक्रोकॉज़्म का रूप दे देती है।
एक ओर, अपने साहसिक और बेबाक मंचन के ज़रिए, साहिल आहूजा की निर्देशकीय अंतर्दृष्टि लेखक मंटो और उनके पात्रों की बेचैनियों को उनके नाटक देखने वाले दर्शकों के चिंतन के स्तर तक ले जाने की कोशिश करती है। नाटक में, मंटो दावा करते हैं कि वे उस समाज कपड़े नहीं उतार सकते हैं जो पहले से बे-लिबास है। उनके साहसिक और असहज करने वाले साहित्य को नाटक में उसी असर के साथ पेश किया गया है। दूसरी ओर, कई कहानियाँ एक-दूसरे के समानांतर चलती हैं, जो इस प्रस्तुति को समाज की रेप्लिका के रूप में स्थापित करती हैं। इसके साथ-साथ अलग-अलग लगने वाली कहानियों को एक नाट्य प्रस्तुति में पिरोना समकालीन समाज में मुँह बाए मौजूद सांप्रदायिक खाई और अलगाव के नैरेटिव का उत्तर मालूम पड़ती हैं। कहानियों के बीच फासले को भरना, रंगमंच जैसे ज़िम्मेदार कलात्मक माध्यम की कोशिश या बिखराव के मौजूदा डिसकोर्स को चुनौती देने के जैसा ही है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
