प्रतीक और बिंब का गुम्फित होना
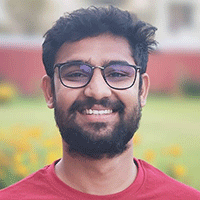 योगेश शर्मा
15 नवम्बर 2025
योगेश शर्मा
15 नवम्बर 2025

इस आलेख-शृंखला से संबंधित दो आलेख—अनुभूति की शुद्धता का सवाल और महान् कविताओं के बिंब कैसे होते हैं!—आप पहले पढ़ चुके हैं। अब पढ़िए यह तीसरा आलेख :
आज बड़ी शानदार सुबह थी। यूनिवर्सिटी की सड़क बारिश में भीग कर नई हो गई थी। साढ़े दस बजे भी धूप कहीं नहीं थी। एक ठंडापन मौसम में पसरा हुआ था। मैंने सड़क से आते हुए महसूस किया कि ऐसे मौसम में जब गाड़ी सड़क पर चलते हुए मेरे पास से गुज़रती है तो उससे निकलने वाली गर्मी में एक ख़ास क़िस्म का आकर्षण होता है। लाइब्रेरी के पीछे लगे सागवान के बड़े-बड़े पत्तों से पानी की बड़ी-बड़ी बूँदें टपक रही थी। मैंने देखा कि वहाँ सागवान के पेड़ों के नीचे आमने-सामने जो दो पत्थर के बैंच लगे हैं, वे आज ख़ाली हैं। ऐसे शानदार मौसम में आमतौर पर वे बैंच ख़ाली नहीं मिलते। मैंने जल्दी से वहाँ जाकर बैंच से पानी हटाया और बैठ गया। वहाँ सारे वातावरण में समोसे तले जाने की ख़ुशबु फैली हुई थी, कोई बहुत नज़दीक से चाय लेकर गुज़रता तो चाय की ख़ुशबु का भी हल्का-सा एहसास होता। गर्म चाय के कप का एहसास हाथों में महसूस होने लगता। अकेले होने की वजह से मैं चाहकर भी अपने लिए चाय नहीं बोल सका और अपने साथी का इंतज़ार करने लगा...
लाइब्रेरी के पीछे अक्सर इस मौसम में हलचल बढ़ ही जाती है। लड़कियाँ और लड़के चाय की दुकानों के पास जमा हो जाते हैं। लड़कियों के चेहरे पर एक अलग क़िस्म का भाव होता है। शायद चंचलता का। बारिश लड़कियों को चंचल बनाती है लेकिन एक शालीनता फिर भी उनके शारीरिक भाषा में नज़र आती रहती है। इसके उलट लड़कों के चेहरों पर ही नहीं उनके सारे शरीर में एक मस्ती होती है और वे इसे बेझिझक होकर बयाँ करते हैं। मैं इस माहौल में डूबा हुआ अपने ग्रेजुएशन के दिनों को याद करने लगा। मैं कहीं खोया हुआ था, अचानक मुझे एक उदास स्वर सुनाई दिया। यह मेरे साथी का स्वर था। वह ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ़ देखा। उसने बड़े चटक नीले रंग की एक शर्ट पहनी हुई थी, जिसके कॉलर तक़रीबन घिस चुके थे और नीचे एक पुरानी जीन्स।
मुझे लगा जैसे उसपर शायद इस मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ा था। उसका स्वर घबराहट और तनाव से भरा हुआ था। वह ऐसा दिखता था मानो किसी बड़े भारी बोझ के तले दबा हो। वह आते ही मेरे सामने वाले बैंच पर बैठ गया।
बैठते ही उसने कहा कि मैंने तुम्हें कई बार आवाज़ लगाई किंतु तुमने ध्यान नहीं दिया। इतना कहकर उसने अपना सर नीचे कर लिया। कुछ क्षण में मैं मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश करने लगा।
मैंने विक्की को दूर से आवाज़ लगाकर चाय बोलने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। भीड़ ज़्यादा थी। विक्की मेरी आवाज़ सुन पाने में असमर्थ था। मैंने अपने साथी को कहा कि तुम दो मिनट बैठो मैं चाय बोलकर आता हूँ।
उसने चाय पीने से मना करते हुए कहा कि मेरा चाय पीने का मन नहीं है।
मैंने उसकी तरफ़ हैरानी से देखा। लेकिन फिर कुछ सोचकर मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा। और मैं वापिस बैंच पर बैठ गया। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
एक अल्प विराम के बाद मैंने कुछ बातचीत शुरू करने के लहजे में हिंदी के एक प्रसिद्ध साठोत्तरी कवि की एक कविता की कुछ शुरूआती पंक्तियाँ पढ़ी—
सहसा हम क्यों चाहने लगते हैं हमारे सिरों पर
छत हो
(जनतांत्रिक) वर्षा में धुली हुई
क्या यह खुली सड़क काफ़ी नहीं है
उसने कुछ अतिरिक्त ज़ोर देते हुए आगे कि एक पंक्ति और जोड़ी, जिसे मैंने एहतियात के तौर पर जानबूझकर छोड़ दिया था।
सच्चाई और शोहरत के बीच बिछी हुई संसद तक—यह पंक्ति पढ़ने के बाद उसने उदास भाव से मुस्कुराते हुए मेरी आँखों में झाँका। मैं चौंक गया। मुझे लगा जैसे उसने मेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उसे तक़रीबन-तक़रीबन मेरी आत्मा में झाँकता हुआ महसूस किया।
अचानक उसने कहा कि “मुझे पिछले कुछ दिनों से सपने आ रहे हैं। सपने प्रायः एक ही जैसे हैं। मेरे पीछे लोग पड़े हैं और मैं भागते-भागते उड़ने लगता हूँ। मुझे महसूस होता है जैसे मेरे पास असलियत में पंख हैं। यह एहसास बहुत तीव्र होता है।”
“अच्छा।” मैंने कहा।
“हाँ। यही कई दिनों से हो रहा है। जब मैं जगता हूँ तो लगता है जैसे मुझसे किसी ने कुछ छीन लिया है। यक़ीनन मैंने महसूस किया है कि मैं उड़ते हुए मैं अच्छा महसूस करता हूँ। उसने बात बढ़ाते हुए कहा।”
“तो इसमें कुछ दिक़्क़त है?” मैंने प्रश्न करने के लहजे में पूछा।
उसने गर्दन उचकाते हुए कहा—“पता नहीं। लेकिन मुझे उठते ही महसूस होता है कि यह वैसा ही है जैसा उस लंबी कविता में एक रक्तालोक स्नात पुरुष...” और वह कहते-कहते रुक गया।
मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी ना थी। मैं ठिठक गया। कई देर तक हमारे बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया।
अचानक आवाज़ आई, “दो चाय!”
मैंने गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो दुबे दो चाय लेकर हमारे बग़ल में खड़ा था। मैंने पूछा कि हमने तो अभी तक चाय के लिए नहीं कहा। दुबे ने कहा कि “विक्की ने चाय भेजी है। कम मीठा और पत्ती तेज़।” मैंने विक्की कि तरफ़ देखा, वह मुस्कुरा रहा था और चाय पीने का इशारा कर रहा था। मैं भी विक्की की तरफ़ कृतज्ञ भाव से मुस्कुरा दिया। दुबे ने चाय बैंच पर रख दी।
मैंने अपने साथी की तरफ़ देखा। उसके चेहरे पर भाव कुछ बदल चुके थे। वह मेरी तरफ़ ऐसे देख रहा था जैसे वह कुछ कहना भी चाहता है और जानना भी।
“तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो?” मैंने उससे प्रश्न किया।
उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर रूककर उसने आगे झुककर अपना चाय का कप उठा लिया और दुबारा मेरे चेहरे की तरफ़ अजीब अनमने भाव से देखने लगा।
मैंने जान लिया था कि इस तरह वह आज अधिक बातचीत नहीं करेगा। बाहरी मौसम और उसके भीतरी तनाव के अंतर्द्वंद्व ने शायद उसका मूड कुछ बिगाड़ दिया था। फिर भी मैंने एक प्रयास किया जिससे बात अधिक बिगड़ सकती थी, किंतु मुझे बस यही सुझा—“क्या तुम अपने आप को बड़ा कवि समझने लगे हो?”
“नहीं ऐसा नहीं है।” उसने मेरी आशा के ठीक विपरीत उत्तर दिया और बोलना जारी रखा— “बात दरअस्ल यह है दोस्त कि मुझे लगता है उस लंबी कविता में जो बिंब कवि ने गढ़े हैं, उनके निर्माण में ज़रूर कवि के अवचेतन का एक बड़ा हाथ है। एक बड़ी कविता में बिंब कालातीत होते हैं, और जो बिंब कालातीत होते हैं—वे प्रायः व्यापक मानवीय परिप्रेक्ष्य में निर्मित होते हैं, फिर भले ही उनका संदर्भ कवि का निजी जीवन ही क्यों ना हो... और शायद धीरे-धीरे वे बिंब ही कविता में प्रतीक का काम करने लगते हैं... क्या मैं सही समझा हूँ? पिछली बार तुम ऐसी ही कुछ बात कर रहे थे ना?”
“हाँ तुम तक़रीबन-तक़रीबन सही समझे हो। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार बिंब बिल्कुल कल्पना प्रसूत होते हैं, जो कथा या काव्य वस्तु के संदर्भ में निर्मित होते हैं। वे बिंब प्रायः उस कविता या कहानी के संदर्भ में ही उपयोगी होते हैं, किंतु कई बिंब यह सीमा लांघ जाते हैं और कालांतर में एक प्रतीक का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे उस लंबी कविता में वह ‘रक्तालोक स्नात पुरुष’ या वह प्रोसेशन आज वर्तमान में महज़ एक बिंब नहीं है अपितु प्रतीक बन गए हैं। ख़ैर चलो यह तो बात ठीक है, लेकिन तुमने अपने सपने के साथ इसका ज़िक्र क्यों किया”, बात कहते-कहते मैं अचानक बीच में बोल पड़ा।
“हम्म!” उसने एक लंबी साँस ली और कुछ देर के लिए वह कुछ सोचने लगा। फिर उसने थोड़ा गंभीर दिखने का अभिनय किया। उसने अपनी बीड़ी निकाल ली।
मैं अपनी कामयाबी पर अंदर ही अंदर ख़ुश हो रहा था। आख़िर वह बातचीत के मूड में आ गया था।
उसने चाय का एक घूँट भर के बीड़ी का एक कश मारा और फिर बोलने लगा—“बात दरअस्ल यह है कि मैंने अभी हाल ही में एक छोटी-सी कविता पढ़ी थी। ‘जो मार खा रोईं नहीं’ वह पूरी कविता एक उत्कृष्ट बिंब का उदाहरण हो सकती है, लेकिन वहाँ मुझे सिर्फ़ बिंब ही बिंब नजर आया इसके बरक्स जो सपना मैं देखता हूँ, मुझे पता है कि वह मेरे जीवन के तनाव से संबद्ध है। मैं मेरे जीवन की किसी परेशानी से मुक्ति चाहता हूँ। यह उसी की तरफ़ संकेत करता है। और ज़रूर यह बना भी किसी ऐसी घटना से है जिसमें मैं ख़ुश रहा होऊँगा। वह घटना हो सकता है मेरे अवचेतन में कहीं हो। अब यदि इसे मैं किसी कविता में प्रयोग करूँ, और मान लो मैं कोई बड़ा और प्रतिष्ठित कवि हूँ तो हो सकता है यह भावना किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की भावना के साथ मेल खा जाए, हो सकता है कि ऐसा ना भी हो। किंतु सोचो यदि ऐसा होता है तो ज़ाहिर तौर पर यह दृश्य रूढ़ होकर एक मनोविश्लेषणवादी प्रतीक बन जाए। मुझे लगता है कि ऐसा उस लंबी कविता में हुआ है। जो तुमने वह बात कही अभी मैं उससे सहमत हूँ।”
“हाँ, लेकिन जिस पाठक के जीवन में तनाव है ही नहीं, वो क्या उन बिंबों को प्रतीक के रूप ग्रहण कर पाएगा?” मैंने पूछा।
“तो तुम पूछना चाहते हो कि क्या बिंबों का प्रतीक के रूप में साधारणीकरण हो सकता है। जैसे रसों का होता है।”
“हाँ मैं यही पूछना चाहता हूँ। और यह भी कि कविता, कहानी और नाटक में बिंब क्या एक ही तरह से काम करते हैं?”
वह मेरी तरफ़ हिक़ारत भरी नज़रों से देखने लगा। उसने बीड़ी का धुआँ तक़रीबन मेरे मुँह पर छोड़ते हुए कहा, “मैं जानता हूँ तुम मुझे फँसाना चाहते हो इसलिए ही यह प्रश्न कर रहे हो। ठीक है, मैं मानता हूँ मुझे इतनी समझ नहीं है। तुम बताओ तुम इन प्रश्नों के बारे में क्या सोचते हो?”
मेरी चाय ख़त्म हो गई थी और उसकी चाय ठंडी। उसने बाक़ी बची चाय सागवान के पेड़ की जड़ में बेपरवाही का अभिनय करते हुए फेंक दी और कप नीचे रख दिया। वह मेरी तरफ़ ऐसे भाव से देखने लगा जैसे उसे मेरा मज़ाक़ बनाने का मौक़ा मिलने ही वाला है। एक अरसे से मैं उसके चेहरे के इस भाव से वाक़िफ़ था।
मैंने बोलना शुरू किया—“देखो मित्र, किसी भी बिंब को कोई पाठक किस परिमाण में ग्रहण करता है, यह वाक़ई उसके अपने विवेक, ज्ञान, अनुभव और अनुभूतियों पर निर्भर करता है।”
“यह कोई नई बात नहीं है। यह बात सब समझते हैं।” उसने बेमुरव्वत ढंग से कहा।
“हाँ। ठीक है। तुम एम.ए. को पढ़ाते हो। मैं समझता हूँ।” मैंने अपनी बात कही। वह झेंप गया।
“एक बार बात पूरी तो सुनो। फिर कुछ कह लेना।” मैंने आगे कहा।
“ठीक है कहो।” मेरे साथी का स्वर कुछ विनम्र हो गया।
मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा—“देखो कविता हो या कहानी या नाटक सभी में बिंब वर्णन के लिए तो आते हैं, किंतु कविता में बिंबों का निर्माण अधिक सघन होता है और वे अधिक तीव्रता के साथ पाठक को संप्रेषित होते हैं। कविता के बिंबों में प्रायः एक लय विद्यमान होती है, वे एक छवि का निर्माण करते हैं और अधिकतर वे सटीक, स्पष्ट और केंद्रीभूत होते हैं। अच्छी कविताओं में ऐसे भ्रामक शब्दों से परहेज़ किया जाता है जोकि उस छवि निर्माण में, उसके प्रस्तुतीकरण में बाधक बनते हों।”
“तो तुम कहना चाहते हो कि बिंब किसी दृश्य के अच्छे ब्यौरे होते हैं?”
“नहीं”, मैंने कहा। “ऐसा क़तई नहीं है। असाधारण बिंब कविता में कल्पना और यथार्थ के योग से बनते हैं और रसास्वादन की प्रक्रिया में अपना महत्त्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं। वे कवि की कल्पना को दृश्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे उस दृश्य का निर्माण करते हैं जो कोई रचनाकार देखता है और उसका भी जिसकी कोई रचनाकार कल्पना करता है। असल में वे रचनाकार के उन अनुभवों और अनुभूतियों को भी चित्रित करते हैं जो समय और स्थान से परे जाकर वह महसूस करता है। कविता में बिंब असल में पूर्णतः विकसित दृश्यों की बजाय किसी दृश्य के प्रतिनिधि प्रतीकों को स्थान दे सकते हैं, जैसे—रात को कंबल की तरह ओढ़ते हुए चित्रित करना कविता की भाषा में ही संभव है मेरे दोस्त, और कोई हैरानी नहीं कि पाठक इस तरह की किसी पंक्ति को पढ़कर एक धुँधले से दृश्य का निर्माण भी अपने मस्तिष्क में कर ले।”
“कविता में प्रायः बिंब एक समय के बाद प्रतीक का रूप लेते हैं। कविता में बिंबों का प्रतीक के रूप में गुम्फित होना आलोचकीय पाठों, सामान्य पाठकों के अर्थ ग्रहण की क्षमता तथा समाज की गतिशीलता के संदर्भ में तय होता है।” मैंने कहना जारी रखा...
“इसके बरक्स कहानी में बिंबों का प्रयोग प्रायः वर्णन के उद्देश्य से होता है, किंतु कभी-कभी कुछ कहानियों में भी बिंब प्रतीक बनकर आते हैं जैसे एक कहानी है ‘मछलियाँ’ उसमें जो चाय उबलने का बिंब है, वह महज़ बिंब नहीं है अपितु एक प्रतीक भी है। यह कथाक्रम में निर्धारित होता है कि कौन-सा बिंब किस तरह के प्रतीक के रूप में कार्य करेगा। यह उस लेखक कि सफलता है कि वह कथा-क्रम में दृश्यों का इतना सघन निर्माण कर सका है। उस बिंदु पर जहाँ प्रतीक और बिंब गुम्फित होते हैं, वे केवल ऐंद्रिय अनुभव ही नहीं बनाते बल्कि एक विशेष बौद्धिक प्रभाव भी पैदा करते हैं जिसका असर पाठक पर लंबे समय तक रहता है। और यही उस रचना को समय के पार ले जाता है। रही बात नाटक की तो नाटक का केंद्रीय विषय ही दृश्य है तो वह दृश्य प्रधान विधा है। उसमें बिंब दृश्य को ही समृद्ध करते हैं। आगे दृश्य अपना काम करता है। बिंब अप्रस्तुत होते हैं, पाठक अपनी कल्पना से अपना दृश्य ख़ुद बनाता है, जबकि नाटक में दृश्य प्रस्तुत होते हैं। उसमें दर्शक के लिए कल्पना की गुंजाइश कम ही होती है। ऐसा मुझे लगता है।”
“जब तुम्हें इतनी बात का पता था तो तुमने मुझसे प्रश्न क्यों किया? और दूसरे प्रश्न के संदर्भ में तो बात ठीक है, लेकिन पहले प्रश्न का जवाब तुम गोल कर गए। बताओ क्या बिंबों का प्रतीक रूप में स्थापित होना पाठक पर निर्भर करता है? या वे इससे स्वतंत्र हैं?”
मुझे लग ही रहा था कि उसका जवाब कुछ ऐसा ही होगा।
“यह इतना आसान नहीं है। बिंब और प्रतीक का गुम्फित होना एक जटिल प्रक्रिया के बाद का परिणाम होता है—जिसमें पाठक, रचना के आलोचकीय पाठ और देशकाल की परिस्थितियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं। अकादमिक दायरों के बाहर सामान्य पाठकों के साथ उस रचना का जुड़ाव किस स्तर पर होता है, यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सकता है।”
“बिल्कुल, जैसे उस जन नाट्य मंच द्वारा उस लंबी कविता के एक हिस्से को नाटक के रूप में खेला गया था।” उसने बीच में मुझे रोकते हुए कहा।
“हाँ, तुमने सही पकड़ा। इसी तरह एक समय के बाद कविता में बिंब और प्रतीक गुम्फित होने लगते हैं...”
“और वे रचना की उम्र भी बढ़ाते हैं।” उसने फिर से बीच में बोला।
“हाँ, यह भी एक महत्त्वपूर्ण बात है। लेकिन कोई बड़ा रचनाकार इस उद्देश्य से कविता में बिंबों का निर्माण नहीं करता। उसका उद्देश्य पाठकीय अनुभव को समृद्ध करना ही होता है। इसलिए कविता में वे इतने सघन रूप में निर्मित होते हैं।”
“एक समय बाद वे मिथक भी बन जाएँ और संस्कृतियों का निर्माण करने लगे तो भी कोई हैरानी की बात नहीं...” इतना कहकर वह हे-हे-हे करके हँसने लगा। ठीक है अब मुझे चलना होगा।
मैं उसके इस मज़ाक़ पर सोच में पड़ गया। “क्या वाक़ई मिथक संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या सच में उनमें इतनी शक्ति होती है?”
“ठीक है तुम जाओ, हम कल मिथकों के विषय में बातचीत करेंगे।”
“नहीं कल मुझे घर जाना है। एक ज़रूरी काम है। कुछ दिन बाद मिलेंगे। इतना कहकर वह चला गया।”
उसके जाने के बाद मेरा ध्यान दुबारा मौसम पर गया, बादल छंट रहे थे, धीरे-धीरे सागवान के बड़े-बड़े पत्तों पर हल्की-हल्की सुनहरी धूप दिखने लगी थी...
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
