प्रतिउत्तर : ‘नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद’
 वागीश शुक्ल
15 नवम्बर 2025
वागीश शुक्ल
15 नवम्बर 2025
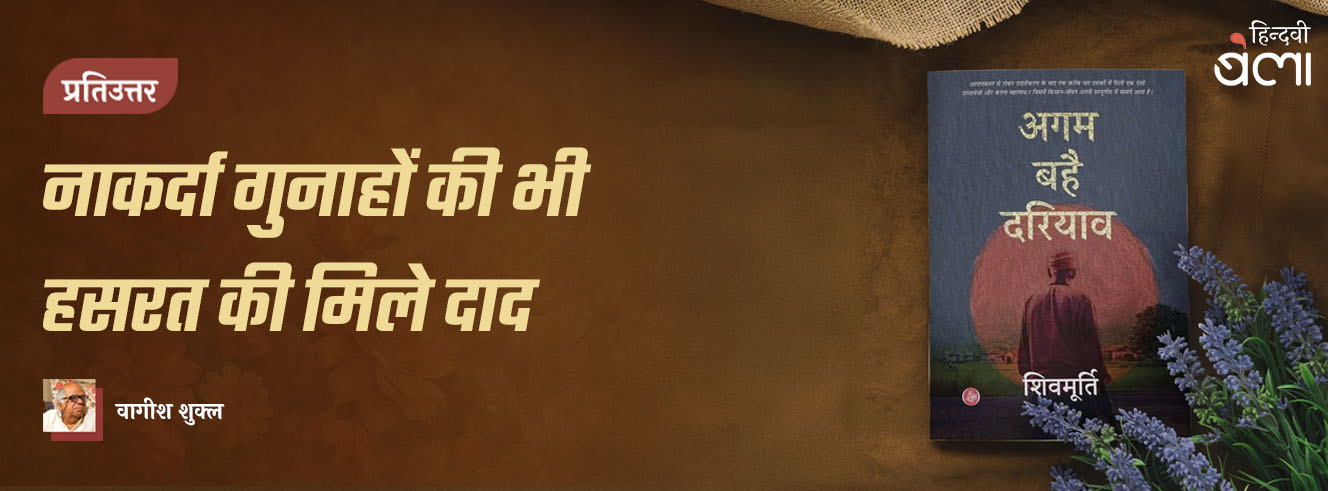
शिवमूर्ति जी ने ‘अगम बहै दरियाव’ पर मेरी आलोचना देखकर एक प्रतिलेख लिखा है और ग़ालिब की यह मनःकामना मेरे हित में पूरी कर दी :
नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिले दाद
या रब! अगर इन कर्दा गुनाहों की सज़ा है
यह प्रतिलेख पढ़ने के समय पुस्तक मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं दिल्ली से बस्ती आ गया था। मैं अष्टभुजा शुक्ल का आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी प्रति मुझे देकर मुझे ‘अगम बहै दरियाव’ दुबारा पढ़ने का अवसर दिया, जिससे मैं कुछ लिख पा रहा हूँ।
1. प्रतिलेख के कुल ग्यारह बिंदुओं में से पहले सातवाँ :
मैंने यह तो कहीं नहीं लिखा है कि जंगू जनसेवक के खेले वाली जिस हस्तलिखित पुस्तिका को बैताली पढ़ रहा है; उसी में चौबोला भी है। चौबोला जिस किताब में है, उसे तूफ़ानी ढूँढ़कर देगा—उसी के लिए मैंने लिखा था कि उसे लंदन पहुँचकर मार्क्स की क़ब्र की ज़ियारत करनी चाहिए; क्योंकि जिस ‘समय बदलने वाला खेला’ में यह चौबोला है, उसकी शुरुआती इबारत वहीं खुदी हुई है।
‘लंदन में लिखी’ एक हस्तलिखित पुस्तिका की बात मैंने ज़रूर की थी, जिसके निर्देशों के अनुसार हिंदी का समकालीन लेखन एक ज़माने से चल रहा है। यह पुस्तिका चौबोला वाले खेला को कमानी ऑडिटोरियम से नुक्कड़ पर लाने वाला नाट्यलेख है, जो जंगू जनसेवक वाले खेले में कारें-मोटरसाइकिलें-दुकान-मकान फूँकते और सिर तन से जुदा करते हुए सड़कों, आबादियों और गली-कूचों में खेला जाता है।
2. इसी सातवें बिंदु से जुड़ा उनका छठवाँ बिंदु है—मेरे द्वारा ‘उधिराना’ को ‘उधियाना’ पढ़ा जाना। यह ग़लती ज़रूर मुझसे हुई, किंतु इससे मेरा कहा हुआ निरस्त नहीं होता; क्योंकि शिवमूर्ति जी द्वारा दिया गया अर्थ ‘उधिराना = आतंक फैलाना, बदमाशी करना’ सही नहीं है। ‘उधिराना’ वही है जो ‘उधियाना—अंतर यह है कि ‘उधिराना’ केवल समूह-वाचक है और ‘उधियाना’ व्यक्ति-वाचक भी संभव है। अराजक माहौल में चोर-डाकू ‘उधिराते हैं’, बरसात में पतंगे उधिराते हैं। झुंड की झुंड चींटियाँ ‘उधिराती हैं।’ टिड्ढे उधिराते हैं। इन जगहों पर ‘उधियाते/उधियाती’ भी लिख सकते थे; लेकिन जिसकी रिश्तेदारी में कोई थानेदार हो जाता है, वह ‘उधियाता’ है। ‘उधिराता’ नहीं। यहाँ जंगू का उधियाना ही लिखना चाहिए था। और इसका तात्पर्य वही है—सूरज की किरन उतना नहीं दुख देती, जितना उसकी गर्मी से तपी हुई बालू... और यह शब्द फ़सल की ओसौनी से ही आया है।
3. प्रतिलेख का पहला बिंदु यह है कि तूफ़ानी सिंह पासी जाति के हैं और यह ‘स्पष्ट’ है।
पृष्ठ 47 के अनुसार ‘दलित जातियों’ ने एक महापंचायत की है, जिसके निर्णय हैं—तीन किलो मज़दूरी चाहिए, कोई दलित किसी के घूरे की खाद सिर पर नहीं ढोएगा, और चमड़े की एवज़ में मरे हुए जानवर नहीं उठाएगा, नक़द भुगतान चाहिए।
फिर पारस सिंह की हत्या के जुर्म में झूरी की बिरादरी से वह ख़ुद, उनके दोनों बेटे, और उनके दोनों पोते बदरी और तूफ़ानी पकड़े जाते हैं। यह तूफ़ानी ही है, जिसका ‘पासी जाति का होना स्पष्ट है।’ इस स्पष्टता का सुराग़ ढूँढ़ने पर सूरत से बुलाए गए झूरी के भाई परमेसरी का पृष्ठ 56 पर यह कथन मिलता है—‘‘हमारी बिरादरी में राजा-महाराजा हुए हैं। हम झुक नहीं सकते। ठन गई तो ठन गई। उनके दरवाज़े ताज़िंदगी नहीं जाएँगे। जिनके बाप-दादा सवर्णों की पनही उठाते आ रहे हैं, वे जाकर उठावें।’’
ये पनही उठाने वाले कौन हैं, यह भी वहीं स्पष्ट कर दिया गया है—छत्रधारी सिंह ने ‘‘टोले की चमार बिरादरी की स्त्रियों को काम करने के लिए राज़ी कर लिया।’’
लेकिन टोला एक ही है—‘सियरहवा टोला’ या ‘दलित टोला’। मेरी भूल यह हुई कि मैं यह भूल गया कि Mixed Neighborhood की अवधारणा अमरीका से पहले सुल्तानपुर में क्रियान्वित हुई थी—मैंने यह समझा कि जिस टोले के बाशिंदों ने चमड़े के बदले मरे जानवर न उठाने का फ़ैसला लिया है, उस टोले का बाशिंदा तूफ़ानी उन्हीं में से होगा। दरअस्ल, मैं अभी तक यह समझता था कि पासियों का टोला अलग होता है और उनका टोला अलग, जो मरे जानवर उठाते हैं—चाहे वे एक ही ‘सियरहवा भीटे’ पर क्यों न बसे हों। भारतीय जाति-व्यवस्था में हर जाति के पास उससे नीची एक जाति है, जिससे वह रोटी-बेटी और बसावट में दूरी बनाकर रखती है। किंतु ‘अगम बहै दरियाव’ शायद किसी दूसरे सुल्तानपुर की कहानी है, जिसमें ‘दलित टोला’ नाम की एक बसावट है। यह बसावट इसलिए बसाई गई है कि
टोले के बारह लोग पकड़कर जेल भेजे गए। झूरी की बिरादरी के ख़ुद झूरी, उनके दोनों बेटे—विक्रम और शेरू, उनके दोनों पोते—बदरी और तूफ़ानी। उनका भतीजा—बिरजू और जगेसर तथा झगरू की बिरादरी के झगरू, कोदई, संपत, बिपत और पहाड़ी।
— अगम बहै दरियाव, पृष्ठ 55-56
इसी ‘दलित टोले’ में बसने के नाते तूफ़ानी सिंह अम्बेडकर पासी होते हुए भी टी.डी. सिंह के फगुए में ‘हमारी जाति को गाली, हमारी औरतों को गाली’ (पृष्ठ 341) ढूँढ़ पा रहे हैं; तो जहाँ इतनी समरसता है कि झूरी की बिरादरी और झगरू की बिरादरी एक ही टोले में रहती हैं और झगरू की जाति को गाली झूरी की जाति को गाली मानी जाती है, वहाँ कौन न मानेगा कि मुख़्तार साहब के घर में रसोई का काम ‘सवर्णों की पनही उठाने वाली बिरादरी’ से आने वाली जंगू की माँ सँभालती है (पृष्ठ 156) जबकि ‘भूले बिसरे चित्र’ के मुंशी शिवलाल छिनकी कहारिन का भी बनाया नहीं खाते थे और उनके लिए रसोई बनाने का उनसे हुक्म पाने पर छिनकी रोने लगती है।
4. प्रतिलेख के आठवें बिंदु में बताया गया है, ‘‘बयनामा 1972 का है इसलिए उनकी पत्नी का बयनामे पर हस्ताक्षर होने और उनसे पूछताछ होने का प्रश्न ही नहीं है।’’
प्रतिलेख की यह सूचना तो सत्य है कि 2002 से पहले क्रेता का हस्ताक्षर बयनामे पर नहीं होता था—पता लगाने पर मुझे भी मालूम हुआ कि क्रेता का हस्ताक्षर होने की अनिवार्यता 20 मई 2002 की अधिसूचना से हुई है। इसलिए मेरा यह कहना तो ग़लत था कि छत्रधारी सिंह की पत्नी के भी हस्ताक्षर बयनामे पर होने चाहिए। किंतु यह आदेश राजस्व विभाग का है, इससे सिर्फ़ यह साबित होता है कि उस हस्ताक्षर के बिना भी मनराज कुँवरि जौजे छत्रधारी सिंह का नाम ज़मीन पर चढ़ सकता था। लेकिन चूँकि बयनामा मंसूख़ी का अधिकार राजस्व विभाग के पास नहीं होता, इसलिए मुक़दमा तो दीवानी का है—उसमें अगर छत्रधारी सिंह को नोटिस गया है और वह अपना ज़वाब दाख़िल करने पर मजबूर किए गए हैं, तो मनराज कुँवरि को क्यों ज़वाब दाख़िल नहीं करना पड़ेगा—‘‘उनसे पूछताछ होने का प्रश्न’’ क्यों नहीं उठेगा? ख़रीदार के पति से पूछताछ होगी, लेकिन ख़रीदार से नहीं? क्या शिवमूर्ति जी की क़ानूनी किताब में यही अदालती प्रक्रिया लिखी हुई है कि यह सिविल सूट ‘नेसेसरी पार्टी’ मनराज कुँवरि के बिना केवल उनके पति छत्रधारी सिंह के ख़िलाफ़ चल सकता है जो सिर्फ़ ‘प्रापर पार्टी’ हैं? जाल-बट्टे का फ़ौजदारी मुक़दमा छत्रधारी सिंह के ख़िलाफ़ दर्ज़ होगा और जिसके नाम जाली बयनामा है, उससे ‘‘पूछताछ होने का प्रश्न ही नहीं है?’’
इतना ही ‘फ़ैक्ट-चेक’ करना था तो पृष्ठ 15 पर बयनामा ‘मनराज कुँवरि जौजे छत्रधारी सिंह’ के नाम करवा देने के बाद, पृष्ठ 20 पर यह सूचना देने की क्या ज़रूरत थी कि छत्रधारी सिंह की पत्नी का नाम ‘इंदिरा’ है? क्या छत्रधारी सिंह किसी और तरीक़े से ‘कांग्रेसी’ नहीं बताए जा सकते थे? क्या जिन बेईमान मिल-मालिकों ने पहलवान के गन्ने का दाम बक़ाया रखा है, उन्होंने छत्रधारी सिंह के कांग्रेसी होने या रामबादी होने के नाते चुपके से उनके गन्ने का भुगतान कर दिया है?
समीक्षा में संदर्भ तो इस उपन्यास में आए स्त्री-पात्रों के ‘स-शक्त’ होने का था और मेरा सवाल यह था कि छत्रधारी सिंह की पत्नी मनराज कुँवरि कितनी ‘स-शक्त’ हैं—और उपन्यासकार से नहीं था; उन समीक्षकों से था, जिन्होंने इस उपन्यास में ‘सशक्त’ स्त्रियाँ देखी हैं। क्या प्रतिलेख में इसी का उत्तर दिया गया है?
5. प्रतिलेख के चौथे बिंदु में शिवमूर्ति जी का तर्क है कि ‘‘जब खेलावन के गाँव में मुसलमान पात्र हैं ही नहीं तो वह मुसलमान बराती कैसे ले जाते?’’
क्या किसी बरात में केवल ‘गाँव के लोग’ जाते हैं? ‘पड़ोसी गाँव के ट्रैक्टर वाले ख़ान’ जो पृष्ठ 575 पर एक ट्रॉली गन्ना और अपनी अम्मी को लेकर किसान-प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं, क्या खेलावन के अपरिचित हैं?
मेरा कहना यह नहीं था कि खेलावन को मुसलमान भी अपनी बरात में ज़रूर ले जाने चाहिए थे—मेरा कहना यह था कि बरात में सभी जातियों के लोग जाते हैं और इसलिए तूफ़ानी सिंह अम्बेडकर तथा खेलावन का यह उभयपक्षीय संकोच उचित नहीं है कि तूफ़ानी के रहने से असहज स्थिति उत्पन्न होगी। क्या खेलावन की बरात में एक भी दलित है, और अगर नहीं है तो क्या यह स्वाभाविक है?
6. प्रतिलेख के नवें बिंदु में शिवमूर्ति जी ने कहा है, ‘‘संतोखी बिना किसी प्रतिरोध के अपने खेत पर क़ाबिज़ हो जाते हैं; यह क़ब्ज़ा किसी कोर्ट के आदेश से नहीं, जंगू के एक छोटे से रुक्के से हुआ।’’
घटना-क्रम क्या है? रुक्के से कुछ नहीं हुआ, रुक्का पाकर छत्रधारी सिंह अपने बचाव का इंतिज़ाम करते हैं—जंगू उन पर ‘टाँग तोरि बैठाया हो’ का मंतर नहीं इस्तेमाल कर पाता है। जो हुआ है; शकुंतला के अपहरण से हुआ है, जो केवल इसलिए हो पाया कि किसी को यह ख़याल नहीं आया कि नागपंचमी में झूला झूल रही लड़कियों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। अपहरण करने के लिए जंगू ख़ुद नहीं आता, दो ग़ुंडों को भेजता है जो शकुंतला को पहचानते भी नहीं हैं—उसका नाम पूछकर उसे ले जाते हैं। यह छत्रधारी सिंह के विरुद्ध कृत्य नहीं है, गाँव को चेतावनी है कि आगे से अपनी लड़कियों को तभी झूला झूलने भेजें, जब उनके साथ बंदूक़धारी सुरक्षा हेतु तैनात हों।
इसके बाद छत्रधारी सिंह को अपनी पौत्री शकुंतला के अपहरण का समाचार सुनकर फ़ालिज मार जाता है, जिसके बाद उनके इलाज के चक्कर में उनके घर के लोग गाँव में ध्यान नहीं दे पाते और संतोखी के खेत में छत्रधारी सिंह की लगाई फ़सल यों ही झड़ जाती है; छत्रधारी तो क्या, गाय-भैंस भी उसमें नहीं घुसते। लेकिन फ़ालिज छत्रधारी सिंह को मारा है, उनके उद्दंड भतीजे और उनके दरोग़ा बेटे को नहीं—जो संतोखी पहले भी एक बार अदालत और पुलिस के बल पर ‘क़ाबिज़’ हो गए थे और अपनी फ़सल नहीं काट पाए, वे क्या इस अपहरण के बल पर पाए क़ब्ज़े से हमेशा के लिए ‘क़ाबिज़’ रह सकते हैं? ‘निर्विरोध क़ाबिज़’ रहने की अवधि कब तक है?
मेरी जिज्ञासा यह है कि उपन्यास—और अब और मुखर रूप में अपने प्रतिलेख—द्वारा शिवमूर्ति जी कह क्या रहे हैं? जिससे लड़ना है, उसकी लड़की उठा लो? यह कोई नया तरीक़ा तो नहीं है—यह ‘समय बदलने वाला खेला’ नहीं है; यह वही खेला है, जो समय की शुरुआत से खेला जा रहा है और समय के अंत तक खेला जाएगा। जंगू ने कोई नया रुक्का नहीं भेजा है—SABINAE RAPTAE = The Rape of Sabine Women के भी पहले से ये रुक्के भेजे जाते रहे हैं और आज भी बंद नहीं हुए। ऐसे ही रुक्के भेजकर जंगू जैसे तमाम जनसेवक जनसेवा करते आए हैं और करते रहेंगे।
‘अन्याय-बोध’ केवल उन किसानों को ही नहीं है, जिनके गन्ने का दाम मिल-मालिक नहीं देता, मिल-मालिक भी यही समझता है कि उसने गन्ना-मिल में पैसा फँसाकर घाटे का सौदा किया। ट्रंप भी यही मानते हैं कि अमरीका के साथ अन्य देश अन्याय कर रहे हैं। फिर जिसके पास जो हथियार न्याय-प्राप्ति का होता है, आज़माता है।
इस उपन्यास में जंगू जनसेवक का चरित्र नागर जी के ‘नाच्यौ बहुत गुपाल’ के मोहन से पॉलिश करके तैयार किया गया है—जो अंतर है, वह यह कि जहाँ मोहन के द्वारा सवर्ण लड़कियों की ‘बेइज़्ज़ती’ और उसकी डकैतियाँ छिपाई नहीं गई हैं, वहीं इस उपन्यास में शकुंतला के साथ जंगू बलात्कार नहीं करता और उसने पुलिस कप्तान को लिखा है कि उसने कोई डाका भी नहीं डाला। फिर भी उसके पास एक बंदूक़ है, जिसे पृष्ठ 464 पर ऊपर उठाए हुए नदी में तैरता हुआ वह पुलिस से बच निकलता है। यह बंदूक़ उसे किसने दी? इसके ख़रीदने में पैसा लगता है और छत्रधारी सिंह की बंदूक़ से ज़ियादा लगा होगा, क्योंकि जंगू के पास लाइसेंस भी न होगा। जिस मोटरसाइकिल पर शकुंतला को उठाया जाता है, उसका दाम किसने दिया है?
‘सशस्त्र संघर्ष’ बिना पैसे के नहीं होता और पैसा उसी का ख़र्च होता है, जिसके पास होता है। जंगू छोटा जनसेवक है—बड़े जनसेवकों को लैंड-माइंस दी जाती हैं, कुछ और बड़े जनसेवक रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी-एयरक्राफ़्ट गंस, मिसाइल्स आदि के योग्य माने जाते हैं। प्रशासन कभी ‘कार सेवकों’ की लाशें बिछाता है, कभी ‘जन सेवकों’ की—अपने पसंदीदा अस्थि-कलश लिए लोग आपस में वकैती-लठैती करते रहते हैं। ‘समय बदलने का खेला’ कौन खेल रहा है?
जो जनसेवक डाका नहीं डालते; उनसे प्राप्त जिन सात घड़ियों, तीन चेनों, छह अँगूठियों को हथियाने के लिए पुलिस वाले पृष्ठ 467 पर आपस में झाँव-झाँव कर रहे हैं, वे क्या हिंदी लेखकों ने चंदा कर के दी हैं?
जनसेवा में जो पैसा ख़र्च होता है, वह कहाँ से आता है?
जनसेवा के लिए पैसा ही नहीं, सरकार में अपने आदमी भी चाहिए। होमगार्ड अबरार से जंगू की जो मैत्री पृष्ठ 549 पर दिखाई गई है, उसके अभाव में जंगू जनसेवक कैसे बच निकलता?
शिवमूर्ति जी जिस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, वह Law of Diminished Responsibility कहलाता है—सवर्ण द्वारा दलित की हत्या या पति द्वारा पत्नी की हत्या उत्पीड़न है, किंतु दलित द्वारा सवर्ण की हत्या या पत्नी द्वारा पति की हत्या प्रतिक्रिया है। इसी के चलते ये तर्क दिए जाते हैं कि आदिवासी तो कभी बलात्कार करते नहीं; सो यदि आदिवासी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है, तो ग़ैर-आदिवासी ने ही किया होगा।
उपन्यास के अगले संस्करण में हो सकता है कि जंगू जनसेवक थाने में चीख़ता हुआ सरेंडर करे—मैंने उस राक्षस की बेटी उठा ली है—और तूफ़ानी सिंह अम्बेडकर उनका मुक़दमा अदालत में लड़ें, जिसमें बचाव-पक्ष की ओर से समकालीन हिंदी कविता पेश की जाए। लेकिन इस खेले से भी समय नहीं बदलेगा।
शिवमूर्ति जी ने अंत में लिखा है, ‘‘यदि कोई वास्तविक चूक सामने आती है, तो उसे दुरुस्त करने में मुझे ख़ुशी होगी।’’ क्या वह समझते हैं कि यह समीक्षा चूक वास्तविक या अ-वास्तविक—ढूँढ़ने के लिए लिखी गई थी? ‘चूक’ मौसम के हिसाब से होती है। अपने उपन्यास में उन्होंने अदालती प्रक्रिया पर बहुत सवाल खड़े किए हैं; किंतु जब वह उपन्यास लिख रहे थे, तब ‘‘क्यों दिया हाई कोर्ट ने ऐसा फ़ैसला?’’ (पृष्ठ 498) पूछना प्रगतिशील होने का प्रमाण था, उपन्यास बिकने की नौबत आते-आते यह पूछना ‘सांप्रदायिक उन्माद’ फैलाना हो चुका है।
हिंदी साहित्य की ‘इठलाती आती ग्राम-युवति’ जिस ‘टेढ़े-मेढ़े रास्ते’ से गुज़रती हुई इस उपन्यास में पहुँची है; दरअस्ल, वह रांगेय राघव का ‘सीधा-सादा रास्ता’ ही है। रेणु और श्रीलाल शुक्ल ने कम से कम यह किया था कि अगर आपको अपनी दीवारें ख़राब होने का डर सता रहा हो; तो आप एक कपड़े पर बनी तस्वीर अपने लिविंग रूम में लटका सकते हैं, जिसमें लहलहाती फ़सल को मारता हुआ पाला जस का तस दिखता है। अब यह हो रहा है कि मुरझाए बैंगन पर तेल पोतकर उसे माल में सजाया जा रहा है, जिससे लोकल को ग्लोबल किया जा सके।
यह उपन्यास जिस इलाक़े में है, उसमें शिवमूर्ति जी ने अपना जीवन बिताया है और उससे मेरा संपर्क इतना ही है कि रिश्तेदारी के चलते इलाहाबाद में पढ़ते समय मैं कभी-कभार पड़ोसी ज़िले प्रतापगढ़ में चला जाता था। इसलिए जहाँ तक ‘तथ्यात्मक प्रामाणिकता’ का प्रश्न है; वे ही प्रामाणिक हैं, मैं नहीं। किंतु बाउर पाँड़े के पौत्र और भगवत पाँड़े के पुत्र प्रभाकर पाँड़े को साइकिल पर चलते-चलते ‘दाहिने हाथ से जेब से रोटी निकालकर उसे गोल चोंगा बनाकर काट-काटकर’ खाते हुए (पृष्ठ 502) मैंने 1961-65 में नहीं देखा था और शिवमूर्ति जी ने भी 2012 तक नहीं देखा होगा—ऐसा केवल वे ही करते हैं, जो ‘समय बदलने वाला खेला’ खेलते हैं। हाँ, जब मैं पेरिस में था तो लोगों को राह चलते बगेत (= Baguette) इस तरह खाते हुए ज़रूर देखा था।
•••
वागीश शुक्ल का आलेख यहाँ पढ़ सकते हैं : अगम बहै दरियाव, पाँड़े! सुगम अहै मरि जाव
वागीश शुक्ल के आलेख पर शिवमूर्ति का प्रतिलेख यहाँ पढ़ सकते हैं : ‘अगम बहै दरियाव’ पर वागीश शुक्ल की आलोचना के बारे में कुछ तथ्य
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
