निर्वाण से नरक तक : जेंडर पुनर्मूल्यांकन सर्जरी के लिए जूझता भारतीय ट्रांसजेंडर
 किंशुक गुप्ता
01 जनवरी 2025
किंशुक गुप्ता
01 जनवरी 2025
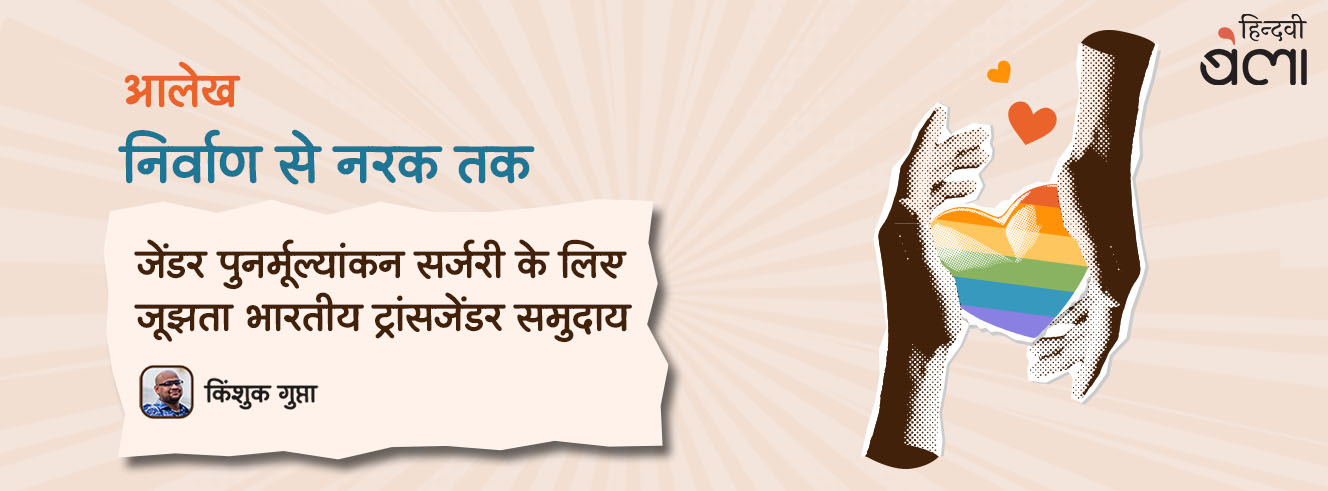
ट्रांस महिला रीता फ़ौजदार को जेंडर पुनर्मूल्यांकन सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के दौरान यह नहीं पता था कि उसे ऑपरेशन के बाद भी डेढ़ महीने तक कड़ी देखभाल की ज़रूरत होगी। उसके डॉक्टर ने ऑपरेशन की हर पेचीदगी को तथ्यात्मक रूप से तो समझाया था, लेकिन किसी पर इतना ज़ोर नहीं दिया था कि वह उन पर उस तरह से ध्यान दे। उदाहरण के लिए—डॉक्टर ने कहा था कि अगर रोज़ाना योनि को चौड़ा करने की प्रक्रिया का सख़्ती से पालन नहीं किया गया तो उसके सिकुड़ने का ख़तरा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया था कि इस प्रक्रिया के दौरान उसे असहनीय दर्द झेलना होगा जिसके कारण वह बिस्तर से उठ तक नहीं पाएगी।
सड़कों पर भीख माँगना या नवविवाहितों और नवजात शिशुओं के घरों तक जाकर बधाई माँगना तो दूर की बात है। सफल सर्जरी के शुरुआती उत्साह के ठंडे पड़ने पर फ़ौजदार को असलियत का एहसास हुआ। कुछ समय तक उसके बॉयफ़्रेड ने उसका साथ दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह उसे छोड़कर चला गया।
“सेक्स के बिना आप एक आदमी को कब तक साथ रख सकते हैं?” उसने मुझसे सवाल पूछा। जैविक परिवार तो उसे बहुत पहले ही बेदखल कर चुका था और दिल्ली जैसे नए महानगर में वह ट्रांस समुदाय के ज़्यादा लोगों को जानती भी नहीं थी।
“मुझे सपने में भी नोट दिखाई देते हैं। [ट्रांस] समुदाय के कुछ साथियों ने कुछ दिनों के लिए मेरे खाने का इंतज़ाम किया। पर जब वो ख़ुद ही बमुश्किल अपना गुज़ारा कर पाते हैं तब उनके लिए मेरा साथ देना कब तक मुमकिन था?” उसके प्रेमी ने उसे दूसरी महिला के लिए छोड़ दिया, दोस्तों का दायरा सिकुड़ता गया, और इसके साथ ही योनि को चौड़ा करने की उसकी इच्छा भी ख़त्म हो गई।
“अब यह बस एक गहरा घाव है…” उसने सपाट तरह से पूछा।
फ़ौजदार की कहानी एक सफल जेंडर पुनर्मूल्यांकन सर्जरी (जी.आर.एस.) के बाद अच्छी पोस्ट-ऑप देखभाल की आवश्यकता को उजागर करती है, लेकिन भारतीय ट्रांस समुदाय के लिए सर्जरी तक पहुँचना भी आसान नहीं है। पहले एस.आर.एस. के नाम से जाने जानी वाली यह एक अत्यधिक परिष्कृत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य जन्म के समय निर्धारित जेंडर को व्यक्ति के मनवांछित जेंडर में परिवर्तित करना है।
यह एक बहु-चरणीय प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से शुरू होती है जिसके द्वारा एक ट्रांस व्यक्ति को अपने निर्धारित जेंडर के अनुरूप शारीरिक विशिष्टताएँ प्रदान की जाती हैं। जिसके बाद टॉप और बॉटम सर्जरी की जाती हैं जिनके द्वारा जननांग परिवर्तित किए जाते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसे पूरा होने में कुछ सालों का समय लग सकता है।
पुराने समय में ट्रांस व्यक्तियों को हिजड़ा समुदाय में शामिल होने के लिए छिबराने की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता था। वह एक पीड़ादायक और हिंस्र प्रक्रिया होती थी जो आधुनिक समय के कैस्ट्रेशन से मिलती-जुलती है। हालाँकि यह शेविंग ब्लेड और देसी दारू से लैस दाइयों और हकीमों द्वारा किया जाता था जो बिना बेहोश किए पुरुष लिंग को काट देते थे। प्रक्रिया के सफल होने पर ट्रांस व्यक्ति को निर्वाण (मोक्ष) की प्राप्ति होती थी।
“1980 से 1990 के दशक में इस प्रक्रिया के लिए बहुत सारे संदेहपूर्ण क्लीनिक खुल रहे थे। सर्जन अधिक पैसा कमाने के लिए बिना किसी विशेषज्ञता के इसे अंजाम देते थे। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित एक ट्रांस महिला को उसके डेरा गुरु ने मज़बूर किया। सर्जन को बीमारी के बारे में नहीं पता था क्योंकि उसने पहले से कोई भी टेस्ट नहीं करवाया था और ख़ून न रोक पाने के कारण उस महिला की मृत्यु हो गई।” —उस युग में सक्रिय ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता और हिंदी लेखक सुभाष अखिल ने मुझे बताया।
“जी.आर.एस. की लोकप्रियता केवल शहरी क्षेत्रों और शिक्षित ट्रांस व्यक्तियों के बीच ही बढ़ी है। वंचित समुदायों के बीच छिबरवाने की क्रूर और अवैज्ञानिक प्रथा अभी भी जारी है।”—तमिलनाडु की एक ज़मीनी कार्यकर्ता शालिन मारिया ने जोड़ा।
गुरु-शिष्य परंपरा में शामिल न होने वाले ट्रांस व्यक्तियों के बीच धनाभाव चिंता का मुख्य विषय है। आय का स्रोत बधाई माँगना या वेश्यावृत्ति है—जो अनियमित हैं। रोज़ कमाकर खाने वाले ये ट्रांस व्यक्ति बहुत कठिनाइयों का सामना करके ऑपरेशन के लिए रुपए इकट्ठे कर पाते हैं। “पैसे इकट्ठा करने में सालों लग जाते हैं। साहूकार ब्याज पर रुपए नहीं देते और जो अगर देते हैं वो शारीरिक शोषण करते हैं। बहुत बार हम समुदाय में अपने दोस्तों से ऋण लेते हैं।” फ़ौजदार ने मुझे बताया।
कई बार तो यह भी पर्याप्त नहीं होता। अकेले टॉप या बॉटम सर्जरी में 3 से 5 लाख तक का ख़र्च आ सकता है। इसके अलावा चिकित्सीय परामर्श, दवाओं, हॉर्मोन, अस्पताल में रहने आदि का ख़र्च ऊपर से होता है।
एक ट्रांस मैन और ओला टैक्सी ड्राइवर, नीरज पर्याप्त रुपयों की कमी के कारण अपनी पसंद के डॉक्टर के पास नहीं जा सका। लंबे समय तक टेस्टोस्टेरोन की गोलियों के बावजूद आकस्मिक रक्तस्राव के कारण वह जनकपुरी स्थित दूसरे डॉक्टर के पास जाने पर विवश हो गया जिसने कम रुपयों में इलाज करने का वायदा किया।
नीरज आज भी उस फैसले पर पछताता है। डॉक्टर ने उसे एक ख़ाली सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और स्तन-उच्छेदन के लिए उसकी पसंद की प्रक्रिया को कोई वरीयता नहीं दी। नीरज ने डॉक्टर को इसके लिए भी माफ़ कर दिया होता, लेकिन डॉक्टर ने उसके स्तन के ऊतकों के कुछ हिस्सों को अंदर ही छोड़ दिया।
“आपको क्या लगता है कि एक ट्रांस मैन टॉप सर्जरी क्यों करवाता है?” वह मेरी तरफ़ सवाल दागता है और कुछ देर बाद ख़ुद ही जोड़ देता है—“ताकि वह बिना क़मीज़ के घूम सके। अपना जिम-टॉन्ड शरीर दिखा सके।” नीरज ने डॉक्टर से मुफ़्त या न्यूनतम राशि पर फिर से सर्जरी कर बचे हुए हिस्से को निकालने की माँग रखी जिसे डॉक्टर ने सिरे से नकार दिया। उल्टा उसे धमकाया कि यदि उसने उन्हें ज़्यादा परेशान किया तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।
“माना कि ख़ाली काग़ज़ पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए थे। इस बार ग़लती मेरी है लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो क्या गारंटी है कि पुलिस मेरी बात सुनती?”
डॉक्टरों द्वारा इस तरह का अमानवीय व्यवहार अपवाद होने के बजाय रोज़मर्रा की बात है। ख़ासकर, अशिक्षित और अनभिज्ञ ट्रांस लोगों के बीच, जिनके पास नियमित आय का स्रोत नहीं है और जो आसानी से डॉक्टरों द्वारा कम क़ीमत में ऑपरेशन के लालच में आ जाते हैं।
2022 में अनन्या कुमारी-एलेक्स और उसके साथी की आत्महत्या का उदाहरण हमारे सामने है, जब एक असफल जेंडर पुनर्मूल्यांकन सर्जरी ने उसकी बुनियादी मानवीय गरिमा को छीन लिया। ऑपरेशन के सहमति पत्र कई बार ख़ाली पन्ने होते हैं और कई बार अँग्रेज़ी भाषा में लिखे होते हैं जिन पर ट्रांस व्यक्तियों को मजबूरन हस्ताक्षर करना होता है। मरीज़ों को कभी भी सभी उपलब्ध विकल्पों के बारे में नहीं बताया जाता है। डॉक्टर जो भी सही समझते हैं, अपनी मनमर्ज़ी से वही ऑपरेशन कर देते हैं।
राज्य सरकारों ने इन समस्याओं के निवारण के लिए क़ानून में नए प्रावधान जोड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में जी.आर.एस बिना किसी ख़र्च या न्यूनतम लागत पर किया जाना जिनमें से एक है। तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने जी.आर.एस. को पूरी तरह से मुफ़्त करने का आश्वासन दिया है। हालाँकि ज़मीनी स्तर पर इनमें बहुत सारी दिक़्क़तें हैं। इंतज़ार का समय लंबा है। डॉक्टरों और संसाधनों के अभाव में यह कुछ सालों तक भी खिंच सकता है।
पैरामेडिकल स्टाफ़ और नर्स ट्रांस-अफ़र्मेटिव व्यवहार और भाषा से ठीक तरह से परिचित नहीं हैं। ट्रांसजेंडर मरीज़ों के लिए अस्पताल में अलग से वॉशरूम या वार्ड की व्यवस्था नहीं की जा सकी है, जबकि इसका प्रावधान तो 2019 में पारित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम में दिया जा चुका था।
नीरज ने मुझे अपने दोस्त के बारे में बताया जो ऑपरेशन के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र लेने के लिए दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में मनोचिकित्सक के पास चार साल तक जाता रहा। मनोचिकित्सक उसे अपने भ्रामक सवालों में इस तरह उलझाता रहा कि ट्रांसमैन ने आत्मविश्वास ही खो दिया। उसे लगने लगा कि उसका ऑपरेशन का निर्णय ग़लत है।
यहाँ आधार कार्ड और ट्रांसजेंडर पहचान पत्र (टी.जी.) प्राप्त करने में नौकरशाही बाधाओं का उल्लेख भी किया जाना चाहिए, जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए मूलभूत आवश्यकता है।
शिव—एक इंटरसेक्स व्यक्ति, आधार प्राधिकरण केंद्र का मालिक, जिसने पुणे की अपनी नौकरी छोड़ दी और सतोली में अपने घर लौट आया क्योंकि गाँव में उसकी सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत थी। “एक ट्रांसजेंडर के लिए सरकारी कार्यालयों में जाना एक दुःस्वप्न साबित हो सकता है। पर्याप्त रूप से संवेदनशील न होने पर अधिकारी ट्रांस व्यक्तियों को गहरा आघात पहुँचा सकते हैं।”
नीरज ने मुझे बताया कि उसे दिल्ली के बाहरी इलाके में टी.जी. कार्ड प्रसंस्करण के लिए एक केंद्र आवंटित किया गया था, जहाँ पर यह अपनी तरह का पहला मामला था। अधिकारियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह ट्रांसमैन है क्योंकि वह एक सामान्य पुरुष जैसा दिखता था। “अच्छा खासा आदमी तो है, तुझे कार्ड क्यों चाहिए?” हालाँकि उन्होंने कोई अपमानजनक टिप्पणी तो नहीं की, पर उसे देखकर हैरान ज़रूर हुए।
“उन्होंने एक ट्रांस महिला को वीडियो कॉल करके मेरी बात करवाई जिसने मुझसे प्रसिद्ध ट्रांसमैन आइकन आर्यन पाशा के बारे में पूछा। मेरे अपने कहने के ज़्यादा उन्हें उस महिला की बात पर विश्वास था।”
इन सभी दिक़्क़तों को मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने हाल-फिलहाल में ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य के लिए एक समर्पित ओ.पी.डी. का राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उद्घाटन किया है। ऐसे प्रयास सराहनीय है, हालाँकि यह सभी प्रयास समुद्र में एक बूंद जितने हैं।
(यह रिपोर्ताज लाडली मीडिया फ़ेलोशिप के सहयोग से लिखा गया है। यह लेखक के अपने विचार हैं। लाडली मीडिया और यू. एन. एफ. पी. ए. की कोई ज़िम्मेदारी नहीं।)
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
