जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ : बिना काटे भिटवा गड़हिया न पटिहैं
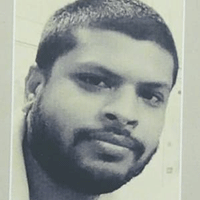 शैलेंद्र कुमार शुक्ल
17 अगस्त 2024
शैलेंद्र कुमार शुक्ल
17 अगस्त 2024
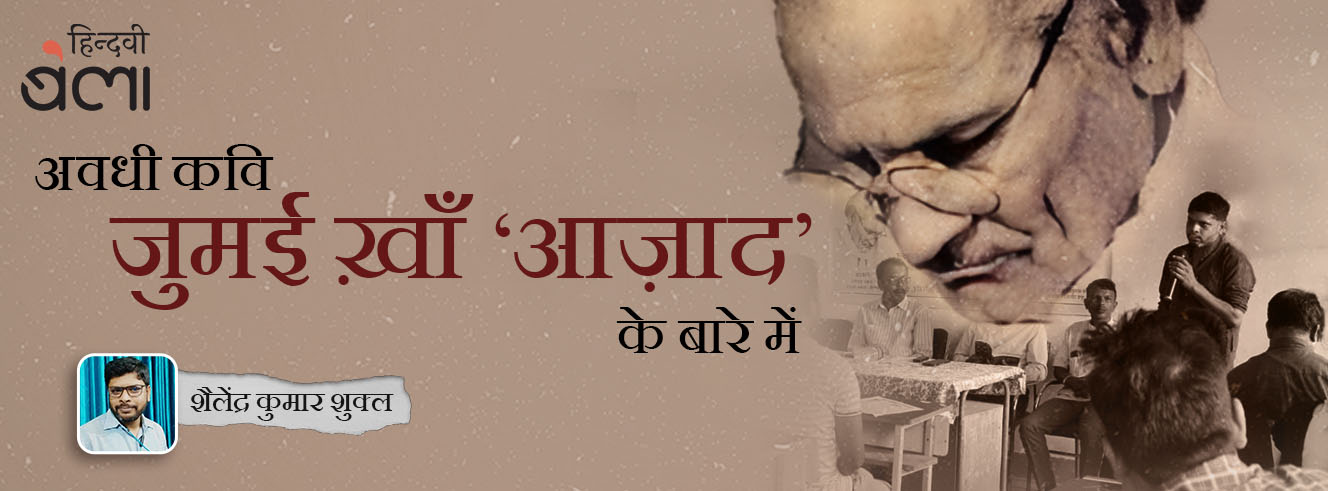
कवि जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ (1930-2013) अवधी भाषा के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। उनकी जन्मतिथि के अवसर पर जन संस्कृति मंच, गिरिडीह और ‘परिवर्तन’ पत्रिका के साझे प्रयत्न से जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ स्मृति संवाद कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ की कविताओं का पाठ किया गया और उनकी कविताओं पर हिंदी के कवि-आलोचक शैलेंद्र कुमार शुक्ल ने व्याख्यान दिया। यहाँ प्रस्तुत है यह व्याख्यान :
आधुनिक अवधी कविता अपनी स्वाभाविकता में वर्ग-संघर्ष की जो चेतना लेकर आगे बढ़ी, वह आज भी तमाम मातृभाषाओं में विरल है। यह चेतना जिस समय अवधी में अपनी पुरुजोर ताक़त के साथ दिखाई दी, उस समय हिंदी में छायावाद चल रहा था। अवधी में कितनी प्रगतिशील और क्रांतिकारी कविताएँ लिखी जा रही थीं, यह बात यदि जाननी हो तो 1933 ई. में नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से छपी बलभद्र प्रसाद दीक्षित ‘पढ़ीस’ की किताब ‘चकल्लस’ की कविताएँ और उस में दर्ज निराला जी की भूमिका देखी जा सकती है।
यह प्रगतिशील परंपरा आज भी अनवरत अवधी साहित्य में अपनी नवीन-नवीन प्रासंगिकताओं के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बलभद्र प्रसाद दीक्षित ‘पढ़ीस’, वंशीधर शुक्ल, लक्ष्मण प्रसाद मित्र, गुरुप्रसाद सिंह ‘मृगेश’, चंद्रभूषण त्रिवेदी ‘रमई काका’, त्रिलोचन, माता प्रसाद ‘मितई’, बेकल उत्साही, विश्वनाथ पाठक, पारसनाथ मिश्र ‘भ्रमर’, रफ़ीक़ शादानी, आद्याप्रसाद ‘उन्मत्त’, युक्तिभद्र दीक्षित ‘पुतान’, लवकुश दीक्षित, विद्या विंदु सिंह, सुशील सिद्धार्थ, भारतेंदु मिश्र, रमाशंकर यादव ‘विद्रोही’, प्रदीप शुक्ल, रामशंकर वर्मा, बजरंग बिहारी ‘बजरू’, आशाराम जागरथ, अमरेंद्र अवधिया, संदीप तिवारी, अंकिता यादव और नम्रता मिश्रा तक यह परंपरा आज देखी जा सकती है।
‘पढ़ीस’ और उनके समकालीन काव्य-परंपरा की ख़ासियत यह है कि कविता के लिए आयातित पाश्चात्य साम्यवादी दर्शन की कोरी सैद्धांतिक कलाबाज़ी क़तई नहीं है। ये कवि किसानी और कामगार जीवन जीते हुए कविताई कर रहे थे। इनका भरपूर असर अवधी की आगे की कविता पर ख़ूब देखा जा सकता है। ये कवि सामंतवाद और पूँजीवाद के बीच पिसते हुए—किसान, मज़दूर, दलित और स्त्री की प्रताड़ित ज़िंदगियों को अपनी कविता में गाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हें अपने युग-दर्शन और परिवेश की जैसी समझ है, वह हिंदी में आज भी दुर्लभ है। इसी परंपरा में एक क्रांतिकारी कवि हुए हैं—जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’।
जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ का जन्म 5 अगस्त 1930 में प्रतापगढ़ ज़िले के गोबरी गाँव में हुआ। यह गाँव जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। ‘आज़ाद’ जी के दोनों पुत्र मुस्तफ़ा जाफ़री और मुर्तज़ा जाफ़री आज भी इसी गाँव में कृषक जीवन की कठिन राह पर संघर्षरत हैं। मुर्तज़ा बताते हैं कि ‘आज़ाद’ जी 1950 से 1980 तक राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के साथ समाजवादी राजनीति में ख़ूब सक्रिय रहे।
सोशलिस्ट पार्टी के जनांदोलनों में भाग लेने के कारण वह कई बार जेल भी गए। ‘आज़ाद’ जी प्रतापगढ़ में सोशलिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे। लोहिया जी के बाद वह धीरे-धीरे पार्टी से अलग होते गए, लेकिन उनकी रचनाओं में प्रगतिशील समाजवादी चिंतन अंत तक बना रहा। वह किसान-मज़दूरों के साथ उन्हीं का जीवन जीने वाले सजग रचनाकार थे।
जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ की कविताओं को पढ़कर कोई भी समझदार साहित्यिक यह कह सकता है कि ‘पढ़ीस’ के बाद सबसे सजग वर्ग-चेतना ‘आज़ाद’ की अवधी कविताओं में दिखाई पड़ती है। वह सीमांत किसान थे और खेती ही उनकी जीविका का साधन। किसानी जीवन का संघर्ष झेलते हुए, वह लोहिया के सोशलिस्ट मूवमेंट में सक्रियता से जुड़ते हैं। बाद में आंदोलन से अलग हो जीवन भर खेती और कविता करते हुए, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए, चुपके से इस दुनिया से 29 दिसंबर 2013 को विदा हो जाते हैं।
उनके जीते-जी एक साहित्यिक क्रांतिकारी के रूप में उनकी बहुत उपेक्षा हुई और उनके जाने के बाद उनका विपुल अत्यंत महत्त्वपूर्ण साहित्य आज भी उपेक्षाओं का शिकार है, जिसे दीमक चाट रही हैं। ‘आज़ाद जी’ की अवधी और हिंदी में इक्कीस रचनाएँ प्रकाशित होने की जानकारी मिलती है—आर्य भारत, हमारी सीख, त्याग और बलिदान, उपहार, जीवन-संगम, तूफ़ान, जनता की तलवार, चिंगारी, मालिक और मज़दूर, गागर में सागर, भारत-सुरक्षा, हिमालय बचाओ, क्रांति-संदेश, इंक़लाब, धरती के गीत, अवधी-संगम, नव विहान, केवट, पहरुवा, अधूरा स्वप्न और कथरी। इनमें से अधिकतर कृतियों की अब कोई पता नहीं है। इनमें अंतिम चार रचनाएँ अभी उनके सुपुत्रों के पास हैं।
यह कितना दुखद है कि अवधी के इतने बड़े रचनाकार की आज कोई भी किताब बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। यदि उपलब्ध कृतियों का पुनरुद्धार यथाशीघ्र न हुआ तो आने वाले समय में यह भी साहित्य काल-कवलित हो जाएगा।
आज अवधी ही नहीं और भी तमाम मातृभाषाओं के लेखकों, कवियों का साहित्य विलुप्त होने के कगार पर है। जिस अवधी के जायसी, तुलसी और रहीम पर हिंदी एकेडमिया गुमान करता रहा, उसी भाषा के आधुनिक साहित्य का वहाँ कोई नामलेवा नहीं है। जुमई ख़ाँ के समय से लेकर आज तक उनके अवधी गीतों और कविताओं को अवध ही नहीं, अवध के आस-पास वाला ग़रीब-ग़ुरबा, मज़दूर-किसान गाता आ रहा है। अपने संघर्षशील को ये कविताएँ एक संबल की तरह सहारा देती रही हैं। जिनके जनगीत आज भी प्रगतिशील आंदोलनों में जनता के कंठाहार बने हुए हैं, उस उत्कृष्ट साहित्य और उसके साहित्यकार को आज भी लोग नहीं जानते।
जन संस्कृति मंच के हिरावल दस्ते ने उनका लिखा ‘धोबी गीत’ ख़ूब गाया है, लेकिन वहाँ भी लेखक के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। इस गीत को और दूसरे अत्याधुनिक बैंड समूहों ने भी गाया है, वहाँ तो इस गीत को भोजपुरी गीत तक कह दिया गया, यह भी एक विडंबना है। इस अद्भुत गीत को देश-दुनिया में तरक़्क़ी-पसंद लोगों ने ख़ूब पसंद किया और ख़ूब गाया, लेकिन लोग इसके रचनाकार को बहुत कम या बिल्कुल ही नहीं जानते। गीत है—
बड़ी बड़ी कोठिया सजाया पूँजीपतिया
दुखिया कै रोटिया चोराय चोराय।
अपनी महलिया मा केह्या उजियारवा
तू झोपड़ी मा अगिया लगाय लगाय॥
इस गीत की लय ही नहीं तेवर भी कवि ने धोबी-समाज की श्रम-संस्कृति के लोक-गीतों से लिया है। धोबियहवा लोकगीतों की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि समूह गान में प्रश्नोत्तर पद्धतियों के बड़े चुटीले संवाद उसमें होते हैं। ख़ास श्रम-संस्कृति के गीतों की लय उनकी श्रम-ध्वनियों से निकल कर नृत्य-गीतों में आती रही हैं। ये गीत और नृत्य अपनी संरचना की स्वाभाविकता में इतना एकाकार है कि उनकी प्रस्तुति परंपरागत कलाकारों द्वारा विलग रूप में संभव ही नहीं होती। यह इन लोकगीतों की ताक़त है कि परंपरा और श्रम-संस्कृति से परिचित जन झूम उठता है।
इन श्रम-संस्कृतियों से लय और ओज लेकर जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ ने अपने समकालीन सवालों और चुनौतियों को उठाया है तथा इन सवालों का समाधान भी बड़ी बेबाक़ी से प्रस्तुत किया है। यह ‘धोबी-गीत’ वर्ग-संघर्ष और समाज में व्याप्त असमानता की विसंगति के सवालों को पुरज़ोर तौर पर उठाता ही नहीं, बल्कि एकमात्र लंबी लड़ाई से उसका क्रांतिकारी हल भी प्रस्तुत करता है—
बिना काटे भिटवा गड़हिया न पटिहैं
अपनी खुसी से धन धरती न बटिहैं
जनता कै तलवा तिजोरिया मा लगिहैं
महलिया मा बजना बजाय बजाय
जालसाजी से खड़े हुए पूँजी और वर्चस्व के ऊँचे टीलों को जब तक नहीं काटा जाएगा, शोषित-प्रताड़ित असमानता की खलार गढ़ही नहीं पाटी जा सकती। धरती और धन पर समतापूर्ण बँटवारा वर्चस्वशाली बेईमान वर्ग कभी नहीं मंज़ूर करेगा। इसके लिए शोषित-वर्ग को आज नहीं तो कल विद्रोह करना ही पड़ेगा। जब तक सच्चे श्रमशीलों को उनका हक़ नहीं मिलेगा, यह असमानता की मृत-पूँजी ज़िंदा मेहनत का लहू पीती रहेगी और अन्याय बढ़ता रहेगा।
आज इस दुनिया में जितना भी मनुष्य का बनाया हुआ विकास दिखाई दे रहा है, यह सब का सब मज़दूरों और किसानों ने अपने ख़ून-पसीने से सिरजा है; जिसे धन्ना सेठों ने तिकड़म से हथिया लिया है। यह सब का सब इन्हीं मेहनतकशों का है। आज लोकतंत्र की आड़ में सामंती-पूँजीवाद मज़दूर-किसानों पर क़हर बनकर टूट रहा है। महँगाई बढ़ती जा रही है, अन्याय बढ़ते जा रहे हैं, शोषण बढ़ता जा रहा है। श्रमशील जनता के सरकारी खजाने पर जब तक वह स्वयं ताला नहीं लगाएगी, जनता की गाढ़ी कमाई बेईमान पूँजीपति और वर्चस्वशाली ठेकेदार हड़पते रहेंगे। जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ असमानता के बेईमान तिकड़म से निकलने के लिए मज़दूरों-किसानों-दलितों-स्त्रियों को उन्हीं की भाषा और गीतों में क्रांति के लिए ललकारते हैं।
इसी तरह जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ ने अपनी तमाम कविताओं और गीतों में बिरहा, चहलारी, फागुआ, चइता, चइती, सोहर, सरिया, कहरवा, कोंहरउवा, नउवा झकोर, पचरा, निर्गुण, जोगीरा इत्यादि लयों और उनके स्वभाव को बरकरार रखते हुए बहुत सुंदर और शानदार प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। अवध की वह सांस्कृतिक विरासत जिसे राजनीतिक खल-कामियों ने बल भर बर्बाद किया है, उसे सँजोने का काम करती है ‘आज़ाद’ की कविता।
यह कवि जानता है कि जब तक श्रमशीलों को उनका हक़ नहीं मिलेगा, उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समता के अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक उनकी संस्कृति की कोई रक्षा नहीं कर सकता। वे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समता से ग़रीब-ग़ुरबा, किसान-मज़दूर, स्त्री-दलित को उबारने के लिए ज़ोरदार पक्षधरता उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के गीतों में करते हुए दिखाई देते हैं।
'आज़ाद’ की कविता का एक और पहलू है धार्मिक सद्भाव का। कम्युनिस्ट, धर्म को जहाँ अफ़ीम कह कर सिरे से खारिज़ करते हैं, वहीं जुमई ख़ाँ उसे भारतीयता की ख़ूबसूरती के रूप में सांस्कृतिक रंग देते दिखाई देते हैं। दरअस्ल यूरोप में धार्मिक कट्टरता ने विज्ञान विरोधी तांडव कर जिस तरह मानवता को शर्मसार किया, वैसा भारत में कभी नहीं हुआ था और दूसरा भारतीय दर्शन में जिसे धर्म कहा गया, वह संप्रदाय की वस्तु पहले नहीं था। आधुनिकता के आगमन के साथ सांप्रदायिकता ने यहाँ धर्म को विकृत कर स्वार्थी और पूँजीवाद का सहयोगी बना दिया।
धर्म यहाँ पहले धर्म ही था, हिंदू और सनातन का द्योतक धर्म आधुनिकता की पूँजीवादी साजिश ही है। जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ पूँजीवाद की धार्मिक तिकड़म को ख़ूब समझते थे, इसीलिए वह पूँजीवादी धार्मिक कट्टरता की साज़िशों को तो फटकारते हैं, लेकिन मनुष्यता के लिए हितकारी सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यों की वह अवहेलना नहीं करते। वह गोस्वामी तुलसीदास पर अपनी कविता में लिखते हैं—
जब धर्म की नाव मा पोल भवा
तुलसी तब मोम लगाय गये
खुद खाड़ी पहाड़ी भले अटके
मुल अवधी का चोटी चढ़ाइ गये
धर्म की नाव के पोल को तुलसी समझते थे—‘बेंचहि बेद धरम दुहि लेहीं’। उनके हेतु और प्रयोजन मानवतावादी ही थे। लेकिन उनकी अपनी सीमाएँ थीं, इसलिए जुमई ख़ाँ यह लिखना नहीं चूकते कि वह असमानता की खाड़ी-पहाड़ी याने ‘भीटा और गड़ही’ के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए, कहीं-कहीं अटक गए हैं। लेकिन लोक जन की भाषा जो उनकी भावनाओं की तरह निर्मल है, जिसमें कामना है ‘सुरसरि सम सब कंह हित होई’ को उन्होंने शिखर तक पहुँचाने का जो काम किया है, वह सराहनीय है।
जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ सांप्रदायिक पूँजीवादियों द्वारा धर्म की आड़ में समता का हनन करते देख, उनकी सारी पोल खोलकर रख देते हैं। वह कहते हैं—धर्म ख़तरे में नहीं, तुम्हारी लूट से देश ख़तरे में है। वह कबीर की तरह ही नहीं तुलसी की भाषा में भी फटकारते हैं—
हथवा मा तसबी गटइया मा माला
खोय के इमनवा बटोर्या धन काला
देसवा का गहिरे लुटि केनी खाया
तू काइयौ गुना दमवा बढ़ाय बढ़ाय
आज आवारा पूँजी के उत्तर-औपनिवेशिक दौर में धर्म धंधा बनकर रह गया है। सामंतवाद लोकतंत्र का मुखौटा लगाए ऊँट की चोरी निहुरे-निहुरे कर रहा है, लेकिन जनता की आँखों पर बहुत शातिर कल्पित विश्वासों का आडंबरपूर्ण पर्दा झूल रहा है। उसे तरह-तरह की तुच्छ स्वार्थों में भटका कर सत्ताओं को पूँजीवाद ने अपना उत्पाद बना लिया है। जनता समझती है कि यही ‘शक्तिमान’ है, लेकिन ‘गंगाधर’ पूँजीपतियों का वफ़ादार नौकर से अधिक कुछ भी नहीं। तुलसीदास ने अपने युग में इस माया के मध्यकालिक चरण को कलयुग कहा था। विसंगति और विडंबना इसके लक्षण हैं। ‘तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलि कौतुक तात न जात कही॥’ तुलसी कहीं-कहीं इसकी माया को पकड़ते हैं, लेकिन अधिकतर उनकी बूढ़ी आँखें धोखा दे जाती हैं।
जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’ बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। वह बताते हैं—आज धर्म सिर्फ़ पूँजीवाद के उद्योग-धंधा के अतिरिक्त और कोई आस्तित्व नहीं रखता। यह किसी एक धर्म की बात नहीं दुनिया भर के धर्मों की सच्चाई है। वह कहते हैं—हाथ में तस्बीह लिए मौलाना हों या गले में रुद्राक्ष ढोते पंडित हो, इनका ईमान से कोई लेना-देना नहीं। ये भोली-भाली और मूर्ख जनता को भ्रमित कर उन्हें ठगते हैं, क्योंकि पूँजी के प्राथमिक स्रोत वही हैं। इन्हीं के श्रम पर दुनिया भर के ठग मज़ा चाभ रहे हैं और ये ग़रीबी और जहालत में जूझ रहे हैं।
आज ईश्वरवादी मठाधीश ईश्वर को मरभुक्खों में बाँटते हैं, और बदले में किसान-मज़दूरों की गाढ़ी कमाई ऐंठ कर अरबों-खरबों की मल्टीनेश्नल कंपनियों के मालिक बने बैठे हैं। ‘आज़ाद’ कहते हैं, देश पूँजीपतियों से नहीं, किसान-मज़दूरों से बना जिनकी गाढ़ी कमाई नोच खाने वाले कमीने कुत्तों ने देश और राष्ट्र दोनों को रसातल में पहुँचा दिया है। आज की स्थिति यह है कि इन जल्लादों से जो बचता है, उस पर इनके मुलाज़िम हुकूमत की राष्ट्रवादी चटक चुनरी ओढ़ जीएसटी और एफ़डीआई जैसी अनंत मेखें ठोंक कर वसूल कर लेते हैं। ‘आज़ाद’ अपने ईमान से इन्हें लानत भेजते हैं और जनता को जगाने का काम अपनी कविता से करते हैं।
जुमई ख़ाँ अपने वतन की अवाम को उन्हीं की मादरी ज़बान में यक़ीनन कलाम में यह बताते हैं कि आज़ादी से क़ीमती मानव समाज में कोई मूल्य नहीं है। इसके लिए हमारे बाप-दादों ने लठियाँ खाईं हैं, जेलें काटी हैं, गोलियाँ खाईं हैं, फाँसी के फँदे चूमें हैं कि हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद रह सकें। दुनिया के महान् दार्शनिकों ने जीवन और इतिहास के अनुभवों से यह माना कि ग़ुलामी मृत्यु से भी भयावह है।
अहिंसा के प्रबल पक्षधर, जिन्हें नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने ‘राष्ट्रपिता’ कहा था, महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि यदि आपको ग़ुलामी और हिंसा में से कोई एक रास्ता चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, तो महात्मा कहते हैं—तब मैं हिंसा को चुनना पसंद करूँगा। चौदह साल की बाली उम्र में आज़ादी के लिए क़ुर्बानी देने वाले खुदीराम बोस हों, या अस्सी साल की बूढ़ी हड्डियों से ग़ुलामी की ज़ंजीरे तोड़ते हुए शहादत देने वाले वीर कुँवर सिंह, उनके सरीखे हज़ारों बलिदानियों ने आज़ादी के लिए जान की बाज़ी लगाते हुए, क्या कभी सोचा होगा कि हम जिनके लिए अपनी जान दे रहे हैं वे आज़ादी के मूल्य इतनी जल्दी भूल, ग़ुलामी-पसंद हो जाएँगे! आज़ाद बहुत भारी मन से कहते हैं—
कवन बाजा बजत बाटै
कवन सुरताल रगिया मा
लगावा दाग जिन यारौं
अरे पुरीखन की पगिया मा
सुना आवाज आवति बा
सहीदन की मजारन से
बड़ी मुसकिल से आवा बा
ई मौसम आजु बगियन मा
‘सा विद्या या विमुक्तये’ के सूक्त वाक्य देने वाला दर्शन आज अपने पथ पर लड़खड़ाता जा रहा है। सत्ताएँ आज अपने मद में अंधी हो, ग़रीबी और अमीरी की खाई चौड़ी करती जा रही हैं। ग़रीब को और भी ग़रीब, और अमीर को और भी अमीर बनाने वाली विद्याएँ सरकारों के डिप्लोमेट रटकर चाटुकारिता में विद्वता के घंट बजा रहे हैं।
अराजकता चहुँ ओर कुलाँचे भरती हुई विकास के विनाश रथ पर देवासुर संग्राम लड़ रही है। जिन्होंने इस देश को कठिनतम श्रम के संघर्ष के बूते अन्न दिया, धन दिया, जीवन दिया उसी को अपमानित किया जा रहा है। जिन्होंने सड़कें बनाई, कारख़ाने चलाएँ, महल बनाएँ, क़िले खड़े किए और वह जो नंगी आँखों से मनुष्य का बनाया हुआ आप देख रहे हैं, सब कुछ मज़दूरों ने बनाया है, उसे नई क़ाबिलियत से प्रताड़ित किया जा रहा है, लूटा जा रहा। बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं।
क्या इन किसान-मज़दूरों के पुरखे इसी दिन के लिए आज़ादी की लड़ाई में शहादत दे रहे थे। क्या इनके बिना कोई माई का लाल आज़ादी की लड़ाई की कल्पना कर सकता था। सत्तावादी चाटुकार जल्लादो! यह देश तुम्हारा नहीं, देश से प्रेम करने वाले किसानों-मज़दूरों का है।
इस देश को किसने बनाया है और कौन इसे प्यार करता है, जुमई ख़ाँ ‘आजाद’ अपने समय का श्रेष्ठतम रूपक देते हुए एक महान कविता में प्रस्तुत करते हैं। और यह बात मैं पूरे होशो-हवास के साथ कह रहा हूँ कि मानस के बाद अवधी में ‘कथरी’ जैसी महान् रूपक-रचना कोई दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा महान रूपक है कथरी—
‘जेस फुलवइ कुरबानी कयिके आपनि देहियाँ नथवाय देयँ
दूसरी की गटई की खातिर आपनि गटई लटकाय देयँ
वइसे तू हमरे बरे फुरइ सुइया डोरवा से प्यार किहू
मन मरा नहीं तन छेदि उठा खुब दीनन कै उपकार किहू
बस यही से महिमा बढ़त अहै कथरी तोहर यहि नगरी मा
कथरी तोहर गुन ऊ जानै जे करै गुजारा कथरी मा’
अवधी में कथरी, भोजपुरी में लेवा, खोरठा में गेंदरा जिसे कहते हैं, यह सिर्फ़ एक वस्तु नहीं हमारी अस्मिता का सबसे दिग्विजयी मूल्य है यह। ‘आज़ाद’ कहते हैं—यह बाज़ारों में ख़रीदी नहीं जा सकती, यह अनमोल है; लेकिन इसने स्वाधीनता के स्वाभिमानी इंसानी-सिंह-शावकों को बड़े दुलार से पाला है। कवि भारतीय अस्मिता के उस वर्ग-संघर्ष को खाँड़े की धार पर अलगाते हुए कहता है कि हम उस तरफ़ वाले हैं, जिन्हें यह ‘गर्वीली-ग़रीब’ गोद का स्वाभिमान मिला, हमें इसी कथरी की ममता ने पाल-पोसकर बड़ा किया। हम इसी कथरी के लाल हैं, जिसने कभी गांधी और गौतम सरीखे हमारे पुरखों को पाला-पोसा-सिरजा।
कथरी का कवि कहता है—आज़ादी की अस्मिता को ज़िंदा रखने के लिए बलिदान भावना का पौरुष इसकी संरचना से ही हमें मिला महान् पुरुषार्थ है। जैसे फूल एक माला बनने के लिए अपनी देह नाथवा देता है, वैसे ही घर के फटे-पुराने लगभग चिथड़े बन चुके कपड़े नेह का बिछावन बनने के लिए सुई डोरा से प्रेम करते हुए अपनी देह छेदवाते-नधवते यह बलिदानी नाम पाते हैं—कथरी।
‘आज़ाद’ कहते हैं, आजादी के लिए क़ुर्बानी की भावना तो हमारी मातृक प्रेरणा है। इसीलिए कथरी के सपूतों ने अपनी गर्वीली-ग़रीब भावनाओं पर मर मिटने से कभी गुरेज़ नहीं किया। आज़ादी की लड़ाई में फूल जैसे इन्हीं वीरों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं, मुहब्बत की ऐसी मिसालें क़ायम की हैं कि जिनकी गौरव गाथाएँ सुन दिग्गजों के उन्नत शीश सदैव झुकते रहेंगे।
यह आज़ादी जिनके गर्वीले-ग़रीब स्वाभिमान से हासिल हुई, आज उसी बेशक़ीमती थाती में पूँजीवादी अजगर पैदा हो गए हैं। ये इस देश के असली हक़दारों का हिस्सा हड़पकर हमारी अस्मिता पर ख़तरा बन गए हैं। ‘आज़ाद’ कहते हैं—यह अन्याय देश की जनता लंबे समय तक नहीं सह सकती। कभी न कभी इस असमानता और शोषण के ख़िलाफ़ देश के असली दावेदार ज़रूर खड़े होंगे। जब तक धरती और धन सामाजिक न्याय से नहीं बँटेगा आज़ादी की लड़ाई अधूरी रहेगी।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
