क्या आप भी रील-रोग से ग्रस्त हैं?
 अतुल तिवारी
07 अक्तूबर 2025
अतुल तिवारी
07 अक्तूबर 2025
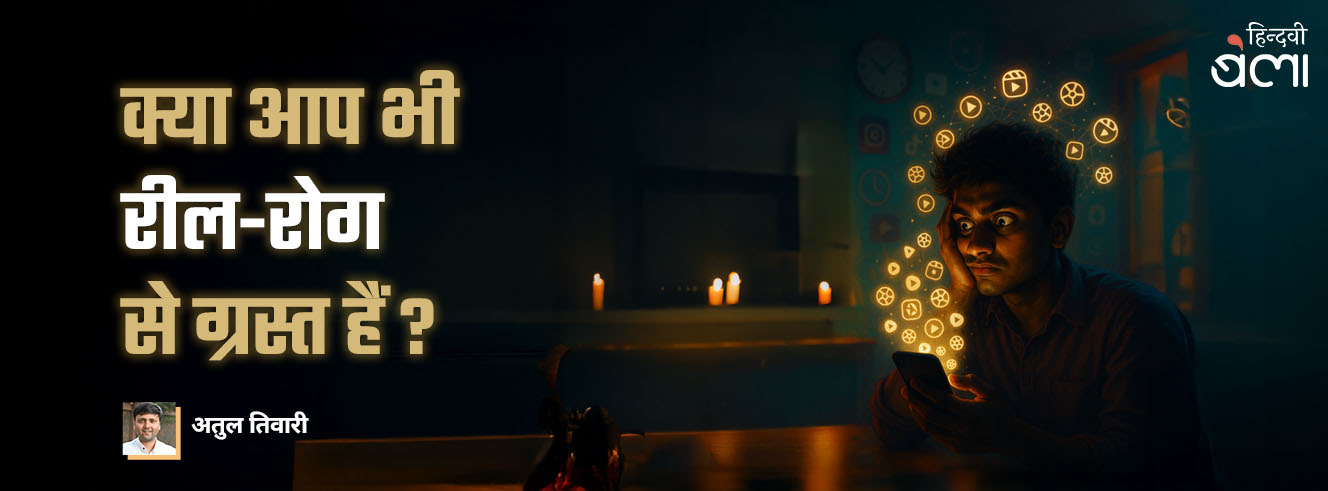
रील-रोग से ग्रस्त और कुछ-कुछ कुपित एक रीलर-इन्फ़्लुएंसरों मित्र ने बेहद ऊबकर मुझसे पिछले दिनों कोई किताब पढ़ने की जिज्ञासा व्यक्त की। उन्हें शुरुआत करने में मुश्किल आ रही थी। मित्र पूरब के निवासी हैं, तो मैंने प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ने की सलाह दी। इस सलाह पर वह थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। एक पॉज़ के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम खोला, चार रील सरकाई और सिर खुजाने लगे। इसके बाद उन्होंने एक सिगरेट जलाई और धुएँ की एक लकीर खींचते हुए बोले, ‘‘देखो! प्रेमचंद तो मुंशी था। मुंशियों का काम ही लिखना-पढ़ना होता है। ...और स्साला प्रेम तो हमने किया। एक नहीं, तीन-तीन बार। घनघोर प्रेम। तो प्रेमचंद तो हम हुए न बे! हम क्यों प्रेमचंद को पढ़ें?’’ उन्हें पाँच सेकेंड में हल जोतता किसान और तीन सेकेंड में ज़ुल्म करता ज़मींदार चाहिए था।
उन्होंने आगे कहा कि मुझे आँचल से आँसू पोंछने वाली प्रेमचंद की नायिका के बारे में नहीं जानना। मज़ा तो तब है, जब आँसू गिरने से पहले ही वह कैमरे की ओर देखे और एक ट्रेंडिंग गीत बज उठे। इससे पहले कि वह ‘सेवासदन’ को सेल्फ़ी-सदन और ‘गोदान’ को गरम गोदाम से काटते मैंने रुख़्सती की इजाज़त माँग ली।
जगजीत सिंह गाए जा रहे थे और ग़ुलाम अली गुनगुनाए। ज्ञानेंद्रपति की ट्राम, आलोकधन्वा की भारतीय रेलें और गुलज़ार का सारा दिन सड़कों पे ख़ाली रिक्शे-सा चलने वाला लड़का और किशोर कुमार की दिल ही दिल में जलने, बिगड़ी-बिगड़ी-सी चलने वाली भीगी-भागी लड़की से लेकर अस्मितामूलक और अश्लीलतामूलक प्रसंग के असंख्य दृश्य और बातें मैं इंस्टाग्राम पर उँगलियों के सहारे सोख रहा था... कि मुझे अचानक एक चप्पल दिखी। चप्पल रिलैक्सो की थी। लिखा हुआ था कानपुर में बनी है। गीतों की लयात्मकता त्याग कर मैं अचानक चप्पल की स्मृतियों में चला गया जो कई बार बरसात में फिसली, कीचड़ में धँसी, एक बार मोहब्बत में भागते लड़की के साथ टूटी और अंत में कबाड़ी की बोरी में समा गई। चप्पल ने जितना जीवन देखा, उतना उसके मालिक ने भी नहीं देखा था। उसी चप्पल को पहनकर 2020 की उस गर्मी में जब मैं तीसरी बार इस्तीफ़ा देकर पाँचवीं बार नौकरी शुरू कर चुका था, तब मुझे याद आया था कि एक बार 2019 में मैंने यही सब नहीं करने का निश्चय किया था। यह भी याद आया कि उसी साल मैंने उससे विदा ली थी। विदा से पहले हम गले लगे थे। उससे पहले झगड़ा हुआ था। उससे पहले हँसी आई थी। उससे पहले चाय गिरी थी। उससे पहले वह आई थी। उससे पहले मैं इंतिज़ार कर रहा था।
लेकिन रील किसी ‘केवल’ तक सीमित कहाँ रहती है! अगली रील में अटल जी बोल रहे थे उसके अगली में गोविंदा लाल शर्ट के साथ नीली पैंट के साथ पीली बेल्ट और सफ़ेद मोज़े के साथ भूरे जूते के साथ पसीने की बूँदों से चमकते हास्य और थकान के साथ अद्भुत नृत्य लिए अजीब भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत हुए। रील में और क्या-क्या था? कभी एक लड़की रोते हुए बता रही होती कि उसे आज भी 2007 की वही पेंसिल याद है। आम, लीची, जामुन और ट्रैफ़िक, सिर-दर्द जैसे सबसे सस्ते बहाने और बचपन की चोरी, पहली मोहब्बत जैसे सबसे गहरे और सघन रहस्य से दिमाग़ आनंद-शोक-रूमानियत से गड्डमड्ड हो ही रहा था कि मैं चौंका!
मैने देखा कि एक मीडिया आलोचक/लेखक/प्रोफ़ेसर भी आज रीलर हो गए। यह मीडिया आलोचक/लेखक/प्रोफ़ेसर बीते बीस सालों से चाय-ब्रेड-पकौड़ा-धनिया-पुदीना-कटहल-कोआ पर लिख रहे थे। मुझे समझ आया कि बीते बीस सालों से उनकी क़लम आख़िर क्यों मटमैली पड़ी थी। उनके विवेक और लेखन का विकास इसलिए नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम की रील-रोशनी अस्तित्व में नहीं थी। अगली रील में वह शिकायत कर रहे थे कि चौलाई के साग की अगर कहीं रील बनी हो तो बता दीजिए! जो बीस साल में नहीं हुआ, वह बीस सेकेंड में हो गया। चौलाई का साग अगर वायरल हो सकता है तो मीडिया-आलोचना और किचन-सांगोपांग की पूरी परंपरा भी—इस पर उन्हें भरोसा हो चला था। अगली सारी रीलों में शायद वह सारी उपलब्ध अश्लीलताओं को आम-पना (गर्मियों में) और जाड़े में फूल गोभी और निमोना से काटना चाह रहे थे।
ये दुर्लभताएँ कैसे संभव होतीं, अगर रील की विधा न होती। क्या होता उस जिम-ट्रेनर का जो अपने बाइसेप्स को ऐसे मरोड़ रहा था, जैसे धर्मग्रंथ की कोई नई व्याख्या दे रहा हो। उस दार्शनिक का क्या होता जो सड़क किनारे गुटखा थूक कर कहता कि ज़िंदगी ऐसे ही चलती है भाई! बिना रील के तो वह बस-अड्डे का आवारा होता। साबुन से बुलबुले बनाकर कैमरे की तरफ़ उड़ाने वाला बिना रील के बस गली का गंदा नाक बहाता लड़का होता। “रात अकेली है, बिस्तर ख़ाली है” गाकर अपनी जीभ निकालने वाली लड़की का क्या होता? रील नहीं होती तो वह दो कौड़ी का कवि भी किसी शराबख़ाने का फूहड़ शाइर होता। “DM me for fun” लिखने वाला लड़का बिना रील के पान की गुमटी के पास खड़ा अधपका आशिक़ होता!
रील एक नया सार्वभौमिक सत्य है। यह केवल एक तकनीकी सुविधा नहीं; न ही केवल एक मनोरंजन का माध्यम; यह अब जीवन का एक औद्योगिक उपकरण बन चुका है—जिस पर श्रम, भूख, आत्मसम्मान और मोहब्बत सब ही किसी न किसी रूप में इसके चाक पर घूमते हैं। रील ने रोटी दी तो रोटी छीन भी ली। उसने कुछ को मंच दिया, पर कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ भी निगल लीं। जो रील नहीं बना रहे, वे अब इसके उपभोक्ता भर बनकर रह गए हैं। रोज़गार, उल्लास, दुख, पहचान... सब कुछ रील में परोसा जा रहा है—हँसते-हँसते निगलने के लिए। यह शहरी-ग्रामीण, विशिष्ट-अविशिष्ट, प्रतिष्ठित-अनापेक्षित—हर विभाज्य का समेकन है। कड़कड़डूमा के कोर्टरूम से लेकर अशोक नगर के उपांत की चौखट तक, कच्छ के नमक-सी सुंदरता से लेकर नेपाल के संसद-सम्मुख—हर जगह अब रील-अभिव्यक्ति हो रही है। न्याय के भ्रष्टावशेष, गाँव-रसोई की दुल्हन, मरुभूमि का तहसीलदार किरोड़ी, संसद की गंभीरता—सब कुछ रील के तेज़ लेंस के भीतर समाकर, एक मिनट के भीतर आत्म-निर्वाचन का शिकार हो जाता है।
सब लोग सब कुछ बेच रहे हैं। अस्मिता, अनुभूति, अनुभव, अज्ञान, अपसंस्कृति, अफ़वाह। ...इस सदी का अपवाद भी रील-उत्पाद बन चुका है। विचारों की तेज़ कटिंग, भावना की त्वरित पिटाई और हास्य की तत्कालिक पॉलिश। जो कभी रातों को टेबल-लाइट के नीचे टाइप करते थे, अब उसी रात को रील-फ़्रेम के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं। लोग तीर्थ-स्थल से रील बनाकर लौट रहे हैं। तीर्थ-स्थल का मौन रील की चकाचौंध में विलुप्त हो रहा है। कहीं न कहीं यह रीलरों के राहत का आवरण है, जिसमें छिपकर वे अपनी बेचैनी भुला लेना चाहते हैं। भाषा का शोषण, भाव का विक्रय और स्मृति का विकृतिपूर्ण व्यापार रील के बाज़ार में विनिमय-योग्य वस्तु बनकर रह गया है। एक अजीब तरह की तिरछी कला भी उभरी। ख़राब कवियों-लेखकों का उदय, वांछित कवियों का विकृत प्रतिरूप और अवांछित पेशों का अभिनव रूपांतरण। इस स्थिति में हर पल एक नया कंटेंट जेनरेट होता है। रील ने लोक-कला को ग्लिच कर दिया, लेकिन उस ग्लिच में भी कुछ सच्चाइयाँ चमकती हैं। एक अनौपचारिकता, एक सपाटता जो अस्सी साल की मुर्दा अलमारी खोलकर कुछ अनसुने गीतों को कभी-कभी बाहर कर देती है।
क्या रील-युग साहित्य का अंत है? क्या शब्दों का आलिंगन अब केवल एक फ़िल्टर में संपन्न होगा? क्या रील-उत्पाद का यह युग हमारी आत्म-परिचय की धरोहर पर हमला कर रहा है? क्या यही आधुनिक रचना का उद्धार है—मैं नहीं जानता। पर इतना जानता हूँ कि यह अजीब है—यह चरित्र और यह समय बदला हुआ है। ज़ाहिर है कि लोग कहेंगे, ‘‘रील ने हमें कुछ दिया भी है।’’ किसी अनजान गाँव की लड़की का नाटक अचानक राष्ट्रीय भावनाओं का विषय बन जाता है। सड़क के कोने का संगीत रातों-रात लोकप्रिय हो जाता है और छोटे-छोटे सत्य बड़े दर्शकों तक पहुँचते हैं। यही उसके गणित का उजला पक्ष है—वहाँ बेतहाशा समानता की संभावना है, जहाँ प्रसिद्धि का द्वार हर किसी के लिए खुला दिखता है। पर इस उजले पक्ष का मूल्य क्या है? जब क़ीमत आपकी सततता और आपकी अंतर्लयता हो? ...और फिर वह सवाल जो विवशता की सीधी परछाईं है—क्या अंततः सबको रीलर ही बनना पड़ेगा? क्या हर कवि, हर अध्यापक, हर न्यायाधीश, हर काँवड़िया और हर आम आदमी को आज के इस रील-राष्ट्रीयकरण में अपना हिस्सा देना होगा? या क्या रील एक अतिव्यापी मौसम मात्र है—तेज़, हिंसक और बाद में ग़ायब हो जाने को अभिशप्त? मैं नहीं जानता कि भविष्य क्या तय करेगा पर मुझे वह घोर कल्पना सताती है जिसमें समाज का हर सांस्कृतिक प्रावधान एक छोटे फ़्रेम में समेटा जा रहा है और हमारी बड़ी कथाएँ, हमारे उपन्यास, हमारी लंबी कविताएँ, हमारी धीमी बहसें—कहीं पीछे छूटकर कुल मिलाकर अनसुनी हो रही हैं।
रील ने हमें संभावना दी है, पर वह संभावना भी शर्तों के साथ है। शर्तें—जिनमें गति, चमक और समझौता अनिवार्य है। यदि ये शर्तें बढ़ती रहीं तो हाँ! शायद एक दिन सबको रीलर बनना पड़ेगा। पर मनुष्य की क्षमता अजीब है, वह नई तक़नीक़ को अपनाता भी है और उसके विरुद्ध एक महीन-सी रक्षा-रेखा भी खींच लेता है। अंतः धीमी कविता, दीर्घकाय कहानी, सारगर्भित नाटक—ये सब किसी न किसी रूप में ज़िंदा रहेंगे। पर क्या उस ज़िंदा रहने के लिए हमारी अनुभूतियाँ रील के फ़्रेम में अपना रंग बदल देंगी? यह अभी तय नहीं है; पर यह तय है कि हम आज एक ऐसे युग के बीच खड़े हैं, जिसने हमारी गंभीरताओं और सार्वजनिकताओं और गोपनीयताओं को छोटी- छोटी क्लिप्स में बाँटना शुरू कर दिया है।
...और यहीं यह सवाल कटुता के साथ फिर उभरता है कि क्या हम, अंततः, अपने आपको इन मिनटों के भीतर समेट लेने के लिए विवश कर लेंगे? या फिर कहीं कोई नया रूप, कोई नया धीमा और गहरा प्रतिरोध; इस रील-युग के भीतर जन्म लेगा? मेरे मित्र किताब पढ़ना चाहते थे, लेकिन किताब में किसान धीरे-धीरे हल जोतता है। ज़मींदार धीरे-धीरे खलिहान लूटता है। धीमी साँस और जीवन का लंबा वाक्य उनके धैर्य के बाहर हो चुका था।
अतिशयोक्ति में कहा जाए तो हर मोबाइल-यूजर की दुनिया अब जन्म-मृत्यु और शोक के रीलकरण से संचालित होगी। राजनीति में रील-रणनीतिकरण का नवाचार होगा। धर्म और तीर्थ के नए रील-आयाम तलाशे जाएँगे, बचपन का अपहरण करने से शुरू होकर पारिवारिक रिश्तों के रील-संस्करण प्रस्तुत होंगे और बुज़ुर्गों के रील-उपसंहार को प्राप्त हो जाएँगे। अंत में मुझे प्रेमचंद की नहीं कही एक बात याद आ रही है, ‘‘देखना एक दिन सब कुछ अपलोड हो जाएगा...’’
•••
अतुल तिवारी को और पढ़िए : पिन-कैप्चा-कोड की दुनिया में पिता के दस्तख़त | प्रेम जब अपराध नहीं, सौंदर्य की तरह देखा जाएगा | बीएड वाली लड़कियाँ
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
