भारतेंदु मिश्र : तरफराति पिंजरा है काठ कै चिरइया
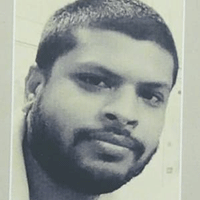 शैलेंद्र कुमार शुक्ल
28 अक्तूबर 2025
शैलेंद्र कुमार शुक्ल
28 अक्तूबर 2025

कितना दारुण है यह लिखना—स्वर्गीय भारतेंदु मिश्र। मैं उन्हें दद्दा कहता रहा हूँ। अब दद्दा स्मृतियों में रहेंगे, उनकी आत्मीयताओं का बतरस कानों में बजता रहेगा, उनकी कविताओं की पंक्तियाँ वजह-बे-वजह मस्तिष्क के अवचेतन से निकल एकाएक चमक उठा करेंगी, नेह से गदगद उनके चेहरे पर आशीष की उज्जवल आभा स्मृति में अक्सर उभरती रहेगी। उनका यह कहना कि “परेशान न हो भैया, हम हन ना!” और आज दद्दा नहीं हैं। आज जब वह नहीं हैं, फिर भी उनका न होना बचा है! यह न होना संपूर्ण अमरता के साथ जीवित रहेगा। मुझे इस वक़्त इसी माटी के कवि केशव तिवारी की कविता ‘जाते हुए’ की कुछ पंक्तियाँ बड़ी अधीरता से याद आ रही हैं—
हमारा जिया
औरों के लिए
छूट जाएगा
मन यह नहीं मानता
पर कुछ चीज़ें
अपनी छायाओं के साथ लौटती हैं
कुछ क़रीब-क़रीब की ध्वनियों के साथ
कोई न पूरा का पूरा जाता है
और न पूरा का पूरा लौटता है
दद्दा इसी अवध और अवधी में रहेंगे, जैसे अवध और अवधी रहेंगे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान इसी धरती पर। सब कुछ का रहना तय है, जैसे सब कुछ के न रहने तक।
अवधी साहित्य में भारतेंदु मिश्र के योग को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह चिर स्मरणीय रहेंगे। वही सन् 2014-15 की बात रही होगी, जब मैं वर्धा स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग से ‘अवधी कविता : स्वभाव और प्रवृत्तियाँ’ (1850-2010) विषय पर शोध कर रहा था। भारतेंदु दद्दा से बातें होती रहती थीं। उनके सुझाव और सहयोग मुझे मिलते रहते थे। मुझे अपने शोध के निमित्त बहुत शोध सामाग्री जुटानी थी और मैं दर-दर भटक रहा था। मैंने पुस्तकालयों से लेकर दिवंगत हो चुके अवधी साहित्यकारों के द्वार की धूल ले डाली थी। ख़ैर, जैसे-तैसे सामाग्री जुटाई। लेकिन यह कह सकता हूँ कि इस उपक्रम में जो परेशानियाँ झेलनी पढ़ीं उसकी कहानियाँ लिखूँ तो दूसरा प्रबंध बन जाए। तमाम परेशानियों के बीच जब-जब दद्दा से बात होती वह कहते “परेसान न हो भइया, प्रयास किहे रहौ, धीरे-धीरे सामाग्री जुटि जाई। हिम्मति न हारौ।” दद्दा के पास बची अवधी कविता की किताब ‘कस परजवटि बिसारी’ (2000) की अंतिम दो प्रतियों में से एक उन्होंने मेरे लिए भेज दी थी। शोध के दौरान मुझे इस बात का बहुत ज़रूरी अनुभव हुआ कि शोध का काम पूरा करने के बाद एक अवधी की पत्रिका निकालूँगा, जिसके माध्यम से उपलब्ध अवधी साहित्य का संरक्षण करने का काम करूँगा। मैं तब से भारतेंदु दद्दा से पत्रिका निकालने की योजनाएँ बनाया करता था। लेकिन तब ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि ‘खरखइंचा’ का पहला अंक भारतेंदु मिश्र अंक के रूप में निकालना पड़ेगा। ख़ैर, तमाम जीवन संघर्षों और नौकरी के झंझटों के बीच यह टलता गया। फिर इधर दो-ढाई साल पहले एक वज्रपात-सी दारुण ख़बर सुन मैं अवाक् रह गया कि भारतेंदु दद्दा एक असाध्य बीमारी के शिकार हो गए हैं। मेरा मन विकल हो उठा, दद्दा ने बताया “भइया अब हमरे पास ज़्यादा समय नाय है।” मुझसे कुछ कहते नहीं बना। कुछ समय तक अवसाद की पीड़ा से परेशान रहा, फिर सोचा अब इस दुख से उबरने का एक ही तरीक़ा है कि कुछ काम कर डालूँ कि दुख विरेचित हो सके। मैंने ‘खरखइंचा’ के भारतेंदु मिश्र अंक के लिए एक इश्तिहार तैयार किया और साहित्यिक सहृदयों को पत्रिका में लिखने लिए आमंत्रित करने लगा। एक साल लग गया पत्रिका के लिए सामाग्री जुटाने और कठिन संपादकीय कर्म करने में। दद्दा को जब पहली बार बताया था कि आप के अवधी साहित्य पर केंद्रित ‘खरखइंचा’ का पहला अंक निकालने की योजना बना ली है तो वह बहुत सकुचाये फिर उन्होंने कहा “भइया अइस न होय हमरौ मजाक उड़ै औ तुमहूँ सरमिंदा होएउ।” फिर जैसे-जैसे लेख और संस्मरण आने लगे, मैं दद्दा को पढ़ने के लिए भेज देता, दद्दा पढ़ते और उनका मन एक तोष के आनंद से भर जाता। वह अपनी प्रशंसा पर अक्सर मौन हो जाते और मुझे उनकी एक अवधी ग़ज़ल की याद आ जाती जिसे मैंने पत्रिका के आवरण पश्चय-पृष्ठ पर जंतर की तरह बाँध दिया है—
केतने दिन बादि राह लिन्हे हौ
खैरियत है कि चाह लिन्हे हौ
टूट रिस्ता जुड़ा मुहब्बति का
यार, की ते सलाह लिन्हे हौ
पत्रिका जब छपने के लिए प्रकाशक के पास जा चुकी थी और प्रूफ़ रीडिंग का काम चल रहा था। मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाने का एक आकर्षण यह भी था कि भारतेंदु दद्दा से मुलाक़ात हो जाएगी। मैं अपना काम निपटाकर ख़ाली हुआ था तो दद्दा को फोन किया, उधर से आवाज़ आई “मिश्रा जी अभी आईसीयू में हैं, बात नहीं हो पाएगी।” और फ़ोन कट गया। मुझे लगा कि मोबाइल फ़ोन अस्पताल के किसी कर्मचारी के पास था। मैं दिल्ली गया और दद्दा से मिलने का संयोग न बन सका और मैं दूसरे दिन दिल्ली से लौट आया। उनकी हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती गई। बाद में दद्दा ने बताया कि बीच-बीच में ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल जाना होता है और फ़ोन बिटिया के पास था। आज जब वह नहीं हैं तो बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लखनऊ के कार्यक्रम में हुई दद्दा से पहली मुलाक़ात ही आख़िरी मुलाक़ात बन कर रह गई।
दिल्ली से लौटने के बाद रात-रात जग कर दो बार और प्रूफ़ रीडिंग हुई और कुछ ही दिन बाद सर्व भाषा ट्रस्ट प्रकाशन से पत्रिका छप कर आ गई। मैंने अपनी तरफ़ से ख़ूब कोशिश की थी कि अंक जितनी जल्दी आ सके। अंक आया भी लेकिन तब तक दद्दा की आवाज़ जा चुकी थी, नली के माध्यम से रस और पानी पर वह जी रहे थे। उनका आख़िरी मैसेज 23 सितंबर 2025 का है—“आज से केवल जूस और पानी पर रहना है। अब हालात ठीक नहीं है। बाक़ी तुम जनतै हौ। आज पत्रिका आ गई। बहुत सुंदर लग रही है। आपको हार्दिक आभार, धन्यवाद, आशीर्वाद।” इसके बाद 5 नवंबर 1959 ई. में जन्में भारतेंदु दद्दा 10 अक्तूबर 2025 को दिवंगत हो गए। उनसे मैंने अवधी आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, जिसे वह कुछ वर्षों से लिख रहे थे—जिसका कुछ हिस्सा ‘खरखइंचा’ के भारतेंदु मिश्र अंक में प्रकाशित हुआ है। अपने अंतिम दिनों में इसे पूर्ण कर मुझे दे गए हैं दद्दा, यह किताब जल्दी ही प्रकाशित होगी। उनकी आत्मकथा इतनी रोचक और महत्त्वपूर्ण है कि मैं तो इसे पढ़कर आश्चर्यचकित हूँ।
कभी अवधी साहित्य में उनके योग पर मैंने ख़ूब सोच-समझ कर उन्हें समकालीन अवधी का अगुआ कहा था। उन्होंने अवधी गद्य में वही प्रतिबद्ध काम किया है जो पढ़ीस ने कभी अवधी कविता में किया था। वह सच्चे अर्थों में अवधी गद्य के पढ़ीस हैं। हालाँकि यह कहकर उनके अवधी काव्य का महत्व कम नहीं कर रहा हूँ। उनकी कविताएँ और गीत अवधी की लोक चेतना से संस्कृति को परिमार्जित करने का काम करते हैं। उनके इसी पक्ष पर पूर्व में गई बातें आज फिर प्रासंगिक लग रही हैं।
भारतेंदु मिश्र ने जब अवधी कविता के धराधाम में चरण धरे तो पढ़ीस, वंशीधर शुक्ल और चंद्रभूषण त्रिवेदी की काव्यगूँज अपनी गंभीर झंकार की छाप छोड़ चुकी थी तथा मृगेश, विश्वनाथ पाठक तथा जुमईं खाँ भी अपनी चमक के साथ बहुत कुछ मार्ग प्रशस्त कर चुके थे। अवधी कविता ने अपने पुरखों से मिले सांस्कृतिक मूल्यों को प्रासंगिकता की कसौटी पर कसते हुए टुच्चे स्वार्थों को ठोकर मारकर समरसता के साम्य धर्मी रक्षार्थ त्याग और बलिदान के तप को गले लगाया। इससे एक स्वाभाविक स्वाभिमान पैदा हुआ, जिसने अज्ञानी अहंकार को पास फटकने तक न दिया। सन् नब्बे के दशक में अवधी कविता में एक नई पीढ़ी सामने आती है जिनके कवि और उनकी कविता को देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह अमर वाक्य याद आता है—“ज्यों-ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए-नए आवरण चढ़ते जाएँगे त्यों-त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा।” अवधी कविता के लिए भी नब्बे का दौर कम कठिन नहीं रहा। नवउदारवाद के टुटहे दरवाज़े से एक घनघोर बाज़ार की शुरुआत हुई, यह पहले के बाज़ार से विलक्षण था, जिसके लक्षण सहजता से लोग नहीं पहचान सके। उत्तर-आधुनिकता और उत्तर-सत्य की सैद्धांतिकी से बिल्कुल अपरिचित होते हुए भी इसकी तमाम प्रवृत्तियाँ समाज में घर करती गईं। कविता के प्रयोजन और हेतु बड़ी शातिर चालाक़ी से बदल गए। नए कवि आए और उनकी नई कविता। इस पीढ़ी में कुछ सच्चे कवि थे जिनकी सोहबत का इस्तेमाल कर नक़ली जालसाज़ भी कवि बन निकले। ये कवि नहीं बल्कि डॉ. बच्चन सिंह की शब्दावली में कहूँ तो कविता के सौदागर थे। अवधी के सच्चे कवियों में भारतेंदु मिश्र और सुशील सिद्धार्थ के नाम याद आते हैं और सौदागर कवियों के नेता रामबहादुर मिश्र एवं जगदीश पीयूष सरीखे लोग रहे। व्यावहारिक जीवन में मित्रवत लेकिन प्रयोजन के स्तर पर भारी भिन्नताएँ रहीं, जिनकी मिसाल हैं उनकी कविताएँ।
भारतेंदु मिश्र संस्कृत साहित्य के गंभीर अध्येता हैं। उन्होंने लोक की ताक़त से शास्त्र का अर्जन किया और शास्त्र के वैश्विक मानवीय ज्ञान को लोक व्यवहार के धरातल पर साहित्य के माध्यम से उतारने का काम किया। वह साहित्य से लोक परमार्थ की डगर पर निर्द्वंद्व बढ़ते रहे। सच्चे अर्थों में भारतेंदु मिश्र लोक पक्षधर रचनाकार हैं। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत उन्होंने ‘अमरुकशतक का साहित्यशास्त्रीय अध्ययन’ (शोध-समीक्षा), ‘भारतकालीन कलाएँ’ (शोध-संदर्भ), ‘कालय तस्मै नमः’ (सतसई), एवं ‘अभिनवगुप्तपादाचार्य’ (खंडकाव्य) इत्यादि कृतियों की रचना की। हिंदी में ‘पारो’ (नवगीत), ‘अनुभव की सीढ़ी’ (गीत संग्रह), ‘काव्याख्यान’ (लंबी कविताएँ), ‘अधेड़ हो गई है गोले’ (विकलांगता विमर्श की कविताएँ), ‘अध्यापक की डायरी’ (डायरी), ‘समकालीन छंद प्रसंग’ (आलोचना), ‘खिड़की वाली सीट’ (कहानी संग्रह) इत्यादि पुस्तकें हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने नाटक एवं उपन्यास भी हिंदी में लिखे हैं। यह लेखन भी उनका महत्त्वपूर्ण है लेकिन भारतेंदु मिश्र की पहचान अवधी कवि और गद्यकार के रूप में सबसे प्रभावी है। अवधी में उनकी पहली किताब ‘कस परजवटि बिसारी’ सन् 2000 में प्रकाशित हुई, इसमें कविताएँ, गीत एवं ललित निबंध संकलित हैं। अवधी काव्य तो उनका प्रशंसित हैं ही, लेकिन उन्होंने अवधी गद्य को बहुआयामी प्रतिष्ठा तक पहुँचाने का बहुत ही ज़रूरी काम किया। वह बताते हैं अवधी गद्य की ओर उन्हें प्रेरित करने का काम हिंदी के प्रतिष्ठित कवि त्रिलोचन ने किया।
‘चंदावती’(2012) नाम से उन्होंने अवधी में बहुप्रशंसित उपन्यास लिखा। इसके अतिरिक्त अभी हाल में ही उनके रेखाचित्र-संस्मरणों की कोटि में आने वाले लेखों की एक किताब ‘हम परजा हन’ (2023) नाम से प्रकाशित हुई है। अवधी गद्य के विकास में भारतेंदु मिश्र ने जो काम किया है, उसे अवधी साहित्य के इतिहास से कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसी गद्य की आधारशिला पर अवधी का भव्य भवन निर्मित होगा, जिसके भारतेंदु मिश्र पुरस्कर्ता हैं।
भारतेंदु मिश्र के पास सिर्फ़ अपनी मातृभाषा ही नहीं उस भाषा के जातीय संस्कारों को जीने का प्रासंगिक अनुभव भी रहा। यह अनुभव प्रासंगिकता की परवाह की ज़िम्मेदारी का निर्वहन कर सके, लेखक के लिए आवश्यक होता है। सिर्फ़ स्वार्थ में मोह बिंबों को रचनात्मक क्षणों के हवाले कर, न लोक धर्म निभाया जा सकता है और न ही कवि कर्म किया जा सकता है। आज करवट बदलते समय में स्वार्थता के मोह बिंबों से लदीफँदी भावुकता लोकभाषा के नाम पर बाज़ारों में ख़ूब बिक रही है। यह ठगी का सस्ता साधन है। कविता के नाम पर स्वार्थ साधे जा रहे हैं, बाज़ार गरम किए जा रहे हैं। लोक से कटे हुए लोग लोक से सटे होने का स्वांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सच्चाई को पहचानने का एक सहज तरीक़ा है रचना की प्रासंगिकता को परखना। यह परख रचनाकार और पाठक दोनों को होनी चाहिए। भारतेंदु मिश्र की रचनाएँ इस कसौटी पर अपनी सचेतता का परिचय देती है। प्रसिद्ध विधेयवादी चिंतक एडोल्फ़ तेन ने सच्चे साहित्य को परखने के लिए प्रजाति, परिवेश और युग दर्शन को कसौटी माना था, यह आज भी रचना और रचनाकार को थाहने के लिए प्रामाणिक है। भारतेंदु मिश्र की रचनाओं को इन कसौटियों पर परखने से उनकी प्रासंगिक प्रतिबद्धता का पता चलता है और उनके समकालीन रचनाकारों से उन्हें निरख कर अलगाया जा सकता है।
प्रारंभ में उन्हें नवगीतकार के रूप में ख़ूब प्रशंसा मिली। इसका कारण यही है कि उन्हें लोकगीतों के परिवेश और युगदर्शन की गहरी समझ है। वह प्रासंगिकता को दरकिनार कर मोहातुर स्वार्थी बिंब नहीं रचते, उनके यहाँ लोक की ज़िम्मेदार नागरिकता बोलती है। भारतेंदु मिश्र के यहाँ मूल्यहीन होते समय की लौहित टीस करुणामय स्वाभाविक धर्मबोध के कोरे कागद पर रस-रैखीय आखर लोकतत्विक लय रूप में कविता बनते हैं। उनके यहाँ बड़ी सहजता से जो आया है, उसकी जड़े गहरी हैं। भारतेंदु की किताब ‘कस परजवटि बिसारी’ का पहला ही नवगीत है—रीति रिवाज पच्छिमी हुइगे/चलै लाग पछियाहु/बीति गवै फागुन की बेला/आय गवा बैसाख/सबियों धरती आँवाँ लागै/धूरि भई अब राख/सहरन की लँग भाजि रहे हैं/लरिका अउर जवान/हम जइसे बुढ़वन के जिउमा/अब ना बचा उछाहु।
ध्यान देने की बात यह है कि जिस पश्चिम को अपनी आधुनिकता के लिए संसार में जाना जाता है। जो तर्क और विज्ञान से रीति रिवाजों की प्रबल खंडनकारी छाप धरे गर्व से खड़ा था, पूर्व के महान् ‘देश’ में भी बहुत कुछ बदला, लेकिन जहाँ वह नहीं पहुँच पाया उस ‘देस’ में उसका प्रेत पहुँचा। अर्थात् रीति-रिवाजों का खंडनकारी स्वयं फ़ैशनेबुल रीति-रिवाज बन कर ‘देश के देस में’ जा पहुँचा। यह विडंबना ही हमारी उत्तर-आधुनिकता है। भारतेंदु मिश्र इसी ओर इशारा कर रहे हैं। पश्चिम के संस्कारों वाली आधुनिकता की पनिहावन देस में अचढ़ खेत के ऊँचे हार तक कभी नहीं पहुँची। इस ‘जेनरेशन गैप’ को भी कवि, कविता में बड़ी सजगता से दर्शाता है। फागुन हमारे पुराने बीत रहे संवत का आख़िरी महीना है और वैसाख नए साल का दूसरा माह। चैत की रिक्तता आधुनिकता की शून्यता ही है। हमारी ‘बहुनी ही बिगर गई’ है। ‘देस’ अर्थात् सुदूर गाँवों के तरुण अंधमुख शहर की तरफ़ भागे जा रहे हैं। यह पलायन सिर्फ़ मजबूरी ही नहीं है, फ़ैशन-लोभ भी है। यह पलायन सिर्फ़ दैहिक या भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक या आध्यात्मिक अधिक है। गाँवों से मिट रहे गाँव की अनायास दुर्दशा लोक मन को साल रही है—आपनि-आपनि सब रीति बनाये/अपनै-अपन सुनावैं/ख्यात-पात सब झूर परे/घर बैठि मल्हारै गावैं। यह हमारे विकास की स्वाभाविक धारा क़तई नहीं है।
कवि हमारे लोक के चित्ताकर्षक प्रयोजनों में लोभातुर होते समाज की वृत्तियों को अनुभवी आँखों से देख रहा है। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी के संसाधनों से सुविधाभोगी प्रजाति तमाम लोकबद्ध ही नहीं मानवीय मूल्यों से भी हाथ धोती जा रही है। आज जो जितना अधिक श्रम करता है, उसकी हालात उतनी ही दयनीय होती जाती है। पुरखों की यह नैतिक सीख कि मेहनत और ईमानदारी का परिणाम मधुर होता है, नए समय में कोरी बकवास ही इसे तरुण मानते हैं, क्योंकि यथार्थ उनके सामने भयावह है। जो मेहनत और ईमान में सद्वृत्ति से जीते हैं, हमारे समाज का वैभव उन्हें धन और प्रतिष्ठा से पदच्युत कर अपमानित करता रहता है। और जो कायरता एवं बेईमानी की सीढ़ियाँ बड़ी चालाक़ी से चढ़ते गए, वे धनकुबेर हुए। उन्होंने प्रतिष्ठा को अपनी दासी बना लिया। इस उलटफेर से युग की गंगा ही उलटा बहने लगी। इसमें सबसे आहत मनुष्यता और लोक संस्कृति ही हुई। नेतागिरी हरामख़ोरी का पर्याय हो गई और विद्वता संप्रभुता की बाँदी। ऐसे में समाज का नायकत्व जिस डगर पर चल पड़ा उसी का एक चित्र देखिए—तीनि-पाँच बइमानी कइकै/भे बड़कउनू भैया/लोटिया जिनकी बूड़ि रहै/अब पइरै उनकी नैया।
एक लोक कवि के लिए आज अपने युग दर्शन को पहचानना सबसे जटिल काम होता जा रहा है। मातृभाषाओं में जो कवि आज कविता लिख रहे हैं, वे अक्सर लोक के नाम पर पुरातन की वस्तुएँ बड़े सलीक़े से सजाकर एक अजायबघर बनाने में व्यस्त हैं और उसी में अप्रासंगिक मोहग्रस्तता के शिकार होते जाते हैं। उनकी नज़र पारखी नहीं कि अपने युग-दर्शन के शातिर स्वभाव को पहचान सकें। सतही काव्यबोध सरलता में मूल या यथार्थ से दूर उसकी प्रच्छन्न छाया पर प्रहार करता है जो सिर्फ़ भावुकता ही साबित होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ‘कविता क्या है’ निबंध में लिखते हैं—“पर यह प्रच्छन्न रूप वैसा मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता। इसी से प्रच्छन्नता का उद्घाटन कवि-कर्म का एक मुख्य अंग है। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती जाएगी, त्यों-त्यों कवियों के लिए यह काम बढ़ता जाएगा।” इस प्रच्छन्नता को पहचानना अपने युग-दर्शन से सचेत कोई कवि द्वारा ही संभव है। भारतेंदु मिश्र ने अपने युग के दर्शन को बड़ी संजीदगी से पहचाना है—दगाबाज दुनिया है सबै कुछु रूपइया/तरफराति पिंजरा है काठ कै चिरइया।
अपने युग के दर्शन की इतनी प्रभावशाली अभिव्यति हिंदी कविता में भी मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी। तड़प तो पिंजरा रहा है, उसके भीतर की चिड़िया तो काठ की है। कवि कह रहा है—हमारी आत्मा मर चुकी है, सिर्फ़ देह हरकत कर रही है। मतलब हमने अपना स्वभाव खो दिया है और हमारी तड़प सिर्फ़ प्रवृत्तियों का आडंबर-व्यापार बन कर रह गई हैं। हमने दर्शन के क़िले को नष्ट कर विमर्श के कांगड़े तैयार किए हैं। आज हम अपने विलोम युग के बेईमान क्रीतदास बन कर रह गए हैं। ऐसे समय में सच्चे कवि की ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि अपने समय की मनुजता को समाज की सम्मान पालकी में बैठाकर अपने ईमानदार कंधों पर सच्चा कवि कहार ही तो है जो जनपथ की विजयनी यात्रा पर लेकर उसे बढ़ सकता है। मानुष प्रेम की मूल्यवान परजवटि को कभी न भूलने का वचन उसी का है, संस्कृति उसी की ही बूढ़ी महतारी है—
हम कहार हन ई पुरवा के कस परजवटि बिसारी
बासन अबहूँ तक माँजति है मोरि बूढ़ि महतारी।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
