स्त्री और माँ
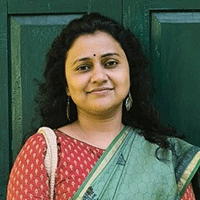 श्रुति कुमुद
04 जनवरी 2026
श्रुति कुमुद
04 जनवरी 2026

प्रस्तुत लेख ‘हिन्दवी’ पर प्रकाशित ‘बेला’—‘सदी की आख़िरी माँएँ’, प्रणव मिश्र तेजस के लेख की प्रतिक्रिया में लिखा गया है। ‘सदी की आख़िरी माँएँ’ (मूल लेख) प्रथम—23 नवंबर को ‘हिन्दवी’ पर प्रकाशित हुआ। इसे दुबारा 'दैनिक भास्कर' ने—‘हिन्दवी’ से विशेष अनुबंध के तहत—संपादित (‘हमने देखी हैं इस बदलती सदी की आख़िरी माँएँ!’) में 28 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया।
‘हिन्दवी’ पर एक लेख पढ़ा—‘सदी की आख़िरी माँएँ’, प्रणव मिश्र तेजस ने इस लेख को लिखा है, बाद में यह लेख 'दैनिक भास्कर' में (‘हमने देखी हैं इस बदलती सदी की आख़िरी माँएँ!’) भी प्रकाशित हुआ है। ‘हिन्दवी’ पर रोज़ाना प्रकाशित होने वाले लेखों में से भास्कर ने इसे ही क्यों चुना, यह प्रश्न मन में आया। जब इसे दुबारा पढ़ना शुरू किया (पहली बार विनीत कुमार के नोट के साथ पढ़ा था) तब पाया कि माँ से जुड़े प्रसंगों को याद करते हुए यह आलेख स्त्री-अधिकारों के लिए हुए संघर्षों तथा हर उस वैचारिकता का विरोध करता है जो स्त्री को ‘स्त्री’ की तरह देखने की बात करती है।
लेखक लिखते हैं, “प्रगतिशील समाज ने स्त्रियों के मान-सम्मान के लिए न जाने कितने विमर्श खड़े किए, लेकिन प्रगतिशीलता का वह स्तर अब तक नहीं छू पाए, जिसे हमारी अम्मा की अम्मा या उनकी सास ने वर्षों पहले जी लिया था।” यह स्थापना उस समूचे संघर्षों के विरुद्ध है जिसे पिछली सदी और इस सदी की जागरूक स्त्रियों ने किया है। लेखक ने इस स्थापना के पक्ष में एक भी उदाहरण देना उचित नहीं समझा है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि प्रगतिशीलता के वह स्तर जो इस सदी की स्त्रियाँ जी पा रही हैं, वह पिछली से पिछली पीढ़ी की स्त्रियों के लिए संभव नहीं था। अगर ‘मातृत्व–अवकाश’ की बात करें तो इसके लिए जो लड़ाई पिछली सदी के तीसरे दशक से शुरू हुई, अब जाकर कुछ स्वरूप ले सकी है। वर्ष 2017 के क़ानूनी सुधार तक पहुँचने के लिए लंबा रास्ता उन प्रगतिशील समाज की स्त्रियों ने ही तय किया है, जो मातृत्व अवकाश के महत्त्व को समझती रही हैं। 1927 में जब यह पहली बार मातृत्व अवकाश अपने आधे-अधूरेपन से लागू हुआ था, तब पुरुष समाज इस तरह ईर्ष्या से भर गया था कि स्त्रियों को नौकरी मिलनी बंद हो गई थी। लेखक के उपयुक्त कथन में मैं सौ वर्ष पूर्व के पुरुष समाज को देख पा रही हूँ। संघर्षों के बाद ही बारह हफ़्ते और फिर अनेक संघर्षों के बाद छब्बीस हफ़्तों का मातृत्व अवकाश मिलना शुरू हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो स्त्रियों के उन अधिकारों से जुड़े हैं जो उन्हें विमर्शजन्य संघर्षों से मिले हैं।
सुंदर वाक्यों के सहारे स्त्री-विमर्श को ख़ारिज करने की चेष्टा से चालाकी ही झलकती है, लेखकीय ईमानदारी नहीं दिखती। वरना माँ की प्रशंसा करने हेतु आपको प्रगतिशील समाज या स्त्री-विमर्श की आलोचना नहीं करनी पड़ती। इस लेख की समस्याग्रस्त अनेक बातों में से एक बात यह भी है कि लेखक पुरानी पीढ़ियों की माँओं की प्रशंसा नई पीढ़ी की माँओं को ख़ारिज करके करना चाहता है।
इस लेख के कुछ बिंदु अंतर्विरोधी भी हैं। एक तरफ़ लिखा है, “जिसे (प्रगतिशीलता को) हमारी अम्मा की अम्मा या उनकी सास ने वर्षों पहले ही जी लिया था” और दूसरी तरफ़ लिखते हैं, “अम्मा सदैव घर में क़ैद रहने वाली महिला हैं, जिन्होंने कभी आज़ादी के लिए कोई आंदोलन नहीं किया... सहनशीलता, इस पीढी की औरतों की सबसे बड़ी विरासत है।”
लेखक को माँ जब भी याद आती है—काम में लगी हुई ही याद आती है। किसी सामाजिक कंडीशनिंग के कारण उत्पन्न अवयवों का महिमामंडन अनुचित है। यह त्रासदी है कि लेखक कभी ख़ुद को माँ के काम में हाथ बँटाते हुए याद नहीं आता, पिता कभी घर के काम में हाथ बँटाते हुए याद नहीं आते और आख़िर में ऐसे रोमांटिक वाक्यों के सहारे माँ को प्रमाणपत्र देते हैं। यह असंवेदनशीलता है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी को हल्का कर देखते हैं। डिप्रेशन एक सच्चाई है। लेखक का मंतव्य कुछ इस तरह है कि जो व्यस्त है वह डिप्रेशन या अन्य ऐसी बीमारियों का शिकार नहीं हो सकता।
लेखक आधुनिक माँओं को कोसने के लिए डायपर का विरोध करता है। नई पीढ़ी की माँओं के प्रति इतनी असंवेदनशीलता से भरे ये लोग कभी नहीं समझ सकते कि डायपर ने एक माँ और बच्चे का जीवन किस क़दर आसान किया है। क्या आप माँओं को हमेशा परेशान और काम में मुब्तिला ही देखना चाहते हैं? डायपर पहनना और न पहनना गर्व का विषय नहीं है। इन्होंने या तो आधुनिक माँओं को देखा नहीं है या समय-समाज से पूरी तरह कट गए हैं।
यह आलेख प्रतिगामी मूल्यों को जाने-अनजाने स्थापित करता है। लेखक लिखता है—“हमारी बीमारियों पर रात-दिन प्रार्थनाएँ की गईं”, प्रतिगामी मूल्यों के धनी लेख शब्दों को इस तरह बरतते हैं कि जैसे वे बच निकलने का ढंग ढूँढ़ते हों। यह वाक्य इस तरह लिखा गया है जैसे पिछली पीढ़ी की माँएँ ही अपने बच्चों के बीमार पड़ने पर परेशान होती थीं। न चाहते हुए भी एक व्यक्तिगत उदाहरण देना पड़ रहा है (हालाँकि इस लेख के लेखक ने भी व्यक्तिगत उदाहरणों के बहाने ही अपनी बात कही है)—जब मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ, तब कोविड-19 की दूसरी लहर निकल चुकी थी, लेकिन हवा में उसका भय उपस्थित था और कुछ दिक़्क़तों के कारण समय से पहले ‘डिलीवरी’ का निर्णय लेना पड़ा। इसलिए हमारे घर से कोई न आ सका। मैं अस्पताल में थी और मेरे पार्टनर अस्पताल से घर के बीच देख रहे थे, क्योंकि बड़े बेटे घर पर थे और वहाँ भी सब नैनी के भरोसे था, जिसकी मदद लेने वाली माँओं को संदर्भित आलेख के लेखक ने हिक़ारत से देखा है। चार दिन बाद जब नवजात को लेकर हम घर पहुँचे, तब तक बदलते मौसम के कारण बड़े बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी थी। इलाज आदि शुरू होने के बाद भी सातवें दिन तक उनका ऑक्सीजन लेवल जब नब्बे से नीचे के स्तर को छूने लगा था, तब रात के दो बजे पार्टनर उन्हें लेकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग भागे। मैं बिस्तर पर थी, सर्जरी के घाव सूखे नहीं थे, करवट लेना सोचने से भी डर लगता था, खड़ा होना भी किसी सहारे से ही हो पाता था जिसमें दो-तीन मिनट लग जाते थे। लेटना तब उससे भी बड़ी मुश्किल थी। इन सबके बावजूद मेरा मन नहीं मान रहा था। दिमाग़ लगातार बड़े बेटे के पास पहुँच जाने का उपाय ढूँढ़ रहा था। अस्पताल से सारी जानकारी बार-बार मिल रही थी, लेकिन बेटे के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब भी सोचती हूँ तो दिल काँप जाता है। घर के सामने से ऑटो करके अस्पताल तक जाने में कितनी बार लगता रहा था कि पेट का घाव खुल जाएगा। हर झटके से मर्मान्तक पीड़ा उठ रही थी, लेकिन जब तक बच्चे को देख नहीं लिया तब तक रोती ही रही।
यह सिर्फ़ मेरी बात नहीं है। हर माँ अपने बच्चे के लिए इस तरह या इससे भी कठिन संघर्ष करती है, इससे भी बुरे वक़्त को झेलती है। हम सब इस सदी की माँएँ हैं और पिछली सदी की अनेक माँएँ लालन-पालन के हमारे तरीक़ों की तारीफ़ करती हैं, इसलिए कोई भी निर्णायक वक्तव्य आपकी वैचारिकता से परिचय कराता है, वस्तुस्थिति से नहीं।
लेखक को एक यह दंभ भी है कि “हमारी परवरिश किसी नैनी ने नहीं की।” कामगार और नौकरीपेशा स्त्रियों का जीवन आपने देखा होता तो ऐसे दंभ नहीं पालते। मेरे जीवन में नैनी वरदान की तरह रही हैं। मैं अपने अब तक के जीवन में सर्वाधिक शुक्रगुज़ार अपनी सहायिकाओं की हूँ। नैनी अथवा सहायिकाएँ हमारी मातृत्व योजनाओं में सहयोगी होती हैं। नैनी के होने भर से माँएँ निश्चिंत नहीं हो जातीं। मातृत्व संबंधी सारी ज़िम्मेदारियाँ मन-मस्तिष्क में अनवरत बजती रहती हैं। नौकरी के बाद का सारा समय बच्चों के साथ और बच्चों के लिए ही बीतता है, लेकिन जिन कुछ घंटों के लिए बच्चे नैनी’ज़ के भरोसे रहते हैं, वे घंटे हमें उनके प्रति सर्वाधिक शुक्रगुज़ार बनाते हैं। लोग स्त्रियों के स्वप्नों की बलि लेकर, उन्हें माँ का इकलौता किरदार थमाकर, ऐसा दंभ पालना चाहते हैं कि आपके जीवन में नैनी’ज़ का कोई योगदान नहीं है। एक अन्य बात की तरफ़ ध्यान दिलाना चाहूँगी कि पहले के ज़माने में नैनी या सहायिकाओं का किरदार भले न रहा हो, लेकिन संयुक्त परिवार के कारण बुआ, चाची, दादी, ताई तथा घनिष्ठ पड़ोसियों की उपस्थिति से माँओं को जो कुछ मोहलत मिलती थी, वह बड़ी बात होती थी। आज के ज़माने में किसी के पास दूसरे के लिए समय नहीं है। इस पर विस्तार से लिखना चाहूँगी।
प्रणव का यह लेख स्त्री को माँ और ममत्व तक सीमित करने का प्रयास है तथा सांत्वना पुरस्कार के बतौर उसमें त्याग तथा दूसरे भाव ढूँढ़ने की कोशिश है। प्रणव से पहले भी ऐसे लेख लिखे गए हैं, लेकिन ‘हिन्दवी’ और 'दैनिक भास्कर' जैसे लोकप्रिय मंचों पर प्रकाशन से यह आलेख उन लोगों के लिए नज़ीर बनता है जो स्त्रियों को माँ की परिभाषा के भीतर तक सीमित कर देना चाहते हैं। मारग्रेट एटवुड के उपन्यास ‘दी हैंडमेड’स टेल’ पर बनी इसी नाम की फ़िल्म को देखते हुए समाज का उद्देश्य साफ़ समझ में आता है कि यह समाज जब पूर्णत: पुरुषों द्वारा, पुरुषों के लिए, पुरुषों का शासन बन जाएगा, तब स्त्रियाँ बच्चा पैदा करने की मशीन से अधिक कुछ नहीं रह जाएँगी। उस फ़िल्म की मूल संवेदना वह बिंदु है—जहाँ स्त्रियों को पहले संतानोत्पत्ति का औज़ार बनाया जाता है और अंतत: उनसे वह अधिकार भी छीन लिया जाता है जिसे संतानोत्पत्ति का अधिकार कहते हैं। अर्थात् स्त्रियों के बजाय पुरुष ही यह निर्णय लेंगे कि स्त्रियाँ संतानों की उत्पत्ति से जुड़े इस कार्य-व्यापार में कब और कैसे शामिल हों? यह निर्णय भी स्त्रियाँ नहीं ले सकतीं। हालाँकि सामंती समाज के लोगों को लगेगा कि इस फ़िल्म में फ़ंतासी कहाँ है!
माँ के बग़ैर जीवन कल्पनातीत है। प्रकृति के नियम ने स्त्री को ही क्यों चुना; यह इस आलेख का विषय नहीं है, बल्कि यह कि स्त्री के माँ-स्वरूप के ही क़सीदे क्यों पढ़े जाते हैं? या क्या कोई भी क़सीदा माँ के उस दौर को या उस कष्ट को व्याख्यायित कर सकता है जो गर्भ-धारण से प्रसव-वेदना, प्रसव के दौरान और पश्चात् की पीड़ा को प्रस्तुत कर सके। मेरे भी दो बेटे हैं, लेकिन भविष्य में कभी अगर मेरे ममत्व की पड़ताल हो तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे मुझे इस पैमाने पर देखें कि मैंने उनसे कैसा व्यवहार किया? कितनी रातें जागीं? कैसे जीवन भर के लिए पीठ-दर्द और कमर-दर्द की सौगात पा ली? यह सब कहना-सुनना बच्चों पर बेरहमी है। लेकिन साथ ही माँ के क़सीदों से ऐसा लगता है कि किसी प्रोजेक्ट के तहत समाज के प्रतिगामी मूल्यों को स्थापित किया जा रहा है। माँ को उसके ममत्व तक सीमित किया जा रहा है।
मैं इस टिप्पणी को स्त्री-अधिकारों के व्यापक मुद्दे की तरफ़ न ले जाकर एक अपेक्षाकृत सीधी बात पर केंद्रित करना चाहती हूँ कि अगर किसी माँ की ममता को जाँचने का अधिकार हमने हासिल कर ही लिया है तो किस मानक पर जाँचेंगे? यह अधिकार मिलना ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि ममत्व की पड़ताल पुरुष समाज करे और फिर सदीवार तुलना पेश करे। लेकिन अगर यह काम आपने हाथ में लिया है तो माँ की पड़ताल इस पैमाने पर नहीं होगी कि उसने अपने बच्चों को कितना प्यार किया। यह कोई पैमाना नहीं है। एक स्त्री का माँ-रूपी व्यवहार तब कैसा होता है, जब उसके घर एक नया शख़्स अर्थात् उसकी बहू आती है? अगर आप सास अच्छी नहीं हों तो आप यक़ीनन अच्छी माँ नहीं रही हैं। स्त्री को माँ के रूप में सीमित कर देखना एक ख़राब बात है, लेकिन अगर आप इसी पर तुले हैं तो उस स्थिति में भी माँ के महान् होने का लिटमस-टेस्ट उसका सास होना है। इस बात को समझे बिना अगर आप महज़ इस आधार पर माँ को देखते हैं कि उसने अपनी संतान से कैसा प्रेम जताया तो आप उस जाल का या उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते जा रहे हैं जो समाज के दुर्भावनाग्रस्त क़ायदों को लागू करने का जतन कर रहा है। नई बहू अपने साथ सिर्फ़ यह प्रार्थना लेकर आती है कि उसका नया घर पुरसुकून हो। वह विश्वास, वह ऊर्जा किसी भी दूसरे विस्थापन में नहीं देखी जा सकती है। वह विश्वास किसी भी दूसरे रिश्ते में नहीं देखा जा सकता है। जिस पीढ़ी की माँओं की बात प्रणव कर रहे हैं, उस दौर के उन अपराध-रिपोर्ट्स को देखा जाना चाहिए जो बहुओं पर हुए अत्याचार से जुड़े हैं। यह रिपोर्ट देखने भर से वे लोग अपने प्रोजक्ट से पीछे होने लगेंगे जो ममत्व की खूँटी से स्त्रियों को बाँधना चाहते हैं। आप कह सकते हैं कि माँओं की ट्रेनिंग नहीं है कि वे अच्छी सास हो सकें; यह एक महत्त्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन क्या उन्हें बेहतर इंसान होने की भी ट्रेनिंग नहीं मिली है?
भविष्य में अगर मेरे बेटे ब्याह के बंधनों में बँधते हैं, तब अगर मैं उन संभावित बहुओं को सुकून और भरोसे का माहौल न दे सकी तो मैं समझूँगी कि मेरा ममत्व अधूरा और असफल रहा। कुछ समय पहले एक्सिस बैंक का एक विज्ञापन आया था, वह विज्ञापन लोन से संबंधित था। उसमें एक बारीक बात थी जो आज याद आ रही है। माँ और बेटे कार में बैठे हैं। बेटा कार चला रहा है (काश वह दृश्य ऐसा होता कि माँ कार चला रही होती), बेटा पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? माँ बताती है कि बैंक से बात हो गई है, वह चाहती है कि बेटा अपना घर/फ़्लैट ख़रीद ले। बेटा चकित होकर कहता है कि शादी हो जाने दो, बहू आ जाने दो। माँ कहती है—मैं चाहती हूँ कि बहू नए घर में आए। उस विज्ञापन में कहानी कुछ इस तरह ही बढ़ती है जिसमें माँ समझाती है कि पहले दिन से उनके बच्चे की अपनी गृहस्थी हो।
कुछ भी कहने से पहले यह याद रहे कि यह विज्ञापन लोन का था, अपने लोन-उत्पाद के लिए नया ग्राहक-वर्ग ढूँढ़ने का था.., कई अन्य पहलू आलोच्य थे, लेकिन यह एक संदेश था कि नए वर-वधू की नई गृहस्थी में बेटे की माँ/बहू की सास का दख़ल कितना सकारात्मक हो सकता है।
माँ होना, ममत्व का होना, स्त्री का अधिकार है। उसकी दुर्बलता नहीं है। इस सदी की स्त्री भी उतनी ही अच्छी माँ है, जितनी पिछली सदी की हुआ करती होंगी। ममत्व एक चिरस्थायी नदी है, लेकिन इकलौती नहीं है। स्त्री का ‘स्त्री’ होना समुद्र है और एकाध नदियों के पानी को ही समुद्र का स्रोत बना देना बड़े अफ़सोस की बात है।
मेरे अपने निर्माण में माँ की भूमिका सर्वाधिक है, लेकिन मेरी माँ जिस अक्षय ऊर्जा से जीवन भर संचालित रही हैं, घर को जिस तरह सँभाला, उसका दस फ़ीसद भी ममत्व का मुहावरा नहीं समेट सकता। मैं अगर अपनी माँ की कहानी लिखूँगी तब उनके संघर्षों की कहानी लिखूँगी, ताकि नज़ीर बनाकर पेश करने वाली जमात उस नज़ीर के सहारे किसी स्त्री को उसके हद में बाँधने की कोशिश न करे। मैं उनके ममत्व को याद करना चाहूँगी और मन ही मन ख़ूब याद करती हूँ, लेकिन उसे लिखने से बचूँगी क्योंकि कल को कोई उस बुज़ुर्ग स्त्री के ममत्व की कहानी को अपनी पत्नी या प्रेमिका को उदाहरण बनाकर सुनाएगा और चाहेगा कि उसे माँ की परिभाषा में जकड़कर रख ले।
प्रणव के आलेख में उद्धृत संदर्भ को देखें तो उनकी माँ द्वारा अपने बेटे के लिए पैसे निकालकर देने का प्रसंग उस स्वाभिमानी क़दम का हिस्सा है, जिसे हर स्त्री उठाना चाहती है। उन्हीं क़दमों की तैयारी में वे सारे संघर्ष हुए जिसके निषेध में यह संसार खड़ा है और माँ को स्त्री से अलग करते हुए देखता है। माँ को याद करने वाले लोग अगर उनके स्त्री रूप को याद करने लगें तो निश्चय ही बात-बात पर स्त्री-द्वेष जताने वाली जमात घबराएगी, उनका मनोबल टूटेगा।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
