बकुला मरलें, बकुली रूसल जाली! : कथा और कथा की समझ
 बलभद्र
12 दिसम्बर 2025
बलभद्र
12 दिसम्बर 2025
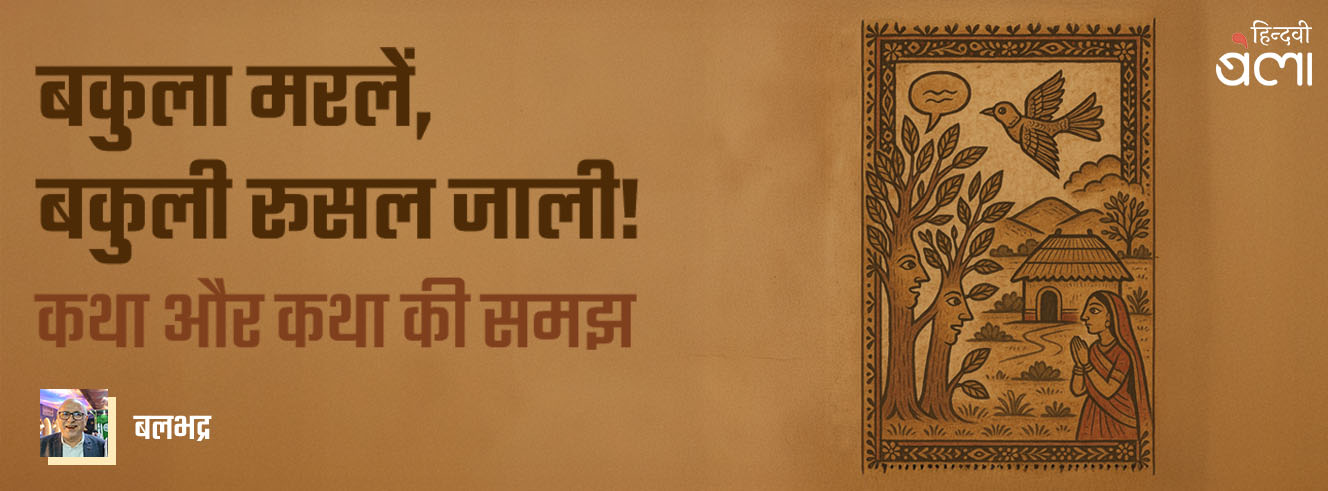
भोजपुरी में न जाने कितनी लोककथाएँ हैं। कुछ तो लोक में ख़ूब प्रचलित हैं और बहुतेरी कथाएँ लगभग विलुप्ति के कगार पर हैं। न जाने कितनी विलुप्त हो गई हैं। और इन सभी लोक कथाओं को एक जगह करना बहुत मुश्किल काम है। लोककथाओं के भंडार कहे जाने वाले लोग—वैसे लोग जिनकी स्मृतियों में ढेर सारी कथाएँ हुआ करती थीं—मुश्किल से गिनती के बचे होंगे। कथाओं के संग्रह के कुछ क़ाबिल-ए-तारीफ़ प्रयास भी हुए हैं, लेकिन वे काफ़ी नहीं कहे जा सकते। वे दादी-नानियाँ अब नहीं रहीं जो घर-गृहस्थी के कार्यों को गीतों के चढ़ाव-उतार के साथ संपन्न करती थीं। वैसे कथक्कड़ भी तो अब नहीं रहे, जो साँझ को गीतों और कथाओं से रौशन किया करते थे। यहाँ कहना उचित समझता हूँ कि इन्हीं कथक्कड़ों में हमारी दादी हंसमुखा देवी और बड़की माई फूला देवी थीं। इन लोगों से न जाने हम भाई-बहनों ने कितनी कथाएँ सुनी होंगी। बाबा राम अवतार सिंह जिनको हम लोग खइनिया बाबा कहते थे, भूत-प्रेत की बातें सुनाया करते थे। हमारे बच्चों को भी अपनी दादियों से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सुनी हुई कथाओं से एक कथा यहाँ सुनाना चाहता हूँ। आप सब सुनें और सुनने के बाद जो मैंने समझा है, गुना है, उसको भी साझा करना चाहता हूँ। लोककथाओं के अंत में वाचक यह ज़रूर कहता था, जिसे आज भी कहा जाना चाहिए कि “कथा गइल बन में, सोचऽ अपना मन में।”
एगो बकुला रहलें, एगो बकुली रहली। ओह लोग के आपन घर-गिरहस्ती रहे। बकुला आ बकुली दूनो लोग रोज संगे निकले, मछरी मारे। घरे आके बकुली चूल्हा-चाकी करे। मछरी निर्हे, बरतन माजे, पानी भरे। रात खा मछरी के कांट-कूट प दूनो लोग सूत जाए।
एक दिन दूनो लोग में कवनो बात के बीच परल। बकुला बकुला रहले, मरद। बकुली बकुली रहली, मेहरारू। बकुला आव देखले ना ताव। हाथ छोड़ देलें बकुली प। बकुली रोअली-गवली, जवन कर सकत रहली कइली। रूस-फूल घर छोड़ चलली।
राह में आम के पेड़ रहे। बकुली के अकेले आ उदास देखते बूझ गइल कि बात कुछ गड़बड़ बा। राह चलत केहू से हाल-चाल पूछल तब लोक-व्यवहार रहे।
बकुली से पूछलें—“बकुली-बकुली कहां जालू!”
बकुली कहली—“बकुला मरलें, बकुली रूसल जाली!”
आम कहलस—“हमरा संगे रहबू!”
बकुली पूछली—“का खिअइबऽ, का पिअइबऽ, काथिए सुतइबऽ, का ओढ़इबऽ!”
आम कहलस—“आम खिआइब, गड़हा के पानी पिआइब, डार प सुताइब, पतई ओढ़ाइब।”
बकुली कहली—“उहूं, ना रहब, ना रहब।”
उहूं कह बकुली आगे बढ़ चलली।
राह त राह ह। राही से बोलल, कुछ पूछल-आछल ना रहे मना।
राह के महुआ के रहाइल ना बेपूछले—“बकुली-बकुली कहां जालू!”
“बकुला मरले, बकुली रूसल जाली।”
“हमरा संगे रहबू!”
“का खिअइबऽ, का पिअइबऽ, काथिए सुतइबऽ, का ओढ़इबऽ!”
“महुआ खिआइब, गढ़हा के पानी पिआइब, डार प सुताइब, पतई ओढ़ाइब।”
“उहूं, ना रहब, ना रहब!”
उनको के “उहूं” कह चल भइली बकुली।
राह त राह, ना चलवइया के कमी, ना पुछवइया के। बकुली के उतरल चेहरा देख कटहर कइसे ना पूछे।
“बकुली-बकुली कहां जालू!”
“बकुला मरले, बकुली रूसल जाली।”
“हमरा संगे रहबू!”
“का खिअइबऽ, का पिअइबऽ, काथिए सुतइबऽ, का ओढ़इब ऽ!”
“कोआ खिआइब, गड़ही के पानी पिआइब, डारे सुताइब, पतई ओढ़ाइब।”
“उहूं, ना रहब!”
एहिजो मुँह घुमा चल देली बकुली।
कुछ दूर, राह में एगो बकुला गड़हा में मछरी मारत रहे। ओकर नजर बकुली प परल।
पूछलस—“ बकुली-बकुली कहां जालू!”
बकुली कहली—“बकुला मरले, बकुली रूसल जाली।”
बकुला कहलस—“हमरा संगे रहबू।”
“का खिअइबऽ, का पिअइबऽ, कथी प सुतइबऽ, का ओढ़इबऽ!”—बकुली पुछली!
“मछरी खिआइब, पोखरा के पानी पिआइब, मछरी के कांट प सुताइब, पांख ओढ़ाइब।”—बकुला कहलें।
बकुली कहली—“रहब, रहब!”
दूनो परानी एक संगे रहे लगलें। बकुला मछरी मारे आ बकुली ओके धो धा के निर्हे।
एक दिन बकुली मछरी चूल्हा प चढ़ा के ओह में पानी डाल के, जब डभके लागल त बकुला से देखे के कह के, चल गइली इनार प पानी भरे, ओह दिन ऊ पहिले से पानी ना भर पवले रही।
मछरी के कड़ाही में डभकत देख रहाइल ना बकुला से। टप से चोंच मरले, चोंच जरल। चेंगुरा से निकाले चहलें, चेंगुरा जरल। पाँख से निकललें, पाँख जरल। आ बकुला ओहिजे अइंठा के मू गइलें।
पानी लेके बकुली जब अइली त देखली कि बकुला पाँख छितरवले मुअल परल बाड़न। ऊ विलाप करे लगली—“आमवा तेजलीं, महुइया तेजलीं, कटहरवा तेजलीं तोरा के ना तेजलीं बकुलवा, ऊ हू हू हू...!”
यह रही बकुला-बकुली की कथा। हम लोगों ने अपनी दादी से सुनी थी, हमारे बच्चों ने अपनी दादी से। अब के बच्चे शायद ही सुन पाएँ। सुनें भी तो उनको मज़ा न आए। और जब मज़ा ही न आए तो कोई क्यों सुने? मज़ा अब दूसरी चीज़ों में ज़्यादा है, बहुत तीव्र। अब इस स्लो मोशन की क्या पूछ!
अब तो बहुत-सी चीज़ें बदल गई हैं। गाँव बदल गए हैं, शहर बदल गए हैं, खेती-गृहस्थी बदल गई है, कमाने-धमाने के तरीक़े ,साधन और रहन-सहन बदल गए हैं। पढ़ाई-लिखाई भी बदल गई है। ऐसे में, यह या इस तरह की कथाएँ, जिनको लोककथा कहते हैं, अपने पुराने रूपों में ही कैसे बची रह पाएँगी। इनके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। इनको नए माध्यमों में ही बचाया जा सकता है। इनका फ़िल्मांकन ज़रूरी है। साथ ही, इनको मूल रूपों में भी संरक्षित किया जाना चाहिए। इस दिशा में कुछ महत्त्वपूर्ण काम हुए भी हैं।
अब चलिए इस कथा पर कुछ बातचीत हो जाए। पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि इन कथाओं को हम लोगों ने बच्चों को सुनाई जाने वाली कथा कहकर समझ लिया है कि बहुत कुछ कह दिया। इन कथाओं को ‘बालबझावन’ कथा कहा, साँझ को बच्चों को बझाए रखने का माध्यम। और इन पर कायदे से विचार नहीं किया। न इनके शिल्प पर, न इनमें चित्रित जीवन और समाज पर, न इनके संदेश पर और न ही जीवन पर पड़ने वाले इनके व्यापक प्रभावों पर। भोजपुरी लोककथाओं पर भोजपुरी अंचल के कुछ विश्वविद्यालयों में पीएचडी उपाधि के लिए शोधकार्य भी हुए हैं, लेकिन वहाँ ज़्यादातर उनके कथ्य के आधार पर श्रेणी—विभाजन, यथा सामाजिक लोककथा, धार्मिक लोककथा, सांस्कृतिक लोककथा पर ही अधिक बातें हुई हैं। यहाँ उन शोधकार्यों पर बात नहीं की जाएगी। उन पर कभी बाद में विचार किया जाएगा।
आज भी मुझे याद है कि इस बकुला-बकुली की कथा का आख़िरी हिस्सा जहाँ बकुली विलाप कर रही है, बचपन में पूरी तरह याद था और इस कथा की जो स्मृति आज तक है, उसमें इस हिस्से की बड़ी भूमिका है। यह कथा विस्मृत हो चली थी, लेकिन, बकुली-विलाप के छोर को पकड़ पूरी कथा याद आ गई, और मन ही मन उसे कह डाला। याद है कि बचपन में बकुली के विलाप की शैली की खेल-खेल में ही कभी-कभार नक़ल भी कर लिया करता था। थोड़ा बड़ा हुआ तब से आज तक मृत्युशोक में औरतों को इसी तरह विलाप करते हुए देखता हूँ। साथ ही, यह कथा इस विलाप-शैली के साथ-साथ आम, महुआ, कटहल और बकुली के संवाद में याद है। किसी भी कथा को लंबे समय तक याद रखने के सूत्र उस कथा में ही मौजूद होते हैं। सचमुच, कितने दिलचस्प हैं तीन पेड़ों के प्रस्ताव, जो तीन तरह के नहीं, एक ही तरह के हैं, जिनको बकुली सहज ही अस्वीकार कर देती है। वह प्रस्ताव बकुला से मार खाई घर छोड़ निकली बकुली से है। अकुंठ प्रस्ताव और समझदार अस्वीकृति। समझदार अस्वीकृति का मतलब यह है कि बकुली की स्वाभाविक संगति तो बकुले की ही होनी चाहिए। सहानुभूति बेशक बहुत महत्त्वपूर्ण है, लेकिन स्वाभाविक संगति के तर्क को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसको भी समझने की ज़रूरत है। बकुली की जगह अपने समाज की किसी स्त्री को रखकर देखने की ज़रूरत है। मामला साफ़-साफ़ समझ में आता नज़र आएगा। घर से नाराज़ हो निकली किसी बकुली (स्त्री) के साथ कोई बोलबाज़ी नहीं, बस कारण पूछना और साथ रहने का प्रस्ताव रखना। प्रस्ताव की अस्वीकृति पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं, बेरोक आगे जाने का खुला मार्ग। किसी भी समाज में पति की मनमानी या उसके हिंसक या अशोभनीय व्यवहार से नाराज़ स्त्री का घर छोड़ना आज भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसी स्त्री को हज़ार-हज़ार गालियों से नवाज़ते हैं। बदचलन कहना तो आम बात है। यह पुरुषवादी दृष्टि या वर्चस्व बकुली के व्यवहार से टूटता हुआ दिखता है। भले आगे चलकर उसे किसी दूसरे बगुले के साथ रहना पड़ता है। एक गृहस्थ की भूमिका में ही। लेकिन, अपमान पर नाराज़ होकर घर से निकल पड़ना और नई संगति की तलाश पर तो ग़ौर किया ही जाना चाहिए। हालाँकि, एक सतही निष्कर्ष तो लोग निकाल ही सकते हैं कि घर से निकल नई संगति की तलाश का हासिल ही क्या है? नए साथी (बगुला) का साथ भी तो नहीं रहा। अपनी जीभचटोरी में उसे प्राण ही गँवाने पड़े। उसके साथ भी तो बकुली को चूल्हा-चौका करना पड़ा। लेकिन, इसको इस तरह समझना अथवा कथा में चित्रित जीवन की इस तरह व्याख्या क़तई ठीक नहीं है। एक स्त्री को एक संबंध से अलग होने और नए संबंध की तलाश का पूरा हक़ है। परिणामवादी नज़रिए से विचार करना ठीक नहीं। इस तरह की कथाओं की ख़ासियत होती है कि वह बहुत-सी बातों को अपने में ऐसे गूँथकर चलती हैं कि ठीक से नहीं पढ़ने और सोचने पर वे बहुत-सी बातें पकड़ में आती ही नहीं हैं। दरअस्ल हुआ यह है कि लोक-साहित्य की अकादमिक जगत में अजीबोग़रीब व्याख्याएँ हुई हैं और उसमें भी ख़ासकर लोककथाओं की। उसको नैतिक मानदंडों के आधार पर ही समझा जाता रहा है। उसकी नैतिक शिक्षा तक ही पहुँच हो पाई है।
बकुला-बकुली के दाम्पत्य में कुलीन समाजों का दाम्पत्य चित्रित नहीं हुआ है। कुलीन समाजों में स्त्रियाँ घरों में तो काम करती हैं, बाहर नहीं। इस लोककथा के दोनों पात्र साथ-साथ काम करते हैं। मछली साथ-साथ मारते हैं। पर, उसे धोती-बनाती है बकुली। सवाल हो सकते हैं कि बगुले तो मछली चट पकड़ते हैं और पट हजम कर जाते हैं। यह धोना और बनाना कहाँ से आ गया। तो इसका सीधा-सा उत्तर तो यही होगा कि यह कथा है, और उसमें भी लोककथा। जब सियार और कबूतर आदमी की भाषा बोल-समझ सकते हैं तो यह दाम्पत्य और गृहस्थी भी संभव है।
कथा में जो दाम्पत्य है वह आम ग़रीब पिछड़े समुदाय का है, जहाँ स्त्री-पुरुष दोनों श्रम में भागीदार होते हैं। जहाँ घरेलू काम स्त्रियों के ही ज़िम्मे होते हैं, कुलीन परिवारों की ही तरह, पर, शत-प्रतिशत नहीं। यह उस समाज का दाम्पत्य है और बकुली उस समाज के स्त्री-पात्र की प्रतीक है, जहाँ अपमान पर नाराज़ होना और दूसरी संगति की तलाश पर कोई नैतिक प्रतिबंध नहीं है। यह भी ग़ौरतलब है कि बकुली ख़ुद मेहनत करने वाली है, फिर भी जिसके साथ रहना है उसकी स्थिति जानना चाहती है कि जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ कैसी हैं। दाना-पानी चुगने में ख़ुद जो सक्षम है, वह भी जीवनसाथी तय करने में जीवनयापन की मूलभूत सुविधाओं को लेकर चिंतित है। स्त्री की पुरुष पर निर्भरता वाली लोक मानसिकता के अनुरूप बकुली की गढ़न है।
इस कथा के शिल्प में ऐसा क्या है जिसको ख़ासकर उद्धृत किया जाना चाहिए। उस लिहाज से देखें तो पहले तो बकुली के विलाप यानी उसके रोने पर ध्यान जाता है। उसके विलाप में पहली संगति के छूटने का कोई अफ़सोस नहीं है। पर, राह के आम, महुआ और कटहल के प्रस्ताव को नकारने का अफ़सोस ज़रूर प्रकट है—“आमवा तेजलीं, महुइया तेजलीं, कटहरवा तेजलीं”, और अंत में बकुले को अपनाने और उसके न रहने की वेदना है—“तोरा के ना तेजलीं बकुलवा।”
भोजपुरी लोककथाएँ गीतात्मक होती हैं। इसमें गीतात्मकता प्रत्यक्षतः अंत में बकुली के विलाप में है। साथ ही, ग़ौर करने की बात है कि कथा की राह में बकुली के समक्ष साथ रहने के तीन पेड़-पात्रों के प्रस्ताव के उत्तर में बकुली ने जो कहा वह तीनों के लिए एक ही है, एक पंक्ति की है और वह लिरिकल है। तीनों पेड़-पात्रों के बकुली से एक ही तरह के सवाल हैं—“बकुली-बकुली कहाँ जालू?” प्रस्ताव भी एक ही तरह के—“हमरा साथे रहबू!” शब्दों की यह मितव्ययिता भी देखनी चाहिए। दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे तीन पेड़ों के साथ कथा के प्रवाह में चौथा पेड़ भी हो सकता है।
बेशक यह बालोपयोगी कथा है। एक ही बात बारम्बार कहने का लाभ यह भी है कि बच्चों को याद रखने में ज़्यादा सुविधा होती है। ‘चिरई और दाल’ की कथा का भी शिल्प कुछ इसी तरह है। ‘अमोला और चंपा’ का भी शिल्प। ‘अझोला’ की कथा का भी। लोककथा के शिल्प की इस ख़ासियत पर अलग से बात होनी चाहिए।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
