‘कई चाँद थे सरे-आसमाँ’ को फिर से पढ़ते हुए
 निशांत कौशिक
13 अक्तूबर 2024
निशांत कौशिक
13 अक्तूबर 2024
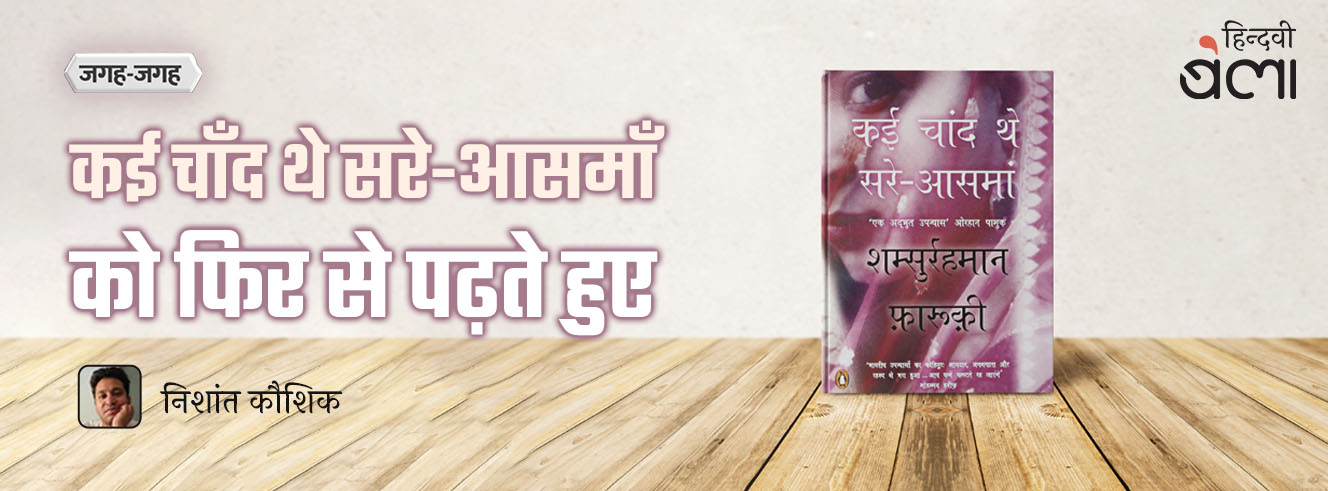
शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी के उपन्यास 'कई चाँद थे सरे-आसमाँ' को पहली बार 2019 में पढ़ा। इसके हिंदी तथा अँग्रेज़ी, क्रमशः रूपांतरित तथा अनूदित संस्करणों के पाठ 2024 की तीसरी तिमाही में समाप्त किए।
तब से अब तक और आगे भी, उपन्यास पर यह चर्चा होती रहेगी कि अपने स्वरूप, योजना तथा विस्तार में यह उपन्यास कितना महत्त्वाकांक्षी एवं बहुआयामी है। इन चर्चाओं में उपन्यास के उद्देश्य और उसके स्वरूप पर बहुत-सी और अक्सर एक-सी बातें हुई हैं। मसलन किस तरह यह हिंद-इस्लामी तहज़ीब का कोलाज और क़ौमी एकजुटता की दास्तान है या फिर मिटती हुई बादशाहत के साये में फलने-फूलने वाली बादशाहत का मंज़रनामा है। गंगा-जमुनी डायनैमिक्स ढूँढ़ने और दुहराते रहने की हमारी आदत न पाठ के साथ न्याय कर पा रही है, न ही किताब के साथ। लिहाज़ा, मैं ये बातें नहीं दोहराऊँगा या उससे बचूँगा।
कुछ एक वर्षों से मैंने शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी के अन्य कामों में रुचि लेना शुरू किया जिसमें उर्दू में विधाओं का वर्गीकरण, उपन्यास तथा लघुकथा की कला, उर्दू लिपि से संबंधित समस्याएँ, उर्दू साहित्य की शुरुआत से संबंधित स्थापनाएँ, ‘शबख़ून’ पत्रिका तथा आधुनिकता संबंधी बहसें।
इन सबसे परिचय के बाद मेरे लिए 'कई चाँद थे सरे-आसमाँ' का पाठ केवल उपन्यासकार द्वारा लिखित एक किताब का पाठ नहीं रह गया। आगे लिखी हुई बातों में मैंने उपन्यास को उसी नज़रिये से दर्शाने की कोशिश की है।
समय
किताब की शुरुआत में वज़ीर ख़ानम और उसके जीवन में घटित घटनाओं के लिए कुछ हवाले और संस्मरण दिए गए हैं। उपन्यास में घटी कुछ अन्य घटनाओं को भी दस्तावेज़ों और याददाश्तों से सत्यापित किया गया है।
शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी पर बात करते हुए यह नुक़्ता अक्सर छेड़ा जाता है कि आलोचना, ग़ज़ल की विषयवस्तु, उपन्यास तथा कहानियों में वह आधुनिकता के पैरोकार रहे तथा इस आधुनिकता को ज़ोर देकर तरक़्क़ीपसंदों की आधुनिकता (प्रगतिशील आंदोलन) से अलग रखते रहे। इसके बावजूद, अपने उपन्यास में वह 150-200 साल पीछे चले गए।
यह दृष्टिकोण दोषपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय कथा के माध्यम से उपन्यास उन विशेषताओं पर ही ज़ोर देता है; जिन्हें हम पूरी तरह आधुनिक न सही, विवेकजन्य ज़रूर कह सकते हैं। यह वज़ीर ख़ानम की अदम्य जिजीविषा और उन्मुक्तता की कहानी है, जिसमें उसे विपरीत परिस्थितियों में विरोधाभासी निर्णय लेने हैं।
किताब में कई ऐसे प्रसंग हैं जहाँ वज़ीर ख़ानम की निष्ठाओं, जीवन मूल्यों और स्वतंत्रता पर फ़ब्तियाँ कसी जा रही हैं। एक ऐसा ही प्रसंग तब है जब दाग़ देहलवी उसे मनाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि वज़ीर ख़ानम के लिए अब कौन-सा क़दम उठाना जरूरी है। वज़ीर ख़ानम स्पष्ट रूप से यह जताती हैं कि पुरुष होने के नाते वह दाग़ के विचारों की थाह, पूर्वाग्रह और सीमा समझती हैं। लेकिन इसी बातचीत के दौरान, उसका ममतामयी पक्ष भी उजागर होता है। एक ही दृश्य में, वज़ीर ख़ानम दो परस्पर विरोधी तत्त्वों के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं। उसके चुनावों और निर्णयों में किसी तरह का ठंडापन या जिए जा सकने की विवशता नहीं, बल्कि अर्थ स्थापित करने की सजग कोशिश है।
उपन्यास की कला
किताब ‘अफ़साने की हिमायत में’ में शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी यद्यपि कथा-उपन्यास की बहस के माध्यम से उर्दू साहित्य में विधाओं के वर्गीकरण की चर्चा को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनका झुकाव उपन्यास की तरफ़ साफ़ दिखता है। दरअस्ल, यह किताब उपन्यास की हिमायत में लिखी हुई प्रतीत होती है, हालाँकि यह कोई समस्या नहीं है।
उपन्यासों के केंद्रीय तत्त्वों और सुविधाओं में से एक उसका विवरण उन्मुख होना है। इसी परिप्रेक्ष्य से देखें तो 'कई चाँद थे सरे-आसमाँ' में घोषित नॉस्टेल्जिया नहीं है; लेकिन जीवन-शैली, वेशभूषा और रहवास पर इतने विस्तृत विवरण हैं कि वे उपन्यास के विशिष्ट होने का कारण और समय के गौरव-गान का प्रमाण स्वतः ही बन जाते हैं।
पंडित नंदकिशोर से वज़ीर ख़ानम की मुलाक़ात होती है, उस ख़ाके में से बानगी देखिए :
‘‘...उस उंगली में गौरैया के अंडे के बराबर सब्ज़-भूरा लहसुनिया, चाँदी की कश्ती जैसी अँगूठी में यूँ चमक रहा था गोया शुक्र ग्रह पर सूरज उग रहा हो।
लहसुनिया की ढाई लकीरें यमन की बर्छी की तरह जगमगा रही थीं। लहसुनिया में एक या हद से हद डेढ़ लकीर होती है। दो लकीरों का लहसुनिया और नायाब, ढाई लकीरों का लहसुनिया एक पूरी बादशाही के ख़िराज से बढ़कर समझा जाता है।’’
इसी तरह उपन्यास के शुरू में किताब के पुराने होने का दृश्य है, उस विवरण से यह हवाला :
‘‘...चमड़ा जहाँ-जहाँ से सूखकर तड़क गया था। बादामी गत्ता उसके नीचे साफ़ नज़र आने लगा था। मैं जब भी कोई लफ़्ज़ देखने के लिए ‘रिशहाते-सफ़ीर’ खोलता तो चमड़े पर हल्की-सी क्रीम या ज़ैतून का तेल ज़रूर फेर देता कि चमड़ा कुछ नर्म हो जाए और उसमें आगे दरारें न पड़ें। यूरोप और अमेरिका वाले ऐसे कामों के लिए बर्फ़ानी लोमड़ी के तेल की बनी गाढ़ी पॉलिश इस्तेमाल करते हैं।’’
देवदार के जंगल, बनी-ठनी (राधा का चित्र), कश्मीर का मौसम, रेगिस्तान से यात्रा, राइफ़ल (रिफ़ल), ठगों के गिरोह और ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ कई सौ शब्द की ज़रूरत होने पर, लेकिन सूक्तियों से चित्र खींचे गए हैं। उपन्यास का बेशतर हिस्सा इन घटनाओं तथा दृश्यों के दिलचस्प विवरण में ख़र्च होता है।
भाषा
(...कि गुज़रा हुआ ज़माना एक अजनबी मुल्क है और बाहर से आने वाले इसकी ज़बान नहीं समझ सकते। वो कहते थे कि पुराने लफ़्ज़ों को नए लफ़्ज़ों में बयान किया जा सकता है बस हम-आहंगी और हम-आग़ोशी चाहिए।)
— ख़लील असग़र फ़ारूक़ी की याददाश्तों से, ‘कई चाँद थे सरे-आसमाँ’
किताब ‘उर्दू का इब्तेदाई ज़माना’ में शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी ने उर्दू को उसके प्रचलित अर्थ (छावनी, कैम्प) से मुक्त करने का सैद्धांतिक प्रयास किया। उस किताब में वर्णित स्थापनाएँ अभी भी अकाट्य ही हैं; लेकिन उन बातों की पुष्टि या खंडन मेरा विषय, रुचि तथा क्षेत्र नहीं। इस तरफ़ ध्यान दिलाना ज़रूरी हो जाता है कि भाषा ही इस उपन्यास में समय को स्थापित करने का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।
‘कई चाँद थे सरे-आसमाँ’ की भाषा पर बात करते हुए उपरोक्त पहलू सबसे अहम है। कहानी के लगभग 40-50 सालों के इस कालक्रम में फ़ारूक़ी बहुत सावधानी से रेख़्ता, हिंदी, गूजरी जैसे शब्दों का ऐतिहासिक क्रम में इस्तेमाल करते हैं। विलियम फ़्रेज़र के घर की दावत, जहाँ मिर्ज़ा ग़ालिब अपना फ़ारसी कलाम सुना रहे हैं; दाद पाकर कुछ ‘हिंदी’ कलाम प्रस्तुत करते हैं। अगर मेरी याददाश्त सही है, लगभग 600 पृष्ठों तक ‘उर्दू’ शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। यही सावधानी अँग्रेज़ी शब्दों के साथ भी बरती गई है, जैसे एक जगह कथा के बीच में ‘लैंटर्न’ शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कोष्ठक में यह सूचना है कि ‘लफ़्ज़ लालटेन अभी चला न था’।
हुक़्क़ा या शीशा जैसे शब्द भी जो पुराने सुनाई पड़ते हैं, उपन्यास के आख़िरी के कुछ अध्यायों में पढ़ने में आते हैं। उनकी जगह भिंडा, मुँहनाल, फ़तहपेच, पेचवान या फ़र्शी जैसे शब्द दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह अमीरून्निसा बेगम से वज़ीर ख़ानम की बातचीत में ‘सुलट लेंगे’ इस्तेमाल हुआ है।
गुजरात, कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा (मेवात, लोहारू) सभी जगहों के पात्र अपनी भाषा में इलाक़ाई तथा समय की छाप लिए हुए हैं। जहाँ भी चलन से हटती हुई भाषा का इस्तेमाल हुआ है, वहाँ फ़ौरन एक सूचना चस्पाँ है कि उसकी भाषा में मेवाती, पहाड़ी, कश्मीरी, अवधी या पंजाबी की झलक थी।
एक उदाहरण यह देखिए :
‘‘लेकिन रदीफ़ हो ज़रा ठनकती वी सी कि घोड़े की तरियों कड़क दौड़ती हुए जाए, ज़रा इन मियाँ साहब को पता लगे कि रामपुर से पोइयाँ-पोइयाँ क्योंकर दिल्ली आते हैं...’’
लोग, पहचानें और समुदाय
किताब में कई घटनाएँ कथानक को धक्का देकर अचानक आगे बढ़ा देती हैं। वह उपन्यास के पहचानी हुई गति, तथाकथित एवं अपेक्षित उद्देश्य और अनुमान को धता बताती हैं। इन सभी की पहचानें हैं, मान्यताएँ हैं, उद्देश्य हैं और कहानी इन सभी की मौजूदगी के प्रति आलोचनात्मक या पूर्वाग्रही दृष्टि नहीं बरतती। कुछ उदाहरण ये हैं :
‘‘...तो तुम लोग मुसलमान नहीं हो? मुहम्मद याहया ने पूछा।
जी नहीं, हम में से कुछ चितेरे हैं, कुछ मीरासी हैं। हम लोग औरतों, मर्दों की तसवीरें बनाते या बंगाल के राजा गोपीचंद और उज्जैन के राजा भरथरी की गाथाएँ सुनाते हैं।’’
‘‘नस्ल के लिहाज़ से उन्हें ‘सीदी’ और काम के एतबार से ‘खोजिया’ कहा जाता था और वो क़दम के निशान पहचानने, फ़रारों का पता लगाने और लापता चीज़ों को ढूँढ़ने में महारत रखते थे। हालाँकि शुरू-शुरू में वो अफ़्रीका के साहिलों से ग़ुलाम की तरह गुजरात और दकन में लाए गए थे। ...उनकी क़दर पहचानने वालों का दायरा देहली, अवध और रुहेलखंड तक फैल गया था। ...आपस में वो अब भी स्वाहिली बोलते थे, कभी-कभी गुजराती; लेकिन ज़्यादातर गूजरी यानी हिंदी में बात करते थे।’’
इसी क्रम में किशनगढ़ के चित्रकारों, कश्मीर के चित्रकारों, ठगों और उनकी महाकाली पर आस्था तथा अन्य मान्यताओं, पहेलीबाज़ों आदि का विस्तृत ज़िक्र है और ‘रिफ़ाई रातिबदारों’ का भी जो जानलेवा खेल करते-दिखाते थे, सदियों पहले इराक़ से आए थे और सूफ़ी सिलसिला के सदस्य थे।
शाइरी
‘कई चाँद थे सरे-आसमाँ’ में बेशुमार अश’आर, ग़ज़लें, क़ता, रुबाइयाँ और नौहे (शोक-कविता) हैं। इनमें से अधिकतम फ़ारसी में हैं। सिवाय कुछ जगहों पर वह शे’र मिलते हैं जिसकी भाषा हम उर्दू/हिंदी कह सकते हैं।
फ़ारसी की ग़ज़लों और अश’आरों में अविश्वसनीय विविधता है। जीवन के लगभग हर पहलू में यहाँ तक कि अंतरंग प्रसंगों में भी पात्र एक दूसरे को फ़ारसी में शे’र सुना रहे हैं।
भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी के लिए हाफ़िज़ का दीवान खोलकर उसके किसी शे’र के अर्थ से जीवन की गुत्थियाँ खोल रहे हैं। मिर्ज़ा फ़ख़रू के साथ अंतरंग प्रसंग में हाफ़िज़ की एक ग़ज़ल ऐसी वर्णित है, जिसका एक मिसरा फ़ारसी में है और दूसरा अरबी में :
‘‘दारम मन अज़ फिराक़त दर दीदा सद अलामत
लैसत दमूऊ-ऐनी हाज़ा लनल अलामह’’
(मेरी आँखों में तुम्हारे बिछोह की सैकड़ों निशानियाँ हैं। क्या मेरी आँख के आँसू हम आशिक़ों के लिए इसकी निशानी नहीं है।)
हमारे सबसे परिचित और पढ़े गए शाइर भी वह अश’आर सुना रहे हैं जो हमने नहीं पढ़े या सुने होंगे। इसमें फ़ारसी के शाइरों के अलावा ख़ुद ग़ालिब और दाग़ भी शामिल हैं। विलियम फ़्रेज़र की मौत पर ग़ालिब का यह शे’र देखिए :
ग़ालिब सितम निगर कि चूँ विलियम फ़्रेज़रे
जीं सां ज़ चीरादस्ती-ए-आदा शवद हलाक
(ऐ ग़ालिब, ये अत्याचार तो देखो कि विलियम फ़्रेज़र जैसा शख़्स दुश्मनों की बर्बरियत के हाथों मारा जाए।)
फ़ारूक़ी और मीर तक़ी मीर
शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी का मीर पर काम प्रतिष्ठित और चर्चित है। उनकी आलोचनात्मक क़वायदों का बहुत बड़ा हिस्सा मीर पर केंद्रित या उसके हवाले से है। इस क़वायद के कई रंग हैं। इसमें एक रंग यह भी है कि मीर के काव्य और उसकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना में तत्कालीन राजनीतिक पहलुओं पर भी ग़ैरमामूली ढंग से रोशनी डालते हैं। उपन्यास में उन्होंने गाहे-बगाहे मीर का ज़िक्र किया है और जब भी किया है, सभी शाइर और बाशिंदे मीर के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते दिखे हैं। उपन्यास के अंत में दाग़ से जुड़ा हुआ यह प्रसंग देखिए :
‘‘...दाद के डोंगरों के बीच दाग़ ने मक़्ता पढ़ा :
होशो हवासो-ताबो-तवाँ दाग़ जा चुके
अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया
जब दाद का शोर कुछ थमा तो एक बुज़ुर्ग ने फ़रमाया, “सुब्हानल्लाह, यह उम्र और यह शेर!’’
एक और साहब ने हँसकर कहा, “साहबजादे, अभी तो नामे-ख़ुदा उठती जवानी है, अभी से यह मज़मून कहाँ से सूझ गया?”
“जी, मैं अर्ज़ करूँ?” ढलती उम्र के एक शख़्स ने, जो सूरत से किसी मदरसे के मौलवी मालूम होते थे, ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा।
“ज़रूर, मौलवी साहब, ज़रूर फरमाएँ" मजमे से आवाजें आईं।
मौलवी साहब ने खँखारकर कहा, “अजी हज़्ज़त, यह मज़मून ख़ुदा-ए-सुख़न मीर तक़ी साहब मीर साहब का है।” फिर उन्होंने नीचे के शे’र पढ़े :
क्या फ़हम क्या फ़िरासत ज़ौक़-बसर समाअत
ताबो-तवानो-ताक़त ये कर गए सफ़र अब
मंज़िल को मर्ग की था आख़िर मुझे पहुँचना
भेजा है मैंने अपना असबाब पेशतर सब
एक पल के लिए ख़ामोशी छा गई। फिर नवाब मुस्तफा ख़ाँ शेफ़्ता ने फ़रमाया, “भई, यह तो दुरुस्त है कि मीर साहब इस मज़मून को पहले बाँध गए हैं, लेकिन मियाँ दाग़ के मक़्ते में एक बरजस्तगी है जो बहुत भली मालूम होती है...”
प्रसंग आगे और हैं, लेकिन इसकी समाप्ति इस बात से होती है :
‘‘...आम तौर पर लोगों का ख़याल था कि दाग़ ने अगर चोरी भी की तो बड़े लुत्फ़ के साथ और उसका इल्ज़ामी जवाब भी ख़ूब था।’’
उपन्यास के अनुवाद
अनुवाद ने इधर जिस तरह की गति पकड़ी है और जिस तरह की संस्कृति उसके इर्द-गिर्द पिछले एक दशक में पनपी है, वह तसल्लीबख़्श है।
शम्सुर्रहमान फ़ारूक़ी ने ‘कई चाँद थे सरे-आसमाँ’ को लगभग 960 पन्नों में अँग्रेज़ी में स्वयं ही अनूदित किया। इतनी विशाल परियोजना पर काम करने की उनकी रुचि, क्षमता, साहस और ऊर्जा निस्संदेह प्रशंसनीय है। उन्होंने अनुवाद में उस समय के Idiom का ख़ास ध्यान रखा है। अँग्रेज़ी अनुवाद में शब्दों, उनकी व्युत्पत्ति तथा चलन का बहुत ध्यान रखा गया है, और यही सावधानी उपन्यास में ग़ज़लों और शे’रों के अनुवाद में भी देखी जाती है।
वे कभी-कभी 'कनीज़' का अनुवाद 'Servitor' के रूप में करते हैं, और कहीं-कहीं उचित ही शाब्दिक अनुवाद मिलेंगे जैसे जबकि वज़ीर ख़ानम के साथ चर्चा के दौरान हबीबुन्निसा उससे कहती है, ‘‘We are your Salt-eater.’’ इसी तरह मल्लिका-ए-दौराँ का अनुवाद The queen of the age किया गया है।
दुख की बात यह है कि अँग्रेज़ी के इस अनुवाद को जितनी सराहना मिली है, उर्दू से हिंदी में अनुवाद को उतनी प्रशंसा नहीं मिली। नरेश नदीम ने सराहनीय काम किया है और जिन्होंने उपन्यास के उर्दू और हिंदी दोनों संस्करण पढ़े हैं, वे जानते हैं कि इस जटिल और शास्त्रीयता से भरे टेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। यद्यपि मैंने ऊपर इसको ‘रूपांतरण’ कहा है, किंतु कई पद सीधे-सीधे हिंदी में अनूदित हैं। बाग़-ए-वस्ल को मिलनबाड़ी कर सकना एक दिलचस्प दिखता प्रयास है। उतना ही ध्यान फ़ारसी और हाफ़िज़ की वर्णित ग़ज़ल (अरबी-फ़ारसी) ग़ज़ल के अनुवाद में भी रखा गया है।
और अंत में, वे सारे हिस्से, वर्णन या दृश्य जिसको पाठक तोलस्तोय, थॉमस मान और प्रूस्त के यहाँ चाव से पढता है; यही पाठक और लेखक भारत पहुँचते-पहुँचते ‘कला के उद्देश्य’ के घोड़े पर सवार हो जाता है और फिर न कला घोड़े से उतर पाती है न लेखक। यह कहे बग़ैर आलेख समाप्त नहीं होगा कि यह उपन्यास भारतीय उपन्यासों के इतिहास में एक उपलब्धि है और अपने कैनवास में विश्व साहित्य की कई कृतियों से बराबरी या बरतरी का दर्जा रखता है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
