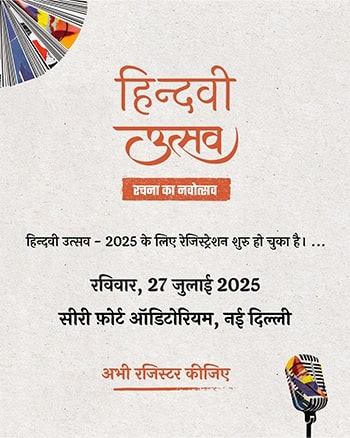सिनेमा पर सिनेमा सिनेमा लेखन
सिनेमा ऐसा कला-रूप है
जहाँ साहित्य, संगीत, अभिनय, नृत्य जैसे कलासिक कला-रूपों के साथ ही फ़ोटोग्राफी, एनीमेशन, डिजिटल एडिटिंग, ग्राफ़िक्स जैसे अन्य आधुनिक कला-रूप प्रतिबिंबित होते हैं। आधुनिक समाज और सिनेमा का अनन्य संबंध देखा जाता है, जहाँ दोनों एक-दूसरे की प्रवृत्तियों का अनुकरण करते नज़र आते हैं। इस चयन में सिनेमा विषयक कविताओं का संकलन किया गया है।
1. 1896 में, लुमियर के आविष्कार के भारत में प्रदर्शन के बाद सिनेमा को उत्साह के साथ अपनाने में देश को कोई ज़ियादा वक़्त नहीं लगा। 1913 में दादा साहब फाल्के पौराणिक फ़िल्म बना चुके थे। आगामी तीन वर्षों में देश के अन्य भागों में और भी फ़िल्में बनीं। शताब्दी के मध्य में भारत दुनिया का सबसे बड़ा कथा-चित्र निर्माता देश बन गया। सिनेमा ने लोगों के सबसे बड़े और इकलौते मनोरंजन माध्यम के रूप में जगह बना ली। टेलीविज़न द्वारा इसकी महत्वपूर्ण जगह ले लेने के पहले इसके इतिहास में संचार के जन-माध्यम के रूप में देश की पंद्रह फ़ीसदी से भी कहीं अधिक जनसंख्या तक पहुँचने की इसने विशेषता अर्जित कर रखी थी।
2. मनोरंजन के प्रमुख माध्यम के रूप में विकसित होकर सिनेमा ने पौराणिक, ऐतिहासिक प्रेम कथाओं, गीत, नृत्य और अन्य मनोरंजन के पारंपरिक रूपों के ख़ास तत्वों को समाहित कर लिया। ये सभी सफलतापूर्वक या सफलतापूर्वक नहीं; फ़िल्म माध्यम में अनुकूलित कर लिए गए। फ़िल्मों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण में तकनीकी के समावेश ने इसे नागर माध्यम बना दिया। इसलिए सिनेमा के लिए स्वाभाविक ही था कि वह नागर संवेदना को रूपायित करे। इस संवेदना की अनुगूँज दर्शकों में पाई गई जो कि सर्वाधिक तौर पर शहरी थी। यदि आप फ़िल्मों को देखें, ख़ासकर शताब्दी के पहले चार दशकों की, तो अधिकांश फ़िल्मों की विषय-सामग्री की अभिकल्पना नागर भारत की मनोरंजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की थी। तो भी, वहाँ कुछेक अपवाद भी हैं। यह भारत के उन हिस्सों में हुआ जहाँ सिनेमा अर्द्धनगरीय और कुछ हद तक ग्रामीण जनसंख्या तक पहुँच सका। मराठी, तेलुगु और तमिल भाषा की कुछ फ़िल्में ग्रामीण लोकाचार को प्रतिबिंबित कर सकीं। पर फिर भी, इस दौर की अधिकांश फ़िल्में नागर भारत के सामाजिक और वैयक्तिक सरोकारों को प्रतिबिंबित कर सकीं, परिवार व्यवस्था की पवित्रता, राष्ट्रीय पहचान, प्रजाई औद्योगिकीकरण से प्रसूत अव्यवस्था और सामाजिक आदर्शों का निरंतर प्रबलीकरण जो ग्रामीण से नगरीय अस्तित्व में अभिघातज भय में प्रकट होता है।
3. स्वतंत्रता के बाद यह सब नाटकीय ढंग से बदल गया। औद्योगीकरण के प्रसार, जनसंख्या के दौड़-पथ में विस्तार और इसकी शहरों में बाढ़, नागर शहरी क्षेत्रों के पूरे देश में अंकुरण से सिनेमा दर्शकों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस बढ़ी हुई दर्शक संख्या की अपेक्षाओं को पूरा करने में फ़िल्मों का चरित्र ही बदल गया। अत्यंत विपरीत आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले नितांत अलग-अलग नए दर्शकों के लिए एक आम हर का विचार करना पड़ा। फ़िल्मों ने दर्शकों में हुए परिवर्तन को प्रतिबिंबित करना आरंभ कर दिया। आख़िरी तीन दशकों में पुराने कथा-तत्व और पारंपरिक कहानी के प्रति आग्रह बदल गए और नए सनसनी तत्वों पर भरोसा करने के पर ज़ोर दिया जाने लगा। तत्वों, अभिनय की स्थूलता, हिंसा, सेक्स और बर्बरता पर आसान पहचान के लिए भरोसा करने पर भी ज़ोर बढ़ा, बनिस्बतन आरंभिक संवेदी स्तर के। दूसरे शब्दों में, वहाँ संवेदनाओं का ‘लुंपेन’ आकांक्षाओं की ओर एक सामान्य पतन था। वहाँ इस अधोगमन के लिए अनेक वजहें थीं। यहाँ मैं उन पर नहीं जाऊँगा क्योंकि इनके लिए भी एक आवश्यक गहराई के साथ विचार करना होगा। यह कहना पर्याप्त होगा कि भारत पर उपनिवेशवाद के अत्यंत गहरे प्रभाव और असर के कारण हम ख़ुद अपने आपको एक उपनिवेशवादी निगाह से देखने लगे हैं। इसका सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम यह रहा कि हम अपनी परिस्थितियों का सहज और मूलभूत तरीक़ों से सामना करने में असफल रहे। इससे स्पष्ट है कि हम पुराने विचारों से कटकर, जिनकी अब कोई ज़ियादा विश्वसनीयता भी नहीं रह गई है, न ही मौलिक अवधारणाएँ, विचारधाराएँ, दर्शन रच सके हैं और हमारा रुझान महज़ पश्चिम से हरेक चीज़ की साहित्यिक चोरी या नक़ल का रह गया है। इसका जो सर्वश्रेष्ठ है, वह यह कि राष्ट्रीयता की हमारी अवधारणा और प्रजातंत्र के अधिमान पश्चिम से ही आए हैं और इसका जो सबसे निकृष्ट है कि इसने हमें एक दोयम दर्जे की संवेदना में विकसित किया है। हमारी फ़िल्में निरंतर रूप से इस पक्ष का प्रदर्शन करती हैं। जब वे किन्हीं कहानियों, कथानकों, थीम या विचार का प्रयोग करती हैं तो वे तत्काल ही कोई नक़ल या साहित्यिक चोरी हैं। इस मापदंड से सर्वाधिक रचनाशील मनोवेग धकिया दिए गए हैं, जिसका अंतिम परिणाम प्रामाणिक अभिव्यक्ति की कमी ही होगा।
1950 के दौरान बंगाल के कुछेक फ़िल्मकारों ने, जिनमें सत्यजीत राय सबसे प्रमुख थे, इसे दो-टूक महसूस किया था। दृश्य में आगे दो दशकों के बाद मेरा अपना अनुभव भी वही था। देश की मुख्यधारा की फ़िल्में किन्हीं निजी या सामाजिक सरोकारों की अभिव्यक्ति में निरी असफल थीं। ये केवल फ़ॉर्मूलों से अभिभूत दिखाई देती थीं और ख़ुद को नक़ल से नया बनाती थीं। यथार्थ के अभाव ने मुख्यधारा सिनेमा को अपने उद्देश्यों में चालबाज़ बना दिया। इसकी सबसे बड़ी सफलता इसी में थी कि इसने अपनी चालबाज़ियों के निष्पादन में दर्शकों को भी सहयोगशील बना लिया था। इस प्रकार मुख्यधारा सिनेमा का निर्माण पूर्णतः शोषण है।
परिस्थिति एक नई संवेदना, एक नए कथ्य और एक नए रूप के लिए तरस गई। मनोरंजन को उस घेरे से पुर्नपरिभाषित किए जाने की ज़रूरत थी जिसमें यह जकड़ लिया गया था। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों के प्रति फैली उदासीनता से लड़ने की ज़रूरत थी। यह भावना बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं लेकिन हमारे समाज में बहुत लंबे समय से महसूस की जाती रही। सिनेमा में यह दिखना आरंभ हुई बंगाल में 1950 में, बाद में केरल और कर्नाटक में 1960 के उत्तरार्द्ध में और हिंदी सिनेमा में 1970 में। सफलता के परिवर्तित होते अंशों के साथ नए सिनेमा ने हमारे समाज और संस्कृति में हो रहे परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया से आरंभ किया। आज चीज़ें जैसी हैं, इसका थोड़ा बहुत गतिबल ख़त्म हो गया नज़र आता है, लेकिन यह असफलता आंदोलन की उतनी नहीं है जितनी यह इसका एक 'विकास’ है। व्यक्तिशः फ़िल्मकारों के सरोकार ज़ियादातर अपने तक ही सीमित हैं, ब-निस्बतन अपनी निजी आवाज़ें खोजने के। संभवतः प्रक्रिया में, वे शायद नए सौंदर्यशास्त्रीय सिद्धांतों को रच सकें और मौलिक ढंग से सिनेमा शब्दकोष को विस्तृत कर सकें, जिससे भारतीय सिनेमा की दृढ़ बुनियाद रखी जा सके।
इस प्रकार, मैंने मुख्यतः बतौर मनोरंजन माध्यम भारतीय सिनेमा के इतिहास और विकास पर विचार किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ़िल्म माध्यम अनेक उपयोगों के लिए समर्थ है। और सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इसका सूचनात्मक और शैक्षिक उपयोग हो सकता है। कोई कह सकता है कि इसका निदेशात्मक उपयोग भी है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत शासन ने राष्ट्र और राज्य, दोनों ही की जनता को सूचना देने के लिए फ़िल्म माध्यम का उपयोग करने के लिए फ़िल्म्स डिवीज़न की स्थापना की, साथ ही साथ त्वरित विकास के अर्थों में विकासात्मक प्रक्रिया में सहयोग के लिए भी फ़िल्म का वृत्तात्मक रूप या सृजनात्मक अर्थों में यथार्थ के प्रतिनिधित्व के लिए फ़िल्म का संभावित उपयोग इस उद्देश्य के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। दुर्भाग्यवश, यह उद्देश्य बड़े पैमाने पर अपूरित ही रह गया। यहाँ इसके कारण बहुत ही साधारण से हैं। यदि वे पूरे हुए भी तो बहुत ही सतही तौर पर सूचना प्रदान करने की जगह प्रचार पर ज़ोर दिया गया। राष्ट्रीय योजनाएँ और कार्यक्रम बड़े विस्तार के साथ उजागर किए गए लेकिन क्रियान्वयन की समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। सफलता का दावा वहाँ किया गया जहाँ कुछ था ही नहीं। सूचना की अवधारणा एक दुर्घटना के रूप में सामने आई।
तो बिल्कुल कभी-कभार, यदि हुआ भी तो विकासात्मक प्रक्रिया प्रतिबिंबित हुई, इसका समाज पर प्रभाव सामाजिक क्रांति और परिवर्तन ये सब अनिवार्य रूप से इसके परिणामस्वरूप उभरना ही चाहिए। न उपयोगी दृष्टिकोण, न ही राजनीतिक युक्तिकरण, न ही सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों में उनका रूपांतरण कभी संभव हुआ। कुछेक फ़िल्मों ने इसकी कोशिश भी की तो वे या तो निरस्त कर दी गईं या फिर जारी होने से ही रोक दी गईं। सिनेमा एक निदेशात्मक माध्यम है, इसीलिए यह जनता द्वारा अप्रतिष्ठित ही रह जाता है। वृत्तचित्र की अनुक्रिया पूर्णतः नगण्य है और इसीलिए दिलचस्पी में पूर्णतः कमी भी है। फिर भी, 1960 के उत्तरार्द्ध में और 1970 के पूर्वार्द्ध में एक दौर रहा है जब फ़िल्म्स डिवीज़न में उल्लेखनीय काम हुआ है। यह तब ही हुआ जब इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहकर काम कर पाना संभव हुआ। वृत्तचित्र के रूप में फ़िल्म का निदेशात्मक इस्तेमाल तब भी संभव है जब यह जनता के लिए सुगम हो। इसमें लोगों की सहभागिता अनिवार्य है। यह एक उत्प्रेरक के रूप भी हो सकती है, तब जबकि इसमें जनता बतौर विकासात्मक प्रक्रिया शिरकत करे। मेरी नज़र में, वृत्तचित्र के लिए जो अकेला भविष्य बचा हुआ है तब जबकि समुदाय इसके निर्माण में बिना सरकार पर निर्भर या भरोसा किए शिरकत करे। ऐसी फ़िल्मों में से जो उल्लेखनीय फ़िल्में हैं, वे हैं आनंद पटवर्धन की ‘बॉम्बे: आर सिटी’ और सुहासिनी मुळे की ‘भोपाल ट्रेजेडी’। हाल ही में टेलीविज़न के लिए भी बहुत उत्कृष्ट काम हुआ है। उनमें उल्लेखनीय नलिनी सिंह के दो वृत्तचित्र- ‘बूथ कैप्चरिंग’ और ‘भागलपुर रायट्स’ हैं।
इसके बाद हम टेलीविज़न पर आते हैं। जब टेलीविज़न भारत आया, या कहें कि दिल्ली में, कोई तीन दशक पहले, तब इसके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट थे—माध्यम का उपयोग सूचनाओं के प्रसार, शिक्षा के प्रचार, और उसी क्रम में मनोरंजन की उपलब्धता के लिए। समय के साथ यह आज की स्थिति में विकसित हुआ। लक्ष्य तो वही बने रहे लेकिन आज यथार्थ पूरी तौर पर बदल गया है। सिनेमा से अलग भारत में टेलीविज़न पर राज्य का एकाधिकार हुआ और वह देश की राजधानी में केंद्रीभूत हो गया है। यह दोनों ही, एक तरफ़ लाभ भी है और साथ ही साथ भारी हानि भी—यह हानि देश की जनता से संबद्ध है। भारत एक जटिल विभिन्नताओं का देश है। इसकी सांस्कृतिक विभिन्नताएँ एक वर्णक्रम में महसूस नहीं की जा सकतीं। भारत में टेलीविज़न का उपयोग जिस तरह होता है, वह एकाश्मक और एक समांगी शक्ति के रूप में दिखार्इ पड़ता है। दुर्भाग्यवश यह ठीक वैसा ही नहीं है। इसके प्रोजेक्शन का तरीक़ा आरोपण का है और इसका संदेश सभी के द्वारा समानुरूप ढंग से नहीं लिया जाता। मुझे स्पष्ट करने दीजिए कि कोई भी संचार, ग्रहिता की समझ के स्तर पर ही ग्रहण होता है।
शब्द संसार की निकटता से ही संचार को और अधिक पूर्णता मिलती है। एक केंद्रीभूत संचार प्रणाली भारतीय टेलीविज़न की तरह अक्सर अनपेक्षित तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे संकेत हैं, वे उससे अलग जिस पर्यावरण में ग्रहीत किये जा रहे हैं, उसमें ही पठित होते है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता वस्तुओं का गाँवों में विज्ञापन।
तो उनके उद्देश्यों पर फिर से लौटें। कोई सूचनात्मक या शैक्षिक संचार तब सर्वश्रेष्ठ काम करता है जब द्विपथ संचार हो। टेलीविज़न को इन क्षेत्रों में एक मूल्यवान उपकरण होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि विकेंद्रीकरण हो और वह दर्शकों के लिए सुगम हो। टेलीविज़न द्वारा समुदायों और समूहों के लिए कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए कि वे इनमें शिरकत कर सकें। जैसा कि यह यथार्थ में है, उससे कहीं अधिक क्रांतिकारी लग सकता है। आज टेलीविजन में जो हो रहा है, वह दो कारणों से हो रहा है। कोई सरकार सत्ता में आने के बाद देखती है कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग स्थायीकरण के लिए किया जा सकता है। दूसरे, विशाल दर्शक समुदाय की अपेक्षाओं को परिपूरित करने के लिए कार्यक्रमों को लोकप्रिय मिज़ाज का बना दिया जाता है। चाहे कोई इसे पसंद करे न करे लेकिन कार्यक्रमों का अधिक लोकप्रियकरण, उससे अधिक राजस्व की आमदनी और ठीक इससे उलट भी। इससे मुक्त हो पाना अब मुश्किल हो गया है। इन दबावों से एकबारगी इसमें फँस सकते हैं, परिणामस्वरूप टेलीविज़न देश में सबसे बड़े मनोरंजन माध्यम के रूप में उभर आया है। और एक बार फिर मनोरंजन, जैसा कि सिनेमा द्वारा परिभाषित किया गया है। क्या टेलीविज़न स्वतः इससे मुक्त हो सकता है?—संभवतः यह सवाल के रूप में भी उपस्थित नहीं है। क्या टेलीविज़न इस परिस्थिति से स्वतः बाहर निकल आना चाहता है? मैं सोचता हूँ कि नहीं, क्योंकि जो राजस्व मिल रहा है, वह अविचारणीय नहीं है। क्या कुछ किया जा सकता है? मुझे विश्वास है कि परिस्थिति बदली जा सकती है। शुरूआत के लिए गुणवत्ता के मानदंड बदलना चाहिए। आरंभ के लिए, गुणवत्ता के मानदंड स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। एक पीठ (Bench) चिन्ह जैसा कि यह था। यह सब करने के क्रम में एक सौंदर्यशास्त्रीय और बौद्धिक विशेषता के कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता है। हमेशा इसे किसी संस्थान पर, बतौर दूरदर्शन या सरकार के करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। यह फ़िल्म और टेलीविजन निर्माताओं द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए टेलीविज़न में मेरा काम समर्पित रहा है। हमें मानदंड बनाने होंगे, चाहे वे मनोरंजन में हों या शिक्षा में।
अनुवाद: श्रीराम तिवारी (लेखक, संपादक और अनुवादक। ‘पटकथा’ पत्रिका के संपादन में योगदान।)
हिंदुस्तान की जो दार्शनिक पद्धतियाँ हैं उनमें जिसे हम आत्म कहते हैं, वह बहुत अलग है, वह इन सब सृष्टियों से परे है जो आदमी प्रकट कर रहा है। प्रकट तो वह प्रकृति के माध्यम से करता है। उसे प्रकृति कह लीजिए या पारंपरिक तौर पर माया कह लीजिए, उसी के माध्यम से प्रकट करता है। भ्रम प्रकट करने का एक साधन है। माया एक साधन है। समझे तो मज़ा ही इसी ‘भ्रम’ में है, चाहे वह फ़िल्म हो चाहे कविता हो। हरेक में सृजनात्मकता का एक ऐसा भ्रम यानी एक सृष्टि का ऐसा भ्रम है कि भ्रम के बग़ैर वह रची ही नहीं जाती और जो सेल्फ़ की कल्पना है वहाँ ऐसा कोई भ्रम नहीं है। वहाँ ऐसा सब कुछ नहीं है। इन दोनों में सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन है। जो पश्चिम की परंपरा से वाक़िफ़ हैं−और यह परंपरा सारी दुनिया में चल रही है−वो यह परेशानी महसूस करते हैं। उनके लिए यह सामंजस्य बैठाना मुश्किल है : ऐसा सेल्फ़ जिसमें कुछ नहीं है जो सब चीज़ों से परे है और जिसकी शुरूआत और अंत का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन तब भी है। अपने आप में अनुभव−मात्र है। एक तरफ़ ऐसा सेल्फ़ और दूसरी ओर सृजनात्मकता का आनंद। तरह-तरह की सृजनात्मकता का आनंद, पेंटिंग में, संगीत में, लेखन में।
यह आनंद आदमी को समझ से आता है। एसा हमने सुना है। जब वो कोई चीज़ समझ जाता है तब उसे उसका आनंद महसूस होता है। हमें समझना यह है कि तभी आदमी को आनंद महसूस होता है, जैसे बच्चे को भी कोई चीज़ समझ में आ जाए तो हँस पड़ेगा। मुझे लगता है कि फ़िल्म में और संगीत में भी कोई चीज़ जब समझ में आ जाती है तो आनंद महसूस होता है। इसको और सेल्फ़ के विचार को जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो कभी ऐसी कोशिश तक नहीं की। मुझे लगता है कि आत्म की अंतर्निष्ठता वो है जिससे आपकी सृजनात्मकता का बहुत सीधा तअल्लुक़ हो सकता है। अगर कोई ऐसा अंतर्निष्ठ सेल्फ़ है तो हमें लगेगा कि वह वही सृजन कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कलाकार में जो रचा रहा है उसे कलाकार का ‘मैं’ कहा जा सकता है। हमें लगता है कि कलाकार के जितने विचार हैं वे बिना बुलाए आ जाते हैं। ‘मैं सोच रहा हूँ’ इससे कुछ बनता नहीं है। आपने एक ऐसा सवाल छेड़ दिया है जो आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है। उसका कोई रूप नहीं है, वह कुछ नहीं है, उसको किसी भी चीज़ से बाँधना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए कि वह ‘मैं’ नहीं है तो किस तरह से वह सृजन करता है, यह जानना भी बहुत मुश्किल है। आपका अंतर्निष्ठ सेल्फ़ का जो विचार है उसमें आप सेल्फ़ की परिभाषा क्या देते हैं?
आनंद किसका है−सेल्फ़ का अपना अथवा विषय की उपलब्धि का? जब तक समझ नहीं रहा, एक विचलित अवस्था रहती है। समझते ही शांत हो जाती है−उस क्षण के लिए कम-से-कम, आनंद उस शांति से जुड़ा है। ऐसी बुद्धियाँ भी होंगी जो विचलित होती ही नहीं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे किसी व्यापक आनंद में व्यस्त हैं। विचलित होने से ही शांत समझना। आनंद में तो न विचलित न शांत। आकांक्षा विचार से पूर्व है। पूर्व विचार। जन्म से ही सिद्ध है। बच्चा, आदमी का अथवा जानवर का, सीधा माँ से स्तन को ढूँढता है, जन्मते ही। आकांक्षा को समझने के लिए इसे एक तरह मान लें। बच्चे और स्तन को। आकांक्षाओं के सिद्ध होने और न होने में ही विचार छिपा है। न होने में अधिक, यदि वह उस दु:ख के प्रण को सह ले। विचार में समझ, समझ में आनंद। एक वाक्य है : अच्छा लगता है। इसके तीन भाग हैं। एक ‘है’ दूसरा ‘लगता है', तीसरा ‘अच्छा लगता है’। ‘अच्छा’ ‘लगता है’ तक पहुँचा देता है।