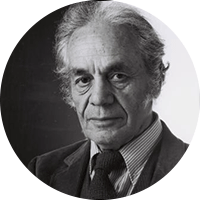सोचो, बच्चो,
कैंसर-घुनी इस जबान के बारे में ज़रा सोचो!
मैं एक गुमनाम-से स्कूल में मुदर्रिस हूँ
और क्लासों में पढ़ाते-पढ़ाते मैंने अपनी आवाज़ खो दी है
(वैसे, कहने को, मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ और मेरे काम का हफ़्ता
महज़ चालीस घंटे का है)।
और भला, थुर-थुर कर पिचका डाले गए
मेरे बदशक्ल चेहरे से क्या ज़ाहिर होता है?
सच, मेरी तरफ़ देखोगे तो परेशान हो उठोगे।
और भला, खड़िया की झरती सफ़ेदी से सड़ी-बुसी
मेरी नाक के बारे में तुम्हारा क्या कहना है?...
अब मेरी आँखों पर आओ!
पता है, महज़ तीन गज की दूरी से
मैं अपनी माँ तक को नहीं पहचान सकता—
जिसने मुझे पैदा किया है!
यह...यह मुझे हो क्या गया है?
शायद कुछ ख़ास नहीं—
क्लासों में पढ़ाते-पढ़ाते दरअस्ल मैंने अपनी आँखें गवाँ दी हैं :
धुँधली रोशनी—तपता सूरज
मनहूस और ज़हरीला चाँद...
और यह सब किसके लिए?
—महज़ एक रोटी की मजबूरी के लिए—
रोटी, जो एक महाजन के चेहरे जैसी ऐंठी हुई और बेस्वाद है
जिसमें बस्स् ख़ून की गंध और ख़ून का ही स्वाद है।
सोचता हूँ, आख़िरश् हमने क्यों ओढ़ा था आदमी का लबादा
अगर जानवरनुमा ज़िंदगी ही जीने का था इरादा!
कभी-कभी, जब मैं जुटा होता हूँ बेतादाद काम को निबटाने में
तो हवा में मुझे दिखाई देती हैं अजनबी शक्लें,
सुनाई देती है वहशी क़दमों की खड़खड़ाहट,
अट्टहास और ज़राइमपेशा फुसफुसाहट।
और ज़रा, लाश जैसे सफ़ेद इन हाथों को देखो,
इन बे-आब गालों को?
बस यही थोड़े-से बाल बचे हैं
ये जहन्नुमज़ार काली झुर्रियाँ!
बच्चो, कभी मैं भी हू-ब-हू तुम्हारे जैसा था—
तुम्हारे ही जैसा चुस्त और उसूलपसंद,
ख़्वाबआलूदा थी मेरी ज़िंदगी :
ख़्वाब पिघलते ताँबे के,
हीरों के पहलू चमकाते हुए ख़्वाब...
आह, तब ज़िंदगी में कितना था आब!
और अब उन ख़्वाबों ने मुझे यहाँ ला पटका है—
यहाँ, इस तकलीफ़देह मेज़ के सामने,
जिसकी सतह पर लिखा है फ़क़त एक जुमला :
'पाँच सौ घंटे का काम का हफ़्ता।'
- पुस्तक : रोशनी की खिड़कियाँ (पृष्ठ 269)
- रचनाकार : निकानोर पार्रा
- प्रकाशन : मेधा बुक्स
- संस्करण : 2003
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.