लेखकों की समस्याएँ : व्यष्टि और समष्टि
lekhkon ki samasyayenhavyashti aur samshti
उपेंद्रनाथ अश्क
Upendranath Ashk
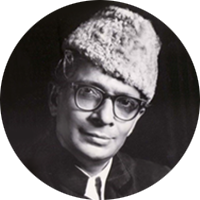
लेखकों की समस्याएँ : व्यष्टि और समष्टि
lekhkon ki samasyayenhavyashti aur samshti
Upendranath Ashk
उपेंद्रनाथ अश्क
और अधिकउपेंद्रनाथ अश्क
व्यष्टि और समष्टि—व्यक्ति और समाज—कहानी लेखन के संदर्भ में एक को हटाकर मैं दूसरे की कल्पना नहीं कर सकता। आदमी जिस क्षण आँख खोलता है, देखने-सुनने लगता है, बाहर होने वाले कार्य-व्यापार को वह अपने मन के आईने पर प्रतिबिंबित करके देखता है। देखने वाला, सुनने वाला, और उस देखे-सुने को अपने मन में ग्रहण करने और मस्तष्क की तुला पर तौलकर उसे फिर बाहर पाठकों को संप्रेषित करने वाला व्यक्ति ही है, सो उसके बिना कथा नाम की रचना असंभव है। तब प्रश्न उठता है—क्या समाज के बिना कथा संभव है? मेरे ख़याल में—नहीं; संसार में नितांत अकेला आदमी कहानी लिख सकेगा, इसमें मुझे संदेह है। हो सकता है, अपने थके, ऊबे अथवा दुखी मन को बहलाने के लिए वह गुनगुनाने या पशु-पक्षियों के संग नाचने लगे, पर वह कथा लिखेगा, इसका मुझे विश्वास नहीं।
कथा कहने के लिए सुनने अथवा पढ़ने वाले की अपेक्षा है। यह ठीक है कि कहानी रचने वाला लेखक व्यक्ति होता है। यह भी सच है कि ऐसा वह प्रायः अपने मन के सुख के लिए या फिर व्यष्टि अथवा समष्टि की किसी समस्या के भार से मुक्त होने के लिए करता है। (केवल धन के लिए लिखने वाला मेरी बहस के दायरे से बाहर है।) लेकिन इस बात की अपेक्षा कथाकार को ज़रूर रहती है कि उसके लिखे को दूसरा सुने अथवा पढ़े। जलयान के नष्ट हो जाने के बाद निर्जन द्वीप में नितांत अकेले रह जाने पर, ज़िंदगी का साथ बनाए रखने के लिए रॉबिंसन क्रूसो ने और जो कुछ भी किया हो, उसने कहानियाँ नहीं लिखीं। क्रूसो के रचयिता ने अपने नायक को ऐलेग्ज़ैंडर सेलकर्क नामक एक नाविक के जीवन से लिया था, जो अपने कप्तान से लड़कर एक निर्जन द्वीप में चार वर्ष और चार महीने रह गया था। अपने अकेलेपन को भुलाने के लिए, उन कुछ पुस्तकों को, जो उसके पास थीं, उसने बार-बार पढ़ा। कुछ समय बाद जब उसके पास बंदूक़ के कारतूस ख़त्म हो गए, उसने केवल हाथों के बल शिकार करना और नंगे पैरों हिरनों ऐसा तेज़ भागना सीख लिया। उसने जंगली बकरियों को पकड़ा। उन्हें सधाया। अपनी ऊब के क्षणों में वह गाता-गुनगुनाता भी था और पालतू बकरियों के साथ नाचता भी था, पर धीरे-धीरे पेट की समस्या उसके लिए सर्वोपरि हो गई और लिखना तो दूर रहा, जब चार वर्ष बाद एक जलयान ने उसे देखा और उसे सभ्य संसार में वापस लाया गया तो उसकी स्थिति जंगली पशुओं से भिन्न नहीं थी। वह सभ्य समाज के तौर-तरीक़े और खाने-पीने का स्वाद तक भूल गया था।
कभी जब मैं आलोचनाओं में ‘व्यष्टिवादी’ अथवा ‘समष्टिवादी’ शब्द पढ़ता हूँ तो मुझे हँसी आती है, क्योंकि आज कोई कहानी शत-प्रतिशत व्यक्तिवादी अथवा समष्टिवादी नहीं होती। आलोचकों ने कहानियों के प्रमुख स्वरों को जनाने के लिए ये शब्द गढ़ लिए हैं और उन्हीं अर्थों में यहाँ मैं उनका प्रयोग भी करूँगा। परम व्यक्तिवादी कहानी पर समाज का, लेखक के अपने परिवेश का, कोई प्रभाव या दबाव नहीं होता—मैं ऐसा नहीं मानता और न ही परम समष्टिवादी कहानी लेखक-व्यक्ति के चिंतन-मनन के प्रभावों अथवा परिणामों से मुक्त होती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी विधा हो व्यक्ति के चिंतन-मनन पर समाज के उत्तरोत्तर बढ़ते प्रभाव और दबाव का परिणाम है।
समाज का यह प्रभाव या दबाव व्यक्ति पर दो तरह से पड़ता है। कभी प्रत्यक्ष और कभी परोक्ष। कभी सीधा और कभी टेढ़ा। कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक। समष्टिवादी रचनाएँ मेरे ख़याल में तब लिखी जाती हैं, जब समाज को स्वीकारते हुए, लेखक उसे बेहतर बनाना चाहता है और इसके लिए स्पष्ट और अस्पष्ट संकेत देता है। और व्यक्तिवादी तब, जब अपने जीवन अथवा समाज के दबाव के कारण वह समाज-विमुख हो, उपेक्षा से या क्रोध से या आभिजात्यि-सुलभ अहं के कारण अंतरोन्मुख हो जाता है।
वे अंतरोन्मुख व्यक्तिवादी रचनाएँ समाज के बिना संभव हैं, मैं ऐसा नहीं मानता और कई बार जब लेखक सामाजिक परिवेश के अंदर घुटते हुए व्यक्ति-मन में झाँकता है तो वे रचनाएँ सीधी समष्टिवादी रचनाओं की अपेक्षा समाज पर ज़्यादा करारा व्यंग्य करती हैं और व्यक्ति तथा समाज को समझने में अधिक सहायता देती हैं।
आज के संदर्भ में लेखक के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने दिनों-दिन भ्रष्ट और खोखले होते समाज का क्या करे?—उसके प्रभावों और दबावों से कैसे जूझे? क्या वह इस समाज का, जिसमें कि वह रहता है, हू-ब-हू चित्रण करे? क्या इस संबंध में उसकी कोई प्रतिबद्धता है? अथवा वह उससे विमुख होकर अपने में रम जाए? या फिर उससे भागकर आत्मा और परमात्मा, जीवन और मृत्यु अथवा ऐसे ही शाश्वत सत्यों के उद्घाटन की उस चिरंतन ख़ोज में लग जाए, जो मानव को सदा अपनी ओर आकर्षित करती रही है?
समाज के सीधे प्रभाव और चित्रण का सरल और रूप प्रेमचंद के यहाँ मिलता है। प्रेमचंद समाज के प्रति पूर्णतः प्रतिश्रुत थे और उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में समाज का वर्णन ऐसे कथाकार के नाते किया, जो समाज को आदर्श की ओर ले जाना चाहता है। जब ज़िंदगी के आख़िरी दिनों में उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने यथार्थवादी आँखों से जीवन को देखना शुरू किया, तो भी वे समाज-विमुख नहीं हुए। उन्होंने उसके यथार्थ का चित्रण करने का प्रयास किया और अपने उपन्यास ‘गोदान’ में ही नहीं, अपनी कहानियों—‘कफ़न’, ‘बड़े भाई साहब’, ‘नशा’, ‘मनोवृत्तियाँ’, आदि में व्यक्ति और समाज के यथार्थ का चित्रण किया। उसी ज़माने में प्रसाद ने व्यक्तिमूलक कहानियाँ लिखीं। अपने ज़माने के समाज को न लेकर उन्होंने इतिहास को कुरेदा। प्रेमचंद ने जहाँ यथार्थ को समष्टि-सत्य की कसौटी पर परखा, वहाँ प्रसाद ने वास्तव को व्यक्ति-सत्य के धरातल पर आँका। (आदर्शोन्मुख दोनों रहे।) क्या कान्य, क्या नाटक और क्या कहानी, प्रसाद ने अपने ज़माने को प्रायः नहीं छुआ, जबकि प्रेमचंद ने यदि इतिहास से भी कोई कथानक अथवा पात्र लिया तो उसे भी अपने जमाने की समस्याओं के समाधान का माध्यम बनाया।
एक ही नगर में, एक ही काल में रहने के बावजूद इन दोनों लेखकों की दृष्टि में इतना अंतर क्यों रहा? यदि हम इस प्रश्न की गहराई में जाएँ तो हमें मालूम होगा कि :
लेखक के जीने का उसके लेखन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वह जैसे जीता है, जिस दृष्टि से जीता है, ज़िंदगी से उसकी जो आकांक्षा है, उसी के अनुसार उसका लेखन ढलता है।
जिस आदमी ने ज़िंदगी में वास्तविक संघर्ष नहीं देखा, वह महज़ कल्पना से उस संघर्ष का चित्रण नहीं कर सकता।
अपनी एक कोठरी को जलता देखकर आदमी जो महसूस कर सकता है, वह दूसरे के सारे भवन को जलते देखकर नहीं कर सकता।
ज़िंदगी को लिखने के लिए ज़िंदगी का सीधा संपर्क ज़रूरी है।
प्रेमचंद ने इसीलिए समाज का चित्रण किया कि उन्होंने ज़िंदगी भर समाज का सीधा संपर्क पाया। बचपन से लेकर निरंतर घोर संघर्ष किया और उसी में समाप्त हो गए। नौकरी और अपनी स्वतंत्रता में उन्होंने स्वतंत्रता को चुना। सुख-आराम की ज़िंदगी के मुक़ाबिले में अनवरत संघर्ष की ज़िंदगी को अपनाया। फ़िल्मी दुनिया में गए तो वहाँ रह नहीं पाए। ऐसा आदमी ही वह लिख सकता था, जो प्रेमचंद ने लिखा। प्रसाद को उस तरह का कमरतोड़ संघर्ष नही करना पड़ा। संपन्न व्यापारी घराने में पैदा हुए। प्रतिभा संपन्न थे, इसलिए अपनी अवकाश की घड़ियों में पढ़ते-लिखते थे। जीवन से सीधा संपर्क न होने से कल्पना के सहारे लिखते रहे, इसीलिए उनकी दृष्टि सामाजिक सत्यों की ओर नहीं गई, व्यक्ति-सत्यों की ओर ही गई। अथवा यों कहा जाए कि आरोपित व्यक्ति-सत्यों अथवा काल्पनिक व्यक्ति-सत्यों की ओर गई। चूँकि समाज और व्यक्ति का प्रेमचंद जैसा उनका अनुभव नहीं था, इसलिए सारे सौंदर्य और आदर्श के बावजूद उनके पात्र कठपुतलियों से लगते हैं, हाड़-मांस के नहीं लगते। उनकी भाषा भी कृत्रिम है। व्यष्टि-सत्य का निरूपण उनके यहाँ होता है, पर जिस माध्यम से होता है, यह विश्वसनीय नहीं लगता। एक आलोचक ने लिखा है कि प्रसाद कवि थे और प्रेमचंद गद्यकार, इसीलिए प्रेमचंद के यहाँ विचार का पुट अधिक है और प्रसाद के यहाँ भाव का। मेरा विनम्र निवेदन है कि उस जीवन के साथ, जो प्रेमचंद ने जिया और उस संघर्ष के साथ, जो उन्होने किया, यदि ये कविता लिखते तो उसमें भी समष्टि-मूलक तत्व आ जाते और ये अपनी कविताओं में भी समाज ही का चित्रण करते। इसके विपरीत प्रसाद ने गद्य लिखा तो उसमें भी कल्पना ही का सहारा लेते चलते रहे। प्रसाद के लिए लेखन शौक़ था और प्रेमचंद के लिए जीवन।
प्रसाद के बाद यदि काव्य-क्षेत्र में एक और महादेवी, पंत और अज्ञेय और दूसरी ओर निराला को लें तो हम इस बात को और भी अच्छी तरह समझ सकेंगे। प्रसाद से छायावादी काव्य को उत्तराधिकार में पाकर, यदि पंत और महादेवी उसे नहीं छोड़ सके और अज्ञेय छोड़कर भी ‘आँगन के पार द्वार’ में फिर उसी थाती से आ चिमटे तो इसीलिए कि ये तीनों संपन्न वर्ग में पैदा हुए। वैसा कोई दुख-दैन्य उन्होंने नहीं देखा। बाह्य जीवन तो दूर, पंत और महादेवी ने गृहस्थ जीवन तक का निजी संपर्क नहीं पाया और अज्ञेय घर बसाकर भी ‘छड़े1 उठाई पूँछड़ी गया सौदाई हो’ वाली पंजाबी कहावत को चरितार्थ करते रहे। संतान संबंधी सुख-दुख और संघर्ष उन्होंने नहीं देखा और कुँवारों की तरह लगातार देश-विदेश घूमते रहे।
इन सबसे बरअक्स निराला ने जीवन का कटुतम संघर्ष देखा और इसलिए उन्होंने छायावाद के छद्मतापूर्ण प्रभाव से निकलकर अपने काध्य में समष्टिगत तत्वों का समावेश किया। उनके काव्य में यदि क्लिष्ट संस्कृतनिष्ठ भाषा मिलती है तो सरल रोज़मर्रा की भी। उनके गद्य की भाषा बहुत सरल है। ‘बिल्लेसुर बकरिहा’ की भाषा तो हिंदी-गद्य-साहित्य में अनूठी है। लघु उपन्यासों में उसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह और बात है कि पेशेवर आलोचकों ने उस सशक्त कृति की ओर ध्यान नहीं दिया। अपनी बेटी की मृत्यु पर निराला जैसी कविता लिख सके, अपनी समस्त कल्पना-शक्ति और शब्द-सौष्ठव के बावजूद महादेवी अथवा पंत अथवा अज्ञेय नहीं लिख सकते। महादेवी के चुप हो जाने और अध्यात्म के सागर में पंत और अज्ञेय के डूबने अथवा अनुभव की धरती के बदले चिंतन के आकाशों में विचरने का भी यही कारण है। पंत चूँकि जागरूक कवि हैं, इसलिए भावना के स्तर पर नहीं तो बौद्धिक स्तर पर उन्होंने अपने काव्य में समष्टिगत तत्वों का समावेश किया है। अज्ञेय ने भी प्रगतिशील दौर में वैसी समष्टिगत बौद्धिक कविताएँ लिखीं। महादेवी ने शुरू में ‘श्रृंखला की कड़ियाँ’ और’ अतीत के चलचित्र’ में ज़रूर कुछ समष्टिगत तत्वों को लिया, लेकिन यह बहुत पुरानी बात है। (ये तीनों उत्कृष्ट कवि हैं और मैंने उनके काव्य में बहुत रस पाया है, पर यहाँ व्यष्टि तथा समष्टिवादी दृष्टियों का ज़िक्र है और उसी संदर्भ में मैंने यह बात कही है।)
यह समानता यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। कथा-क्षेत्र में बरकरार नज़र आती है। यशपाल का जीवन देख लीजिए और फिर जैनेंद्र और अज्ञेय का तो तत्काल मालूम हो जाता है कि यशपाल यथार्थवादी ही हो सकते थे और जैनेंद्र और अज्ञेय समाज-विमुख व्यक्तिवादी ही। जैनेंद्र जीवन-यापन के लिए शुरू ही से सेठाश्रयी रहे और प्रकाशन शुरू करने से पहले अपनी आय को वे गर्व से ‘आकाश वृत्ति’ कहते रहे। प्रकाशन ज़माने में भी उन्हें साधारण प्रकाशक का-सा संघर्ष नहीं करना पड़ा कि अपनी किताबों का बैग लिए हुए वे शहर-शहर और दुकान-दुकान घूमते और जीवन-संघर्ष से उनका सीधा वास्ता पड़ता। कांग्रेस और मंत्रियों से अपने संपर्कों के कारण अपनी पुस्तकों की ख़रीद में उन्हें कभी कठिनाई नहीं हुई। अज्ञेय अपने अभिजात्य को बरकरार रखने के लिए जैसी ही बड़ी नौकरियाँ पाने और वैसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करते रहे। क्रांतिकारी दल में वे भी शामिल हुए, पर यशपाल की तरह देश की ग़ुलामी से प्रताड़ित होकर नहीं, अपने अहं की संतुष्टि और अभिजातवर्गीय ‘एडवेंचर’ के शौक़ को पूरा करने के लिए ही। समाज से सीधा संपर्क उनका कभी नहीं रहा। इसलिए चाहने पर भी उसके लिए यशपाल (या अश्क) जैसी कहानियाँ लिखना असंभव था।
यहीं जिज्ञासु पाठक के मन में एक दूसरा प्रश्न उठता है। इन बड़े लेखकों की बात छोड़िए, वह कहता है, आज अगणित ऐसे लेखक हैं, जो निम्न मध्य वर्ग से उठे हैं, जिन्होंने भूख और बेकारी देखी है, पर जो घोर व्यक्तिवादी कहानियाँ लिखते हैं। इनमें कुछ की कहानियाँ यदि जैनेंद्र या अज्ञेय की तरह व्यक्तिवादी नहीं, तो प्रेमचंद और यशपाल की तरह समष्टिवादी भी नहीं। और वह पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों है? कुछ में तो अजीब-सी वीभत्सता का चित्रण है। मेरा ख़याल है कि इसका कारण देशी और विदेशी प्रभावों और दबावों के कारण विकुंचित हो जाने वाला नए लेखकों का जीवन तथा उसकी विकुंचित दृष्टि ही है। यदि पुराने लेखकों का संपर्क समाज के साथ सीधा नहीं था तो आज के इन लेखकों का भी वैसी नहीं रहा। यदि वहाँ अपनी अभिजातवर्गीय रुचियों के कारण जीवन से पलायन था, तो आज के अधिकांश नितांत नए लेखकों में, एक ओर बाहर से आने वाले फ़ैशनों के कारण और दूसरी ओर स्वातंत्र्योत्तर समाज के आदर्शच्युत हो जाने की घोर वितृष्णा के फलस्वरूप अपने परिवेश से पलायन है। इसी कारण वे समाज-बिमुख ही, अंतरोन्मुख हो गए है।
यहीं एक और बात की ओर मैं पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रेमचंद-जैसी सीधी-सपाट कहानियाँ आज लिखना संभव भी नहीं। स्वयं उनकी कहानियों में 1935-36 के क़रीब व्यक्तिमूलक तत्व आ गए थे...’कफ़न’, ‘नशा’, ‘बड़े भाई साहब’, मैं व्यष्टि-समष्टिगत दृष्टियों का कुछ अजीब सा मिश्रण है। मुझे स्मरण है कि उन्हीं से प्रभावित होकर स्वयं मैंने सीधी-सपाट कहानियाँ लिखना छोड़ दिया था और मेरी कहानियाँ ‘डाची’, ‘मनुष्य—यह’, ‘अंकुर’ और ‘पिंजरा’ उसी ज़माने की याद है और बाद में इन दोनों दृष्टियों का समावेश मेरे सारे साहित्य में रहा; और आज भी ‘आकाशचारी’, ‘मरना और मरना’ और मेरी ताज़ा कहानी ‘अजगर’ तक में यह विद्यमान है।
प्रगतिशील आंदोलन के उरूज का-सा जोश और सीधी दृष्टि आज नहीं है। बीसवीं कांग्रेस में ख्रुश्चोव द्वारा स्तालिन-युग के ज़ुल्मों से पर्दा उठाने और भारत-चीन विवाद तथा हाल ही में रूस द्वारा पाकिस्तानी ‘थ्युरोकेसी’ के समर्थन ने उस दृष्टि को बुरी तरह धुँधला दिया है और नए लेखकों को तमाम दुर्गुणों के बावजूद हमारा ‘प्रजातंत्र’ अच्छा लगता है। लेकिन जब उसके अधीन होने वाले देशव्यापी भ्रष्टाचार और मूल्यों के विघटन की ओर निगाह जाती है तो नए लेखक के लिए वैसी आस्था-भरी कहानियाँ लिखना असंभव हो जाता है और वह अंतरोन्मुख होकर व्यक्तिपरक कहानियाँ लिखता है। लेकिन इस बात की दाद नए लेखकों को देनी पड़ेगी कि उनकी व्यक्तिपरक रचनाओं में भी प्रसाद या जैनेंद्र के जैसे झूठे पात्र नहीं, न अज्ञेय के पात्रों जैसे ठंडे। उनमें अनुभूति की आग है और जहाँ सत्य पश्चिम से उधार लिया गया या आरोपित नहीं—अनुभूत है—वहाँ पात्र विश्वसनीय हो गए हैं और कहानी का आधारभूत विचार निश्तर-सा सीने में उतर जाता है। दूधनाथसिंह की कहानी ‘रीछ’ अथवा ज्ञानरंजन की ‘संबंध’ या फिर सुदर्शन चोपड़ा की ‘सड़क दुर्घटना’ में जिस तीव्र अनुभूति का स्पर्श मिलता है वैसी अनुभूति जैनेंद्र अथवा अज्ञेय की गत दस वर्षों में लिखी किसी रचना में हो तो वह मेरी नज़र से नहीं गुज़री। पाठक ध्यान से इन नई कहानियों को पढ़ेंगे तो पाएँगे कि ऐसी अनुभूति-बहुल कहानियाँ वैसी व्यक्तिवादी भी नहीं रहतीं, जैसी प्रसाद या जैनेंद्र या अज्ञेय की। उनमें समिष्टगत तत्व आपसे-आप आ जाते हैं और वे तत्व समाज की उस व्यवस्था अथवा धारणाओं में परिवर्तन की माँग करते हैं, जो व्यक्ति के मन में ऐसे अँधेरे गर्त पैदा करती हैं, जिनमें समाज का अंग होते हुए भी व्यक्ति-जीवन क्षय-ग्रस्त हो रहा है और पुराने संबंध टूट रहे हैं। ऐसी कहानियों में परोक्ष रूप से समष्टिगत तत्व अभिव्यंजित रहते हैं। मेरा यह निश्चित मत है कि कल्पना के बल पर किसी व्यथित-सत्य का उद्घाटन करने के बदले, जो कथाकार अनुभूति के बल पर किसी व्यक्ति-सत्य का उद्घाटन करता है, वह समष्टि-सत्य के तत्व अजाने भी कहानी में ले आता है। फ़ादर इमेज (father-image) के टूटने और बनने के व्यक्ति-सत्य को लेकर सारिका के ताज़ा अंक में छपी वेदी की अद्वितीय कहानी ‘सिर्फ़ एक सिगरेट’ मेरे कथन का प्रमाण है। नए कथाकारों में भीमसेन त्यागी की ‘एक और विदाई’ तथा ‘ज्ञानोदय’ के अप्रैल अंक में छपी उसकी ‘शमशेर’, रवींद्र कालिया की ‘बड़े शहर का आदमी’ और महेंद्र भल्ला की ‘कुत्तेगीरी’ ऐसी ही कहानियाँ हैं।...ज्ञानरंजन की उपरोक्त कहानी ‘संबंध’ ही को लीजिए। सरसरी नज़र से देखने पर यह घोर व्यक्तिवादी और कुछ स्थलों पर (जहाँ पर लड़का माँ के प्रति वितृष्णा दर्शाता है और भाई की मृत्यु की कल्पना करता है और उसकी प्रस्तावित आत्महत्या को उचित करार देकर सुख पाता है) बेतरह चौंकाती और मन में जुगुप्सा उपजाती है, पर ज़रा गहराई में जाने पर क्या यह उस समाज और उस परिवार के प्रति सोचने पर विवश नहीं करती, जहाँ परंपरागत संबंधों में ये दरारे पड़ गईं हैं। क्यों पड़ गई है, इसके बड़े सूक्ष्म व्यंग्य-भरे संकेत कहानी में हैं और उन्हीं के कारण समष्टिगत तत्व का समावेश लेखक के जाने या अंजाने कहानी में हो गया है। यह और बात है कि उन्हें जानने के लिए तनिक गहरे में उतरना पड़ता है। कहानी व्यंग्य दोधारी तलवार-सा काम करता है और अपने परिवार पर ही नहीं, कहानी का नायक अपने-आप पर भी व्यंग्य करता चलता है। ज्ञानरंजन की अन्य कहानियाँ—‘पिता’, ‘खलनायिका और ‘बारूद के फूल’, और ‘यात्रा’—सभी में यह दोहरा व्यंग्य है। ये सब और ऐसी ही कई कहानियाँ हैं जिन्हें शत-प्रतिशत व्यक्तिवादी नहीं कहा जा सकता। यहाँ व्यष्टि गौर समष्टि के सत्य अनुभूति के खरल में पिसकर कुछ ऐसा नया रूप घर लेते हैं कि उन्हें एक नाम दे देना कठिन हो जाता है।
लेकिन नए कथाकारों में ऐसे लेखक न हों, जिनके यहाँ समष्टिगत तत्व अपेक्षाकृत अधिक हैं—ऐसी बात नहीं। गिरिराज किशोर, भीमसेन त्यागी और ज्ञानप्रकाश की कहानियों में समष्टिवादी स्वर प्रखर है। इधर ‘आवेश’, के प्रवेशांक में सुदर्शन चोपड़ा की उपरोक्त कहानी ‘सड़क दुर्घटना’ इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। सुदर्शन मुख्यतः व्यक्तिवादी कथाकार हैं, पर उनकी यह कहानी व्यवस्था पर ऐसा करारा व्यंग्य है, जो सीधा दिल में उतर जाता है। यही कारण है कि ज्ञानरंजन की ‘यात्रा’ के साथ सुदर्शन चोपड़ा की उस कहानी ने पाठकों का ध्यान खींचा। मैंने उस कहानी को दोबारा पढ़ा तो मुझे और भी अच्छी लगी।
आज़ादी के पहले लेखक का जीवन आज के लेखक से भिन्न था। अपने लिखने का उसे कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। स्वातंत्र्य-संग्राम ज़ोरों पर था। उसके जोश में आए दिन लोग बड़े-बड़े त्याग करते थे। लेखक भी पैसे के लिए नहीं लिखता था अथवा उसकी उसे चिंता नहीं थी, क्योंकि प्रायः उसे अपने लिखे का कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था और लेखन को कैरियर के रूप में भी लिया जा सकता है, यह वह कभी सोचता भी नहीं था। यदि कोई फ़्रीलांसर था भी तो इसलिए कि लिखे बिना रह नहीं सकता था और दूसरे किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। पर आज ऐसी स्थिति नहीं। 1947 के पूर्व हमारा समाज अपनी तमाम गंदगी, ग़लाज़त और ग़ुलामी के बावजूद आदर्श के जो सपने देखता था, आज के युवा लेखक ने ये सपने नहीं देखे। उसने जिस समाज में आँखें खोली हैं, या जिसमें जवानी बिताई है, वह उसे नितांत भ्रष्ट, पतनशील और गलघोटू दिखाई देता है और लेखक के लिए उसमे साँस लेना कठिन हो गया है। चूँकि आदर्शवादी का-सा अमर्ष उसके यहाँ नहीं है और आदर्शच्युत हो जाने के कारण, यथा राजा तथा प्रजा के अनुरूप दस दूसरी मसलहतें उसके साथ हैं, इसलिए वह समाज का जस-का-तस चित्रण नहीं कर पाता और जब वह सुनता है कि अमुक या अमुक मंत्री ने कभी बड़ी कुर्बानियों को थी तो उसे विश्वास नहीं होता। वर्तमान नेताओं का जीवन उसे निहायत भ्रष्ट लगता है और यह इसे ही मानव की सहज नियति मानता है। इसके अतिरिक्त अधिकांश युवक लेखकों के सामने कैरियर का प्रश्न रहता है—कोई सरकारी और कोई सरकार से अनुदान पाने वाली अर्द्ध-सरकारी संस्था में मूलाज़मत चाहता है। किसी अन्य के सामने किसी सेठ के आश्रय में चलने बाले मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक की संपादकी या उसमें लिखने-लिखाने और पारिश्रमिक पाने की समस्या है। कोई तीसरा किसी बड़े प्रकाशन-गृह से पुस्तक छपवाना चाहता है। प्रकट ही कैरियर की इन गणनाओं का प्रभाव लेखक की रचनाओं पर भी पड़ता है।...हमारे वर्तमान समाज में चूँकि अधिकांश धाँधली पूँजीवादी व्यवस्था ही के कारण है, जो यह चाहती है कि लेखकों का ध्यान समाज की ओर न जाए, वे अपने में रमे रहें और उन्हीं की पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भारत में बीटनिकों का धुआँधार प्रचार होता रहा है और घोर व्यक्तिपरक रचनाओं को प्रश्रय मिलता रहा है। इन्हीं सब कारणों से नए लेखक समाज के भ्रष्टाचार, चोरबाज़ारी या दूसरी समष्टिगत बुराइयों का चित्रण नहीं कर पाते—अंतरोन्मुख होकर सेक्स और प्रेम के चीथड़े उधेड़ते हैं। यदि वे संघर्ष-रत नहीं हैं और बड़ी नौकरियों पर प्रतिष्ठित हैं, तो वे आकाशी अथवा वायवी बातें करते हैं अथवा प्रतीकों और बिंबों का सहारा लेते हैं।...यही नहीं, अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए ऐसे सारे लेखक समष्टि के सुख-दुखों, गंदगी और ग़लाज़त का चित्रण करने वालों को झूठे और अपने को ‘जेनुइन’ लेखक भी कहते हैं, जबकि कुछ अपवादों को छोड़, शेष के पास न सत्य अपने होते हैं न अनुभव और वे अपने झूठ को छिपाने के लिए सच्चे को झूठा घोषित कर सुख पाते हैं। लेकिन जैसी रचनाएँ वे करते हैं, वे भ्रष्ट समाज अथवा वैसे कमज़ोर लेखकों के बिना संभव भी नहीं होतीं। इनमें से यदि एकाध कला की दृष्टि से उत्कृष्ट उतरती है, तो शेष का वार नितांत भोथरा साबित होता है।
फिर यों भी होता है कि कोई लेखक दोहा व्यक्तित्व जीता है। समाज में रहते हुए, उसने छल-छंद में पूरा योग देते हुए झूठ, दग़ा, फ़रेब, चाटुकारिता, घूसख़ोरी, टुच्चापन, नीचता आदि के दुर्गुण, उसके स्वभाव का अंग होते हैं। लेकिन चूँकि अपने दुर्गुणों के विरुद्ध उसके मन में तनिक भी क्रोध अथवा ग्लानि नहीं होती, इन्हें वह मानव की सहज नियति समझता है और इनका चित्रण करने और इन पर प्रहार करने की ज़रूरत नहीं समझता (सच्ची बात यह है कि उसे रुचि ही नहीं होती) इसलिए वह यदि पुराना लेखक है तो अपने रचनाकार को इस गंदगी और ग़लाज़त से ऊपर रख, संसृति के रहस्यों अथवा अध्यात्म के ऊँचे आकाशों में ले जाता है और उठते-बैठते ऊर्ध्व चेतना की बात करता है। यदि नया है तो चेतन, अचेतन, उपचेतन और अवचेतन में डूबता उतराता रहता है। पहली स्थिति में समाज का दबाव उसे धरती से ऊपर उठा देता है, दूसरी में अंदेखी-अंजानी गहराइयों में गोते खाने को छोड़ देता है। कई आलोचक इसी प्रक्रिया में लिखे जाने वाले साहित्य के संदर्भ में कीचड़ में से कमल निकालने का मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब जनता के आंदोलन ज़ोर पकड़ते हैं, जब आदमी कैरियरों और नौकरियों की परवाह न करके अपने मन में उठने वाले तूफ़ानों को स्वर देते हैं तो वे सब रचनाएँ जो मानव को अपनी स्थिति भुलाती हैं, समाज से विमुख करती हैं, अफ़ीम का नाम पाती हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक ही रचना एक युग में कमल और दूसरे में पोस्त हो जाती है, जब कि उसकी उत्कृष्टता में कोई अंतर नहीं आता। यह समष्टिवादी के दबाव और प्रभाव अयवा उसके अभाव ही के कारण होता है। मैं उस रचना को बेहतर मानता हूँ, जो दोनों युगों में समान रूप से पड़ी और पसंद की जा सके।
समष्टि के संदर्भ में आज के लेखक की समस्या यह है कि वह कौन-सा रास्ता अपनाए?— क्या विदेशी सरकार के ज़ुल्म-तले पिसने के बावजूद अपना स्वर ऊँचा उठाने में नितांत अशक्त छायावादियों की तरह आत्मा और परमात्मा के रहस्योद्घाटन अथवा प्रकृति के सौंदर्य में अपने साथ पाठकों को भुलाए अथवा यथार्थ जीवन के संघर्ष से भागकर सेक्स की ‘ऐबेरेशंज़’, परवर्शंज़’ या फिर ज़िंदगी की सीलन और सड़न का चित्रण कर ज़िंदगी की घोर व्यर्थता को संकेतित करे और पाठकों की आत्मघाती वृत्तियों को उभारे?
जैसाकि मैंने पहले कहा, हर लेखक हर तरह नहीं लिख सकता। जैसी ज़िंदगी वह जीएगा, जितने समझौते करेगा, उन्हीं के अनुसार लिखेगा। ऐसे लेखक विरल होते हैं, जो घृणित जीवन जीते हुए भी उसकी आलोचना पूरी निर्ममता से कर सकें। जो न दूसरों को बड़ों, न अपने-आपको माफ़ करें—आम लेखक जो समझौते करते हैं, उनका प्रभाव उनकी लेखनी पर पड़ता है। मेरे सामने ऐसे लेखक हैं, जिन्होंने लेखक-जीवन का आरंभ विद्रोहियों के रूप में किया। उनकी रचनाएँ पढ़कर लगता था कि उनके विद्रोही स्वर कुछ अत्यंत उच्चकोटि को रचनाएँ देंगे, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरियाँ कर लीं बोर वे ऐसी चीज़ें लिखने लगे, जिनसे गुनाह का मज़ा भी आ जाए और हाथ से जन्नत भी न जाए।
...ऐसे लेखन और कवि भी मेरे सामने हैं, जो कभी ज़बरदस्त प्रगतिशील रहे, लेकिन जब ज़िंदगी के संघर्ष में टूटे और ऐसी संस्थाओं की ओर उन्मुख हुए, जिनके यहाँ नौकरी पाने के लिए समाज-विरोधी रचनाएँ उच्चतम सर्टिफ़िकेट थी, तो उन्होंने निद्वंद्ध होकर समष्टिवादी मुखौटे उतार फेंके और सरेआम नंगे हो गए। न केवल यह, बल्कि अपने नंगेपन के औचित्य में बड़ी-बड़ी बातें भी करने लगे। भारतीय समाज और उसके चित्रण से विमुख हो, उन्होंने अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय मान लिया और पश्चिम के सत्यों को ऐसे ओढ़ लिया, जैसे यहाँ की मिट्टी की गंध ही उन्होंने न पाई हो और वही आँखें खोली हों। और आख़िर वहीं पहुँच गए, जहाँ कि पहुँचने की हबिस उनके दिल में छिपी थी।
मेरे सामने ऐसे कवि का चित्र आता है, जो जीवन के चालीस-पैंतालीस वर्ष प्रगतिशील कविताएँ लिखता रहा। स्वतंत्र रह सके, इसलिए स्वल्प पर जीवन बिताता, तकलीफ़ पाता रहा और जितने लेखक उससे बेहतर जीवन जीते थे, उन्हें दुकानदार कहता रहा। उस दौर में उसने मज़दूरों के जुलूसों, पार्टी कामरेडों और चीनी और रूसी भाइयों पर कविताएँ लिखीं, लेकिन जब टूटा और दूसरों ने उसे ललचाया तो सीधा गिज़बर्ग और एम० आर० ए० की गोद में जा गिरा—अब कुंठित प्रेम की, न समझ में आने वाली ‘एब्सटैक्ट’ चित्र-शैली की कविताएँ लिखता है, जिन्हें भारत में कोई नहीं समझता, लेकिन विदेशों में उनकी व्याख्या की जा रही है। और वह जल्द ही महान कवि घोषित किया जाने वाला है।
लेकिन यहीं एक दूसरा प्रश्न उठता है—क्या लेखक के लिए ज़रूरी है कि वह समाज के प्रति ‘कमिटेड’ (प्रतिश्रुत) रहे?
मेरा ख़याल है कि यदि लेखक अपने और अपनी अनुभूतियों के प्रति प्रतिश्रुत है और उसके लिखने का उद्देश्य महज़ पैसा कमाना, अपने लेखन से महज़ चौंकाना अथवा लेखन को अच्छी नौकरी के लिए सीढ़ी बनाना नही है तो वह जो लिखेगा, व्यक्ति अथवा समाज की जिस स्थिति का उद्घाटन करेगा, जैसाकि मैंने पहले कहा, उसमें सीधे या प्रकारांतर से सामाजिक तत्व अपने-आप था जाएँगे। मैं समझता हूँ कि जो रचना समष्टि अथवा व्यष्टि को जानने-समझने का प्रयास करती है, वह समाज को आगे बढ़ाती है। जब लेखक अधिकांशतः व्यष्टि-मूलक रचनाएँ लिखते हैं और व्यक्ति की कुंठाओं और निराशाओं, कमज़ोरियों और परेशानियों पर ज़ोर देते हैं, तो जैसाकि मैंने ज्ञानरंजन की कहानी के संदर्भ में बताया, प्रकारांतर से हमें यही बताते हैं कि जिस समाज में व्यक्ति की यह दशा हो गई है, वह समाज दूषित है, उसे बदलना चाहिए। लेखक सीधे चाहे न कहे, पर यदि वह अपनी अनुभूतियों को सच्चाई और दयानतदारी से चित्रित करता है, उनसे आक्रांत होकर, आंतरिक कचोट से वशीभूत होकर लिखता है तो उसकी रचनाओं का यही प्रभाव पड़ता है।
यहीं एक और प्रश्न उठता है—क्या समाज के प्रति ‘कमिटेड’ रहे बिना अच्छा साहित्य नहीं लिखा जा सकता?
मेरा विचार है कि लिखा जा सकता है। यह दूसरी बात है कि समाज जब उन रचनाओं में अपनी समस्याओं अथवा अपनी उलझनों का प्रतिबिंब देखना चाहे और उसे वह न मिले तो वह उनसे विमुख हो जाए। रीतिकाल की कविता निकृष्ट कविता है, ऐसा कहना शायद ग़लत होगा, पर सामाजिक जागरूकता के युग में उसका महत्व न रह जाने से उसे पढ़ना अथवा उसमें रस पाना कठिन हो गया है। समाज से कटी महज़ काल्पनिक कहानियों का भी अंततोगत्वा यही हश्र होता है।
यहीं एक तीसरा सवाल पैदा होता है—क्या समाज की टॉपकैलिटी (Topicality) अर्थात् दैनदिन होने वाली घटनाएँ और ग्रह-विग्रह ऊँचा साहित्य उपजा सकते हैं?
साधारणतः यह माना जाता है कि समाज की टॉपिकैलिटी, उसके सीने पर उठने वाली क्षण-भंगुर तरंगें स्थाई रचना के लिए घातक हैं। यही कारण है, कुछ लोग मानते हैं कि युद्ध में अच्छे लेखक चुप लगा जाते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे नहीं मानता। मेरा ख़याल है कि यदि कोई रोज़मर्रा का प्रसंग, बदलते जीवन की कोई सामान्य घटना, लेखक के मन पर स्थाई प्रभाव छोड़ जाती है, उसके मन-मस्तिष्क में रस-बस जाती है, या फिर उसकी अनुभूति का अमिट अंग बन जाती है, तो उसको लेकर लिखी हुई रचना (यदि सधे हाथों से लिखी गई है तो) मन पर स्थाई प्रभाव छोड़ने वाली बनेगी। इसके विपरीत यदि लेखक ने महज़ भावुकतावश अथवा कोरे प्रचार के लिए, बिना उस स्थिति को भोगे, उसे कलम की नोक पर रखा है तो उसका कोई स्थाई प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा।
इसी संदर्भ में मुझे एक रूसी कहानी की याद आती है। दूसरे महायुद्ध की बात है। मॉस्को में छपने वाली मासिक पत्रिका ‘सोवियत लिट्रेचर’ में (जिसका नाम बाद में शायद ‘इंटरनेशनल लिट्रेचर’ हो गया) उन दिनों युद्ध संबंधी सोद्देश्य कहानियाँ छपती थीं। अधिकांश कहानियाँ वैसी ही होती थीं, जैसी कि प्रायः प्रचारात्मक टॉपिकल कहानियाँ होती हैं। लेकिन एक कहानी अपनी तमाम टॉपिकैलिटी के बावजूद मुझे आज भी याद है। हालाँकि न मैंने उस लेखक का कभी नाम सुना और न किसी रूसी संग्रह में वह कहानी ही देखी, पर मेरे दिल पर उसका प्रभाव अमिट है और मेरे ख़याल में वह कहानी विश्व-साहित्य की किसी भी महान कहानी के बराबर रखी जा सकती थी।...यूक्रेन का एक हिस्सा नाज़ियों के चंगुल से छुड़ाया गया है। वहाँ कॉन्सेन्ट्रेशन कैंप में एक अफ़सर की पत्नी मिलती है, जो काफ़ी बीमार है। मिलिट्री अस्पताल में मालूम होता है कि जल्द-से-जल्द उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। मेजर ऑपरेशन होगा, जिसमें प्राणों का संकट भी हो सकता है। उसका पति सूचना पाकर उसे तत्काल अपने शहर में ले आता है। वह लड़ाई से पहले उसी शहर के थिएटर में प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। ऑपरेशन के एक दिन पहले वह अपने पति से थिएटर दिखा लाने का अनुरोध करती है, जहाँ वही नाटक लगा हुआ है, जिसमें वह स्वयं काम किया करती थी। शाम का वक़्त है। मकानों की छतें बर्फ़ से सफ़ेद हैं। सन-शेडों से टपकता पानी धाराओं में जम गया है। उसे वह सब बहुत अच्छा लगता है। वह उस दृश्य से आँखें नहीं हट्टा पाती। बाज़ार, दुकानें, भीड़—उसे लगता है, जैसे वह उस सबको पहली बार देख रही है। वह थिएटर हॉल में अपने पति के साथ बॉक्स में बैठी है। सामने वही नाटक चल रहा है जिसमें वह स्वयं पार्ट किया करती थी। उसकी वाली भूमिका में जो युवती पार्ट कर रही है, वह उसे उस भूमिका के सर्वथा अनुपयुक्त लगती है। वह कौन-सा शब्द ग़लत बोलती है और कौन-सी भंगिमा ठीक से अदा नहीं करती, वह सब नोट करती जाती है। उसकी एक-एक मुद्रा की आलोचना करती हुई वह अपने पति को उसकी त्रुटियाँ बताती जाती है। उसे इस बात का दुख है कि बीमारी के कारण वह फिर कभी उस भूमिका को अदा न कर सकेगी। उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। तसल्ली देता है कि वह अवश्य कर सकेगी। उसका ऑपरेशन ज़रूर सफल होगा।...दूसरे दिन उसका पति उसे अस्पताल के ऑपरेशन-हॉल में पहुँचा देता है और स्वयं बाहर बरामदे में बैठ जाता है। ऑपरेशन को दो घंटे लगने वाले थे। इस अवधि के बीत जाने पर एक-एक क्षण उसके लिए भारी हो जाता है। जब चार-साढ़े-चार घंटे के बाद डॉक्टर बाहर निकलता है और अफ़सर की उत्सुकता-भरी निगाहें उसके चेहरे पर जा टिकती हैं, तो डॉक्टर बढ़कर उसका कंधा थपथपा देता है और कहता है—‘हम नहीं बचा पाए...बड़ा मज़बूत दिल था...बड़ा मुक़ाबिला किया...’
अफ़सर वापस मोर्चे पर आ जाता है। उसका साथी उसकी पत्नी का हाल पूछता है तो वह सारा वृत्तांत सुनाता है। साथी संवेदना प्रकट करता है तो वह कहता है—‘ऐसा तो रोज़ होता है!’
कहानी का शीर्षक है ‘एवरी डे’ और इस अंतिम वाक्य के अलावा एक पंक्ति भी उसमें प्रचार की नहीं है। इसके बावजूद वह कहानी युद्ध और उसके अधीन टूटती ज़िंदगियों के प्रति मन में कुछ अजीब-सी करुणा और युद्धोन्मत्त आतताइयों के लिए एक भयंकर अमर्ष मन में भर देती है। इसमें युद्ध की टॉपिकैलिटी की ज़द में आए हुए दो व्यक्तियों की अनुभूतियों का इतना प्रामाणिक चित्रण है—सीधा सरल, करुण—कि जब-जब कहीं युद्ध छिड़ा है, मुझे यह सरल-सीधी कहानी याद हो आई है। इस कहानी के मुक़ाबिले में द्वितीय महायुद्ध के बारे में ही लिखा हुआ स्तालिन पुरस्कार प्राप्त एलिया एहरनवुर्ग का वृहद उपन्यास ‘तूफ़ान’ मुझे बेकार लगता है।
दैनदिन प्रसंगों पर लिखने वाले के सामने एक समस्या यह भी रहती है कि कई बार ‘टॉपिक’ तत्काल बदल जाते हैं और बिना किसी टॉपिक को मन में रचाए-बसाए लिखने वाले घपले में पड़ जाते हैं। उस वक़्त जब भुट्टो, अयूब और पाकिस्तानियों को हमारे गीतकार और कथाकार गालियाँ दे रहे थे और युद्ध अथवा उसके मोर्चों का कोई अनुभव प्राप्त किए बिना, मोर्चों की कहानियाँ लिख रहे थे, ताशकंद समझौता हो गया और उनकी रचनाएँ, जिसमें कोई स्थाई तत्व न था, बेकार हो गई। टॉपिकल फ़िल्में बनाने वालों की-सी दशा इन लेखकों की हुई।
अंत में दो-तीन दिलचस्प स्थितियों की ओर मैं पाठकों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिस प्रकार 1936 के आसपास प्रगतिशील आंदोलन बड़े ज़ोरों से उठा था, और उसमें बड़े-बड़े व्यक्तिवादियों के पाँव डगमगा गए थे, उसी तरह पिछले कुछ वर्षों में ‘नए’ का नाम धर ‘नई कविता’ की नक़ल में, व्यक्तिपरक कहानियों का आंदोलन कुछ ऐसे उठा (कारण मैं ऊपर बता चुका हूँ) कि न केवल माने हुए प्रगतिशीलों के पाँव डगमगा गए, वरन नया कहाने के चक्कर में उन्होंने भी वैसी ही व्यक्तिमूलक निरुद्देश्य कहानियाँ लिखीं। कुछ बीच के कथाकार तो ऐसे भटके कि फिर अपनी राह पर आ नहीं सके। लेखकों की ही नहीं, स्वयं प्रगतिशील आलोचकों की दृष्टि भी धुँधला गई और ‘नया’ कहाने की प्रतिस्पर्धा में उन्होंने न केवल घोर व्यक्तिपरक कहानियों को सराहा, वरन प्रगतिशील कहानियों की निंदा भी की। ऐसे आलोचकों में नामवर प्रमुख रहे। उन्होंने न केवल निर्मल वर्मा की नितांत व्यक्तिपरक कहानियों में प्रगतिशील तत्व ढूँढ़ निकाले, वरन् विष्णु प्रभाकर की ज़बरदस्त और मन पर अमिट प्रभाव छोड़ने वाली समष्टिमूलक कहानी ‘धरती अब भी घूम रही है’ को फ़ार्मूला कहानी कहकर नकार दिया। बीच के लेखकों में यादव बुरी तरह रपट गए। ‘जहाँ लक्ष्मी क़ैद है’, ‘बिरादरी बाहर’, ‘पास फ़ेल’—जैसी समष्टिमूलक कहानियाँ लिखते हुए उन्होंने ‘छोटे-छोटे ताजमहल’ और ‘प्रतीक्षा’—जैसी कहानियाँ लिखीं। उनका ताज़ा संग्रह ‘अपने पार’ देखता हूँ तो लगता है कि वे बदस्तूर रपटे हुए हैं और अपनी रविश पर पुनः लौटने की उनके यहाँ कोई संभावना नहीं। कमलेश्वर, जिन्होंने ‘खोई हुई दिशाएँ’ और ‘नीली झील’ जैसी समष्टिपरक कहानियाँ लिखी थीं, ‘दुखों के रास्ते’ और जो लिखा नहीं जाता’ जैसी कहानियाँ लिखने लगे। श्रीकांत वर्मा ने लगातार अनुभूतिशून्य कहानियाँ लिखीं। यही नहीं, अपनी मिट्टी तक को नकारकर वे एकदम अंतर्राष्ट्रीय बन गए। मुझे श्रीकांत वर्मा की मजबूरी समझ में आती थी, लेकिन कमलेश्वर अथवा यादव की नहीं—सिवाए इसके कि नए कहाने के फ़ैशन में वे पीछे नहीं रहना चाहते थे। इधर कमलेश्वर के संबंध में भी यह बात साफ़ हो गई कि उनके सामने फ़ैशन का नहीं, श्रीकांत वर्मा की तरह नौकरी का चक्कर था। सेठाश्रय में जाने के लिए पुरानी रविश को छोड़ना ज़रूरी था। रहे यादव तो उनकी स्थिति न ख़ुदा ही मिला न विसाले-सनम’ की-सी-हो गई। वे इन कैरियरिस्टों के पीछे लगकर अपनी रविश से हट भी गए और उनके हाथ भी कुछ नहीं आया।
मैंने इन सब लोगों के वक्तव्य पढ़े हैं और उनमें जो उलझाव हैं, वह वर्तमान सामाजिक और साहित्यिक स्थितियों में मेरी समझ में आता है। जो बात मेरी समझ में नहीं आती, वह यह है कि क्या कोई सचमुच अपनी मिट्टी को पूरी तरह नकार सकता है? क्या राजधानी की किसी ऊँची इमारत के वातानुकूलित कमरे में बैठा कोई भावप्रवण, संवेदनशील लेखक यह भुला सकता है कि गाँव या क़स्बे में उसका एक घर है और घर में उसके कुछ आत्मीय हैं।...इधर ‘पिता’ नाम के जीव को लेकर नए लेखकों ने कई कहानियाँ लिखी हैं और इस संबंध के प्रति अपनी वितृष्णा प्रकट की है। पिता को संबोधित कर कई कविताएँ भी लिखी गई हैं—लेकिन क्या कोई लेखक अपने पिता को, जिसका रक्त उसकी धमनियों में प्रवाहित है, पूरे तौर पर नकार सकता है?—वह जो है, बुरा या भला, उसी के कारण है—उसकी स्पर्धा या प्रतिक्रिया में है। फिर क्या हमारे लेखक नहीं जानते कि वे भारतीय निम्न मध्यवर्ग के हैं और महज़ बौद्धिक आधुनिकता से वे व्यक्तिमूलक या समष्टिमूलक कोई इंकलाब बरपा नहीं कर सकते।...मैंने उनको अंध-परंपरावादियों की तरह बच्चे के जन्म पर बीवी को साथ लेकर अलोपी देवी या विंध्यादेवी या शीतलादेवी की पूजा को जाते देखा है। बीवी को मित्र से ज़रा हँसकर बातें करते देख, ईर्ष्या से प्राण देते और अपनी तथा उसकी ज़िंदगी दूभर बनाते देखा है। सुहागरात में पत्नी के सामने गर्व से अपने इश्क़ के क़िस्से सुनाते और पत्नी को कोई अपना ‘अफ़ेयर’ सुनाने के लिए कोंचते और उस सरला को अपना कोई क़िस्सा सुना देने पर अतीव यंत्रणा देकर उसका त्याग करते या उससे ग़ुलामों का-सा बर्ताव करते देखा है। मैंने उन्हें बच्चों को पीटते, अपने विवाह पर दहेज की बांछा करते और दसियों दूसरी ऐसी हरकतें करते देखा है, जो किसी सच्चे आधुनिक लेखक के लिए लज्जाजनक हैं। हमारे अधिकांश लेखक चमड़ी के नीचे वही पुराने भीरु परंपरावादी हैं, जो परम आज्ञाकारिणी बीवी चाहते हैं, बराबर की संगिनी नहीं—बातें करने में चाहे वे सात्र और मादाम बोबुआ के जीवन को अपना आदर्श बाताएँ! यही कारण है कि उनकी अधिकांश कहानियाँ अनुभूतिशून्य और झूठी उतरती हैं।
रहा नया भाव-बोध और विद्रोह, तो कल्पना कीजिए कि कल किसी कारण अचानक सेठों के आश्रय में निकलने वाली सभी पत्र-पत्रिकाएँ प्रगतिशील लोगों के अधिकार में आ जाती हैं। वे अच्छा पारिश्रमिक देती हैं और समष्टिपरक रचनाओं की माँग करती हैं। तब, क्या कोई बता सकता है कि आज के इतने सारे नए लेखकों में से कितने ऐसे नहीं हैं, जो समष्टि के दुख-दर्द का, उसकी गंदगी-ग़लाज़त का, उसके दुराचार या भ्रष्टाचार का, उसकी आस्थाओं और आदर्शों का चित्रण न करने लगेंगे और जितने ज़ोर से वे आज परंपराओं से एकदम कट जाने का शोर मचा रहे हैं, उससे दुगुने ज़ोर से परंपराओं के साथ अपने जुड़े होने का शोर न मचाने लगेंगे? आज जो लेखक मज़दूरों की पत्तल छोड़कर सेठों के यहाँ चाँदी की थाली अपना बैठे हैं, तब वे उस थाली को छोड़कर बड़ी हुमक के साथ उसी पत्तल पर आ बैठेंगे। मेरा निश्चित मत है कि अधिकांश ऐसा ही करेंगे। जो नहीं कर पाएँगे, वे चुप हो जाएँगे। एक-दो प्रतिशत ऐसे लेखक होंगे जो सच्चे व्यक्तिवादी होंगे और वे लोग चाहे उन प्रगतिशील पत्र-पत्रिकाओं में न छपें, पर लिखते रहेंगे, और अच्छा लिखते रहेंगे।
आज की धाँधली में, जब बड़ी शक्तियों का करोड़ों रुपया इसलिए यहाँ खर्च हो रहा है कि देश की एक भाषा न हो और अंग्रेज़ी बनी रहे; जब विदेशों से ढेरों पतनशील साहित्य देश में आ रहा है; जब विदेशों के व्यक्तियों को हमारी सेठाश्रयी पत्र-पत्रिकाएँ लगातार उछाल रही हैं; जब इस देश की परंपराओं को तोड़ने, इसे नैतिक रूप से खोखला करके पूँजीवाद के मुनाफ़े की मंडी बनाने की कोई क़सर नहीं उठाई जा रही; जब विदेशी बीटिनिकों के अनुकरण में हमारे नए लेखक गाँजे और चरस के दम लगा रहे हैं और बिना इस बात का ख़याल किए कि यह गर्म मुल्क है, ज़्यादा शराब यहाँ नहीं सुहाती, ऐस्प्रो की गोलियाँ खा-खाकर शराब पी रहे हैं और दो-एक ने तो मिलर के ‘ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर’ के नायकों की नक़ल में जान-बूझकर उपदंश तक मोल ले लिया है—ऐसी भारत-व्यापी धाँधली में कुछ ऐसे लेखक ज़रूर हैं, चाहे वे दो-एक प्रतिशत हो क्यों न हों, जो न केवल भारतीय होने का गर्व कर सकते हैं, बल्कि जिन्हें इस मिट्टी से, इसकी संस्कृति से, इसकी परंपराओं से, इसके इतिहास से प्रेम है। पुराने में जो बुरा है, उसकी कटु आलोचना करते हैं, पर उससे एकदम कटना पसंद नहीं करते। जो समष्टि की मूर्खताओं पर चाहे जितना हँस लें या उसकी आलोचना कर लें, पर उससे पीठ नहीं मोड़ सकते। जो आज़ाद होकर और भी ग़ुलाम नहीं हो गए हैं। जिनके दिमाग़ पर दूसरों का अधिकार नहीं और जो सरकारी आश्रय अथवा सेठाश्रय से मुक्त रहकर स्वतंत्र ढंग से सोच सकते हैं। अपनी अनुभूति और अपने चिंतन-मनन की तुला पर तौलकर समष्टि अथवा व्यष्टिपरक कहानियाँ लिख सकते हैं। जिन्हें मानव कहलाने में शरम नहीं, जो समाज के घावों को देखकर उससे मुँह नहीं मोड़ते, वरन उन पर निश्तर लगाने अथवा उनका इलाज सुझाने के अपने बौद्धिक कर्तव्य से नहीं चूकते। लिखना जिनके लिए शौक़ नहीं, न केवल जीवन-यापन या प्रतिष्ठा या ख्याति का साधन है। लिखना जिनका जीवन है।...बाहर के पाठक जब भारत को देखना चाहेंगे तो इन्हीं लेखकों की रचनाओं में देखेंगे और आने वाली सदियों में आज के भारतीय समाज का चित्रण यदि कहीं मिलेगा तो इन्हीं लेखकों की रचनाओं में मिलेगा—ऐसा मेरा विश्वास है।
- पुस्तक : अश्क 75 द्वितीय भाग (पृष्ठ 253)
- रचनाकार : उपेन्द्रनाथ अश्क
- प्रकाशन : राधाकृष्ण प्रकाशन
- संस्करण : 1986
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.


