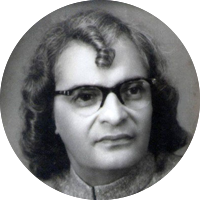भारतीय साहित्य परंपरा में शृंगार और अध्यात्म एक-दूसरे के विरोधी न समझे जाकर परस्पर पूरक ही माने गए है और उनका पोषण, भाई-बहनों की तरह, एक ही साथ, एक ही रस तत्व द्वारा होता आया है। लोक दृष्टि से ये दोनों मूल्य भले ही विभक्त कर दिए गए हों—पर रहस्य, और कुछ अंशों में, भक्ति साहित्य में भी जहाँ कहीं रस चेतना या भावना को अलौकिक का स्पर्श मिला है, वहाँ शृंगार और अध्यात्म के उपादानों एवं प्रतीकों ने एक दूसरे के प्रस्फुटन तथा विकास में सहायता ही दी है। कालिदास ने कुमार-संभव में शिव-पार्वती जैसे उच्चतम चेतना मूल्यों को शृंगार भूमि पर अवतरित करा कर तथा उनकी अंतः रस क्रीड़ा को मानवीय परिधान पहना कर अपनी काव्य कल्पना का चरमोत्कर्ष दिखलाया है। शाकुंतल में भी अध्यात्म की भूमि पर शृंगार ही का परिपाक हुआ है। शृंगार और अध्यात्म भारतीय चैतन्य में श्री राधाकृष्ण के प्रतीकों के रूप में एक दूसरे के अत्यंत निकट आकर परस्पर तन्मय हो गए हैं—उनका एकत्व वहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। शृंगार और अध्यात्म की ऐसी सर्वांगीण अभिव्यक्ति तथा परिपूर्ण एकता श्री राधाकृष्ण के औद्भौम विराट् व्यक्तित्वों के चतुर्दिक निर्मित साहित्य के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। उनके उच्च रस परिप्रोत चरित्र जैसे शृंगार और अध्यात्म के रहस्य मिलन के शाश्वत अभिसार स्थल हैं।
वास्तव में शृंगार का संतुलन तथा उन्नयन ही अध्यात्म है। शृंगारहीन अध्यात्म गीत स्वर लय विहीन रिक्त-हृदय बाँसुरी-सा है। जहाँ अध्यात्म शृंगार की व्यापक धरातलों पर न उठा कर उसके मांसल भार एवं रंगीन परिधान से दब या छिप जाता है वहाँ श्री जयदेव के गीत गोविंद की तरह वह निःसंदेह विकासोन्मुखी न रहकर ह्रासोन्मुखी बन जाता है। हिंदी रीति काव्य के अंतर्गत राधाकृष्ण की लीला का अधिकांश निदर्शन साहित्य में, तथा वाममार्ग की अनेक क्रियाओं एवं पूजन विधियों का निरूपण धर्म में, उपर्युक्त ह्रासयुगीन मनोवृत्ति का अत्यंत स्पष्ट उदाहरण है। कृष्ण-साहित्य में तत्वतः जहाँ श्री राधा परम चेतना तथा स्वरूपा एवं ह्लादिनी शक्ति की प्रतीक हैं वहाँ वह शृंगार सिंधु लहरी भी है—शृंगार की सर्वोच्च शिखर लहरी पर खड़ी परम चेतना की यह वैष्णव कल्पना शृंगार और अध्यात्म के अन्योन्याश्रित संबंध तथा अंतरैक्य के सत्य को जैसे अपनी समग्रता में मूर्तिमान कर, उसे सहृदय जन-साधारण के लिए सहज सुलभ कर देती है।
कबीर की “करले शृंगार चतुर अलबेली साजन के घर जाना होगा” अथवा “घूँघट के पट खोल री” जैसी उक्तियों में हम देखते हैं कि शृंगार अध्यात्म के गले में बाँहें डाल कर स्वयं तो ऊपर उठ ही जाता है वह अध्यात्म को भी भावबोध अथवा रस-बोध के निकट ले आता है। सुंदरता के छवि गृह में ऊर्ध्व दीपशिखा की तरह स्थित अध्यात्म की ज्योति, रस से स्नेह-सिक्त होकर, जीवन सौंदर्य को परिपूर्णता प्रदान करती है। इस प्रकार के अनेकानेक उदाहरण भारतीय साहित्य से उपस्थित किए जा सकते हैं जहाँ शृंगार अध्यात्म की अवतारणा करने के लिए सबसे सबल, स्वच्छ तथा स्पष्ट माध्यम सिद्ध होता है। वाल्मीकि, व्यास तथा कालिदास जैसे क्रांतद्रष्टा एवं कलाप्रवण कवि-ऋषियों तथा सौंदर्य स्रष्टाओं की यह गंभीर साहित्य परंपरा ही रही है कि उन्होंने देह तथा आत्मा को, अथवा प्राण तथा मन को, मानव-सत्य के अविभाज्य अंग मान कर, उनके बहिरंतर के वैभव को एक साथ काव्य सूत्र में गुंफित कर, आलोक को सौंदर्य के करतल पर स्थापित किया है।
मध्ययुगों से भारतीय मानस में जीवन चेतना तथा सांसारिकता के प्रति जो एक निषेध तथा वर्जना की धारणा प्रवेश कर गई है उससे शृंगार तथा अध्यात्म दो विभिन्न विरोधी इकाइयों में सीमित होकर स्वर्ग और नरक के अतिमूल्यों की तरह विभक्त हो गए हैं। हमारी सामंती संस्कृति आध्यात्मिक बौद्धिक प्राणिक तथा भौतिक दृष्टि से श्रीकृष्ण चैतन्य के रूप मे परिपूर्ण अभिव्यक्ति पाकर कालांतर में विघटित होने लगती है। इस विघटन के फलस्वरूप हमारी शृंगार भावना भी अधोमुखी रूप ग्रहण कर लेती है। और अनेक संकीर्ण नैतिक दृष्टिकोण तथा ह्रासयुगीन सामाजिक विकृतियाँ हमारी जीवन दृष्टि को कुंठित कर देती है। रस के मूल आध्यात्मिक स्रोत से विच्छिन्न हो जाने के कारण जातीय मन में अनेक प्रकार के खोखले जीवन-विमुख आदर्श घर कर लेते हैं। सामाजिक यथार्थ को धारणा वैयक्तिक सुखवाद की भावना से ग्रस्त हो जाती है और राग भावना को सामूहिक संतुलन देने के बदले हम उसे नैतिक विरक्ति तथा क्षणभंगुर इंद्रिय तम का रूप देकर उपेक्षणीय तथा हेय मानने लगते है।
जिस प्रकार चेतना ही पदार्थ बनकर अपनी अभिव्यक्ति के लिए भौतिक आधार या माध्यम प्रस्तुत करती है उसी प्रकार अध्यात्म ही शृंगार बनकर नित्य नवीन सौंदर्य-बोध के क्षितिजों को उद्घाटित करता है। मानव सभ्यता के इतिहास की सामंती सीमाओं के कारण–दूसरे शब्दों में भौतिक शक्तियों पर मानव का अधिकार न होने के कारण–पुरानी दुनिया की मानवता का संस्कृतीकरण एक सीमित क्षेत्र के भीतर सीमित रूप ही में संभव हो सका है। संस्कृतीकरण और अध्यात्मीकरण के बीच एक बहुत गहरी और व्यापक खाई रह गई है जिसे जगत के प्रति वैराग्य, जीवन के प्रति निषेध तथा अनेक प्रकार की नैतिक वर्जनाओं आदि से पाट कर व्यक्ति चेतना का मात्र भावना के स्तर पर ही अध्यात्मीकरण अथवा रागोन्नयन संभव हो सका है। इस प्रकार शृंगार और अध्यात्म दो परस्पर घातक, एक-दूसरे से मेल न खाने वाली, सीमित ऋण इकाइयों में बँट गए और उनका आपस का संबंध दृष्टि से ओझल हो जाने के कारण शृंगार इद्रियों के पंक में रेंगने वाली अधोमुखी वृत्ति बन गया और अध्यात्म श्मशानवासी या शुष्क वैराग्य के मरुस्थल में विचरने वाला, आकाश कुसुमवत्, जिसके मूल प्राणों के उर्वर धरातल से कट जाने के कारण वह लौकिक सामाजिक जीवन के लिए धीरे-धीरे अनुपयोगी तथा दुर्लभ हो गया। भारतीय दर्शन की खोज या शोध तो ठीक रही पर उसका उपयोग अलीक तथा भ्रामक रहा। दर्शन की दृष्टि से अद्वैतवादी होने पर भी भौतिक परिस्थितियों की सीमाओं के कारण, हम संस्कृति की दृष्टि से, सदैव द्वैतवादी ही रहे और सहज व्यापक अध्यात्मीकरण का संचरण कुछ क्लिष्ट नैतिक सिद्धांतों का रूप धारण कर कठोररूढ़ि-रीति-गत परंपराओं में जड़ीभूत हो गया, जिसके कारण जातीय जीवन का सतत प्रवाहमान तत्व, शृंगार तथा अध्यात्म की मूल्यांकन संबंधी विषमताओं के कारण, सत्य, शिव तथा सुंदर की अभिव्यक्ति से वंचित रह गया और अपने प्राणिक दारिद्र्य के कारण हम मानसिक, कायिक तथा भौतिक दारिद्र्य से भी ग्रस्त हो गए।
तत्वतः शृंगार और अध्यात्म दोनों ही राग भावना या रागचेतना के दो अविभाज्य छोर हैं और एक के संबंध में ही दूसरे का मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। शृंगार की सक्रिय प्राणवत्ता से विरहित अध्यात्म मात्र वैयक्तिक आत्म रति अथवा शुष्क सामाजिक वैराग्य बनकर रह जाता है। और अध्यात्म से वंचित शृंगार बहिर्जीवन के क्षणिक भोग-विलास में सन कर मलीन हो उठता है। जिस प्रकार देह के आधार के बिना मन तथा चेतना का विकास संभव नहीं—वे एक निष्क्रिय अतींद्रिय स्थिति भर रह जाते हैं, उसी प्रकार शृंगार तत्वों से वियुक्त अध्यात्म भी निर्जीव, नीरस, शून्य-ब्रह्म की उपलब्धि-मात्र रह जाता है। शृंगार चेतना या भावना के सामाजिक समन्वय के अभाव में मात्र अध्यात्म का दंभ भरने वाला समाज, हमारे मध्ययुगीन ढाँचे की तह, निष्क्रिय, निष्प्राण, सौंदर्य तथा लोक मंगल की दृष्टि से, निःशक्त एवं अनुर्वर हो जाता है। शृंगार संतुलित सामाजिक जीवन का सौंदर्य ही आध्यात्मिक चेतना का शरीर है, जिसके बिना उसका अस्तित्व पूर्ण सक्रिय नहीं हो सकता।
आज नारी तन के स्तर पर शृंगार भावना का मूल्य आँकना अनुचित होगा, उसे धरा जीवन के स्तर पर देखना स्वाभाविक होगा। गृहस्थ जीवन के मूल्यों के रूप में शृंगार भावना का आंशिक ही विकास संभव हो सका है। आज विश्व जीवन को हमें एक अधिक उच्च तथा व्यापक चेतना के प्रकाश में देखना है और राग चेतना के चिरंतन सौंदर्यपूर्ण गंभीरतम स्तर, जो अभी प्रच्छन्न एवं अविकसित ही रह गए हैं, उन्हें मानव-जीवन का सक्रिय अंग बनाकर नवीन रांगानुभूति में प्रस्फुटित तथा परिणत करना है। इंद्रिय द्वारों में कुसुमित इस सार्वभौम रागचेतना को नए आध्यात्मिक प्रकाश में नवीन मूल्यों के रूप में ग्रहण कर आज स्त्री-पुरुष के युग्म जीवन को नवीन अनुराग, सौंदर्य तथा आनंद से मड़ित करना है। और उसे प्राचीन मध्ययुगीन अनेक प्रकार के नैतिक निषेधों, वर्जनाओं तथा कुंठाओं से उबार कर उसमें नवीन सामाजिक सामंजस्य, वैयक्तिक संगति तथा मानवीय निखार भरना है। अपनी अनेक रचनाओं में मैंने राग भावना के उन्नयन के साथ ही नवीन प्राणिक जीवन की स्वीकृति पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है और शृंगार और अध्यात्म के बीच पड़ी प्राचीन खाई को तथा मध्ययुगीन नैतिक अवरोधों को अतिक्रम कर नवीन विश्व-जीवन की सौंदर्य चेतना के प्रस्फुट स्वप्न संचरण के शील-सौम्य सौंदर्य-मुखर, गतिमय संगीत को अपने छदों में बाँधने की चेष्टा की है।
“आत्मिका” में मैंने एक स्थान पर कहा है:
भू पर संस्कृत इंद्रिय जीवन, मानव आत्मा को रे अभिमत
ईश्वर को प्रिय नहीं विरागी, संन्यासी, जीवन से उपरत।
आत्मा को प्राणों से बिलगा अधिदर्शन ने की जग की क्षति—इत्यादि
अन्यत्र इसी कविता में मैंने कहा है—
स्वर्ग नरक इह परलोकों में व्यर्थ भटकते धर्ममूढ़ जन
ईश्वर से इंद्रिय जीवन तक एक संचरण रे भू पावन।
शृंगार तथा अध्यात्म को संयोजित करते हुए, मैंने प्राणों एव इंद्रियों के जीवन की महत्ता दिखाते हुए वाणी में कहा है—
प्राण, धन्य तुम, रजत हरित ज्वारों से उठकर
आशा आकांक्षा के मोहित फेनिल सागर,
चंद्र कला को बिठा स्वप्न की ज्वालतरी में
तुम बखेरते रत्न छटा आनंद-तीर पर!
मैं उपकृत इंद्रियों, रूप रस गध स्पर्श स्वर
लीला द्वार खुले अनंत के बाहर भीतर,
अप्सरियों से दीपित सुर-धनुओं के अंबर
निज असीम शोभाओं में तुम पर न्योछावर।
यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूप को ज्वालतरी में बैठी चंद्रकला आध्यात्मिक चेतना ही है। मेरे विचार में शृंगार और अध्यात्म का परिणय, निःसदेह, नवीन जीवन सौंदर्य को जन्म देगा, जिसका अवतरण एवं प्रस्फुटन मानवता के लिए नवीन आशा उल्लास तथा लोक मंगल का सूचक होगा।
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 274)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.