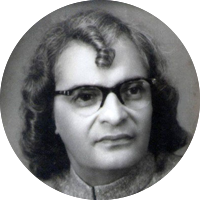मैं स्वतंत्र भारत के नवयुवक कलाकारों का स्वागत करता हूँ। मैं उनकी आँखों में सौंदर्य के स्वप्न, उनके हृदय की धड़कन में संस्कृत भावनाओं का संगीत और उनके सुंदर मुखों पर मनुष्यत्व के गौरव की झलक देखना चाहता हूँ।
आप बुद्धिजीवी तथा कलाकार है। आपका क्षेत्र भीतर का क्षेत्र है, आपको सूक्ष्म का परिचालन करना है। विकसित मस्तिष्क के साथ संस्कृत हृदय की भी आवश्यकता है। विकसित मस्तिष्क से मेरा अभिप्राय युग के प्रति प्रबुद्ध, विश्व-जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक मन से है, और संस्कृत हृदय से मेरा प्रयोजन उस हृदय से है जिसमें राग-द्वेष आदि जैसी विरोधी वृत्तियों में मनन तथा साधना द्वारा संतुलन आ गया हो तथा जो नवीन सांस्कृतिक चेतना के प्रति उद्बुद्ध हो। ऐसा संतुलन साधारण लोकजीवन से ऊँचे ही स्तर पर स्थापित किया जा सकता है और परिस्थितियों की चेतना से ऊपर उठने के लिए एक कला-जीवी सौंदर्य स्रष्टा को प्रारंभ में स्वस्थ अभ्यासों, उन्नत संस्कारो एवं विकसित रुचियों के प्रभावों की आवश्यकता होती है।
मनुष्य के विन्यास में जहाँ मन का स्तर है वहाँ एक प्राणों का भी स्तर है। यह हमारी लालसाओं, आवेगों, प्रवृत्तियों, भावना, आशा, स्वप्न आदि का स्तर है और यही शक्ति का भी स्तर है। महान् कलाकारों में स्वभावत: ही प्राणशक्ति का अधिक प्रवाह तथा प्रसार देखने को मिलता है। यह प्राण-शक्ति शीघ्र ही हमारे अभ्यासों तथा रुचियों का स्वरूप धारण कर लेती है। अतः एक कलाकार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वह किसी मत या वाद के प्रभाव से अथवा तीव्र राग-विराग के कारण विशेष अभ्यासों की सीमाओं के भीतर न बँध जाए। उसे सदैव मुक्त-हृदय, संवेदनशील तथा ग्रहणशील बना रहना चाहिए और अपने प्राणों के आवेष्टन को परिष्कृत कर उसे सौंदर्य-ग्राही, ऊर्ध्वगामी बनाकर द्वेष-क्रोध आदि की निम्न वृत्तियों से ऊपर उठना चाहिए, जिससे उसके प्राणों के प्रवाह में एक संगीत, सामंजस्य, तन्मयता, व्यापकता तथा भिन्न स्वभावधर्मा मानव-समूह के प्रति सौंदर्य तथा सहानुभूति का संचार हो सके।
किसी कलाकृति में मुख्यतः तीन गुणों का समावेश रहना चाहिए—(1) सौंदर्य-बोध, (2) व्यापक गंभीर अनुभूति, (3) उपयोगी सत्य। इनका रहस्य-मिश्रण ही कला-वस्तु में लोकोत्तरानंददायी रस की परिपुष्टि करता है। हमें देखना चाहिए कि कलाकार के सौंदर्य-दर्शन में कितना मार्जन, ऊर्ध्वप्राणता तथा रहस्य-संकेत है। वह किसी विशेष रुचि या अभ्यास से तो कुंठित नहीं, और यदि है तो उसका कारण बाह्य उपादानों में है अथवा अंतर के भाव-सत्य में। दूसरा, हमें देखना चाहिए कि उसकी अनुभूति में कितनी गहराई, व्यापकता तथा ऊँचाई है। उसने जीवन के साथ कितना और किस प्रकार का सामंजस्य स्थापित किया है—भीतर के जिस दर्पण में उसने मानव जीवन के सत्य को ग्रहण तथा प्रतिफलित किया है, वह चेतना कितनी सूक्ष्म, प्रभावशाली तथा अतल-स्पर्शी है। तीसरा, हमें विचार करना चाहिए उस कृति की उपयोगिता पर—अर्थात् वह केंद्रीय सत्य को लोक जीवन की भीतरी-बाहरी परिधियों तक प्रसारित करती है कि नहीं। इसका सबसे उत्तम उदाहरण हमारे पास तुलसीकृत रामायण है, जो व्यक्ति के अंतरतम विकास में भी अपने युग की सीमा के भीतर, सहायता पहुँचाता है तथा लोक समुदाय को भी बल प्रदान करता है।
किंतु इन सबसे महत्त्वपूर्ण, मेरी दृष्टि में, एक और भी वस्तु है, जिसके पूरक उपर्युक्त तीनों मान वह है किसी कलाकृति में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व हैं अर्थात् जो चेतना, जो प्रकाश, जो संस्कार किसी कलाकृति को पढ़ने पर अज्ञात रूप से आपको प्रभावित कर आपका निर्माण करने में सफल होते है जिन सूक्ष्म उपादानों का एक कलाकृति सक्रिय वितरण करती है। आज जबकि हम एक संक्रांतियुग के शिखर पर बैठे हैं, जिसके अंतस्तल में धरती को आंदोलित करने वाली ज्वालामुखी सुलग रही है, हमें सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति सबसे अधिक चैतन्य रहना चाहिए। संस्कृति मानव-चेतना का सारपदार्थ है, जिसमें मानव जीवन के विकास का समस्त संघर्ष, नाम, रूप, गुणों के रूप में संचित है, जिसमें हमारी ऊर्ध्वगामी चेतना या भावनाओं का प्रकाश तथा समतल जीवन और मानसिक उपत्यकाओं की छायाएँ गुंफित है; जिसमें हमें सूक्ष्म और स्थूल, दोनों धरातलों के सत्यों का समन्वय मिलता है। संस्कृति में हमारी धार्मिक, नैतिक तथा रहस्यात्मक अनुभूतियों का ही सार-भाग नहीं रहता, उसमें हमारे सामाजिक जीवन में बरते जाने वाले आचार-विचार एवं व्यवहारों के भी सौंदर्य का समावेश रहता है। यदि हम सोचते हैं कि हम इसी क्षण से एक आमूल नवीन संस्कृति को जन्म दे सकते हैं, तो हम ठीक नहीं सोचते। क्योंकि जो सांस्कृतिक चेतना अथवा सौंदर्य-भावना आज हमारे भीतर काम कर रही है, उसके ताने-बाने में मानव जीवन की सहस्रों वर्षों की अनुभूतियाँ, सुख-दु:ख, सद्-असद्, सत्य-मिथ्या की धारणाएँ, उसका सूक्ष्म ज्ञानजगत् तथा बहिरंतर का समस्त छाया प्रकाश ग्रथित है। जिस प्रकार भाषा एक संगठित सत्य है, उसी प्रकार संस्कृति भी। वह स्वभावजन्य गुण नहीं, विकासक्रम से उपलब्ध वस्तु या सत्य है। मैं कुछ शब्द-ध्वनियों द्वारा, जो हमारी चेतना में सार्थक रूप से संगठित है, आपके मन में कुछ विचारों, भावनाओं एवं संवेदनों को जगा रहा हूँ। यदि मैं कुछ ऐसी ध्वनियों का प्रयोग करूँ, जिनका हमारे भीतर सार्थक संगठन नहीं हैं, तो आप उनसे कुछ भी अभिप्राय नहीं ग्रहण कर सकेंगे। इसी प्रकार हमारा सांस्कृतिक ज्ञान भी हमारी अंतश्चेतना में संगठित गुण है, जो हमें सत्य-मिथ्या का मान देता है और हमारी शिव-अशिव, सुंदर-असुंदर, पाप-पुण्य आदि की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी सांस्कृतिक मान्यताएँ प्राय: हमारी प्राकृतिक स्वभावज लालसाओं तथा ऐंद्रिय संवेदनों की विरोधी भी होती है, हम इन्हें संस्कार कहते हैं।
आप जिस जाति और जिस देश की भी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन करें, आपको उसमें अंत संगठन के नियम मिलेंगे और उनमें बाह्य दृष्टि से विभिन्नता होने पर भी एक आंतरिक साम्य तथा सूक्ष्म एकता मिलेगी। विभेदों का कारण देश-काल की परिस्थितियाँ होती है और एकता का आधार समान मानवीय अनुभूति का सत्य। समस्त सत्य केवल मात्र मानवीय सत्य है, उसके बाहर या ऊपर किसी भी सत्य की कल्पना संभव नहीं है। वनस्पति-जीवन, पशु-जीवन से लेकर—जो मनुष्य चेतना से नीचे के धरातल है—स्वर्गलोक के देवताओं और उनसे भी परे का ज्ञान-विस्तार केवल मानवीय सत्य है। मनुष्य चाहे बाहर जितनी जातियों, धर्मों और वर्गों में विभक्त हो, वह भीतर से एक ही है; इसलिए समस्त मानव जीवन के सत्य को एक तथा अखंडनीय समझना चाहिए।
यद्यपि हम अंत: संगठन के सत्य में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकते, हम उसके विकास के नियमों का अध्ययन कर उसे विशेष युग में विशेष रूप से प्रभावित एवं परिवर्तित कर सकते हैं तथा उसका यथेष्ट रूपांतर भी कर सकते हैं। हमारा युग एक ऐसा ही संक्रांति का युग है। जबकि हमें भिन्न-भिन्न जातियों, वर्गों और धर्मों की संस्कृतियों का समन्वय एवं संश्लेषण कर उन्हें मानव-संस्कृति के एक महान् विश्व-संचरण के रूप में प्रतिष्ठित करना है। आज हमें मानव चेतना के क्षीर-सागर को फिर से मथकर उसके अंतस्तल में छिपे हुए रत्नों को पहचानना है और मौलिक अनुभूतियों के नवीन रत्नों को भी बाहर निकालकर अपने युग पुरुष के स्वर्ण शुभ्र किरीट में उन्हें समय के अनुरूप नवीन सौंदर्य-बोध में जड़ना है, जिससे वह भावी मनुष्यत्व की गरिमा का वहन कर सके। इसलिए हमारे युग के साहित्यिकों तथा कलाकारों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है, जिसे हम साहस, संयम, सद्भाव तथा सहिष्णुता से ही पूरा कर सकते हैं।
सत्ता के संपूर्ण सत्य को समझने के लिए हमें व्यक्ति तथा विश्व के साथ ईश्वर को भी मानना चाहिए। ईश्वर को मानने से मेरा यह अभिप्राय नहीं कि आप विधिवत् पूजा-पाठ अथवा जप-तप करें। यह तो धर्म का क्षेत्र है और आपके स्वभाव, रुचि तथा नाड़ियों के जीवन से संबंध रखने वाली बाते हैं। ईश्वर को मानने का व्यावहारिक रूप मैं एक कलाकार के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि वह अव्यक्त के, सूक्ष्म के, अंतश्चेतना के संचरणों से भी अपने को संयुक्त रखे, और उनके प्रकाश, उनके सौंदर्य तथा शक्तियों का उपयोग कर समाज के अंतर्जीवन का निर्माण करे। उसके कंधों पर वास्तविकता तथा विवेक का ही भार न हो, वे स्वप्नों के बोझ से भी झुके रहें।
संक्षेप में, मैं चाहता हूँ कि स्वाधीन भारत की कलाकृतियाँ लोकोपयोगी सांस्कृतिक तत्वों से ओतप्रोत रहे और नवयुवक कलाकार अपनी कलाओं के माध्यम द्वारा समाज में नवीन मानव-चेतना के आलोक का वितरण करे एवं लोक-जीवन को बाहर भीतर से संस्कृत, सुरुचिपूर्ण तथा संपन्न बनाने में सहायक हो। हमारे युग के सांस्कृतिक सूत्र हैं,—मानव-प्रेम, लोक-जीवन की एकता, जीवन-सौंदर्य का उपभोग तथा विश्व-मानवता का निर्माण। यदि आप अपनी लेखनी और तूली द्वारा युग के इन स्वप्नों में रक्त-मास का सौंदर्य तथा अपनी व्यापक अनुभूति से जीवन फूंक सकें, तो आप अपने तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्य को उसी तरह निबाहेंगे, जिस प्रकार एक राजनीति के क्षेत्र का नायक लोक-संघर्ष के उत्थान-पतनों का संचालन कर जीवन की परिस्थितियों को विश्व-तंत्र का संतुलन प्रदान कर जन समुदाय को नवीन मानवता की ओर अग्रसर कर रहा है।
कलाकार के पास हृदय का यौवन होना चाहिए, जिसे धरती पर उड़ेलकर उसे जीवन की कुरूपता को सुंदर बनाना है। वह सर्वप्रथम सौंदर्य स्रष्टा है। कलाकार की सबसे बड़ी कृति वह स्वयं है। जब तक वह अपना बाहर भीतर से परिमार्जन नहीं करेगा, वह संस्कृति के दिव्य पावक तथा सौंदर्य के स्वर्गीय अलोक का आदान-प्रदान नहीं कर सकेगा। बेसुरी हृदय-वीणा से, जिसके तार चेतना के सूक्ष्म स्पर्शों के लिए सधे न हों, अंतर के संगीत की वृष्टि कैसे हो सकती है? अतएव आप जो स्वतंत्र भारत की चेतना के स्रष्टा हैं, आपको अपने को इस महाप्राण देश के गौरव का वाहक बनाना चाहिए जिसमें आप अंजलि भर-भर कर संस्कृति के स्वर्णिम पावक-ऋण जन-समाज में वितरण कर सकें। तथास्तु।
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 208)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.