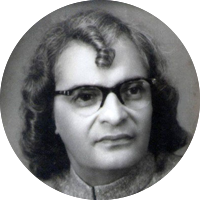मैं अपने यत्किंचित् साहित्यिक प्रयासों को आलोचक की दृष्टि से देखने के लिए उत्सुक नहीं था, किंतु हिंदी साहित्य सम्मेलन की इच्छा मुझे विवश करती है कि मैं प्रस्तुत संग्रह में अपने बारे में स्वयं लिखूँ। संभव है, मैं अपने काव्य की आत्मा को, स्पष्ट और सम्यक् रूप से, पाठको के सामने न रख सकूँ, पर जो कुछ भी प्रकाश मैं उस पर डाल सकूँगा, मुझे आशा है, उससे मेरे दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी। ‘पल्लव’ की भूमिका में काव्य के बहिरंग पर, अपने विचार प्रकट करने के बाद यह प्रथम अवसर है कि मैं अपने विकास की सीमाओं के भीतर से, काव्य के अंतरंग का विवेचन कर रहा हूँ। इस संक्षिप्त पर्यालोचन में जो कुछ भी त्रुटियाँ रह जाएँ, उनके लिए सहृदय सुज्ञ पाठक क्षमा करे।
इस सौ-सवा सौ पृष्ठों के संग्रह में मेरी सभी संग्रहणीय कविताएँ अवश्य नहीं आ सकी हैं, पर जिन पथों का मेरी कल्पना ने अनुसरण किया है, उन पर अंकित पद-चिह्नों का थोड़ा-बहुत आभास इससे मिल सकता है, और, संभव है, अपने युग में प्रवाहित प्रमुख प्रवृत्तियों और विचारधाराओं की अस्पष्ट रूप रेखाएँ भी इसमें मिल जाएँ। अस्तु––
कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कूर्मांचल प्रदेश को है। कवि-जीवन से पहले भी मुझे याद है, मैं घंटों एकांत में बैठा, प्राकृतिक दृश्यों को एकटक देखा करता था; और कोई अज्ञात आकर्षण, मेरे भीतर, एक अव्यक्त सौंदर्य का जाल बुनकर मेरी चेतना को तन्मय कर देता था। जब कभी मैं आँखें मूँदकर लेटता था, तो वह दृश्यपट, चुपचाप, मेरी आँखों के सामने घूमा करता था। अब मैं सोचता हूँ कि क्षितिज में सुदूर तक फैली, एक के ऊपर एक उठी, ये हरित-नील-धूमिल कूर्मांचल की छायांकित पर्वत श्रेणियाँ, जो अपने शिखरों पर रजत मुकुट हिमाचल को धारण किए हुए है, और अपनी ऊँचाई से प्रकाश की अवाक् नीलिमा को और भी ऊपर उठाए हुए है, किसी भी मनुष्य को अपने महान् नीरव सम्मोहन के आश्चर्य में डुबाकर, कुछ काल के लिए, भुला सकती है! और यह शायद पर्वत-प्रांत के वातावरण ही का प्रभाव है कि मेरे भीतर विश्व और जीवन के प्रति एक गंभीर आश्चर्य की भावना, पर्वत ही की तरह, निश्चल रूप से, अवस्थित है। प्रकृति के साहचर्य ने जहाँ एक ओर मुझे सौंदर्य, स्वप्न और कल्पना-जीवी बनाया, वहाँ दूसरी ओर जन-भीरु भी बना दिया। यही कारण है कि जनसमूह से अब भी मैं पर्यालोचन दूर भागता हूँ और मेरे आलोचकों का यह कहना कुछ अंशों तक ठीक ही है कि मेरी कल्पना लोगों के सामने आने में लजाती है।
मेरा विचार है कि ‘वीणा’ से ‘ग्राम्या’ तक मेरी सभी रचनाओं में प्राकृतिक सौंदर्य का प्रेम किसी न किसी रूप में विद्यमान है।
“छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले, तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन?”––
आदि ‘वीणा’ के चित्रण, प्रकृति के प्रति, मेरे अगाध मोह के साक्षी हैं। प्रकृति-निरीक्षण से मुझे अपनी भावनाओं की अभिव्यंजना में अधिक सहायता मिली है, कहीं-कहीं उससे विचारों की भी प्रेरणा मिली है। प्राकृतिक चित्रणों में प्रायः मैंने अपनी भावनाओं का सौंदर्य मिलाकर उन्हें ऐंद्रिय चित्रण बनाया है, कभी-कभी भावनाओं को ही प्राकृतिक सौंदर्य का लिबास पहना दिया है। यद्यपि ‘उच्छ्वास’ ‘आँसू’ ‘बादल’ ‘विश्ववेणु’ ‘एकतारा’ ‘नौकाविहार’ ‘पलाश’ ‘दो मित्र’ ‘झंझा में नीम’ आदि अनेक रचनाओं में मेरे रूप चित्रण के भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं।
प्रकृति को मैंने अपने से अलग, सजीव सत्ता रखने वाली, नारी के रूप में देखा है :
“उस फैली हरियाली में,
कौन अकेली खेल रही, माँ,
वह अपनी वय बाली में”––
पंक्तियाँ मेरी इस धारणा की पोषक है। कभी जब मैंने प्रकृति से तादात्म्य का अनुभव किया है, तब मैंने अपने को भी नारी-रूप में अंकित किया है। मेरी प्रारंभिक रचनाओं में इस प्रकार के हिप्नोटिज़्म के अनेक उदाहरण मिलेंगे।
साधारणतः प्रकृति के सुंदर रूप ही ने मुझे अधिक लुभाया है, पर उसका उग्र रूप भी मैंने ‘परिवर्तन’ में चित्रित किया है। मानव स्वभाव का भी मैंने सुंदर पक्ष ही ग्रहण किया है, इसी से मेरा मन वर्तमान समाज की कुरूपताओं से कटकर भावी समाज की कल्पना की ओर प्रभावित हुआ है। यह सत्य है कि प्रकृति का उग्र रूप मुझे कम रुचता है। यदि में संघर्षप्रिय अथवा निराशावादी होता, तो ‘Nature red in tooth and claw’ वाला कठोर रूप, जो जीव विज्ञान का सत्य है, मुझे अपनी ओर अधिक खींचता, किंतु ‘वह्नि, बाढ़, उल्का, झंझा की भीषण भू पर’ इस ‘कोमल मनुज कलेवर को भविष्य में अधिक से अधिक ‘मनुजोचित साधन’ मिल सकेंगे और वह अपने लिए ऐसा ‘मानवता का प्रासाद निर्माण कर सकेगा, जिसमें ‘मनुष्य जीवन की क्षण धूलि’ अधिक सुरक्षित रह सकेगी––यह आशा मुझे अज्ञात रूप से सदैव आकर्षित करती रही है :
“मनुज प्रेम से जहाँ रह सके––मानव ईश्वर!
और कौन-सा स्वर्ग चाहिए तुझे धरा पर?”
‘वीणा’ और ‘पल्लव’ विशेषतः मेरे प्राकृतिक साहचर्य काल की रचनाएँ हैं। तब प्रकृति की महत्ता पर मुझे विश्वास था और उसके व्यापारों में मुझे पूर्णता का आभास मिलता था। वह मेरी सौंदर्य-लिप्सा की पूर्ति करती थी, जिसके सिवा, उस समय, मुझे कोई वस्तु प्रिय नहीं थी। स्वामी विवेकानंद और रामतीर्थ के अध्ययन प्रकृति-प्रेम के साथ ही मेरे प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान और विश्वास में भी अभिवृद्धि हुई। ‘परिवर्तन’ में इस विचारधारा का काफ़ी प्रभाव है। अब मैं सोचता हूँ कि प्राकृतिक दर्शन, जो एक निष्क्रियता की सीमा ‘सहिष्णुता प्रदान करता है और एक प्रकार से प्रकृति को सर्वशक्तिमयी मानकर उसके प्रति आत्मसमर्पण सिखलाता है, वह सामाजिक जीवन के लिए स्वास्थ्यकर नहीं है।
“एक सौ वर्ष नगर उपवन,––एक सौ वर्ष विजन वन।
यही तो है असार संसार, सृजन, सिंचन, सहार।”
आदि भावनाएँ मनुष्य को अपने केंद्र से च्युत करने के बाद, किसी सक्रिय सामूहिक प्रयोग के लिए अग्रसर नहीं करती, बल्कि उसे जोवन की क्षणभंगुरता का उपदेश-भर देकर रह जाती है। इस प्रकार की प्रभावात्मकता (निगेटिविज़्म) के मूल हमारी संस्कृति में मध्ययुग से भी गहरे घुसे हुए हैं, जिसके कारण, जातीय दृष्टि से, हम अपने में स्वाभाविक आत्म-रक्षण के संस्कारों (सेल्फ़ प्रिज़र्वेटिव इंस्टिक्ट्स) को खो बैठे हैं, और अपने प्रति किए गए अत्याचारों को थोथी दार्शनिकता का रूप देकर, चुपचाप, सहन करना सीख गए हैं। साथ ही हमारा विश्वास मनुष्य की संगठित शक्ति से हटकर आकाश-कुसुमवत् दैवी शक्ति पर अटक गया है, जिसके फलस्वरूप हम देश पर विपत्ति के युगों में सीढ़ी-दर-सीढ़ी नीचे गिरते गए हैं।
‘पल्लव’ और ‘गुंजन’-काल के बीच में मेरी किशोर भावना का सौंदर्य स्वप्न टूट गया। ‘पल्लव’ की ‘परिवर्तन’ कविता, दूसरी दृष्टि से, मेरे इस मानसिक परिवर्तन की भी द्योतक है। इसीलिए वह ‘पल्लव’ में अपना विशेष महत्त्व रखती है। दर्शनशास्त्र और उपनिषदों के अध्ययन ने मेरे रागतत्त्व में मंथन पैदा कर दिया और उसके प्रवाह को दिशा बदल दी। मेरी निजी इच्छाओं के संसार में कुछ समय तक नैराश्य और उदासीनता छा गई। मनुष्य के जीवन के अनुभवों का इतिहास बड़ा ही करुण प्रमाणित हुआ। जन्म के मधुर रूप में मृत्यु दिखाई देने लगो, वसंत के कुसुमित आवरण के भीतर पतझर का अस्थिपंजर!
“खोलता इधर जन्म लोचन,
मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण!”
“वही मधुऋतु की गुंजित डाल
झुकी थी जो यौवन के भार,
अकिंचनता में निज तत्काल
सिहर उठती-जीवन है भार!”
मेरी जीव-दृष्टि का मोह एक प्रकार से छूटने लगा और सहज जीवन व्यतीत करने की भावना में एक तरह का धक्का लगा। इस क्षणभंगुरता के ‘बुद्बुदों के व्याकुल संसार में परिवर्तन ही एकमात्र चिरंतन सत्ता जान पड़ने लगी। मेरे हृदय की समस्त आशा-आकांक्षाएँ और सुख-स्वप्न अपने भीतर और बाहर किसी महान् चिरंतन वास्तविकता का अंग बन जाने के लिए लहरों की तरह, अज्ञात प्रयास की आकुलता में, ऊबडूब करने लगे।
किंतु दर्शन का अध्ययन विश्लेषण की पैनी धार से, जहाँ जीवन के नाम-रूप गुण के छिलके उतारकर मन को शून्य की परिधि में भटकाता है, वहाँ वह छिलके में फल के रस की तरह व्याप्त एक ऐसे सूक्ष्म संश्लेषणात्मक सत्य के आलोक से भी हृदय को स्पर्श करता है कि उसकी सर्वातिशयता चित्त की अलौकिक आनंद से मुग्ध तथा विस्मित कर देती है। भारतीय दर्शन ने मेरे मन को अस्थिर कर दिया।
“जग के उर्वर आँगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन,
बरसो लघु लघु तृण तरु पर हे चिर अव्यय चिर नूतन!”
इसी सविशेष की कल्पना के सहारे, जिसने ‘ज्योत्स्ना’ को और ‘गुंजन’ की ‘अप्सरा’ को जन्म दिया है, मैं ‘पल्लव’ से ‘गुंजन’ में अपने को सुंदरम् से शिवम् की भूमि पर पदार्पण करते हुए पाता हूँ। ‘गुंजन’ में मेरी बहिर्मुखी प्रकृति, सुख-दुख में समत्व स्थापित कर अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न करती है, साथ ही ‘गुंजन’ और ‘ज्योत्स्ना’ में मेरी कल्पना अधिक सूक्ष्म एवं भावात्मक हो गई है। ‘गुंजन’ के भाषा-संगीत में एक सुघरता, मधुरता और श्लक्ष्णता आ गई है, जो पल्लव में नहीं मिलती। ‘गुंजन’ के संगीत में एकता है, ‘पल्लव’ के स्वरों में बहुलता। ‘पल्लव’ की भाषा दृश्य जगत् के रूप-रंग की कल्पना से मांसल और पल्लवित है, ‘गुंजन’ की भाषा भाव और कल्पना के सूक्ष्म सौंदर्य से गुंजित। ‘ज्योत्स्ना’ का वातावरण भी सूक्ष्म की कल्पना से ओतप्रोत है, उसका सांस्कृतिक समन्वय सर्वातिशयता (ट्रेन्सेन्डेन्टलिज़्म) के आलोक (दर्शन) को विकीर्ण करता है।
यह कहा जाता है कि मेरी कविताओं से सुंदरम् और शिवम् से भी बड़े लक्ष्य सत्यम् का बोध नहीं होता, साथ ही उनमें वह अनुभूति की तीव्रता नहीं मिलती, जो सत्य की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। यह सच है कि व्यक्तिगत सुख-दुःख के अथवा अपने मानसिक संघर्ष को मैंने अपनी रचनाओं में वाणी नहीं दी है, क्योंकि वह मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। मैंने उससे ऊपर उठने की चेष्टा की है। ‘गुंजन’ में “तप रे मधुर-मधुर मन तथा में सीख न पाया अब तक सुख से दुख को अपनाना” आदि अनेक रचनाएँ मेरी इस रुचि की द्योतक है। मुझे लगता है कि सत्य शिव में स्वयं निहित है। जिस प्रकार फूल में रूप-रंग है, फल में जीवनोपयोगी रस और फूल की परिणति फल में सत्य के नियमों ही द्वारा होती है, उसी प्रकार सुंदरम् की परिणति शिवम् में सत्य ही द्वारा हो सकती है। संबंध यदि कोई वस्तु उपयोगी (शिव) है, तो उसके आधारभूत कारण उस उपयोगिता से रखने वाले सत्य में अवश्य होने चाहिए, नहीं तो वह उपयोगी नहीं हो सकती। इसी प्रकार अनुभूति की तीव्रता भी सापेक्ष है और मेरी रचनाओं में उसका संबंध मेरे स्वभाव से है। सत्य के दोनों रूप है––शराबी शराब पीता है, यह सत्य है; उसे शराब नहीं पीना चाहिए, यह भी सत्य है। एक उसका वास्तविक (फ़ैक्चुअल) रूप है, दूसरा परिणाम से संबंध रखने वाला। मेरी रचनाओं में सत्य के दूसरे पक्ष के प्रति मोह मिलता है; वह मेरा संस्कार है, आत्मविकास (सब्लिमेशन) की ओर जाना। अनुभूति की तीव्रता का बोध बहिर्मुखी (एक्स्ट्रोवर्ट) स्वभाव अधिक करवा सकता है, मंगल का बोध अंतर्मुखी स्वभाव (इंट्रोवर्ट), क्योंकि दूसरा कारण-रूप अंतर्द्वंद्व को अभिव्यक्त न कर उसके फलस्वरूप कल्याणमयी अनुभूति को वाणी देता है। मेरी ‘पल्लव’––काल की रचनाओं में, तुलनात्मक दृष्टि से, मानसिक संघर्ष और हार्दिकता अधिक मिलती है और बाद की रचनाओं में आत्मोत्कर्ष और सामाजिक अभ्युदय की इच्छा।
यदि मेरा हृदय अपने युग में बरते जाने वाले आदर्शों के प्रति विश्वास न खो बैठता, तो मेरी आगे की रचनाओं में भी हार्दिकता पर्याप्त मात्रा में मिलती। जब वस्तुजगत् के जीवन से हृदय को भोजन अथवा भावना को उद्दीपन नहीं मिलता, तब हृदय का सूनापन बुद्धि के पास, सहायता माँगने के लिए, पुकार भेजता है :
‘आते कैसे सूने पल, जीवन में ये सूने पल,
***
‘खो देती उर की वीणा झंकार मधुर जीवन की’––
आदि उद्गार ‘गुंजन’ में आए हैं। ऐसी अवस्था में मेरा हृदय वर्तमान जीवन के प्रति घृणा या विद्वेष की भावना प्रकट कर सकता, और मैं संदेहवादी या निराशावादी बन सकता था। पर मेरे स्वभाव ने मुझे रोका और मैंने इस बाह्य निश्चेष्टता और सूनेपन के कारणों को बुद्धि से सुलझाने का प्रयत्न किया। यही कारण है कि मेरी आगे की रचनाएँ भावनात्मक न रहकर बौद्धिक बनती गईं––या मेरी भावना का मुख प्रकाशवान् हो गया? ‘ज्योत्स्ना’ में मेरी भावना और बुद्धि के आवेश का मिश्रित चित्रण मिलता है।
जब तक रूप का विश्व मेरे हृदय को आकर्षित करता रहा, जोकि एक किशोर-प्रवृत्ति है, मेरी रचनाओं में ऐंद्रिय चित्रणों की कमी नहीं रही। प्राकृतिक अनुराग की भावना क्रमशः सौंदर्य प्रधान से भावप्रधान और भावप्रधान से ज्ञानप्रधान होती जाती है। बौद्धिकता हार्दिकता ही का दूसरा रूप है, वह हृदय की कृपणता से नहीं आती। ‘परिवर्तन’ में भी मैंने यही बात कही है––
“वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार,
लोचनों मे लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार।”
‘गुंजन’ से पहले, जबकि मैं परिस्थितियों के वश अपनी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाने के लिए बाध्य नहीं हुआ था, मेरे जीवन का समस्त मानसिक संघर्ष और अनुभूति की तीव्रता ‘ग्रंथी’ और ‘परिवर्तन’ में प्रकट हुई। जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, तब मैं प्राकृतिक दर्शन (नैच्युरेलिस्टिक फ़िलासफ़ी) से अधिक प्रभावित था और मानव जाति के ऐतिहासिक संघर्ष के सत्य से अपरिचित था। दर्शन मनुष्य के वैयक्तिक संघर्ष का इतिहास है, विज्ञान सामूहिक संघर्ष का।
“मानव जीवन प्रकृति संचलन में विरोध है निश्चित,
विजित प्रकृति को कर जन ने की विश्व सभ्यता स्थापित।”
जीवन की इस ऐतिहासिक व्याख्या के अनुसार हम संसार में लोकोत्तर मानवता का निर्माण करने के अधिकारी है :
“अचिर विश्व में अखिल,––दिशावधि, कर्म, वचन, मन,
तुम्हीं चिरंतन, हे विवर्तनहीन विवर्तन!”
जीवन की इस प्राकृतिक व्याख्या के अनुसार हमें प्रकृति के नियमों की परिपूर्णता एवं सर्वशक्तिमत्ता के सम्मुख मस्तक नवाने ही में शांति मिल सकती है।
‘गुंजन’ और ‘ज्योत्स्ना’ में मेरी सौंदर्य-कल्पना क्रमश आत्मकल्याण प्रौर विश्व-मंगल की भावना को अभिव्यक्ति करने के लिए उपादान की तरह प्रयुक्त हुई है।
“प्राप्त नहीं मानव जग को यह मर्मोज्वल उल्लास”
“कहाँ मनुज को अवसर देखे मधुर प्रकृति मुख”
अथवा
“प्रकृतिधाम यह तृण तृण कण कण जहाँ प्रफुल्लित जीवित,
जहाँ अकेला मानव ही रे चिर विषण्ण, जीवन्मृत।”
आदि बाद की रचनाओं में मेरे हृदय का आकर्षण मानवजगत् की ओर होता है। ‘ज्योत्स्ना’ तक मेरे सौंदर्य-बोध की भावना मेरे ऐंद्रिय हृदय को प्रभावित करती रही है, मैं तब तक भावना ही से जगत् का परिचय प्राप्त करता रहा, उसके बाद मैं बुद्धि से भी संसार को समझने की चेष्टा करने लगा हूँ। अपनी भावना की सहज दृष्टि को खो बैठने के कारण या उसके दब जाने के कारण मैंने ‘युगांत’ में लिखा है––
“वह एक असीम अखंड विश्व व्यापकता
खो गई तुम्हारी चिर जीवन सार्थकता।”
भावना की समग्रता को खो बैठने के कारण मैं, खंड-खंड रूप में, संसार को जग-जीवन को समझने का प्रयत्न करने लगा। यह कहा जा सकता है कि यहाँ से मेरी काव्यसाधना का दूसरा युग आरंभ होता है। जीवन के प्रति एक अंतविश्वास मेरी बुद्धि को अज्ञात रूप से परिचालित करने लगा और दिशा भ्रम के क्षणों में प्रकाश स्तंभ का काम देने लगा। जैसा कि मैंने ‘युगांत’ में भी लिखा है––
“जीवन लोकोत्तर
बढ़ती लहर, बुद्धि से दुस्तर,
पार करो विश्वास चरण धर।”
अब मैं मानता हूँ कि भावना और बुद्धि से संश्लेषण और विश्लेषण से, हम एक ही परिणाम पर पहुँचते हैं।
‘पल्लव’ से ‘गुंजन’ तक मेरी भाषा में एक प्रकार के अलंकार रहे हैं, और वे अलंकार भाषा-संगीत को प्रेरणा देने वाले तथा भाव-सौंदर्य की पुष्टि करने वाले हैं। बाद की रचनाओं में भाषा के अधिक गति (एब्स्ट्रक्ट) हो जाने के कारण मेरी अलंकारिता अभिव्यक्तिजनित हो गई है।
“नयन नीलिमा के लघु नभ में किस नव सुषमा का संसार
विरल इंद्रधनुषी बादल-सा बदल रहा है रूप अपार?”
की अलंकृत भाषा जिस प्रकार ‘स्वप्न’ का रूप चित्र सामने रखती है, उसी प्रकार गीत-गद्य ‘युगवाणी’ की ‘युग उपकरण’ ‘नव संस्कृति’ आदि रचनाएँ मनोरम विचार-चित्र उपस्थित करती है। ‘पुण्यप्रसू’, ‘घननाद’, ‘रूपसत्य’, ‘जीवनस्पर्श’ आदि रचनाओं में भी विषयानुकूल अलंकारिता का अभाव नहीं है। यदि यह मेरा सृजन आवेशमात्र नहीं है, तो ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ में मेरी कल्पना, ऊर्णनाभ की तरह, सूक्ष्म अमर अंतरजीवन का मधुर वितान तानकर, देश और काल के छोरों को मिलाने में संलग्न रही है। इस ह्रास और विश्लेषण-युग के स्वल्पप्राण लेखक की सृजनशील कल्पना अधिकतर जीवन के नवीन मानो की खोज ही में व्यय हो जाती है, उसका कलाकार स्वभावतः पीछे पड़ जाता है; अतएव उससे अधिक कला-नैपुण्य की आशा रखनी भी नहीं चाहिए।
‘युगवाणी’ का रूप-पूजन समाज के भावी रूप का पूजन है। अभी जो वास्तव में अरूप है, उसके कल्पनात्मक रूप चित्र को स्वभावतः अलंकृत होना चाहिए। ‘युगवाणी’ में कहा भी है––
“बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम
सुन्दर शिव सत्य कला के कल्पित माप- मान
बन गए स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण।”
‘जगत के रूप नाम’ से मेरा अभिप्राय नवीन सामाजिक संबंधों से निर्मित भविष्य के मानव संसार से है। जब हम कला को जीवन की अनुवर्तिनी मानते हैं, तब कला का पक्ष गौण हो जाता है। विकास के युग में जीवन कला का अनुगामी होता है। ‘युगवाणी’ में यह बात कई तरह व्यक्त की गई है कि भावी जीवन और भावी मानवता की सौंदर्य-कल्पना स्वयं ही अपना आभूषण है। ‘रूप रूप बन जाएँ भाव स्वर, चित्र गीत झंकार मनोहर’ द्वारा भविष्य के अरूप-सौंदर्य का रूप के पाश में बँधने के लिए, आवाहन किया गया है।
प्राचीन प्रचलित विचार और जीर्ण आदर्श समय के प्रवाह में अपनी उपयोगिता के साथ अपना सौंदर्य-संगीत भी खो बैठते हैं, उन्हें सजाने की ज़रूरत पड़ती है। नवीन आदर्श और विचार अपनी ही उपयोगिता के कारण संगीतमय एवं अलंकृत होते हैं, क्योंकि उनका रूप चित्र सद्य होता है और उनके रस का स्वाद नवीन। “मधुरता मृदुता-सी तुम प्राण, न जिसका स्वाद स्पर्श कुछ ज्ञात” उनके लिए भी चरितार्थ होता है। इसी से उनकी अभिव्यंजना से अधिक उनका भावतत्त्व काव्यगौरव रखता है :
“तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार
वाणी मेरी, चाहिए तुम्हें क्या अलंकार”
से भी मेरा यही अभिप्राय है कि संक्रांतियुग को वाणी के विचार ही उसके अलंकार है। जिन विचारों की उपयोगिता नष्ट हो गई है, जिनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खिसक गई है, वे पथराए हुए मृत विचार भाषा को बोझिल बनाते हैं। नवीन विचार और भावनाएँ, जो हृदय की रस-पिपासा को मिटाते हैं, उड़नेवाले प्राणियों की तरह, स्वयं हृदय में घर कर लेते है। आने वाले काव्य की भाषा अपने नवीन आदर्शों के प्राणतत्त्व से रसमयी होगी, नवीन विचारों के ऐश्वर्य से सालकार और जीवन के प्रति नवीन अनुराग की दृष्टि से सौंदर्यमयी होगी। इस प्रकार काव्य के अलंकार विकसित और सांकेतिक हो जाएँगे।
छायावाद इसलिए अधिक नहीं रहा कि उसके पास भविष्य के लिए उपयोगी नवीन आदर्शों का प्रकाश, नवीन भावना का सौंदर्यबोध और नवीन विचारों का रस नहीं था। वह काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था। द्विवेदी-युग के काव्य की तुलना में छायावाद इसलिए आधुनिक था कि उसके सौंदर्यबोध और कल्पना में शिल्प और दर्शन पाश्चात्य साहित्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ गया था, और उसका भाव-शरीर द्विवेदी-युग के काव्य की परंपरागत सामाजिकता से पृथक् हो गया था। किंतु वह नए युग की सामाजिकता और विचारधारा का समावेश नहीं कर सका था। उसमें व्यावसायिक क्रांति और विकासवाद के बाद का भावना वैभव तो था, पर महायुद्ध के बाद की ‘अन्नवस्त्र’ की धारणा (वास्तविकता) नहीं आई थी। उसके ‘हास-अश्रु आशा अकांक्षा’ ‘खाद्य-मधुपानी’ नहीं बने थे। इसलिए एक ओर वह निगूढ़ रहस्यात्मक, भावप्रधान (सब्जेक्टिव) और वैयक्तिक हो गया, दूसरी ओर केवल टेकनीक और आवरणमात्र रह गया। दूसरे शब्दों में नवीन सामाजिक जीवन की वास्तविकता को ग्रहण कर सकने से पहले हिंदी कविता, छायावाद के रूप में, ह्रासयुग के वैयक्तिक अनुभवों, ऊर्ध्वमुखी के विकास की प्रवृत्तियों, ऐहिक जीवन की आकांक्षाओं-संबंधी स्वप्नों, निराशा और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने लगी और व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की कठिनाइयों से क्षुब्ध होकर पलायन के रूप में, प्राकृतिक दर्शन के सिद्धांतों के आधार पर, भीतर-बाहर में, सुख-दुःख में, आशा-निराशा और संयोग-वियोग के द्वंद्वों मे सामंजस्य स्थापित करने लगी। सापेक्ष की पराजय उसमें निरपेक्ष की जय के रूप में गौरवांवित होने लगी।
महायुद्ध के बाद की अँग्रेज़ी कविता भी अतिवैयक्तिकता, बौद्धिकता, दुरूहता, संघर्ष, अवसाद, निराशा आदि से भरी हुई है। वह भी उन्नीसवी सदी के कवियों के भाव और सौंदर्य के वातावरण से कटकर अलग हो गई है। किंतु उसकी करुणा और क्षोभ की प्रतिक्रियाएँ व्यक्तिगत असंतोष से संबंध न रखकर वर्ग एवं सामाजिक जीवन की परिस्थितियों से संबंध रखती है। वह वैयक्तिक स्वर्ग की कल्पना से प्रेरित न होकर सामाजिक पुननिर्माण की भावना से अनुप्राणित है। उन्नीसवी सदी का उत्तरार्द्ध इंग्लैंड मे मध्यवर्गीय संस्कृति का चरर्मोन्नत युग रहा है, महायुद्ध के बाद उसमें विघटन के चिह्न प्रकट होने लगे। छायावाद और उत्तरयुद्धकालीन अँग्रेजी-कविता, दोनों, भिन्न-भिन्न रूप से, इस संक्रांतियुग के स्नावयिक विक्षोभ की प्रति-ध्वनियाँ हैं।
‘पल्लव’––काल में मैं उन्नीसवीं सदी के अँग्रेज़ी कवियों––मुख्यतः शेली, वर्ड सवर्थ, कीट्स और टेनिसन—से विशेष रूप से प्रभावित रहा हूँ, क्योंकि इन कवि मशीन-युग का सौंदर्यबोध और मध्यवर्गीय संस्कृति का जीवन स्वप्न दिया है। रविबाबू ने भी भारत की आत्मा को पश्चिम की, मशीन-युग की, सौंदर्य-कल्पना में परिधानित किया है। पूर्व और पश्चिम का मेल उनके युग का नारा भी रहा है। इस प्रकार मैं कवींद्र की प्रतिभा के गहरे प्रभाव को भी कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करता हूँ। और यदि लिखना एक unconsious-conscious process है, तो मेरे उपचेतन ने इन कवियों की निधियों का यत्र-तत्र उपयोग भी किया है, और उसे अपने विकास का अंग बनाने की चेष्टा की है।
ऊपर मैं एक अखंड भावना की व्यापकता को खो बैठने की बात लिख चुका हूँ। अब मैं जानता हूँ कि वह केवल सामंत-युग की सांस्कृतिक भावना थी, जिसे मैंने खोया था, और उसके विनाश के कारण मेरे भीतर नहीं, बल्कि बाहर के जगत् में थे। इस बात को ‘ग्राम्या’ में मैं निश्चयपूर्वक लिख सका हूँ––
“गत संस्कृतियों का आदर्शों का था नियत पराभव!”
“वृद्ध विश्व सामंतकाल का था केवल जड़ खँडहर!”
‘युगांत के ‘बापू’ (‘बापू के प्रति’ में) सामंत-युग के सूक्ष्म के प्रतीक हैं, ‘ग्राम्या’ के ‘महात्मा’ (महात्मा जी के प्रति में) ऐतिहासिक स्थूल के सम्मुख ‘विजित नर वरेण्यं के हो गए हैं, जो वर्तमान युग की पराजय है।
‘हे भारत के हृदय, तुम्हारे साथ आज नि:संशय
चूर्ण हो गया विगत सांस्कृतिक हृदय जगत का जर्जर!”
भावी सांस्कृतिक क्रांति की ओर संकेत करता है।
हम सुधार और जागरण-काल में पैदा हुए, किंतु युग प्रगति से बाध्य होकर हमें संक्रांति-युग की विचारधारा का वाहक बनना पड़ा है। अपने जीवन में हम अपने ही देश में कई प्रकार के सुधार और जागरण के प्रयत्नों को देख चुके हैं। उदाहरणार्थ स्वामी दयानंद जी सुधारवादी थे, जिन्होंने मध्ययुग की संकीर्ण रूढ़ि रीतियों के बंधनों से इस जाति और संप्रदायों में विभक्त हिंदू धर्म का उद्धार करने की चेष्टा की। श्री परमहंस देव और स्वामी विवेकानंद का युग भारतीय दर्शन के जागरण का युग रहा है। उन्होंने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धार्मिक समन्वय करने का प्रयत्न किया। डा० रवींद्रनाथ का युग विश्वव्यापी सांस्कृतिक समन्वय पर जोर देता रहा है :
‘युग युग की संस्कृतियों का चुन तुमने सार सनातन
नव संस्कृति का शिलान्यास करना चाहा भव शुभकर”
कवींद्र की प्रतिभा के लिए भी लागू होता है। वह एक स्थान पर अपने बारे में लिखते भी हैं, “मैं समझ गया कि मुझे इस विभिन्नता में व्याप्त एकता के सत्य का संदेश देना है।” डा० टैगोर के जीवन-मान भारतीय दर्शन के साथ ही मानव-शास्त्र (एन्थ्रोपोलॉजी), विश्ववाद और अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांतों से प्रभावित हुए है। उनके युग का प्रयत्न भिन्न-भिन्न देशों और जातियों की संस्कृतियों के मौलिक सारभाग से मानव जाति के लिए विश्व-संस्कृति का पुननिर्माण करने की ओर रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों से मनुष्य की देश-कालजनित धारणाओं में प्रकारांतर उपस्थित हो जाने शिला और दर्शन के कारण एवं आवागमन की सुविधाओं से भिन्न-भिन्न देशों और जातियों के मनुष्यों में परस्पर का संपर्क बढ़ जाने के कारण उस युग के विचारकों का मानव जाति के आंतरिक (सांस्कृतिक) एकीकरण करने का प्रयत्न स्वाभाविक ही था। महात्मा जी भी, इसी प्रकार, विकसित व्यक्तिवाद के मानों का पुनर्जागरण कर, भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच, संसार में, सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। किंतु इस प्रकार के एकदेशीय, एकजातीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न भी, इस युग में, तभी सफल हो सकते हैं, जब उनको परिचालित करने वाले सिद्धांतों के मूल विकासशील ऐतिहासिक सत्य में हों :
“विश्व सभ्यता का होना था नखसिख नव रूपांतर,
रामराज्य का स्वप्न तुम्हारा हुआ न यों ही निष्फल!”
आने वाला युग जीवन के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन लाना चाहता है। वह सामंत-युग से सगुण (सांस्कृतिक मन) से मानव चेतना को मुक्त कर, मनुष्य के मौलिक संस्कारों का यंत्रयुग की विकसित परिस्थितियों और सुविधा के अनुरूप नवीन रूप से मूल्यांकन करना चाहता है। वह मानव-संस्कृति को एक सामूहिक विकास प्रवाह मानता है। प्रस्तर-युग को जीर्ण सभ्यता मरणासन्न, समापन से इसी प्रकार के युग-परिवर्तन की सूचना मिलती है। दूसरे शब्दों में, आने वाला युग मनुष्य समाज का वैज्ञानिक ढंग से पुननिर्माण करना चाहता है। ज्ञान को सदैव विज्ञान ने वास्तविकता प्रदान की है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भी मानव जाति की नवीन जीवन-कल्पना को पृथ्वी पर अवतरित करने के प्रयत्न में संलग्न है। जिस संक्रांतिकाल से मानव सभ्यता गुज़र रही है, उसके परिणाम के हेतु आशावादी बने रहने के लिए विज्ञान ही हमारे पास अमोघ शक्ति और साधन है। इस विश्व व्यापी युद्ध के रूप में, जैसे, विज्ञान भिन्न-भिन्न जातियों, वर्गों और स्वार्थों में विभक्त आदिम मानव’ (‘आदिम मानव करता अब भी जन में निवास) का संहार कर रहा है, वह भविष्य में नवीन मानव के लिए लोकोपयोगी समाज का भी निर्माण कर सकेगा। ‘ग्राम्या’ में 1940 सन् का संबोधन करते हुए मैंने लिखा है––
“आओ हे दुर्धर्ष वर्ष, लाओ विनाश के साथ नव सृजन,
विश शताब्दों का महान विज्ञान ज्ञान ले, उत्तर यौवन!”
सभ्यता के इतिहास में और भी कई युग बदले हैं और उन्हीं के अनुरूप मनुष्य की आध्यात्मिक धारणा अपने अंतर और बहिर्जगत् के संबंध में परिवर्तित हुई है :
“पशु युग में थे गण देवों के पूजित पशुपति,
थी रुद्रचरों से कुंठित कृषि युग की उन्नति।
श्रीराम रुद्र की शिव में कर जन हित परिणति,
जीवित कर गए अहल्या को, थे सीता-पति।”
श्रीराम, इस दृष्टि से, अपने देश में कृषि क्रांति के प्रवर्तक कहे जा सकते हैं, जिन्होंने कृषि-जीवन की मान-मर्यादाएँ निर्धारित की। स्थिर एवं सुव्यवस्थित कृषि जीवन को व्यवस्था पशु-जीवियों को कष्टसाध्य अस्थिर जीवनचर्या से श्रेष्ठ और लोकोपयोगी प्रमाणित हुई। एक स्त्री-पुरुष का सदाचार कृषि-संस्कृति ही की देन है। कृष्ण का युग कृषि-जीवन के विभव का युग रहा है। भारतवर्ष––जैसे विशाल, उर्वर और संपन्न देश की सामंतकालीन सभ्यता और संस्कृति अपने उत्कर्ष के युग में संसार को जो कुछ दे सकती थी—उसका समस्त वैभव, बहुमूल्य उपादान, उसकी अपार गौरव-गरिमा, ऋद्धि-सिद्धि, दृष्टि चकित कर देने वाले रूप-रंग––उस युग की विशद भावना, बुद्धि, कल्पना, प्रेम, ज्ञान, भक्ति, रहस्य, ईश्वरत्व––उसके समस्त भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उपकरणों को जोड़कर, जैसे, उस युग की चरमोन्नति का प्रतीकस्वरूप, श्रीकृष्ण की प्रतिमा निर्माण की गई है। इससे परिपूर्ण रूप अथवा प्रतीक सामंतयुग को संस्कृति का और हो भी नहीं सकता था। और कृषि-संपन्न भारत के सिवा कोई दूसरा देश, शायद, उसे दे भी नहीं सकता था।
मर्यादापुरुषोत्तम के स्वरूप में कृषि जीवन के आचार-विचार, रीति-नीति संबंधी सात्त्विक चाँदी के तारों से बुने हुए भारतीय संस्कृति के बहुमूल्य पट में विभवमूर्ति कृष्ण ने सोने का सुंदर काम कर उसे रत्नजटित राजसी बेलबूटों से अलंकृत कर दिया। कृष्ण-युग की नारी भी हमारी विभव-युग की नारी है। वह ‘मनसा वाचा कर्मणा जो मेरे मन राम’ वाली एकनिष्ठ पत्नी नहीं––लाख प्रयत्न करने पर भी उसका मन वंशीध्वनि पर मुग्ध हो जाता है, वह विह्वल है, उच्छ्वसित है। सामंतयुग की नैतिकता के तंग अहाते के भीतर श्रीकृष्ण ने, विभव-युग के नर-नारियों के सदाचार में भी, क्रांति उपस्थित की है। श्रीकृष्ण की गोपियाँ, अभ्युदय के युग में, फिर से गोप-संस्कृति का लिबास पहनती हुई दिखाई देती हैं।
भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप हमे मध्ययुग में देखने को मिला है, वह श्री तुलसी के रामायण में सुरक्षित है। तुलसी ने ‘कृषि-मन युग अनुरूप किया निर्मित। देश की पराधीनता और ह्रास के युग में संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रयत्न शुरू हुए। अन्य संस्कृतियों से ग्रहण कर सकने को उसकी प्राणशक्ति मंद पड़ गई, और भारतीय संस्कृति का गतिशील जीवन-द्रव जातियों, संप्रदायों, संघों, मतों, रूढ़ि-रीति-नीतियों और परंपरागत विश्वासों के रूप में जमकर कठोर एवं निर्जीव हो गया। आर्थिक और राजनीतिक पराभव के कारण जनसाधारण में देह को अनित्यता, जीवन का मिथ्यापन, संसार की असारता, मायावाद, प्रारब्धवाद, वैराग्य-भावना आदि ह्रासयुग के अभावात्मक विचारों और आदर्शों का प्रचार बढ़ने लगा। जिस प्रकार कृषि-युग ने पशुजीवी के मनुष्य की अंतर्बाह्य-चेतना में प्रकारांतर उपस्थित कर दिया, उसी प्रकार यंत्र-युग का आगमन सामंत-युग की परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन लाने की सूचना युग देता है। सामंत-युग में भी, समय-समय पर, छोटी-बड़ी विश्लिष्ट युगों की गण-संस्कृतियों का समन्वय हुआ है, तथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांतियाँ हुई हैं, किंतु उन सबके नैतिक मानों और आदर्शों को सामंत-युग की परिस्थितियों ही ने प्रभावित किया है । भविष्य में इस प्रकार के सभी प्रयत्नों से संबंध रखने वाले मौलिक सिद्धांतों और मानो को यंत्र-युग की आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ निर्धारित करेंगी।
यंत्र-युग के दर्शन को हम ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं जो उन्नीसवी सदी के संकीर्ण भौतिकवाद से पृथक् है। नवीन भौतिकवाद, दर्शन और विज्ञान का, मानव-सभ्यता के अंतर्बाह्य विकास का ऐतिहासिक समन्वय है।
“दर्शन युग का अंत, अंत विज्ञानों का संघर्षण,
अब दर्शन-विज्ञान सत्य का करता नव्य निरूपण।”
वह मनुष्य के सामाजिक जीवन विकास के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण है। सामाजिक प्रगति के दर्शन के साथ ही वह उसे सामूहिक वास्तविकता में परिणत करने योग्य नवीन तंत्र (स्टेट) का भी विधायक है।
“विकसित हो बदले जब जब जीवनोपाय के साधन,
युग बदले, शासन बदले, कर गत सभ्यता समापन।
सामाजिक संबंध बने नव अर्थ-भित्ति पर नूतन,
नव विचार, नव रीति नीति, नव नियम, भाव, नव दर्शन।”
इतिहास-विज्ञान के अनुसार जैसे-जैसे जीवनोपाय के साधन स्वरूप हथियारों और यंत्रो का विकास हुआ है, मनुष्य जाति के रहन-सहन और सामाजिक विधान में भी युगांतर हुआ। नवीन आर्थिक व्यवस्था के आधार पर नवीन राजनीतिक प्रणालियाँ और सामाजिक संबंध स्थापित हुए हैं और उन्हीं के प्रतिरूप रीति-नीतियों, विचारों एवं सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ है। साथ ही उत्पादन के नवीन यंत्रों पर जिस वर्ग-विशेष का अधिकार रहा है, उसके हाथ जनसाधारण के शोषण का हथियार भी लगा है, और उसी ने जन-समाज पर अपनी सुविधानुसार राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व भी स्थापित किया है। पूँजीवादी युग ने संसार को जो ‘विविध ज्ञान-विज्ञान, कला-यंत्रों का अद्भुत कौशल दिया है, उसके अनुरूप सभ्यता और मानवता का प्रादुर्भाव न होने का मुख्य कारण पूँजीवादी प्रथा ही है, जिसकी ऐतिहासिक उपयोगिता अब नष्ट हो गई है। आज, जब कि संसार में इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है, और जिसके बाद पूँजीवादी साम्राज्यवाद का––जिसका हिंस्र रूप फ़ासिज़्म है—शायद, अंत भी हो जाए, इस प्रथा के विरोधों का विवेचन करना पिष्टपेषण के समान है। मनुष्य-स्वभाव की सीमाएँ, एक ओर, वर्ग-संघर्ष एवं राजनीतिक युद्धों के रूप में, मानव जाति के रक्त का उग्र प्रयोग करवा रही है, दूसरी ओर मनुष्य की विकास-प्रिय प्रकृति समयानुकूल उपयुक्त साहित्य एवं विचारों का प्रचार कर, नवीन मानवता का वातावरण पैदा करने के लिए सांस्कृतिक प्रयोग भी कर रही है। भले ही इस समय उसकी देन अत्यंत स्वल्प हो और अंधकार की प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिए विजयी हो रही हों, किंतु एक कलाकार और स्वप्नस्रष्टा के नाते मैं दूसरे प्रकार की सांस्कृतिक अभ्युदय की—शक्तियों को बढ़ाने का पक्षपाती हूँ।
‘राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज जगत के सम्मुख,
* * *
‘आज वृहत् सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित,
खंड मनुजता को युग युग की होना है नव निर्मित।’
यंत्रों का पक्ष भी मैंने इसीलिए ग्रहण किया है कि वे मानव-समूह की सांस्कृतिक चेतना के विकास में सहायक हुए हैं।
‘जड़ नहीं यंत्र, वे भाव रूप, संस्कृति द्योतक।
* * *
वे कृत्रिम निर्मित नहीं, जगत क्रम में विकसित
* * *
दार्शनिक सत्य यह नहीं, यंत्र जड़ मानव कृत,
वे है अमूर्तः जीवन विकास की कृति निश्चित!’
मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना उसकी वस्तु-परिस्थितियों से निर्मित सामाजिक संबंधों का प्रतिबिंब है। यदि हम बाह्य परिस्थितियों में परिवर्तन ला सके, तो हमारी आंतरिक धारणाएँ भी उसी के अनुरूप बदल जाएँगी।
‘कहता भौतिकवाद वस्तु जग का कर तत्वान्वेषण,
भौतिक भव ही एक मात्र मानव का अंतर दर्पण।
स्थूल सत्य आधार, सूक्ष्म आधेय, हमारा जो मन,
बाह्य विवर्तन से होता युगपत् अंतर परिवर्तन।’
जब हम कहते हैं कि आने वाला युग आमूल परिवर्तन चाहता है, तो वह बहिरंतर्मुखी दोनों प्रकार का होगा। सामंत-युग की परिस्थितियों की सीमाओं के भीतर व्यक्ति का विकास जिस सापेक्ष पूर्णता तक पहुँच सका अथवा उस युग के सामूहिक विकास की पूर्णता व्यक्ति की चेतना में जिन विशिष्ट गुणों में प्रतिफलित हुई, सामंत-काल के दर्शन ने व्यक्ति के स्वरूप को उसी तरह निर्धारित किया है। यंत्र-युग की सामूहिक विकास की पूर्णता उस धारणा में मौलिक (प्रकार का) परिवर्तन उपस्थित कर सकेगी।
प्रकृति और विवेक की तरह मनुष्य स्वभाव के बारे में भी कोई निश्चयात्मक (पॉज़िटिव) धारणा नहीं बनाई जा सकती। मनुष्य एक विवेकशील पशु है कहना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना उसके मौलिक संस्कारों के संबंध में वस्तु-जगत् की परिस्थितियों से प्रभावित होती है, वे परिस्थितियाँ ऐतिहासिक दिशा में विकसित होती रहती है। मनुष्य के मौलिक संस्कारों का देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार जो मान निर्धारित हो जाता है, अथवा उनके उपयोग के लिए जो सामाजिक प्रणालियाँ बँध जाती हैं, उनका वही व्यावहारिक रूप संस्कृति से संबद्ध है।
हम आने वाले युग के लिए ‘स्थूल’ को (यंत्र-युग की विकसित ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रतीक को) इसलिए ‘सूक्ष्म’ (भावी सांस्कृतिक मानों का प्रतीक) मानते हैं कि हमारे विगत सांस्कृतिक सूक्ष्म की पृष्ठभूमि विकसित व्यक्तिवाद के तत्त्वों से बनी है, और हम जिस स्थूल को कल का ‘शिव सुंदर सत्य’ मानते हैं, वह स्थूल प्रतीक है सामूहिक विकासवाद का।
‘स्थूल युग का शिव सुंदर सत्य, स्थूल ही सूक्ष्म आज, जन-प्राण!’
सामंत-युग में जिस प्रकार सामाजिक रहन-सहन और शिष्टाचार का सत्य राजा से प्रजा की ओर प्रवाहित हुआ है, उसी प्रकार नैतिक सदाचार और आदर्श उस युग के सगुण की दिशा में विकसित व्यक्ति से जनसाधारण की ओर। आज के व्यक्ति की प्रगति सामूहिक विकासवाद की दिशा को होनी चाहिए, न कि सामंत-युग के लिए उपयोगी विकसित व्यक्तिवाद की दिशा को। ‘तब वर्ग व्यक्ति गुण, जन समूह गुण अब विकसित’—सामंत-युग का नैतिक दृष्टिकोण, उस युग की परिस्थितियों के कारण, तथोक्त उच्च वर्ग के गुण (क्वालिटी) से प्रभावित था।
आने वाला युग सामंत-युग की नैतिकता के पाश से मनुष्य को बहुत कुछ अंशों में मुक्त कर सकेगा और उसका ‘पशु’ (मौलिक संस्कारों संबंधी सामंत नैतिक मान), विकसित वस्तु-परिस्थितियों के फलस्वरूप, आध्यात्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तन से, बहुत कुछ अंशों में ‘देव’ (सांस्कृतिक मानो का प्रतीक) बन सकेगा।
‘नहीं रहे जीवनोपाय तब विकसित,
जीवन यापन कर न सके जन इच्छित।
* * *
देव और पशु भावी मे जो सीमित
युग युग में होते परिवर्तित विकसित।’
भावी सामाजिक सदाचार मनुष्य के मौलिक संस्कारों के लिए अधिक विकसित सामाजिक संबंध स्थापित कर सकेगा।
‘अति मानवीय था निश्चय विकसित व्यक्तिवाद,
मनुजों में जिसने भरा देव पशु का प्रमाद’
‘मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर
करता अपूर्ण को पूर्ण असुंदर को सुंदर––
आदि विचार मनुष्य के दैहिक संस्कारों के प्रति इसी प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं।
मनुष्य क्षुधा काम की प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर सामाजिक संगठन की ओर, और जरा-मरण के भय से आध्यात्मिक सत्य की खोज की ओर अग्रसर हुआ है। भौतिक दर्शन का यह दावा ठीक ही जान पड़ता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में, जिसमें कि अधिकाधिक मनुष्यों को क्षुधा-काम की परितृप्ति के लिए पर्याप्त साधन मिल सकते हैं और वे वर्तमान युग की संरक्षण हीनता से मुक्त हो सकते हैं, उन्हें अपने सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी अधिक अवकाश और सुविधाएँ मिल सकेगी। एक ओर समाजवादी विधान, उत्पादन-यंत्रों की सामाजिक उपयोगिता बढ़ाकर, मनुष्य को वर्तमान आर्थिक संघर्ष से मुक्त कर सकेगा, दूसरी ओर वह उसे सामंतवादी सांस्कृतिक मानो की संकीर्णता से मुक्ति दे सकेगा, जिनकी ऐतिहासिक उपयोगिता नहीं रह गई है और जिनकी धारणाएँ आमूल विकसित एवं परिवर्तित हो गई है। यदि भावी समाज मनुष्य को रोटी (जन-आवश्यकताओं का प्रतीक) की चिंता से मुक्त कर सका, तो उसके लिए केवल सांस्कृतिक संघर्ष का प्रश्न ही शेष रह जाएगा। प्रत्येक धर्म और संस्कृति ने अपने देश-काल से संबंध रखने वाले सापेक्ष सत्य को निरपेक्ष (संपूर्ण) सत्य का रूप देकर, मनुष्य के (स्वर्ग-नरक संबंधी) दुःख और भय के संस्कारों से लाभ उठाकर, उसको चेतना में धार्मिक और सामाजिक विधान स्थापित किए हैं जो कि सामंत-युग को परिस्थितियों को सामने रखते हुए, व्यावहारिक दृष्टि से उचित भी था। इस प्रकार प्रत्येक युग पुरुष, राम कृष्ण बुद्ध आदि, जो कि अपने युग के सापेक्ष के प्रतीक हैं, जनता द्वारा शाश्वत पुरुष (निरपेक्ष) की तरह माने और पूजे गए हैं। सामंत-कालीन उदात्त नायक के रूप में हमारे साहित्य के ‘सत्यं शिवं सुंदरम्’ के शाश्वत मान भी केवल उस युग के सगुण से संबंध रखने वालों सापेक्ष धारणाएँ––मात्र है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मनुष्य के मौलिक संस्कार, क्षुधा काम आदि निरपेक्षतः कोई सांस्कृतिक मूल्य नहीं रखते। सभ्यता के युगों को विविध परिस्थितियों के अनुरूप उनका जो व्यावहारिक, सामाजिक और नैतिक मूल्य निर्दिष्ट हो जाता है उसी का प्रभाव मनुष्य के सत्य-शिव-सुंदर की भावनाओं पर भी पड़ता है। मनुष्य की दैहिक प्रवृत्तियों और सामाजिक परिस्थितियों के बीच में जितना विशद सामंजस्य स्थापित किया जा सकेगा, उसी के अनुरूप, जन-समाज की सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हो सकेगा। जिस सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक सदाचार और व्यक्ति की आवश्यकताओं की सीमाएँ एक-दूसरे मे लीन हो जाएगी, उस समाज में व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध मिट जाएगा, व्यक्ति के क्षुद्र देहज्ञान की (अहमत्मिका) भावना विकसित हो जाएगी; उसके भीतर सामाजिक व्यक्तित्व स्वतः कार्य करने लगेगा, और इस प्रकार व्यक्ति अपने सामूहिक विकास की आध्यात्मिक पूर्णता तक पहुँच जाएगा।
सामंत-युग के स्त्री-पुरुष संबंधी सदाचार का दृष्टिकोण अब अत्यंत संकुचित लगता है। उसका नैतिक मानदंड स्त्री की शरीर-यष्टि रहा है! उस सदाचार के एक अंचल-छोर को हमारी मध्ययुग की सती और हमारी बाल-विधवा अपनी छाती से चिपकाए हुए है और दूसरे छोर को उस युग को देन वेश्या। ‘न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति’ के अनुसार उस युग के आर्थिक विधान में भी स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं और वह पुरुष की संपत्ति समझी जाती रही है। स्त्री स्वातंत्र्य संबंधी हमारी भावना का विकास वर्तमान युग की आर्थिक परिस्थितियों के विकास के साथ हो ही रहा है। स्त्रियों का निर्वाचन अधिकार संबंधी आंदोलन बूर्ज्वा-संस्कृति एवं पूँजीवादी युग की आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम। सामंत-युग को नारी नर की छायामात्र रही है।
‘सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित,
पूतयोनि वह : मूल्य चर्म पर केवल उसका अंकित।
वह समाज की नही इकाई––शून्य समान अनिश्चित
उसका जीवन मान, मान पर नर के है अवलंबित।
योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित
उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार अभी सामंत-युग की क्षुद्र नैतिक और सांस्कृतिक भावनाओं ही से युद्ध कर रहा है, पृथ्वी पर अभी यंत्र-युग प्रतिष्ठित नहीं हो सका है। आने वाला युग मनुष्य की क्षुधा-काम की प्रवृत्तियों में विकसित सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर हमारे सदाचार के दृष्टिकोण एवं ‘सत्यं शिवं सुंदरम्’ की धारणाओं में प्रकारांतर उपस्थित कर सकेगा।
ऐतिहासिक भौतिकवाद और भारतीय अध्यात्म-दर्शन में मुझे किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा, क्योंकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याणकारी सांस्कृतिक पक्ष ही ग्रहण किया है। मार्क्सवाद के अंदर श्रमजीवियों के संगठन, वर्ग संघर्ष आदि से संबंध रखने वाले बाह्य दृश्य को, जिसका वास्तविक निर्णय आर्थिक और राजनीतिक क्रांतियाँ ही कर सकती है, मैंने अपनी कल्पना का अंग नहीं बनने दिया है। इस दृष्टि से, मानवता एवं सर्वभूतहित की जितनी विशद भावना मुझे वेदांत में मिली, उतनी ही ऐतिहासिक दर्शन में भी। भारतीय दार्शनिक जहाँ सत्य की खोज में, सापेक्ष के उस पार, ‘अवाङ्मनसगोचर’ की ओर चले गए हैं, वहाँ पाश्चात्य दार्शनिकों ने सापेक्ष के अंतस्तल में डुबकी लगाकर, उसके आलोक में जन-समाज के सांस्कृतिक विकास के उपयुक्त राजनीतिक विधान देने का भी प्रयत्न किया है। पश्चिम में वैधानिक संघर्ष अधिक रहने के कारण नवीनतम समाजवादी विधान का विकास भी वही हो सका है।
फ़्रॉयड जैसे अंतरतम के मनोवैज्ञानिक ‘इड’ के विश्लेषण में सापेक्ष के स्तर से नीचे जाने का आदेश नहीं देते है। वहाँ अचेतन (अनकासस) पर, विवेक का नियंत्रण न होने के कारण, वे भ्रांति पैदा होने का भय बतलाते हैं। भारतीय तत्त्वद्रष्टा, शायद, अपने सूक्ष्म नाड़ी-मनोविज्ञान (योग) के कारण सापेक्ष के उस पार सफलतापूर्वक पहुँचकर ‘तदन्तरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यत’ सत्य का प्रतिष्ठा कर सके है।
मैं, अध्यात्म और भौतिक, दोनों दर्शन सिद्धांतों से प्रभावित हुआ हूँ। पर भारतीय दर्शन की, सामंतकालीन परिस्थितियों के कारण, जो एकांत परिणति व्यक्ति की प्राकृतिक मुक्ति में हुई है (दृश्य जगत् एवं ऐहिक जीवन के माया होने के कारण उसके प्रति विराग आदि की भावना जिसके उपसंहार-मात्र है), और मार्क्स के दर्शन की, पूँजीवादी परिस्थितियों के कारण, जो वर्ग-युद्ध और रक्त क्रांति में परिणति हुई है, ये दोनों परिणाम मुझे सांस्कृतिक दृष्टि से उपयोगी नहीं जान पड़े।
अध्यात्म-दर्शन से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह सापेक्ष जगत् ही सत्य नहीं, इससे परे जो निरपेक्ष सत्य है वह मन और बुद्धि से अतीत है। किंतु इस सापेक्ष जगत् का––जिसका संबंध मानव जाति की संस्कृतियों––आचार-विचार, रीति-नीति और सामाजिक संबंधों से है—विकास किस प्रकार हुआ, इस पर ऐतिहासिक दर्शन ही प्रकाश डालता है। हमारे सांस्कृतिक हृदय के ‘सत्यं शिवं सुंदरम्’ का बोध सापेक्ष है, परम सत्य इस सूक्ष्म से भी परे है––यह अध्यात्म दर्शन की विचारधारा का परिणाम है। जीवन-शक्ति गतिशील (डाइनेमिक) है, सामंतकालीन सूक्ष्म से अथवा विगत सांस्कृतिक मानों और आदर्शों से मानव समाज का संचालन भविष्य में नहीं हो सकता, उसे नवीन जीवन-मानों की आवश्यकता है, जिसके ऐतिहासिक कारण है, आदि, यह आधुनिक भौतिक दर्शन की विचारधारा का परिणाम है। एक जीवन के सत्य को ऊर्ध्वतल पर देखता है, दूसरा समतल पर।
समन्वय के सत्य को मानते हुए भी में जो वस्तु-दर्शन (ऑब्जेक्टिव फ़िलॉसफ़ी) के सिद्धांतों पर इतना ज़ोर दे रहा हूँ, इसका यही कारण है कि परिवर्तन के युग में भाव-दर्शन (सब्जेक्टिव फ़िलॉसफ़ी) की––जोकि अभ्युदय और जागरण-युग की चीज़ है––उपयोगिता प्रायः नष्ट हो जाती है। सच तो यह है कि हमें अपने देश के युगव्यापी अंधकार में फैले, इस मध्यकालीन संस्कृति के तथाकथित ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ को, जड़ और शाखारहित, उखाड़कर फेंक देना होगा। और उस सांस्कृतिक चेतना के विकास के लिए देशव्यापी प्रयत्न और विचार संग्राम करना पड़ेगा, जिसके मूल हमारे युग की प्रगतिशील वस्तुस्थितियों में हों। भारतीय दर्शन की दृष्टि से भी मुझे अपने देश की संस्कृति के मूल उस दर्शन में नहीं मिलते, जिसका चरम विकास अद्वैतवाद में हुआ है। यह मध्यकालीन आकाशलता, शताब्दियों के अंधविश्वासों, रूढ़ियों, प्रथाओं और मत-मतांतरों की शाखा-प्रशाखाओं मे पुँजीभूत और विच्छिन्न होकर, एवं हमारे जातीय जीवन के वृक्ष को जकड़कर, उसकी वृद्धि रोके हुए है। इस जातीय रक्त का शोषण करने वाली व्याधि से मुक्त हुए बिना, और नवीन वास्तविकता के आधारों और सिद्धांतों को ग्रहण किए बिना, हम में वह मानवीय एकता, जातीय संगठन, सक्रिय चैतन्यता, सामूहिक उत्तरदायित्व, परोक्ष और विपत्तियों का निर्भीक साहस के साथ सामना करने की शक्ति और क्षमता नहीं आ सकती, जिसकी कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महाप्राणता भरने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। युग के सृजन एवं निर्माण काल में संस्कृति के मूल सदैव परिस्थितियों की वास्तविकता में होते हैं, वह अधोमूल वास्तविकता, समय के साथ-साथ, विकास एवं उत्कर्ष काल में, ऊर्ध्वमूल (भावरूप) सांस्कृतिक चेतना बन जाती है। आज जबकि पिछले युगों की वास्तविकता आमूल परिवर्तित और विकसित होने जा रही है, हमारी संस्कृति को, नवीन जन्म के प्रयास में, फिर से अधोमूल होना ही पड़ेगा। हम शताब्दियों से एक ही मूल सत्य को नए नवीन रूप (इंटरप्रटेशंस) देते आए हैं, अब उस सामंतगुण की, नवीन वस्तुस्थितियों के अनुरूप, रूपांतरित होने की मौलिक क्षमता समाप्त हो गई है, क्योंकि विगत युगों की वास्तविकता आज तक मात्राओं में घट-बढ़ रही थी, अब वह प्रकार में बदल रही है।
मनुष्य का विकास समाज की दिशा को होता है, समाज का इतिहास की दिशा को,––इस ऐतिहासिक प्रगति के सिद्धांत को हम इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या कहते हैं।
‘अंतर्मुख अद्वैत पड़ा था युग युग से निष्क्रिय निष्प्राण,
जग में उसे प्रतिष्ठित करने दिया साम्य ने वस्तु विधान।’
भौतिक दर्शन ‘आत्मवत् सर्वभूतेषु’ के सत्य को सामाजिक वास्तविकता में परिणत करने योग्य समाजवादी विधान का जन्मदाता है। भारतीय दर्शन के अद्वैतवाद के सत्य को देश-काल के भीतर (संस्कृति के रूप में) प्रतिष्ठित करने के योग्य विधान को जन्म देना सामंत-युग की परिस्थितियों के बाहर था। उसके लिए एक और भौतिक विज्ञान के विकास द्वारा भौतिक शक्तियों पर आधिपत्य प्राप्त करने की ज़रूरत थी, दूसरी ओर मनुष्य की सामूहिक चेतना के विकास की। जीवन की जिस पूर्णता के आदर्श को मनुष्य आज तक अंतर्जगत् में स्थापित किए हुए था, अब उसे, एक सर्वांगपूर्ण तंत्र के रूप में, वह बहिर्जगत् में स्थापित करना चाहता है। रहस्य और अलौकिकता के प्रति अब उसकी धारणा अधिक बौद्धिक और वास्तविक हो रही है। आने वाला युग सामंत-युग के स्वर्ग की अंतर्मुखी कल्पना और स्वप्नों को सामाजिक वास्तविकता का रूप दे सकेगा। मनुष्य को सृजन-शक्ति का ईश्वर लोक-कल्याण के ईश्वर में विकसित हो जाएगा।
‘स्वप्न वस्तु बन जाए सत्य नव, स्वर्ग मानसी ही भौतिक भव,
अंतर जग ही बहिर्जगत बन जावे, वीणा पाणि, इ!’
भौतिक जगत् की प्रारंभिक कठोर परिस्थितियों से कुंठित ‘आदिम मानव की हिस्र आत्मा नवीन परिस्थितियों के प्रकाश में डूबकर आलोकित हो जाएगी। यंत्र-युग के साथ-साथ मानव सभ्यता में स्वर्णयुग पदार्पण कर सकेगा। ऐसी सामाजिकता में मनुष्य-जाति ‘अहिंसा’ को भी व्यावहारिक सत्य में परिणत कर सकेगी।
“मनुष्यत्व का तत्व सिखाता निश्चय हमको गाँधीवाद,
सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना है अविवाद”––
वर्तमान विश्वव्यापी युद्ध के युग में उपर्युक्त विवेचना के लिए शायद ही दो मत हो सकते हैं।
यदि स्वर्णयुग की आशा आज की अतृप्त आकांक्षा को काल्पनिक पूर्ति और पलायन-प्रवृत्ति का स्वप्न भी है, तो वह इस युग की मरणासन्न वास्तविकता से कहीं सत्य और अमूल्य है। यदि इस विज्ञान के युग में, मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रकाश और हृदय की मधुरिमा से, अपने लिए पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण नहीं कर सकता और एक नवीन सामाजिक जीवन आज के रिक्त और संदिग्ध मनुष्य में जीवन के प्रति नवीन अनुराग, नवीन कल्पना और स्वप्न नहीं भर सकता, तो यह कही अच्छा है कि, इस ‘दैन्य जर्जर अभाव ज्वर पीड़ित जाति वर्ग में विभाजित, रक्त की प्यासी मनुष्य-जाति का अंत हो जाए। किंतु जिस जीवन-शक्ति की महिमा युग-युग के दार्शनिक और कवि गाते आए हैं, जिसके क्रिया-कलापों और चमत्कारों का विश्लेषण कर आज के वैज्ञानिक चकित और मुग्ध हैं, वह सर्वमयी शक्ति केवल पृथ्वी के गौरव मानव जाति के विश्व को ही इस प्रकार जीता-जागता नरक बनाए रहेगी, इस पर किसी तरह विश्वास नहीं होता।
इन्हीं विचारधाराओं, स्वप्नों और कल्पनाओं से प्रेरित होकर मैंने ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ को जन्म दिया। ‘ग्राम्या’ के लिए ‘युगवाणी’ पृष्ठभूमि का काम करती है। ‘ग्राम्या’ की भूमिका में मैंने ग्रामीणों के प्रति अपनी जिस बौद्धिक सहानुभूति की बात लिखी है, उस पर मेरे आलोचकों ने मुझ पर आक्षेप किए हैं। ‘ग्राम जीवन में मिलकर, उसके भीतर से’ में इसलिए नहीं लिख सका कि मैंने ग्राम-जनता को ‘रक्त मांस के जीवों के रूप में नहीं देखा है, एक मरणोन्मुखी संस्कृति के अवयव स्वरूप देखा है, और ग्रामों को सामंतयुग के खँडहर के रूप में।
‘यह तो मानव लोक नही रे यह है नरक अपरिचित
यह भारत का ग्राम, सभ्यता, संस्कृति से निर्वासित।’
‘मानव दुर्गति की गाथा से श्रोतप्रोत, मर्मांतक
सदियों के अत्याचारों की सूची यह रोमांचक!’
इसी ग्राम को मैंने ‘ग्राम्या’ की रंगहीन रंगभूमि बनाया है।
‘रूढ़ि रीतियों के प्रचलित पथ, जाति पाँति के बंधन,
नियत कर्म है, नियत कर्मफल,––जीवन चक्र सनातन!’
सांस्कृतिक दृष्टि से जिस प्रिय-अप्रिय या सत्य-मिथ्या के बोध से उनका जीवन परिचालित होता है उसकी ऐतिहासिक उपयोगिता नष्ट हो चुकी है।
‘ये जैसे कठपुतले निर्मित...युग-युग की प्रेतात्मा अविदित
इनकी गतिविधि करती यंत्रित।––
यह बात ‘सारा भारत है आज एक रे महाग्राम’ के लिए भी चरितार्थ होती है। इस प्रकार मैंने ग्रामीणों को भावी के ‘स्वप्नपट’ में चित्रित किया है, जिसमें––
‘आज मिट गए दैन्य दुःख सब क्षुधा तृषा के क्रंदन
भावी स्वप्नों के पट पर युग जीवन करता नर्तन।
ग्राम नहीं वे, नगर नहीं वे,—मुक्त दिशा श्रीक्षण से
जीवन की क्षुद्रता निखिल मिट गई मनुज जीवन से।’
जिसकी तुलना में उनकी वर्तमान दशा ‘ग्राम आज है पृष्ठ जनो की करुण कथा का जीवित’—प्रमाणित हुई है।
किंतु जनता की इस सांस्कृतिक मृत्यु के कारणों पर नवीन विचारधारा पर्याप्त प्रकाश डालती है और वहाँ वे व्यक्ति नहीं रहते, प्रत्युत एक प्रणाली के अंग बन जाते हैं। इसीलिए मैं उन्हें बौद्धिक सहानुभूति दे सका हूँ।
‘आज असुंदर लगते सुंदर, प्रिय पीड़ित शोषित जन,
जीवन के दैन्यो से जर्जर मानव मुख हरता मन!’
अथवा
‘वृथा धर्म गण तंत्र—उन्हें यदि प्रिय न जीव जन जीवन’
‘इन कीड़ों का भी मनुज बीज, यह सोच हृदय उठता पसीज’
आदि पंक्तियाँ हार्दिकता से शून्य नहीं है। यदि मुझे सामंत-युग की संस्कृति के पुनर्जागरण पर विश्वास होता, तो जनता के संस्कारों के प्रति मेरी हार्दिक सहानुभूति भी होती। तब मैं लिखता—इस तालाब में (जन-मन में) काई लग गई है, इसे हटाना भर है, इसके अंदर का जल अभी निर्मल है।—जो पुनर्जागरण की ओर लक्ष्य करता। पर मैंने लिखा है—‘इस तालाब का पानी सड़ गया है, इस कृमिपूर्ण जल से काम नहीं चलेगा, उसमें भविष्य के लिए उपयोगी नया जल (संस्कृति) भरना पड़ेगा।’—जो सांस्कृतिक क्रांति की ओर लक्ष्य करता है। मैंने ‘यहाँ धरा का मुख कुरूप है’ ही नहीं कहा है ‘कुत्सित गहित जन का जीवन’ भी कहा है। जहाँ आलोचनात्मक दृष्टि की आवश्यकता है, वहाँ केवल भावुकता और सहानुभूति से कैसे काम चल सकता है? वह तो ग्रामीणों के दुर्भाग्य पर आँसू बहाने या पराधीन क्षुधा ग्रस्त किसानों को तपस्वी की उपाधि देने के सिवा हमें आगे नहीं ले जा सकती। इस प्रकार की थोथी सहानुभूति या दया-काव्य (पिटी पोयट्री) से मैंने ‘वे आँखें’, ‘गाँव के लड़कें’, ‘वह बुड्ढा’, ‘ग्रामवधू’, ‘नहान’ आदि कविताओं को बचाया है जिनमें, वर्तमान प्रणाली के शिकार, ग्रामीणों की दुर्गति का वर्णन होने के कारण ये बाते सहज ही में आ सकती थीं।
डी० एच० लारेंस ने भी निम्न वर्ग की मानवता का चित्रण किया है और वह उन्हें हार्दिकता दे सका है, पर हम दोनों के साहित्यिक उपकरणों में बड़ा भारी अंतर है। उसकी सर्वहारा (मशीन के संपर्क में आई हुई जनता) की बीमारी उनके राजनीतिक वर्ग-संस्कार है जिनका लारेंस ने चित्रण किया है। अपने देश के जनसमूह (मॉब) की बीमारी उससे कही गहरी, आध्यात्मिकता के नाम में रूढ़ि-रीतियों एवं अंधविश्वासों के रूप मे पथराए हुए (फ़ॉसिलाइज़्ड) उनके सांस्कृतिक संस्कार हैं। लारेंस के पात्र अपनी परिस्थितियों के लिए सचेतन और सक्रिय है। ‘ग्राम्या’ के दरिद्र-नारायण अपनी परिस्थितियों की तरह जड़ और अचेतन।
‘वज्रमूढ़, जड़भूत, हठी, बृष बाघव कर्षक,
ध्रुव, ममत्व की मूर्ति, रूढियों का चिर रक्षक।
फिर लारेंस जीवन के मूल्यों के संबंध में प्राणिशास्त्रीय मनोविज्ञान (बाएलॉजिकल थॉट) से प्रभावित हुआ है, मैं ऐतिहासिक विचारधारा से, जिसका कारण स्पष्ट ही है कि मैं पराधीन देश का कवि हूँ। लारेंस जहाँ द्वंद्व-पीड़न (सेक्स रिप्रसन) से मुक्ति चाहता है, मैं राजनीतिक-आर्थिक शोषण से। फिर भी मुझे विश्वास है कि, ‘ग्राम्या’ को पढ़कर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैंने दरिद्रनारायण के प्रति हृदयहीनता दिखलाई है।
ऐतिहासिक विचारधारा से मैं अधिक प्रभावित इसलिए भी हुआ हूँ कि उसमें कल्पना के स्रोत को विशद और वास्तविक पथ मिलता है। छायावाद के दिशाहीन शून्य आकाश में प्रति काल्पनिक उड़ान भरने वाली अथवा रहस्यवाद के निर्जन अदृश्य शिखर पर कालहीन विराम करनेवाली कल्पना को एक हरी-भरी ठोस जनपूर्ण धरती मिल जाती है।
‘ताक रहे हो गगन? मृत्यु नीलिमा गहन गगन?
निःस्पंद शून्य, निर्जन, निःस्वन?
देखो भु को, स्वर्गिक भू को!
मानव पुण्य प्रसू को!’
इसी लक्ष्य परिवर्तन की ओर इंगित करता है। ‘कितनी चिड़िया उड़े अकास, दाना है धरती के पास’ वाली कहावत के अनुसार ऐतिहासिक भूमि पर उतर आने से कल्पना के लिए जीवन के सत्य का दाना सुलभ और साकार हो जाता है, और कृषि, वाणिज्य, व्यवसाय, कलाकौशल, समाजशास्त्र, साहित्य, नीति, धर्म, दर्शन के रूप में, एवं भिन्न-भिन्न राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाओं में खंड-खंड विभक्त मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना का ज्ञान अधिक यथार्थ हो जाता है।
‘किए प्रयोग नीति सत्यो के तुमने जन जीवन पर,
भावादर्श न सिद्ध कर सके सामूहिक जीवन हित’
के अनुसार मध्य युग के अंतर्मुखी वैयक्तिक प्रगति के सिद्धांतों की जन-समूह के लिए व्यावहारिक उपयोगिता के प्रति मेरा विश्वास उठ गया। और
‘वस्तुविभव पर ही जन गण का भाव विभव अवलंबित’
सत्य के आधार पर मेरा हृदय नवीन युग की सुविधाओं के अनुरूप एक ऐसी सामूहिक सांस्कृतिक चेतना की कल्पना करने लगा जिसमें मनुष्य के हृदय से सामंत-युग की क्षुद्र चेतना का बोध डूब जाए! साथ ही प्रभाव पीड़ित जनसमूह की दृष्टि से, अतृप्त इच्छाओं का सात्विक विकास (सब्लिमेशन) किया जा सकता है—इस नैतिक तथ्य की व्यावहारिकता पर भी मुझे संदेह होने लगा।
छायावादी कवियों पर अतृप्त वासना का लांछन मध्यवर्गीय (बूर्ज्वा) मनोविज्ञान (डेप्थ साइकॉलॉजी) के दृष्टिकोण से नहीं लगाया जा सकता। भारत की मध्य युग की नैतिकता का लक्ष्य ही अतृप्त वासना और मूक वेदना को जन्म देता रहा है, जिससे बंगाल के वैष्णव कवियों के कीर्तन एव सूर-मीरा के पद भी प्रभावित हुए हैं। संसार में सभी देशों की संस्कृतियाँ अभी सामंत-युग की नैतिकता से पीड़ित है। हमारी क्षुधा (संपत्ति)-काम (स्त्री) के लिए अभी वही भावना बनी है। पुरानी दुनिया का सांस्कृतिक सगुण अभी निष्क्रिय नहीं हुआ है, और यंत्र-युग उन परिस्थितियों को जन्म नहीं दे सका है जिन पर अवलंबित सामाजिक संबंधों से उदित नवीन प्रकाश (चेतना) मानव जाति का नवीन सांस्कृतिक हृदय बन सके।
‘गत सगुण आज लय होने को: औं’ नव प्रकाश
नव स्थितियों के सर्जन से हो अब शनै: उदय
बन रहा मनुज की नव आत्मा, सांस्कृतिक हृदय।’
मेरी कल्पना भविष्य की उस मनुष्यता और सामाजिकता को चित्रित करने में सुख का अनुभव करने लगी जिसका आधार ऐतिहासिक सत्य है। ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग में इतिहास-विज्ञान ही के अर्थ में कर रहा हूँ जो दृश्य और द्रष्टा के सामूहिक विकास के नियमों का निरूपण करता है,—‘मानव गुण भव रूप नाम होते परिवर्तित युगपत्।’ में यह भी मानता हूँ कि सामूहिक विकास में बाह्य स्थितियों से प्रेरित होकर मनुष्य की अंतश्चेतना (साइकी), तदनुकूल, पहले ही विकसित हो जाती है; यथा—
‘जग जीवन के अंतर्मुख नियमों से स्वयं प्रवर्तित
मानव का अवचेतन मन हो गया आज परिवर्तित।’
किंतु उसके बाद भी मनुष्य के उपचेतन (सबकांसस) के आश्रित विगत सांस्कृतिक गुणों की प्रक्रियाएँ होती रहती है जिसका परिणाम बाह्य संघर्ष होता है, साथ ही वह नव विकसित अचेतन (अनकासस) की सहायता से प्रबुद्ध होकर नवीन सत्य का समन्वय भी करता जाता है।
अध्ययन से मेरी कल्पना जिन निष्कर्षों पर पहुँच सकी है उनके ऊपर मैंने, संक्षेप में, निरूपण करने का प्रयत्न किया है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ और उसे ईश्वरीय प्रतिभा का अंश भी मानता हूँ। मेरी कल्पना को जिन-जिन विचारधाराओं से प्रेरणा मिली है उन सबका समीकरण करने की मैंने चेष्टा की है। मेरा विचार है कि, ‘वीणा’ से लेकर ‘ग्राम्या’ तक, अपनी सभी रचनाओं में मैंने अपनी कल्पना ही को वाणी दी है, और उसी का प्रभाव उन पर मुख्य रूप से रहा है। शेष सब विचार, भाव, शैली आदि उसकी पुष्टि के लिए गौण रूप से काम करते रहे हैं।
मेरे आलोचकों का कहना है कि मेरी इधर की कृतियों में कला का प्रभाव रहा है। विचार और कला की तुलना में इस युग में विचारों ही को प्राधान्य मिलना चाहिए। जिस युग में विचार (आइडिया) का स्वरूप परिपक्व और स्पष्ट हो जाता है, उस युग में कला का अधिक प्रयोग किया जा सकता है। उन्नीसवीं सदी में कला का कला के लिए भी प्रयोग होने लगा था, वह साहित्य में विचार क्रांति का युग नहीं था। किंतु क्या चित्रकला में, क्या साहित्य में इस युग के कलाकार केवल नवीन टेकनीकों का प्रयोग मात्र कर रहे हैं, जिनका उपयोग भविष्य में अधिक संगतिपूर्ण ढंग से किया जा सकेगा। जागरण-युग के कवियों में, कविगुरु कालिदास और रवींद्रनाथ की तरह, कला का सुचारु मिश्रण और मार्जन देखने को मिलता है। कवींद्र रवींद्र अपनी रचनाओं में सामंत-युग के समस्त कलावैभव का नवीन रूप से उपयोग कर सके हैं। उससे परिपूर्ण, कलात्मक, संगीतमय, भावप्रवण और दार्शनिक कवि एवं साहित्य स्रष्टा शताब्दियों तक दूसरा कोई हो सकता है, इसके लिए ऐतिहासिक कारण भी नहीं है। भारत जैसे संपन्न देश का समस्त सामंतकालीन वाङ्मय, अपने युग के सांस्कृतिक समन्वय का विश्वव्यापी स्वप्न देखने के लिए, बुझने से पहले, जैसे अपनी समस्त शक्ति को व्यय कर, रवि-आलोकित प्रदीप की तरह, एक ही बार में प्रज्वलित होकर अपने अलौकिक सौंदर्य के प्रकाश से संसार को परिप्लावित कर गया है। फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ कि इस विश्लेषण-युग के अशांत, संदिग्ध, पराजित एवं प्रसिद्ध कलाकार को विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति के अनुकूल कला का यथोचित एव यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। अपनी युग-परिस्थितियों से प्रभावित होकर मैं साहित्य में उपयोगितावाद ही को प्रमुख स्थान देता हूँ। लेकिन सोने को सुगंधित करने की चेष्टा स्वप्नकार को अवश्य करनी चाहिए।
प्रगतिवाद उपयोगितावाद ही का दूसरा नाम है। वैसे सभी युगों का लक्ष्य सदैव प्रगति ही की ओर रहा, पर आधुनिक प्रगतिवाद ऐतिहासिक विज्ञान के आधार पर जन-समाज की सामूहिक प्रगति के सिद्धांतों का पक्षपाती है। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य का सामूहिक व्यक्तित्व उसके वैयक्तिक जीवन के सत्य की संपूर्ण अंशों में पूत्ति नहीं करता। उसके व्यक्तिगत सुख, दुःख, नैराश्य, बिछोह आदि की भावनाएँ, उसके स्वभाव और रुचि का वैचित्र्य, उसकी गुण-विशेषता, प्रतिभा आदि का किसी भी सामाजिक जीवन के भीतर अपना पृथक् और विशिष्ट स्थान रहेगा। किंतु इसमें भी संदेह नहीं कि एक विकसित सामाजिक प्रथा का, परस्पर के सौहादर्य और सद्भावना की वृद्धि के कारण, व्यक्ति के निजी सुख-दुखों पर भी अनुकूल ही प्रभाव पड़ सकता है और उसकी प्रतिभा एब विशिष्टता के विकास के लिए उसमें कहीं अधिक सुविधाएँ मिल सकती है। ऐतिहासिक विचारधारा वर्तमान युग की उस स्थिति विशेष का समाधान करती है, जो यंत्रयुग के प्रथम चरण पूंजीवाद ने धनी और निर्धन वर्गों के रूप में पैदा कर दी है, और जिसका उदाहरण सभ्यता के इतिहास में दूसरा नहीं मिलता। मध्ययुगों की ‘अन्न वस्त्र पीड़ित, असभ्य, निर्बुद्धि, पक में पालित’ जनता का इस वाष्पविद्युद्गामी युग में संपूर्ण जीर्णोद्धार न करना उनके मनुष्यत्व के प्रति कृतघ्नता के सिवा और कुछ नहीं है। ‘युगवाणी’ का ‘कर्म का मन’ चेतन और सामूहिक (कासस एंड कलक्टिव) कर्म का दर्शन है, जो सामूहिक सृजन और निर्माण का, ‘भव रूप कर्म’ का संदेश देता है।
विशिष्ट व्यक्ति की चेतना सदैव ही ह्रासोन्मुख समाज की रूढ़ि-रीति-नीतियों से ऊपर होती है, उसके व्यक्तित्व की सार्वजनिक उपयोगिता रहती है। अतएव उसे किसी समाज और युग में मान्यता मिल सकती है। विचार और कर्म में किसका प्रथम स्थान है, हीगल की ‘आइडिया’ प्रमुख है कि मार्क्स का ‘मैटर’ ऐसे तर्क और उहापोह व्यर्थ जान पड़ते हैं। उन्नीसवी सदी के शरीर और मनोविज्ञान संबंधी अथवा आदर्शवाद एवं वस्तुवाद संबंधी विवादों की तरह हमारा अध्यात्म और भौतिकवाद संबंधी मतभेद भी एकांगी है। आधुनिक भौतिकवाद का विषय ऐतिहासिक (सापेक्ष) चेतना है और अध्यात्म का विषय शाश्वत (निरपेक्ष) चेतना। दोनों ही एक दूसरे के अध्ययन और ग्रहण करने में सहायक होते हैं और ज्ञान के सर्वांगीण समन्वय के लिए प्रेरणा देते है!
आज इस संक्षिप्त ‘वीणा-ग्राम्या’ चयन के पृष्ठों पर आरपार दृष्टि डालने से मुझे यही जान पड़ता है कि जहाँ मेरी कल्पना ने मेरा साथ दिया है वहाँ मैं भावी मानवता के सत्य को सफलतापूर्वक वाणी दे सका हूँ और जहाँ में, किसी कारणवश, अपनी कल्पना के केंद्र से च्युत या विलग हो गया हूँ वहाँ मेरी रचनाओं पर मेरे अध्ययन का प्रभाव अधिक प्रबल हो उठा है, और मैं केवल आशिक सत्य को दे सका हूँ। इस भूमिका में मैंने उस प्रश्नावली के उत्तरों का भी समावेश कर दिया है जो सुहृद्वर श्री वात्स्यायन जी ने, मेरे आलोचक की हैसियत से, ऑल इंडिया रेडियो से ब्राडकॉस्ट किए जाने के लिए, तैयार की थी और जिसके बहुत से प्रश्नोत्तरों का आशय प्रस्तुत संग्रह में सम्मिलित रचनाओं पर प्रकाश डालने के लिए मुझे आवश्यक प्रतीत हुआ। इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।
मानव-समाज का भविष्य मुझे जितना उज्ज्वल और प्रकाशमय जान पड़ता है, उसे वर्तमान के अंधकार के भीतर से प्रकट करना उतना ही कठिन भी लगता है। भविष्य के साहित्यिक को इस युग के वाद-विवादों, अर्थशास्त्र और राजनीति के मतांतरों द्वारा, इस संदिग्धकाल के घृणा-द्वेष-कलह के वातावरण के भीतर से अपने को वाणी नहीं देनी पड़ेगी। उसके सामने आज के तर्क, संघर्ष, ज्ञान, विज्ञान, स्वप्न, कल्पना सब घुल-मिल कर एक सजीव सामाजिकता और सांस्कृतिक चेतना के रूप में वास्तविक एवं साकार हो जाएँगे। वर्तमान युद्ध और रक्तपात के उस पार वह एक नवीन, प्रबुद्ध, विकसित और हँसती-बोलती हुई, विश्व निर्माण में निरत, मानवता से अपनी सृजन-सामग्री ग्रहण कर सकेगा। इस परिवर्तन काल के विक्षुब्ध लेखक की अत्यंत सीमाएँ और अपार कठिनाइयाँ हैं। इन पृष्ठों में अपने संबंध में लिखने में यदि कहीं, ज्ञात-अज्ञात रूप से, आत्मश्लाघा का भाव आ गया हो, तो उसके लिए मैं हार्दिक खेद प्रकट करता हूँ। मैने कहीं-कहीं अपने को दुहराया है और शायद विवादपूर्ण सिद्धांतों का विस्तार-पूर्वक समाधान भी नहीं किया है। अंत में मैं ‘ग्राम्या’ की अंतिम रचना ‘विनय’ से दो पंक्तियाँ उद्धृत कर लेखनी को विराम देता हूँ––
‘हो धरिण जनो की: जगत स्वर्ग, जीवन का घर,
नव मानव को दो, प्रभु, भव मानवता का वर।’
(15 दिसंबर 1941)
(आधुनिक कवि, भाग 2 से)
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन प्रथम खंड (पृष्ठ 36)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.