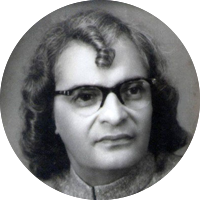आधुनिक काव्य-प्रेरणा के स्रोत
adhunik kavya prerna ke srot
प्रस्तुत वार्ता का विषय है ‘आधुनिक काव्य-प्रेरणा के स्रोत’, जिनसे हमारा अभिप्राय उन मौलिक प्रेरणाओं, मान्यताओं एवं उन धारणाओं तथा प्रवृत्तियों से है जो आधुनिक हिंदी काव्य को जन्म देने में सहायक हुई है और जिन्होंने उसके प्रवाह को निर्दिष्ट दिशा की ओर मोड़ा है। प्रत्येक युग अपनी विशेष विचार-धारा, विशेष भावनाओं के आधार तथा अपना विशेष दृष्टिकोण लेकर आता है; जो उस युग के साहित्य में प्रतिफलित होता है, साहित्यिक अथवा कलाकार का सूक्ष्म भाव-प्रवण हृदय अपने युग की उन विकास तथा प्रगति की शक्तियों को पहचानकर अपनी कला के माध्यम द्वारा उन्हें जन-समाज के लिए सुलभ बना देता है।
काव्यात्मकता केवल रसात्मक वाक्य तक ही सीमित नहीं है। यद्यपि रसात्मक वाक्य होना अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द होना काव्य का सहज नैसर्गिक गुण है। छंदों की झंकृति, वेशभूषा, शब्दों तथा अलंकारों का सौष्ठव, भाषा की चित्रमयी अभिव्यंजना, कल्पना की सतरंगी उड़ान तथा सौंदर्य बोध आदि काव्य के बाह्य उपादान मात्र कहे जा सकते हैं। इन सबसे अधिक उपयोगी काव्य की वह अंतश्चेतना है, जो युग-विशेष के हृदय-मंथन तथा जीवन संघर्ष को प्रतिबिंबित करती हुई उस नवीन आलोक-दिशा का इंगित देती है, जिस ओर युग का जीवन प्रवाहित होता है।
हिंदी काव्य का आधुनिक युग छायावाद से प्रांभ होता है, जो द्विवेदी-युग तथा प्रयोगवादी युग का मध्यवर्ती काल है और जिसकी एक विशेष धारा प्रगतिवादी तथा दूसरी प्रयोगवादी कविता कही जाती है। छायावाद से पहले भी हिंदी काव्य-साहित्य में नवीन प्रेरणाएँ काम करने लग गई थी और एक प्रकार से द्विवेदी-युग से पहले भी श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी कविता में नए विषयों का समावेश होने लगा था। श्री भारतेंदु के भारतदुर्दशा नाटक में देशभक्ति की मार्मिक व्यंजना मिलती है। उनकी स्वतंत्र कविताओं में भी यत्र-तत्र देश के अतीत गौरव की महिमा, वर्तमान अधोगति का वेदनापूर्ण चित्र और भविष्य का उद्बोधनगान पाया जाता है। देश की वर्तमान दशा से क्षुब्ध होकर भारतेंदु कहते हैं :
हाय, वहै भारत भुव भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी।
हाय पचनद, हा पानीपत, अजहुँ रहे तुम घरनि विराजत।
तुम में जल नहिं जमुना गंगा, बढ़हु वेगि किन प्रबल तरंगा।
बोरहु किन झट मथुरा कासी, धोवहु यह कलंक की रासी।
भारतेंदु के इस प्रकार के करुण उद्गारों में देशभक्ति के साथ ही एक शक्तिमयी नयी अभिव्यंजना मिलती है। द्विवेदी युग में भारतीय जागरण के साथ ही देशभक्ति तथा राजनीति से प्रभावित अनेक ओजपूर्ण रचनाएँ लिखी गईं। श्री गुप्त जी की ‘भारत भारती’ ने अपने युग को सबसे अधिक प्रभावित किया। द्विवेदी-युग का मुख्य प्रयत्न खड़ीबोली को गद्य-पद्य के रूप में मार्जित करने की ओर रहा। उनके युग में हिंदी भाषा के सौंदर्य से तो वंचित रही, किंतु उसका आधुनिक रूप निश्चित रूप से निखर आया और उसमें एक प्रकार का संयम तथा सुथरापन आ गया।
द्विवेदी-युग का काव्य अधिकतर गद्यवत्, इतिवृत्तात्मक तथा अभिधा-प्रधान रहा, किंतु उसका भावना-क्षेत्र भारतेंदु युग से कहीं अधिक विस्तृत तथा व्यापक हो गया। उसमें अनेकानेक नवीन विषयों का समावेश होने लगा और उसमें भारतीय पुनर्जागरण की चेतना जन्म लेने लगी। द्विवेदी-युग के कवियों में तीन प्रमुख नाम हमारे सामने आते हैं श्री-श्रीधर पाठक, श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय ‘हरिऔध’ और राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त। वैसे अन्य भी कई कवि उस युग के साहित्य के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगे।
श्रीधर पाठक जी का प्रकृति-वर्णन उस युग के काव्य में अपना विशेष महत्त्व रखता है, उनसे पहले प्रकृति का चित्रण केवल उद्दीपन के रूप में प्रयुक्त होता रहा। पाठक जी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी तथा उपासक थे। उनके शब्दों का चयन भी अत्यंत मधुर तथा सुथरा होता था। उनकी वाणी में जो एक प्रसाद था, वह स्वयं हिंदी काव्य की नवीन चेतना का द्योतक था। उनके प्रकृति-वर्णन का एक उदाहरण लीजिए :
बिजन वन प्रान्त था, प्रकृति-मुख शान्त था,
अटन का समय था, रजनि का उदय था।
प्रसव के काल की लालिमा में लसा,
बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा।
“प्रसवकाल को लालिमा से लसे बाल शशि” की कल्पना में आधुनिकता की छाप है। उनकी “स्वर्गीय वीणा” की पंक्तियों में ध्वनि संकेत की मधुरिमा देखिए :
कहीं पै स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है,
सुरो के संगीत की सी कैसी सुरीली गुजार आ रही है।
कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन, कभी विनय है,
दया है दाक्षिण्य का उदय है, अनेको बानक बना रही है।
भरे गगन मे है जितने तारे, हुए हैं बद मस्त गत पै सारे,
समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है।
वीणा के सुरीले स्वरों पर गगन के तारों तथा समस्त ब्रह्मांड का तन्मय होकर नाच उठना जिस आनंदातिरेक की ओर इंगित करता वह अविमानस की एकता का परिचायक है। पाठक जी ने “श्रांत पथिक” तथा “ऊजड गाम” के नाम से गोल्डस्मिथ के Traveller तथा Deserted Village के भी काव्यमय अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। कश्मीर-सुषमा उनके प्रकृति प्रेम का रमणीय लीलाकक्ष है, उसमें उनका पदविन्यास अत्यंत कोमल तथा ललित होकर निखरा है। पाठक जो की रचनाओं में समाज सुधार की भी भावना मिलती है, इस नवीन धारा का प्रारंभ भारतेंदु-युग में हो चुका था। श्रीधर पाठक वास्तव में एक प्रतिभावान तथा सुरुचि संपन्न कवि थे।
द्विवेदी-युग के कवियों में “हरिऔध” जी का अपना विशिष्ट स्थान है। उन्हें बोल-चाल की भाषा पर भी उतना ही अधिकार था, जितना संस्कृत-गर्भित भाषा पर। उनके “प्रियप्रवास” का शब्द-संगीत छायावाद के शब्द-संगीत के अधिक निकट है :
दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला
तरु शिख पर थी अव राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा।
तरुशिखा पर अस्तमित सूर्य की प्रभा का चित्रण छायावादी अभिव्यंजना है।
रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका, राकेन्दु बिम्बानना
तन्वगी कलहासिनी सुरसिका, क्रीड़ा कला पुत्तली
शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीलामयी
श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधुर्य सन्मूर्ति थी।
इन चरणों की स्वर-झंकृति अधिक मधुर तथा सरल बनकर पीछे छायावाद के संगीत में प्रतिध्वनित हुई। भाव-सौंदर्य की दृष्टि से भी “प्रियप्रवास” में श्री राधा का व्यक्तित्व रीतिकालीन परिपाटी से मुक्त होकर अधिक स्वच्छ तथा आधुनिक बन गया है।
द्विवेदी-युग के कवियों में सबसे अधिक प्राणवान् तथा युगचेतना के प्रतीक स्वरूप महाकवि श्री मैथिलीशरण जी गुप्त हुए। जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं, भारतेंदु-युग की स्वदेश-प्रेम की भावना गुप्त जी की “भारत भारती” में विकसित राष्ट्रभावना का स्वरूप ग्रहण कर सकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में “गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता रही, कालानुसरण की क्षमता अर्थात् उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य-प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निःसंदेह कहे जा सकते हैं। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो स्वरूप धारण किया, उसका पूरा आभास गुप्त जी की रचनाओं में मिलता है। सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्वप्रेम, किसानी और आधुनिक काव्य-प्रेरणा के स्रोत श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी झलक हम उनमें पाते हैं।” गुप्त जी की आधुनिकतम रचनाओं में युग की चेतनात्मक क्रांति तथा विद्रोह के स्वर भी स्पष्ट रूप से मुखरित हो उठे हैं। उनकी ‘झंकार’ छायावादी युग की वस्तु है और ‘पृथ्वी-पुत्र’ प्रगतिवादी युग की। गुप्त जी में पुरातन के प्रति सम्मान और नूतन के प्रति उत्साह तथा आग्रह की भावना मिलती है। उनका यह सामंजस्य छायावादी युग के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि का काम करता है। उन्हें प्रबंध-काव्य तथा आधुनिक प्रगीत-मुक्तकों में समान रूप से सफलता मिली है। उनके मुक्तकों में छायावादी अभिव्यंजना तथा लाक्षणिक प्रयोगों का वैचित्र्य पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। उनके प्रबंध काव्य ‘साकेत’ को काव्य की उपेक्षिता उर्मिला का विरह-वर्णन एक नवीनता प्रदान कर देता है। अनसूया, उर्मिला आदि काव्य की उपेक्षिताओं की ओर गुप्त जी अपने संस्कार में बंगला के अध्ययन से प्रभावित हुए हैं। सर्वप्रथम कवींद्र रवींद्र ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था।
आगे चलकर हम देखेंगे कि हिंदी की नवीन काव्यधारा में बॅंगला कवियों, विशेषकर रवींद्रनाथ, का विशेष प्रभाव पड़ा है। वैसे ही श्री मुकुटधर पांडेय आदि की रचनाओं में छायावाद की सूक्ष्म भावव्यंजना तथा रंगीन कल्पना धीरे-धीरे प्रकट होने लगी थी, जो आगे चलकर प्रसाद जी के युग मे पुष्पित-पल्लवित होकर, एक नूतन चमत्कार एवं चेतना का संस्कार धारण कर, हिंदी काव्य के प्रांगण में नवीन युग के अरुणोदय की तरह मूर्तिमान हो उठी।
प्रसाद जी छायावाद के सर्वप्रथम प्रवर्त्तक माने जाते हैं। उनके युग में आने तक हिंदी-कविता के अंतर्विधान में भी बंगला का, और विशेषकर कवींद्र रवींद्र के काव्य का, अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ चुका था। कवींद्र रवींद्र भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत बनकर आए। उन्होंने भारतीय साहित्य को नवीन चेतना का आलोक, नवीन भावों का वैभव, नवीन कल्पना का सौंदर्य, नवीन छंदों को स्वर झंकृति प्रदान कर उसे विश्व-प्रेम तथा मानववाद के व्यापक धरातल पर उठा दिया। कवींद्र के युग से जो महान् प्रेरणा हिंदी काव्य-साहित्य को मिली, वही वास्तव में छायावाद के रूप में विकसित हुई।
कवींद्र रवींद्र के आगमन के लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो चुकी थी। बँगला में भारतीय पुनर्जागरण का समारंभ हो चुका था। एक ओर श्री रामकृष्ण परमहंस जी के आविर्भाव तथा स्वामी विवेकानंद के प्रभाव से आध्यत्मिक जागरण तथा सर्वधर्म-समन्वय का प्रकाश फैल चुका था, दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन के रूप में राष्ट्रीय तथा राजनीतिक चेतना जाग्रत हो उठी थी। ब्रह्म-समाज के रूप में पूर्व तथा पश्चिम की संस्कृतियों का समन्वय करने की ओर भी कुछ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो चुका था।
रवींद्रनाथ के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर स्वयं भी ब्रह्मसमाजी थे। कवींद्र महान् प्रतिभा से संपन्न होकर आए थे। उन्होंने अपने युग की समस्त जागरण की शक्तियों का मनन कर उनके प्राणप्रद तथा स्वास्थ्यकर सारतत्वों का संग्रह अपने अंतर में कर लिया था। और अनेक छंदों, तालों तथा लयों में अपनी मर्मस्पर्शी वाणी को नित्य नवीन रूप देकर रूढ़िग्रस्त भारतीय चेतना को अपने स्वर के तीव्र मधुर आघातों से जाग्रत, विमुक्त तथा विमुग्ध कर, उसे एक नवीन आकांक्षा के सौंदर्य तथा नवीन आशा के स्वप्नों में मंडित कर दिया था। भारतीय अध्यात्म के प्रकाश को उन्होंने पश्चिम के यंत्रयुग के सौंदर्य में वेष्ठित कर उसे पूर्व तथा पश्चिम दोनों के लिए समान रूप से आकर्षक बना दिया था। इस प्रकार नवीन युग की आत्मा के अनुकूल स्वर-झंकृति प्रस्तुत कर कवींद्र रवींद्र ने एक नवीन सौंदर्यबोध का झरोखा भी कल्पनाशील युवक साहित्यकारों के हृदय में खोल दिया था।
इसी काव्यमय आध्यात्मिक आलोक, सौंदर्य-चेतना तथा सृजन कल्पना की मुक्ति को ग्रहण कर हिंदी में छायावाद ने प्रवेश किया। द्विवेदी-युग की पौराणिक भावना, कला-परंपरा तथा राष्ट्रीय जागरण के स्वर छायावाद के युग में एक नवीन विराट् आध्यात्मिक चेतना, नवीन छंद और शैलियों के प्रयोग तथा एक व्यापक विश्वप्रेम की भावना के रूप में परिणत हो गए। प्रसाद जी का ‘झरना’ जैसे हिंदी में एक नवीन अभिव्यक्ति का झरना था। उनके ‘आँसू’ के कणों में जैसे छायावादी युग की समस्त मूक करुणा तथा भावनात्मक वेदना एक नवीन अभिव्यंजना का वैचित्र्य लेकर उमड़ उठी। प्रसाद जी की ‘कामायनी’ में छायावाद का अंत स्पर्शी गांभीर्य सौंदर्य तथा विचार-सामंजस्य जैसे एक विशाल स्फटिक-प्रासाद के रूप में साकार हो उठा। निराला जी ने छायावादी कविता को छंदों के बंधनों से मुक्त कर उसे एक अधिक व्यापक भूमि पर खड़ा कर दिया। उन्होंने अपनी उज्ज्वल, ओजपूर्ण शैली द्वारा भारतीय दर्शन के आलोक को वितरित किया। ‘परिमल’ तथा ‘गीतिका’ में उनके अनेक प्रगीत गीति-काव्य की परिपूर्णता प्राप्त कर सके है। छायावादी कविता मुख्यतः प्रगीतों का रहस्य-इंगितमय सौंदर्य लेकर प्रस्फुटित हुई। महादेवी जी के प्रगीत इस दृष्टि से विशेष रूप से आकृष्ट करते हैं। दूसरी ओर श्री नवीन जी, भारतीय आत्मा तथा दिनकर जी ने राष्ट्रीय भावना को छायावादी परिधान प्रदान कर उसे अधिक सजीव, सक्रिय, ओजपूर्ण तथा मर्मस्पर्शी बना दिया। छायावाद के आकाश में और भी अनेक नक्षत्र प्रकाशपूर्ण व्यक्तित्व लेकर जगमगा उठे, जिनकी अमर देन से हिंदी का काव्य-साहित्य अनेक रूप से संपन्न हुआ।
छायावाद का विकास प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के मध्यवर्ती काल में हुआ। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रायः सर्वत्र ही युग की वास्तविकता के प्रति मनुष्य की धारणा आधुनिक काव्य-प्रेरणा के स्रोत बदल गई। छायावाद ने जो नवीन सौंदर्य बोव, जो आशा-आकांक्षाओं का वैभव, जो विचार-सामंजस्य तथा समन्वय प्रदान किया था, वह पूँजीवादी युग की विकसित परिस्थितियों की वास्तविकता पर आधारित था। मानव चेतना तब युग की बदलती हुई कठोर वास्तविकता के निकट संपर्क में नहीं आ सकी थी। उसकी समन्वय तथा सामंजस्य की भावना केवल मनोभूमि पर ही प्रतिष्ठित थी। किंतु द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद वह सर्वधर्म समन्वय, सांस्कृतिक समन्वय, ससीम-असीम तथा इहलोक-परलोक-संबंधी समन्वय की अमूर्त भावना अपर्याप्त लगने लगी, जिससे छायावाद ने प्रेरणा ग्रहण की थी। और अनेक कवि तथा कलाकारों की सृजन-कल्पना इस प्रकार के कोरे मानसिक समाधानों से विरक्त होकर अधिक वास्तविक तथा भौतिक धरातल पर उतर आई और मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित होकर प्रगतिवाद के नाम से एक नवीन काव्य चेतना को जन्म देने में संलग्न हो गई। जिस प्रकार मार्क्स के भौतिकवाद ने अर्थनीति तथा राजनीति संबंधी दृष्टिकोणों को प्रभावित किया, उसी प्रकार फ़्रायड युग आदि पश्चिम के मनोविश्लेषकों ने रागवृत्ति संबंधी नैतिक दृष्टिकोण में एक महान् क्रांति उपस्थित कर दी। फलतः छायावादी युग के सूक्ष्म आध्यात्मिक तथा नैतिक विश्वासों के प्रति मन्दिग्ध होकर तथा पश्चिम की भौतिक तथा प्राणिशास्त्रीय विचारधाराओं से अधिक या कम मात्रा में प्रभावित होकर अनेक प्रगतिवादी, प्रयोगवादी तथा प्रतीकवादी कलाकार अपने हृदय के विक्षोभ तथा कुंठित आशा-आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देने के लिए संक्रांति काल की बदलती हुई वास्तविकता से प्रेरणा ग्रहण करने लगे।
किंतु छायावाद की जो सीमाएँ सूक्ष्म धरातल पर थी, प्रगतिवादियों की वही सीमाएँ स्थूल धरातल पर है। छायावादी कवि अथवा कलाकार वास्तव में आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति नहीं प्राप्त कर सका था। वह केवल बौद्धिक अधिदर्शनों, मान्यताओं तथा धारणाओं से प्रभावित हुआ था। इसीलिए वह युग जीवन की कठोर वास्तविकता से कटकर कुछ दार्शनिक एवं मानसिक विरोधों में सामंजस्य स्थापित कर संतुष्ट रहने की चेष्टा करने लगा। इसी प्रकार आज के अधिकांश प्रयोगवादी एवं तथाकथित प्रगतिवादी कलाकार पिछले अंतर्मुख आदर्शों तथा नए बहिर्मुख यथार्थ के बीच प्रतिदिन बढ़ती हुई गहरी खाई में गिरकर तथा सूक्ष्म के प्रति, आदर्श के प्रति, व्यक्ति के प्रति अपना विद्रोह प्रकटकर, संक्रंति काल को ह्रासोन्मुखी प्रवृत्तियों तथा सामूहिक सर्वसाधारणता को वाणी देकर संतोष करना चाहते हैं ।
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 164)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.