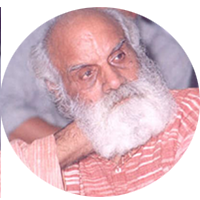निराला की एक कविता : हिन्दी के सुमनों के प्रति पत्र
nirala ki ek kavita ha hindi ke sumnon ke prati patr
रोचक तथ्य
'ओर' के संपादक कवि विजेंद्र ने निराला की कविता 'हिन्दी के सुमनों के प्रति पत्र' पर अपनी व्याख्या लिखने के लिए कवि त्रिलोचन को पत्र लिखा। त्रिलोचन ने 18.5.1988 को सागर से विजेंद्र के नाम एक पत्र लिखते हुए उक्त कविता की व्याख्या लिख भेजी। विजेंद्र को संतोष न हुआ, उन्होंने रामविलास शर्मा की राय माँगी। डॉ. शर्मा ने पत्र द्वारा जो अपनी संक्षिप्त व्याख्या की, वह विजेंद्र जी को जँची। उन्होंने विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा त्रिलोचन से कविता की पुनर्व्याख्या की माँग की। विष्णु जी के प्रश्न और त्रिलोचन जी के उत्तर की शैली में पुनर्व्याख्या भी हुई। यह पूरा प्रकरण सप्रमाण 'ओर' के 14 वें अंक में कवि विजेंद्र ने 'कविता की अन्तर्यात्रा' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है। यहाँ उस प्रकरण से केवल त्रिलोचन की व्याख्या वाले अंश उद्धृत किए जा रहे हैं—पहले त्रिलोचन जी का पत्र, फिर विष्णुचंद्र शर्मा और त्रिलोचन जी का वार्तालाप।
इस शीर्षक में 'पत्र' शब्द कविता का अर्थ खोल देता है। हिन्दी में 'सुमनों के प्रति' पत्र की ओर से बात कही गई है।
'पत्र' शब्द पाँच छंदों की इस कविता में तीसरे छंद की तीसरी पंक्ति में आया है। 'पत्र' के हिन्दी में कई अर्थ हैं; चिट्ठी और पत्ता। इस कविता में ‘दैनिक पत्र' या 'काग़ज़ का पन्ना' आदि अर्थ मुझे आवश्यक नहीं लगते।
सुमनों से बात पत्ता ही कर सकता है और यह पत्ता डाल से गिरा हुआ पत्ता है । 'मैं' पत्ते का 'मैं' है। जो गिर कर ज़मीन पर पड़ा है। 'हिन्दी' शब्द होने से दूसरा अर्थ भी ध्वनित होता है; यानी हिन्दी में कवि और लेखक। यह कविता वानस्पतिक पर्यवेक्षण पर पूरा ध्यान देकर लिखी गई है—
मैं जीर्ण साज बहु छिद्र आज,
तुम सुदल, सुरंग, सुवास, सुमन
मैं हूँ केवल पदतल आसन,
तुम सहज विराजे महाराज।
'मैं' = पत्ता, 'तुम' = सुमन। पत्ता डाल से बिछुड़ कर ज़मीन पर है और बात 'सुमन' से कह रहा है जो वृक्ष पर सबसे ऊपर है। डाल या टहनी का संबंध पत्ते से था। पत्ता पतझर में गिरा है। उसका पीलापन भी सूख कर भिन्न रंग का हो जाता है। 'पत्र' अपने को 'जीर्ण साज' और 'बहुछिद्र' कह रहा है। पत्ते की वर्तमान स्थिति जीर्णता की है और बहुछिद्रता की भी। पतझर के पत्ते जो डाल से गिरते हैं उनमें शीत की अतिशयता के प्रभाव से छिद्र भी हो जाते हैं। आम, महुए और दूसरे पतझर से प्रभावित वृक्षों के गिरे हुए पत्तों पर ध्यान देंगे तो यह छिद्र भी दिख जाएँगे। 'सुमन' को उन्होंने सुदल, सुरंग, सुवास बताया है। फिर 'पत्र' कहता है—‘मैं केवल ‘पदतल आसन’ हूँ और तुम सहज विराजे महाराज (हो)।
दूसरा छंद है—
ईर्ष्या कुछ नहीं मुझे, यद्यपि
मैं ही वसंत का अग्रदूत,
ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत
मैं रहा आज यदि पार्श्वच्छवि।
'पत्र' 'सुमन' से कहता है कि मुझे ईर्ष्या नहीं है (तुम से)। आगे लिखा है 'यद्यपि मैं ही वसंत का अग्रदूत'। 'पत्र' पतझर के कारण गिरते हैं तो लोग जान जाते हैं कि अब वसंत दूर नहीं। अतः पतझर का पत्ता जो ज़मीन पर पड़ा है वह कह रहा है कि वसंत के आने की सूचना मैंने ही दी है अतः मैं वसंत का अग्रदूत हूँ। क्या हुआ यदि में आज 'पार्श्वच्छवि' (किनारे कर दिया गया) जैसे ब्राह्मणों की सभा मैं अछूत (दूर या किनारे बैठाए जाते हैं) इस में 'पत्र' कहता है कि 'मैं' आज यदि 'पार्श्वच्छवि' रहा जैसे ब्राह्मण समाज में अछूत तो क्या हुआ!
तीसरा छंद—
तुम मध्य भाग के महाभाग!
तरु के उर के गौरव-प्रशस्त।
मैं पढ़ा जा चुका पत्र न्यस्त
तुम अलि के नव रस रंग राग।
इस में 'पत्र' कहता है कि तुम महाभाग तरु के उर के प्रशस्त गौरव हो। तुम महाभाग (भाग्यशाली) तरु के उर के (अंतस्थल के) प्रशस्त गौरव हो और मैं पढ़ा जा चुका (अत्यंत परिचित) 'पत्र' (पत्ता) हूँ (जो) न्यस्त (छोड़ दिया गया है) और तुम (सुमन) अलि (भ्रमर) के नए रस-रंग-राग (हो)।
ऊपर के ये तीन छंद बहुत स्पष्ट हैं। अंतिम दो छंद एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब अंतिम दोनों छंद देखें—
देखो, पर क्या तुम पाते 'फल'
देगा जो भिन्न स्वाद रस भर
कर पार तुम्हारा भी अंतर
निकलेगा जो तरु का संबल।
फल सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज़
या तुम बाँध कर रँगा धागा
फल के भी उर का कटु त्यागा;
मेरा आलोचक एक बीज।
इसमें 'पत्र' कहता है—यहाँ 'देखो' का अर्थ होता है देखना। क्योंकि देखने की क्रिया का कोई निदेश नहीं है। देखना है किंतु कि तुम फल क्या (किस प्रकार का, कैसा) पाते (हो)। यहाँ जैसे सुमन पेड़ के अंतर का विकास कहा गया है। वैसे ही फल को सुमन के अंतर का विकास कहा गया है। पहली पंक्ति में यही बात स्पष्ट की गई है। चौथे छंद की दूसरी पंक्ति उसी फल के विषय में संकेत शैली में कहती है जो रस भर कर भिन्न स्वाद देगा; तुम्हारा (सुमन का) भी अंतर पार करके जो तरु का संबल निकलेगा; फल वही श्रेष्ठ है और दुर्लभ वस्तु है।
'फल' पाँचवें छंद का पहला शब्द है। यहाँ आकर वाक्य पूरा होता है। ऊपर के गद्यांश से मिलाने पर स्थिति स्पष्ट है। इसके बाद जो वाक्य चलता है वह पूरा नहीं है। उसे कहना पड़ता है कि कवि ने अपूर्ण ही छोड़ा है। यहाँ वाक्य की अपूर्णता का दोष है! मुझे लगता है यहाँ अपूर्णता पूर्णता की ओर संकेत देती हुई मध्यपथ में विराम ग्रहण करती है। पूरी कविता की शैली बातचीत की है। और बातचीत में कभी-कभी वाक्य अधूरे रह जाते हैं। समझने में कोई बाधा नहीं रह जाती। दूसरी और तीसरी पंक्ति का अन्वय किया हुआ वाक्य और रूप यह है—
या तुम (सुमन) फल के भी उर का कटु त्यागा रँगा धागा बाँध कर—रँगा धागा फल के अंतर में रक्षित बीज-सूत्र को कहते हैं। इस बीज-सूत्र, का पूर्व रूप अनेक फूलों में दंड के आकार का निकलता है। यही रूपांतरित हो कर बीज-सूत्र बनता है। फूलों में पराग रज या दंड रूप में होता है और कुछ फूलों में तरल पदार्थ होता है उसे मकरंद कहते हैं। तो रँगा धागा फूल के अंदर से निकला हुआ फल का बीज-सूत्र बना करता है और दंड के आकार का फूल के भीतर से निकला हुआ हिस्सा यूँ ही मुरझा जाता है उससे फल नहीं बनता। अगर फूल 'रँगा धागा बाँधकर' ही रह जाए तो उसकी जीवन यात्रा फल तक नहीं पहुँचती और फल के ही अन्तः रस से निर्मित है बीज। अंतिम पंक्ति में कहा है 'मेरा आलोचक एक बीज।' 'मेरा आलोचक' का मतलब है मुझे अच्छी तरह देखने वाला यानी पहचानने वाला 'एक बीज' है, 'एक' माने अकेला।
इसमें पत्र, सुमन, फल और बीज ये स्थितियाँ स्पष्ट हैं। इनके सहारे प्रतीकात्मक अर्थ करने में कोई बाधा नहीं है। आधार तो सुमन ही है। वक्ता पत्र है। वह सुमन की और स्थितियों की ओर भी संकेत करता है।
***
मैं (वि. चं. शर्मा) ने पूछा, 'हिन्दी के सुमनों के प्रति पत्र' की व्याख्या करें।
त्रिलोचन : एक अर्थ रामविलास या दूसरे करते हैं। अन्य इसे आत्मपरक कविता समझते हैं! मैं इस कविता को 'वानस्पतिक अनुभव' की कविता मानता हूँ। आप बताएँ 'अग्रदूत' का क्या अर्थ है?'
मैं चुप रहा। फिर कहा : 'नहीं जानता।' वह (त्रिलोचन) न हँसे न आवेश में आए। कहा : 'अग्रदूत', का अर्थ है 'पतझर'। इस कविता में 'पत्र' और 'फूल' का संवाद है। पत्ता बताता है 'मैं पतझर में जीर्ण हूँ।' जीर्ण पत्रों को निराला ने ध्यान से देखा था। उसमें 'बहुछिद्र' यह सूक्ष्म पर्यवेक्षण है—वनस्पति का। दूसरा कोई कवि उस समय प्रकृति का सूक्ष्म पर्यवेक्षक नहीं था। वहीं इस कविता के हर छन्द पर ध्यान देने की बात है। 1, 4, 2, 3, आज/ महाराज और सुमन/ आसन का तुक-विधान और कविताओं में निराला ने नहीं दिया। पत्ता अपना आज का चित्र-परिचय देख कर सुमनों से कहता है—'तुम सुदल, सुरंग, सुवास' हो। आज मैं तुम्हारे मुक़ाबले 'पदतल में पड़ा हुआ हूँ।' वही स्थान मेरा आसन है। तुम सहज रूप में विराजे महाराज हो। हिन्दी में इसे 'आत्मपरक कविता' मानने वाले 'ईर्ष्या' का क्या अर्थ लेंगे? निराला की 'सरोज स्मृति' या दूसरी आत्मपरक कविताओं में लक्षणा का कम प्रयोग मिलता है। वे सीधी यथार्थपरक और अभिधा की शैली वाली कविताएँ हैं। पत्तों को सुमनों से ईर्ष्या नहीं होती। पत्ता स्वीकार करता है 'तुम जो सहज विराजे हुए हो, मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या नहीं। यद्यपि मैं जानता हूँ—मेरा चरित्र वसंत के अग्रदूत यानी 'पतझर' का है। इसलिए मैं पेड़ के चारों ओर फैला हुआ हूँ—पार्श्वच्छवि का आज जीर्ण-साज बहुछिद्र पत्रों का समूह है।' यहाँ ध्यान देने की बात है, पत्रों का जीर्ण-साज बहुछिद्र रूप से ही मिलता हुआ है समाज में ब्राह्मण समाज में अछूतों का जीवन। इसे कविता में कवि का सामाजिक अवदान कहा जा सकता है। इसी कविता के साथ 'अणिमा' की धूल में तुम मुझे भर दो। याद रखो पहली कविता '36 की है, दूसरी '40 की। दूसरी कविता में उसी अनुभव का बिंब सुकर 'पसिर', सुंदर परिसर है। पेड़ की पार्श्वध्वनि का यह बिंब है।
(पूरी कविता त्रिलोचन को याद थी) वह सुना गए। मैं ने (विष्णुचंद्र शर्मा) कविता बाद में पढ़ी।
'पेड़ का मध्य भाग क्या है?' मैंने पूछा।
त्रिलोचन ने कहा, 'पेड़ की नहीं, सुमनों के प्रति कविता है, यह याद रखें। सुमनों का मध्य भाग आप ने देखा है। वह मध्य भाग ही महाभाग होता है। उसी में धागा और पराग देखा जा सकता है। पत्ता बताता है, सुमनों को, तुम मध्यभाग के महाभाग हो। कैसे हो? तरु के उर के गौरव होते हैं—फल। वह प्रशस्त गौरव तुम हो। मैं पत्ता, आज पढ़ा जा चुका पत्र हूँ। यहाँ अवध का लहजा ध्यान में रखें।' पढ़ा जा चुका का अर्थ हुआ 'पहचाना हुआ'। पत्र कभी फेंके नहीं जाते। प्रेम पत्र आपने कभी फेंके न होंगे।
हम दोनों मुस्कुराए।
हाँ तो पत्ता ख़ुद को कहता है : डस्टबिन में फेंका बेकार की चीज़। पर फूल तो बेकार नहीं होते। तरु के उर के गौरव होते हैं। इसीलिए सुमनों में नव रस, रंग, राग देखते चखते रहते हैं, भौंरे।
संवाद का लहज़ा अचानक तीसरे छंद में बदल जाता है। वाक्य कहीं अधूरे रह जाते हैं। विषय संक्षिप्त होते जाते हैं। एक पद, एक वाक्य का काम करता है। यह नाटक का विधान है।
देखो मित्र, पर, तुम जीवन यात्रा (वानस्पतिक उपक्रम) में क्या फल पाते हो। फल जो भी होगा, निश्चित मानो बंधु वह भिन्न स्वाद रस से भी पूरा होगा। इसी 'स्वाद' रस से भी पूरा होगा। इसी 'स्वाद रस' से तुम्हारा अंतर-हृदय जीवन यात्रा को पार करेगा। उसी जीवन यात्रा के अनुभव के जो तरु का संबल निकलेगा, उसी से तरु भास्वर होगा। 'फल' का प्रयोग 'देखो' से चौथे छन्द तक एक वाक्य है। फल जो तरु का संबल है। वह 'सर्वश्रेष्ठ नायाब चीज़' तभी होता है जब फूल के अंतर से फल पैदा होता है। यहाँ वाक्य अधूरा रखा। जान बूझ कर अधूरे वाक्य का प्रयोग निराला ने किया है। ध्यान दें। फूल के अंतर को महाभाग कहा है कवि ने। उस फूल में जो धागा होता है वह रँगा हुआ होता है। वह रँगा धागा जब फूल में आता है तभी फल का दाना आता है। उस धागा को आप चख कर देखें : चने के दोनों दलों के बीच का वह भाग कटु होता है। उसे त्यागा जाता है। तभी फल के उर में बीज आता है। यह फूल से फल और फल से बीज आने की वानस्पतिक प्रक्रिया है।
मैंने कहा, 'कलकत्ता से दूर मैं एक तीर्थ को गया था। वहाँ मैंने एक 'बात' देखी थी। पेड़ में विधवा औरतें अपनी-अपनी कामनाओं के अनुसार धागा बाँधती हैं। बच्चों की कामना में गुलाबी रंग का धागा बाँधा जाता है। क्या निराला जी 'या तुम बाँधकर रँगा धागा' के अर्थ में उस तरह की प्रथा का संकेत नहीं दे रहे हैं। यह प्रथा काशी में गणेश मंदिर में भी मैंने देखी है।'
त्रिलोचन बोले, 'हाँ यह प्रथा हिन्दी क्षेत्र में भी है। यह अर्थ आपने (वि. चं. शर्मा) नया जोड़ा है।'
मैंने पूछा, 'मेरे आलोचक एक बीज' का क्या अर्थ है? बीज तो फूल से पैदा होता है। पत्ता एक बीज को अपना आलोचक कैसे कहेगा?
त्रिलोचन ने कहा, 'बीज रज और वीर्य योग से बनता है। स्त्री मात्र के रज से बच्चे का रूप कभी बनता है? कभी पुरुष के वीर्य से बच्चे पर पिता का रंग-रूप झलकता है? यह पूरी प्रक्रिया तो भावुक नहीं, वैज्ञानिक विचार की प्रक्रिया है, जिसके लिए 'आलोचक' का प्रयोग बड़ा सार्थक है।'
- पुस्तक : ओर-14 (पृष्ठ 505)
- रचनाकार : त्रिलोचन
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.