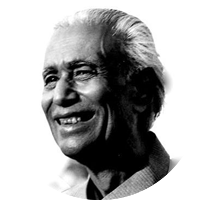‘ठेले पर हिमालय'—खासा दिलचस्प शीर्षक है न! और यकीन कीजिए, इसे बिलकुल ढूँढना नहीं पड़ा। बैठे-बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था कि ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे, चिकने चमकते बर्फ़ में भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्मस्थान अल्मोड़ा है, वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए-खोए से ही बोले, “यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है।” और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ‘ठेले पर हिमालय।’ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई, इसे ले जाएँ ओर इस शीर्षक पर दो-तीन सौ पक्तियाँ बेडोल, बेतुकी लिख डालें—शीर्षक मौज़ू है, और अगर नई कविता से नाराज़ हों, सुललित गीतकार हों तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ़ को डाँटें, “उतर आओ। के शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो? ओ नए कवियो! ठेले पर लदो। पान की दुकानों पर बिको।
ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्रों को बताई भी। वे हँसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है ओर ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर-रेखा को चाँद-तारों से बात करते देखा है, चाँदनी में उजली बर्फ़ को धुंध के हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते मौर जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ, क्यों कि वह बर्फ़ मैने भी देखी हैं।
सच तो यह है कि सिर्फ़ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती हैं, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप हैं वह रास्ता। पानी का कही नाम-निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े-मेढे खेत जो थोड़े से हो तो शायद अच्छे भी लगें पर उनका एकरस सिलसिला बिलकुल शैतान की आँत मालूम पहता है। फिर मझकाली के टेढ़े-मेढे रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर जिसने बस के तमाम मुसाफ़िरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी मुसाफ़िरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौसानी जाने वाले सिर्फ़ हम दो थे, वही उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबियत सुस्त थी और मौसम में उमम थी। दो घंटे बाद दूसरी लारी आ कर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदन शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्हीं ने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था, और ख़ुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते हो हमारी भी सारी थकान काफ़ूर हो जाया करती थी।
पर शुक्ल जी के साथ यह नई मूर्ति कौन है? लंबा-दुबला शरीर, पतला साँवला चेहरा, एमिल जोला-सी दाढी, ढीला-ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जरकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाकुलर। और खासी अटपटी चाल थी बाबू साहब की। यह पतला-दुबला मुझ जैसा ही सींकिया शरीर उस पर आपका झूमते हुए आना... मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने महा “हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है सेन, अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है। उसी रुपए से घूमकर छुट्टियाँ बिता रहे है।” थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सेन घुल-मिल गया, कितना मीठा था हृदय से वह! वैसे उसके करतब आगे चलकर देखने में आए।
कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कल-कल करती हुई कोसी, किनारे के छोटे-छोटे सुंदर गाँव और हरे मलमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी। हरी-भरी। एक के बाद एक बस-स्टेशन पड़ते थे, छोटे-छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी-कभी कोसी या उनमें गिरने वाले नदी-नालों पर बने हुए पुल। कहीं-कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलो से गुज़रती थी। टेढ़ी-मेड़ी, ऊपर-नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर-सी सड़क पर धीरे-धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन हम को और भी तंद्रालस बना रहा था। पर ज्यों-ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, त्यों–त्यों हमारे मन में एक अजीब-सी निराशा छाती जा रही थी; अब तो हम लोग कौसानी के नज़दीक है, कोसी से 18 मील चले आए, कौसानी सिर्फ़ छह मील हैं; पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कौसानी के बारे में सुना जाता था। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि काश्मीर के मुक़ाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा है, गांधी जी ने यहीं अनासक्ति योग लिखा था और कहा था कि स्विटजरलैंड का आभास कौसानी में ही होता है। ये नदी, घाटी, खेत, गाँव, सुंदर है किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं ही है। हम कभी-कभी अपना संशय शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगे ओर ज्यों-ज्यों कौसानी नज़दीक आती गई त्यों-त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में तो क्षोभ हमारे चेहरे पर झलक आया। शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी हमारी इन भावनाओं पर, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिलकुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड लिया और ढाल पर चढ़ने लगी।
सोमेशवर की घाटी के उत्तर में जो ऊँची पर्वतमाला है, उसी पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बना हुआ है। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा-सा, बिल्कुल उजाड़ सा गाँव और बर्फ़ का तो कहीं नाम-निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अनखाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर कि मूर्ति-सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना आपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर के रंग-बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। पचासों मील चौड़ी यह घाटी, हरे मख़मली क़ालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएँ काटकर बने हुए लाल-लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद-सफ़ेद पथरों कि कतार और इधर-उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियाँ-सी नदियाँ। मन में बेसाख़्ता यही आया कि इन बैलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ। आँखों से लगा लूँ। अकस्मात् हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर, पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे-धीरे मेरी निगाहों ने घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन, क्षितिज के धुँधलेपन में, नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया, उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात्ए क हल्का से विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे-धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन चीज़ है जो अटल है। यह छोटा-सा बादल के टुकड़े-सा और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद, ना रूपहला, ना हल्का नीला... पर तीनों का आभास देता हुआ। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है। हाँ जी! बर्फ़ नहीं है तो क्या है? और अकस्मात् बिजली का सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी कल्युर घाटी के पार वह नगाधिराज, पर्वत-सम्राट हिमालय है, इन बादलों ने उसे ढाँक रखा है वैसे यह क्या सामने है; उसका एक छोटा-सा बाल-स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झाँक रहा है। मैं हर्षतिरेक से चीख़ उठा, ”बर्फ़! वह देखो! शुक्ल जी, सेन जी सभी ने देखा पर अकस्मात् वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल-शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झाँक रहा है, कहीं गिर ना पड़े।
पर उस एक क्षण के हिम-दर्शन ने जाने हम में क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराश, थकावट—सब छू-मंत्र हो गई। निराधार गई। इस सब आकुल हो उठें। अभी ये बादल छँट जाएँगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा—निरावृत, असीम सौंदर्य हमारे सामने अभी-अभी अपना घूँघट धीरे से खिसका देगी और... और तब? और तब? सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी-कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था, इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुँह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक-बँगले के खानसामे ने बताया कि, “आप लोग बड़े ख़ुशकिस्मत है साहब! 14 टूरिस्ट आकर हफ़्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं।”
सामान रख दिया गया। पर मैं, मेरी पत्नी, सेन, शुक्ल जी सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे, और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे-धीरे नीचे उतर रहे थे और एक-एक कर नए–नए शिखरों को हिम-रेखाएँ अनावृत हो रही थी। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धँसती जाती हुई हिम-शिखरों की ऊबड़-खाबड़, रहस्यमय, रोमांचक शृंखला। हमारे मन में उम समय क्या भावनाएँ उठ रही यह अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ़ एक धुंधला सा संवेदन अवश्य था कि जैसे बर्फ़ की सिल के सामने खड़े होने पर मुँह पर ठंडी-ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था। ...और अकस्मात् एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी-कितनी पुरानी है यह हिमराशि। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए हिमालय की इस बर्फ़ को कहा है—चिरंतन हिम (एटर्नल स्नो) सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रें, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंतकाल से इन सूने बर्फ़ ढँके दर्रों में सिर्फ़ बर्फ़ के अंधड़ हू-हूँ करते हुए बहते रहे हैं।
सूरज डूबने लगा और धीरे-धीरे ग्लेशियरों में पिघली बहने लगी। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी, घाटियाँ गहरी पीली हो गई। अँधेरा होने लगा तो हम उठे और मुँह-हाथ धोने और चाय पीने में लगे। पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हों। थोड़ी देर में चाँद निकला और हम फिर बाहर निकले... इस बार सब शांत था। जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आरामकुर्सी खींचकर बैठ गया। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने-किसने क्या-क्या नहीं लिखा और यह मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, एक शब्द भी तो नहीं जानता। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिमसम्राट के समक्ष पर धीरे-धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छँट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है जो इसी ऊँचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा, यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे-छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ, कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है—“हिम्मत है? ऊँचे उठोगे?”
और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रवींद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई। और हम सक्रिय हो उठे अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक ख़ुश था सेन, बच्चों की तरह चंचल, चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, “भाई साहब, हम तो बंडरस्ट्रक हैं कि यह भगवान का क्या-क्या करतूत इस हिमालय में होता है।“ इस पर हमारी हँसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, ‘हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा।’ बाद में मालूम हुआ कि वह बंबई की अत्याधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज़ है और कहने लगा, “ओ सब जीनियस लोग शीर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है। इसी से हम भी शीर का बल हिमालय देखता है।“
दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुंचे जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जलराशि में हिमालय की बर्फ़ीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं, उन शिखरों पर कब पहुँचूँ, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंटा, उसमें डूबा रहा।
आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ़ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए उस दर्द को समझता का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊँचाईयाँ बार-बार बुलाती हैं। ...और हम हैं कि चौराहों पर खड़े, ऐसे ही ठेलों पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में, ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था “...कबहुँक हौं यहि रहनि रहौंगो... में क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिमशिखरों की ऊँचाइयों पर?” और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेज दूँ.‘ नहीं बंधु, आऊँगा। मैं फिर लौट-लौट कर वही आऊँगा। उन्ही ऊँचाइयों पर तो मेरा आवास है। वहीं मन रमता है... मैं करूँ तो क्या करूँ?
- पुस्तक : ठेले पर हिमालय (पृष्ठ 3-9)
- रचनाकार : धर्मवीर भारती
- प्रकाशन : भारती प्रेस प्रकाशन, इलाहाबाद
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.