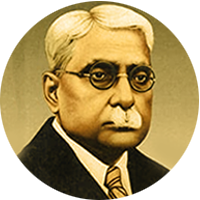भाव या मनोविकार
bhaw ya manowikar
अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे-से हृदय में पहले सुख और दुःख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिह्न हँसना और रोना देखे जाते हैं पर ये अनुभूतियाँ बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं, विशेष-विशेष विषयों की ओर विशेष-विशेष रूपों में ज्ञानपूर्वक उन्मुख नहीं होती।
नाना विषयों के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेकरूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न-भिन्न योग संघटित होते हैं जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। अतः हम कह सकते है कि सुख और दुःख की मूल अनुभूति ही विषय-भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकार का जटिल रूप धारण करती है। जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुःख होगा; पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुःख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे क्रोध कहते हैं। जिस बच्चे को पहले अपने ही दुःख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्यक्रम अनुमान-द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुःख होने लगता है जिसे दया या करुणा कहते हैं। इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से कष्ट पहुँचाने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुःख होता है वह भय कहलाता है। बहुत छोटे बच्चे को, जिसे यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाए तो भी वह विचलित न होगा, क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुःख होगा।
मनोविकारों या मानों की अनुभूतियाँ परस्पर तथा सुख या दुःख की मूल अनुभूति से ऐसी भिन्न होती हैं जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय-बोध की विभिन्नता तथा उसने संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनेकरुपता का विकास होता है। हानि या दुःख के कारण में हानि या दुःख मनाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुःख कहते हैं, बल्कि उसके योग से संघटित क्रोध नामक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। जब हमारी इंद्रियाँ दूर से आती हुई कोशकारिणी बातों का पता देने लगती हैं, हमारा अंतःकरण हमें भावी आपदा निश्चय कराने लगता है; तब हमारा काम दुःख मात्र ने नहीं चल सकता बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भाप से चल सकता है। इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम के वशीभूत होता है।
अपने मुल रूपों में सुख और दुःख दोनों की अनुभूतियाँ कुछ बँधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती है। उनकी भावना इच्छा और प्रयत्न अनेकरूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर बहुत करेंगे—दाँत निकालकर हँसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुँचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे, इसी प्रकार शुद्ध दुःख में हम बहुत करेंगे हाथ-पैर पटकेंगे, रोएँगे या दुःख पहुँचाने वाली वस्तु से हटेंगे पर हम चाहे कितना ही उछल-कूदकर हँसें, कितना ही हाथ-पैर पटककर रोएँ, इस हँसने या रोने को प्रयत्न नहीं कह सकते। ये सुख और दुःख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती।
शरीर-धर्म मात्र के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और पूर्ण व्यंजना हो सकती है। उदाहरण के लिए कंप को लीजिए। कंप शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। अतः जब तक भागना, छिपना या मारना, झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णतया व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने ले लिया है। मुँह से निकले हुए वचन ही अधिकतर भिन्न-भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यंजना किया करते हैं। इसी से साहित्य-मीमांसकों ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है।
क्रोधी चाहे किसी ओर झपटे या न झपटे, उसका यह कहना ही कि 'मैं उसे पीस डालूँगा' क्रोध की व्यंजना के लिए काफ़ी होता है। इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना है कि 'कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती' उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रणक्षेत्र में उछलने-कूदने के वर्णन में नहीं। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं। पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं। उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेकरूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है उतना अनुभाव कहलाने वाले व्यापारों-द्वारा नहीं। क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना-फोड़ना मारना-पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती है। किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के संबंध में समझिए।
समस्त मानव-जीवन के प्रवर्त्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक-रक्षा और लोक-रंजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म-शासन, राज-शासन, मत-शासन-सबमें इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक-कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी।
सब प्रकार के शासन में—चाहे धर्म-शासन हो, चाहे राज-शासन, या संप्रदाय-शासन-मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज-शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ-दिखाते हुए धर्म-शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। इनके द्वारा नय लोभ का प्रवर्त्तक उचित सीमा के बाहर भी प्रायः हुआ है और होता रहता है। जिस प्रकार शासकवर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ-सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं उसी प्रकार धर्म-प्रवर्त्तक और आचार्य आपके स्वरूप-वैचित्र्य की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। शासकवर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हैं। मत-प्रवर्त्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कँपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति को मूर्ति-पूजा करते देख दूसरी जाति के मत-प्रवर्त्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शन तक में पाप लगाया है। भावक्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए।
शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखने वाली शक्ति कविता है जो धर्मक्षेत्र में शक्ति-भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस मंगल के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख-सौंदर्य के साथ हो जाएगा, उसकी रक्षा का भाव तृण-गुल्म, वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, सब की रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत् का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुँचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी बराबर पुकारती आ रही है—
विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ
खेलत फ़िरत तिन्हें खेलन फ़िरन देव।
—ठाकुर
- पुस्तक : निबंधमाला (पृष्ठ 1)
- संपादक : लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय
- रचनाकार : आचार्य रामचंद्र शुक्ल
- प्रकाशन : लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.