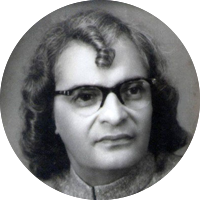मेरे कवि-जीवन के विकास-क्रम को समझने के लिए पहले आप मेरे साथ हिमालय की प्यारी तलहटी में चलिए। आपने अल्मोड़े का नाम सुना होगा। वहाँ से बत्तीस मील और उत्तर की ओर चलने पर आप मेरी जन्म भूमि कौसानी मे पहुँच गए। वह जैसे प्रकृति का रम्य शृंगार गृह है, जहाँ कूर्मांचल की पर्वत श्री एकांत में बैठकर अपना पल-पल-परिवर्तित वेश सँवारती है। आज से चालीस साल पहले की बात कहता हूँ, तब मैं छोटा-सा चंचल भावुक किशोर था। मेरा काव्य कंठ अभी तक फूटा नहीं था, पर प्रकृति मुझे मातृहीन बालक को कवि-जीवन के लिए मेरे बिना जाने ही जैसे तैयार करने लगी थी। मेरे हृदय में वह अपनी मीठी, स्वप्नों से भरी हुई, चुप्पी चकित कर चुकी थी, जो पीछे मेरे भीतर अस्फुट तुतले स्वरों में बज उठी। पहाड़ी पेड़ों का क्षितिज न जान कितने गहरे-हल्के रंगो के फूलों और कोपलों में मर्मर ध्वनि कर मेरे भीतर अपनी सुंदरता की रंगीन सुगंधित तहे जमा चुका था। ‘मधुबाला की मृदु-बोली-सी’ अपनी उस हृदय की गुंजार को मैंने अपने ‘वीणा’ नामक संग्रह में यह तो तुतली बोली में है एक बालिका का उपहार!’ कहा है। पर्वत-प्रदेश के निर्मल चंचल सौंदर्य ने मेरे जीवन के चारों ओर अपने नीरव सौंदर्य का जाल बुनना शुरू कर दिया। मेरे मन के भीतर बरफ़ की ऊँची चमकीली चोटियाँ रहस्य-भरे शिखरों की तरह उठने लगी थी, जिन पर खड़ा हुआ नीला आकाश रेशमी चँदोवे की तरह आँखों के सामने फहराया करता था। कितने ही इंद्रधनुष मेरे कल्पना के पट पर रंगीन रेखाएँ खींच चुके थें, बिजलियाँ बचपन की आँखों को चकाचौंध कर चुकी थी, फेनी के झरने मेरे मन को फुसलाकर अपने साथ गाने के लिए बहा ले जाते और सर्वोपरि हिमालय का आकाशचुंबी सौंदर्य मेरे हृदय पर एक महान् संदेश की तरह, एक स्वर्गोन्मुखी आदर्श की तरह तथा एक विराट् व्यापक आनंद, सौंदर्य तथा तप पूत पवित्रता की तरह प्रतिष्ठित हो चुका था। मैं छुटपन से ही जनभीरु और शर्मीला था। उधर हिम-प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता मुझ पर अपना जादू चला चुकी थी, इधर घर में मुझे ‘मेघदूत’, ‘शकुंतला’ और ‘सरस्वती’ मासिक पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं का मधुर पाठ सुनने को मिलता था, जो मेरे मन में भरे हुए अवाक् सौंदर्य को जैसे वाणी की झंकारों में झनझना उठने के लिए अज्ञात रूप से प्रेरणा देता था। मेरे बड़े भाई साहित्य और काव्य के अनुरागी थे। वे खड़ीबोली में, और पहाड़ी में भी, प्रायः कविता लिखते थे। मेरे मन में तभी से लिखने की ओर आकर्षण पैदा हो गया था, और मेरे प्रारंभिक प्रयास भी शुरू हो गए थे, जिन्हें मुझे किसी को दिखाने का साहस नहीं होता था। तब में दस-ग्यारह साल का रहा हूँगा। उसके बाद मैं अल्मोड़ा हाईस्कूल में पढ़ने चला गया। अल्मोड़ा में उन दिनों जैसे हिंदी की बाढ़ आ गई थी, एक पुस्तकालय की भी स्थापना वहाँ हो चुकी थी और अन्य नवयुवकों के साथ मैं भी उस बाढ़ में बह गया। पंद्रह-सोलह साल की उम्र में मैंने एक प्रकार से नियमित रूप से लिखना आरंभ कर दिया था। मैं तब आठवी कक्षा में था। हिंदी साहित्य में तब जो कुछ भी सुलभ था, उसे मैं बड़े चाव से पढ़ता था। मध्ययुग के काव्य-साहित्य का भी थोड़ा बहुत अध्ययन कर चुका था। श्री मैथिलीशरण गुप्त की ‘भारत-भारती’, ‘जयद्रथ वध’ ‘रंग में भंग’ आदि रचनाओं से प्रभावित होकर मैं हिंदी के प्रचलित छंदों की साधना में तल्लीन रहता था। उस समय के मेरे चपल प्रयास कुछ हस्तलिखित पत्रों में, ‘अल्मोड़ा अख़बार नामक साप्ताहिक में तथा मासिक पत्रिका ‘मर्यादा’ में प्रकाशित हुए थे। इन वर्षों की रचनाओं को मैं प्रयोगकाल की रचनाएँ कहूँगा।
सन् 1918 से 20 तक की अधिकांश रचनाएँ मेरे ‘वीणा’ नामक काव्य संग्रह में छपी है। ‘वीणा’ काल में मैंने प्रकृति की छोटी-मोटी वस्तुओं को अपनी कल्पना की तूली से रँगकर काव्य की सामग्री इकट्ठा की है, फूल-पत्ते और चिड़ियाँ, बादल-इंद्र-धनुष ओस-तारे, नदी-झरने, उषा-संध्या, कलरव, मर्मर और टलमल जैसे गुड़ियों और खिलौनों की तरह नेरी बाल कल्पना की पिटारी को सँजोए हुए है।
‘छोड़ द्रुमों की मृदु छाया,
तोड़ प्रकृति से भी माया,
बाले, तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूँ लोचन?’
––इत्यादि सरल भावनाओं को बिखेरती हुई मेरी काव्य-कल्पना जैसे अपनी समवयस्का बालप्रकृति के गले में बाँहें डाले प्राकृतिक सौंदर्य के छायापथ में विहार कर रही है :
“उस फैली हरियाली में
कौन अकेली खेल रही माँ,
सजा हृदय की थाली में,
क्रीड़ा कौतूहल कोमलता
मोद मधुरिमा हास-विलास
लीला विस्मय अस्फुटता भय
स्नेह पुलक मुख सरल हुलास!”
इन पंक्तियों में चित्रित प्रकृति का रूप ही तब मेरे हृदय को लुभाता रहा है। उस समय का मेरा सौंदर्य-ज्ञान उस ओसों के हँसमुख वन-सा था, जिस पर स्वच्छ निर्मल स्वप्नों से भरी चाँदनी चुपचाप सोई हुई हो। उस शीतल वन में जैसे अभी प्रभात की सुनहली ज्वाला नहीं प्रवेश कर पाई थी। स्निग्ध सुंदर मधुर प्रकृति की गोद माँ की तरह मेरे किशोर जीवन का पालन-परिचालन करती थी। ‘वीणा’ के कई प्रगीत माँ को संबोधन करके लिखे गए हैं :
“माँ, मेरे जीवन की हार
तेरा उज्वल हृदय हार हो अश्रुकणों का यह उपहार”
—आदि रचनाओं में प्रकृति प्रेम के अलावा मेरे भीतर एक उज्ज्वल आदर्श की भावना भी जाग्रत हो चुकी थी। ‘वीणा’ के कई प्रगीतों में मैंने अपने मन के इन्हीं उच्छवासों एवं उद्गारों को भरकर स्वर-साधना की है।
मेरा अध्ययन-प्रेम धीरे-धीरे बढ़ने लगा था। श्रीमती नायडू और कवि ठाकुर की अँग्रेज़ी रचनाओं में मुझे अपने हृदय में छिपे सौंदर्य और रुचि की अधिक मार्जित प्रतिध्वनि मिलती थी। यह सन् 1919 की बात है, मैं तब बनारस में था। मैंने रवींद्र साहित्य बँगला में भी पढ़ना शुरू कर दिया था। ‘रघुवंश’ के कुछ सर्ग भी देख चुका था। ‘रघुवंश’ के उस विशाल स्फटिक प्रासाद के झरोखों और लोचन-कुवलयित गवाक्षों से मुझे रघु के वंशजों के वर्णन के रूप में कालिदास की उदात्त कल्पना की सुंदर झाँकी मिलने लगी थी। मैं तब भावना के सूत्र में शब्दों की गुरियों को अधिक कुशलता से पिरोना सीख रहा था। इन्हीं दिनों मैंने ‘ग्रंथि’ नामक वियोगांत खंड-काव्य लिखा था। ‘ग्रंथि’ के कथानक को दुखांत बनाने की प्रेरणा देकर जैसे विधाता ने उस युवावस्था के आरंभ में ही मेरे जीवन के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी।
‘वीणा’ में प्रकाशित ‘प्रथम रश्मि का आना रगिणि’ नामक कविता ने काव्य-साधना की दृष्टि से नवीन प्रभात की किरण की तरह प्रवेशकर मेरे भीतर ‘पल्लव’ काल के काव्य-जीवन का समारंभ कर दिया था। 1916 की जुलाई में मैं कालेज पढ़ने के लिए प्रयाग आया, तब से करीब दस साल तक प्रयाग ही में रहा। यहाँ मेरा काव्य संबंधी ज्ञान धीरे-धीरे व्यापक होने लगा। शेली, कीट्स, टेनिसन आदि अँग्रेज़ी कवियों से मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे मन में शब्द चयन और ध्वनि-सौंदर्य का बोध पैदा हुआ। ‘पल्लव’ काल की प्रमुख रचनाओं का प्रारंभ इसके बाद ही होता है। प्रकृति-सौंदर्य और प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना ‘पल्लव’ में अधिक प्रांजल एवं परिपक्व रूप में हुई है। ‘वीणा’ की रहस्य-प्रिय बालिका अधिक मासल, सुरुचि, सुरंगपूर्ण बनकर प्रायः मुग्धा युवती का हृदय पाकर जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बन गई है; ‘सोने का गान’, ‘निर्झर गान’, ‘मधुकरी’, ‘निर्झरी’, ‘विश्व-वेणु’, ‘वीचि-विलास’ आदि रचनाओं में वह प्रकृति के रंगजगत् में अभिनय करती-सी दिखाई देती है। अब उसे तुहिन-वन में छिपी स्वर्ण-ज्वाल का आभास मिलने लगा है, उषा की मुसकान कनक-मंदिर लगने लगी है। वह अब इस रहस्य को नहीं छिपाना चाहती कि उसके हृदय में कोमल बाण लग गया है। निर्झरी का अचल अब आँसुओं से गोला जान पड़ना है, उनकी कल-कल ध्वनि उसे मूक व्यथा का मुखर भुलाव प्रतीत होती है। वह मधुकरी साथ फूलों के कटोरों से मधुपान करने को व्याकुल है। सरोवर की चंचल लहरी उनमें आँखमिचौनी खेलकर उसके व्याकुल हृदय को दिव्य प्रेरणा से आश्वासन देने लगी है। वह उससे कहता है :
“मुग्धा की-सी मृदु मुसकान,
खिलते ही लज्जा से म्लान,
स्वर्गिक सुख की-सी आभास
अतिशयता में अचिर, ––महान
दिव्य भूति-सी आ तुम पास
कर जाती हो क्षणिक विलास
आकुल उर को दे आश्वास!”
सन् 1921 के असहयोग आंदोलन में मैंने कालेज छोड़ दिया। इन दो-एक वर्षों के साहित्यिक प्रवास में ही मेरे मन ने किसी तरह जान लिया था कि मेरे जीवन का विधाता ने कविता के साथ ही ग्रंथि-बंधन जोड़ना निश्चय किया है। ‘वीणा’ में मैंने ठीक ही कहा था :
‘प्रेयसि कविते, हे निरुपमिते,
अधरामृत से इन निर्जीवित शब्दों में जीवन लाओ!”
बड़ी-बड़ी अट्टालिकाओं और प्रासादों से लेकर छोटी-छोटी झाड़-फूस की कुटियों से जनाकीर्ण इस जगत् में मुझे रहने के लिए मन का एकांत छायावन मिला, जिसमें वास्तविक विश्व की हलचल चित्रपट की तरह दृश्य बदलती हुई मेरे जीवन को अज्ञात आवेगों से झकझोरती रही है। इसके बाद का मेरा जीवन अध्ययन-मनन और चिंतन ही में अधिक व्यतीत हुआ। 1921 में मैंने ‘उच्छवास’ नामक प्रेम-काव्य लिखा, और उसके बाद ही ‘आँसू’। मेरे तरुण-हृदय का पहला ही आवेश प्रेम का प्रथम स्पर्श पाकर जैसे उच्छ्वास और आँसू बनकर उड़ गया। उच्छवास के सहस्र दृग-सुमन खोले हुए पर्वत की तरह मेरा भविष्य जीवन भी जैसे स्वप्नों और भावनाओं के घने कुहासे से ढँककर अपने ही भीतर छिप गया :
“उड़ गया अचानक, लो, भूधर
फड़का अपार वारिद के पर
रव शेष रह गए है निर्झर,
लो, टूट पड़ा भू पर अंबर!
धँस गए धरा में सभय शाल
उठ रहा धुआँ जल गया ताल,
यो जलद यान मे विचिर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल!”
इसी भूधर की तरह वास्तविकता की ऊँची-ऊँची प्राचीरों से घिरा हुआ यह सामाजिक जगत्, जो मेरे यौवन-सुलभ आशा-आकांक्षाओं से भरे हुए हृदय को, अनंत विचारों, मतांतरों, रूढ़ियों, रीतियों की भूल-भुलैया-सा लगता था, जैसे मेरे आँखों के सामने से ओझल हो गया। यौवन के आवेशों से उठ रहे वाष्पों के ऊपर मेरे हृदय में जैसे एक नवीन अंतरिक्ष उदय होने लगा।
‘पल्लव’ की छोटी-बड़ी अनेक रचनाओं में जीवन के और युग के कई स्तरों को छूती हुई, भावनाओं की सीढ़ियाँ चढ़ती हुई, तथा प्राकृतिक सौंदर्य की झाँकियाँ दिखाती हुई मेरी कल्पना ‘परिवर्तन’ शीर्षक कविता में मेरे उस काल के हृदय-मंथन और बौद्धिक संघर्ष की विशाल दर्पण-सी है, जिसमें ‘पल्लव’ युग का मेरा मानसिक विकास एवं जीवन की संग्रहणीय अनुभूतियाँ तथा राग-विराग का समन्वय बिजलियों से भरे बादल की तरह प्रतिबिंबित है। इस अनित्य जगत् मे नित्य जगत् को खोजने का प्रयत्न मेरे जीवन में जैसे ‘परिवर्तन’ के रचना-काल से ही प्रारंभ हो गया था, ‘परिवर्तन’ उस अनुसंधान का केवल प्रतीक मात्र है। हृदयमंथन का दूसरा रूप आप आगे चलकर ‘गुंजन’ और ‘ज्योत्स्ना’ काल की रचनाओं में पाएँगे।
मैं प्रारंभ मे आपको 40 साल पीछे ले गया हूँ और प्राकृतिक सौंदर्य को, जुगनुओं से जगमगाती हुई, घाटी में घुमाकर धीरे-धीरे कर्म-कोलाहल से भरे संसार की घोर ले आया हूँ। ‘परिवर्तन’ की अंतिम कुछ पंक्तियों में जैसे इन चालीस वर्षों का इतिहास आ गया है :
“अहे महाम्बुधि, लहरों-से शत लोक चराचर
क्रीडा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर।
तुंग तरंगों-से शत युग, शत-शत कल्पांतर
उगल, महोदर में विलीन करते तुम सत्वर!”
मेरा जन्म सन् 1600 में हुआ है, और 1947 तक मैं जैसे इस संक्रमणशील युग के प्रायः अर्द्ध-शताब्दी के उत्थान-पतनों को देख चुका हूँ। अपना देश इन वर्षों में स्वतंत्रता के अदम्य संग्राम से आंदोलित रहा। उसके मनोजगत् को हिलाती हुई नवीन जागरण की उद्दाम आँधी––जैसे
“द्रुत झरो जगत् के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण,
हिमताप पीत मधुवात भीत तुम वीतराग जड़ पुराचीन!”
—का संदेश बिखेरती रही है। दुनिया इन वर्षों में दो महायुद्ध देख चुकी है :
“बहा नर शोणित मूसल धार
रुडमुडों की कर बौछार,
छेड़ खर शस्त्रों की झंकार
महाभारत गाता संसार!––”
‘परिवर्तन’ की इन पंक्तियों में जैसे इन्हीं वर्षों के इतिहास का दिग्घोष भरा हुआ है। मनुष्य जाति की चेतना इन वर्षों में कितने ही परिवर्तनों और हाहाकारों से होकर विकसित हो गई है। कितनी ही प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ धरती के जीर्ण-जर्जर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, बिलों में छेड़े हुए साँपों की तरह, फन उठाकर फूत्कार करती रही है।
यह सब इस युग में क्यों हुआ? मानव जाति प्रलय-वेग से किस ओर जा रही है? मानव सभ्यता का क्या होगा? इस भिन्न-भिन्न जातियों, वर्गों, देशों, राष्ट्रों के स्वार्थों में खोए हुए धरती के जीवन का भावी निर्माण किस दिशा को होना चाहिए?––इन प्रश्नों और शंकाओं का समाधान मैंने ‘ज्योत्स्ना’ नामक नाटिका द्वारा करने का प्रयत्न किया। ‘ज्योत्स्ना’ में वेदव्रत कहना है “जिस प्रकार पूर्व की सभ्यता अपने एकांगी आत्मवाद और अध्यात्मवाद के दुष्परिणामों से नष्ट हुई, उसी प्रकार पश्चिम की सभ्यता भी अपने एकांगी प्रकृतिवाद, विकासवाद और भूतवाद के दुष्परिणाम से विनाश के दलदल में डूब गई। पश्चिम के जड़वाद की मासल प्रतिमा में पूर्व के अध्यात्म-प्रकाश की आत्मा भरकर एवं अध्यात्मवाद के अस्थिपंजर में भूत या जड़-विज्ञान के रूप-रंगों को भरकर हमने आनेवाले युग की मूर्ति का निर्माण किया है।”
‘ज्योत्स्ना’ में मैंने जिस सत्य को सार्वभौमिक दृष्टिकोण से दिखाने का प्रयत्न किया है, ‘गुंजन’ में उसी को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कहा है। ‘गुंजन’ के प्रगीत मेरी व्यक्तिगत साधना से सम्बद्ध है। ‘गुंजन’ की ‘अप्सरी’ में ‘ज्योत्स्ना’ की ही भावना-धारा को व्यक्तित्व दिया गया है। कला की दृष्टि से ‘गुंजन’ की शैली ‘पल्लव’ की तरह मासल एवं ऐंद्रिय रूप-रंगों से भरी हुई नहीं है, उसकी व्यंजना अधिक सूक्ष्म, मधुर तथा भावप्रवण है। उसमें ‘पल्लव’ का-सा कल्पना वैचित्र्य नहीं है, पर भावों की सच्चाई और चिंतन की गहराई है।
‘गुंजन’ काल के इन अनेक वर्षों के ऊहापोह, संघर्ष और संधि-पराभव के बाद आप मुझे ‘युगांत’ के कवि के रूप में देखते है। ‘युगांत’ के मरु में मेरे मानसिक निष्कर्षों के धुंधले पद-चिह्न पड़े हुए हैं। वही चिंतन के भार से डगमगाता हुए पैर जैसे ‘पाँच कहानियों’ की पगडंडियो में भी भटक गए है।
‘युगांत’ में मैं निश्चय रूप से इस परिणाम पर पहुँच गया था कि मानव सभ्यता का पिछला युग अब समाप्त होने को है और नवीन युग का प्रादुर्भाव अवश्यंभावी है। मैंने जिन प्रेरणाओं से प्रभावित होकर यह कहा था, उनका आभास ‘ज्योत्स्ना’ में पहले ही दे चुका हूँ। अपने मानसिक चिंतन और बौद्धिक परिणामों के आधारों का समन्वय मैंने ‘युगवाणी’ के ‘युगदर्शन’ में किया है। ‘युगदर्शन’ में मैंने भौतिकवाद या मार्क्सवाद के सिद्धांतों का जहाँ समर्थन किया है, वहाँ उनका अध्यात्मवाद के साथ समन्वय एवं संश्लेषण भी करने का प्रयत्न किया है; ‘भौतिकवाद के प्रति रचना में, मानव-जीवन की बहिर्गतियों का वैज्ञानिक निरूपण कर मैंने अपने वयोवृद्ध विचारकों में जीवन तथा जगत् के प्रति जो विरक्ति अथवा उपेक्षा पाई जाती है उसे दूर करने का प्रयत्न किया है तथा अध्यात्म-दर्शन के बारे में जो नवशिक्षित युवकों में भ्रांत धारणाएँ फैली है, उस पर भी प्रकाश डाला है। मैंने ‘युगवाणी’ और ‘ग्राम्या’ में मध्ययुग की संकीर्ण नैतिकता का घोर खंडन किया है। ‘ग्राम्या’ को समाप्त करने के बाद आप सन् 1940 में पहुँच गए हैं। इस बीच में हिंदी साहित्य की सृजनशीलता हिंदुस्तानी के स्वादहीन आंदोलन से तथा उसके बाद 1942 के आंदोलन से काफ़ी प्रभावित रही। दोनों आंदोलन से हिंदी की सृजनशील चेतना को अपने-अपने ढंग का धक्का पहुँचा, और दोनों ने ही उसे पर्याप्त मात्रा में चिंतन-मनन के लिए सामग्री भी दी। फिर भी इन वर्षों के साहित्यिक इतिहास के मुख पर एक भारी वितृष्णा-भरे विषाद का घूँघट पड़ा रहा। इसके उपरांत सन् 1926 की तरह मैं अपने मानसिक संघर्ष के कारण प्राय: दो साल तक अस्वस्थ रहा। इधर मेरी नवीन रचनाओं के दो संग्रह ‘स्वर्ण-किरण’ और ‘स्वर्ण-धूलि’ के नामों से प्रकाशित हुए है। ‘स्वर्ण-किरण’ में स्वर्ण का प्रयोग मैंने नवीन चेतना के प्रतीक के रूप में किया है। उसमें मुख्यतः चेतना प्रधान कविताएँ है। ‘स्वर्ण-धूलि’ का धरातल अधिकतर सामाजिक है, जैसे वही नवीन चेतना धरती की धूलि में मिलकर एक नवीन सामाजिक जीवन के रूप में अंकुरित हो उठी हो।
‘स्वर्ण-किरण’ में मैंने, पिछले युगों में जिस प्रकार सांस्कृतिक शक्तियों का विभाजन हुआ है, उनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है। उसमें पाठकों को विश्व-जीवन एवं धरती की चेतना संबंधी समस्याओं का दिग्दर्शन मिलेगा। भिन्न-भिन्न देशों एवं युगों की संस्कृतियों को विकसित मानववाद में बाँधकर मैंने भू-जीवन की नवीन रचना की और संलग्न होने का आग्रह किया है। ‘स्वर्ण-किरण’ में ‘स्वर्णोदय’ शीर्षक रचना इस दृष्टि से अपना विशेष महत्त्व रखती है। उसके कुछ पद उद्धृत कर इस वार्ता को समाप्त करता हूँ :
“भू रचना का भूतिपाद युग हुआ विश्व इतिहास में उदित
सहिष्णुता सद्भाव शांति से हो गत संस्कृति धर्म समन्वित!
वृथा पूर्व पश्चिम का दिग्भ्रम मानवता को करे न खंडित
बहिर्नयन विज्ञान हो महत् अंतर्दृष्टि ज्ञान से योजित।
एक निखिल धरणी का जीवन, एक मनुजता का संघर्षण,
विपुल ज्ञान संग्रह भव-पथ का विश्व क्षेम का करे उन्नयन!”
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 139)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.