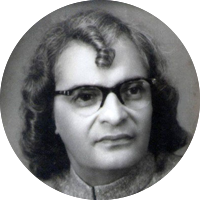“मानसी” मैंने सन् 1946 में लिखी थी। तब दक्षिण भारत में था। मानसी मनुष्य की राग भावना अथवा राग चेतना का प्रतीक रूपक है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि आज के संक्रांति युग में जबकि हम अपनी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मान्यताओं में नवीन संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मनुष्य की पिछड़ी हुई आदिम राग भावना को भी निरखने-परखने की आवश्यकता है तथा उसमें मानव की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही नवीन संतुलन एवं रूपांतर लाने की अपेक्षा है। इस वैज्ञानिक युग में एक विकसित भौतिक तथा बौद्धिक सामाजिकता के लिए हमारी नर-नारी संबंधी सामंत युगीन मान्यताएँ अपर्याप्त तथा असंतोषकर लगती है। विकसित राग चेतना ही मानव संस्कृति की आधारशिला बन सकती है। पुरुष और नारी इस राग चेतना के अभिन्न तथा अनिवार्य अंग है।
प्रारंभ का अंश, जो इस संगीत रूपक के लिए आवश्यक है, मानव राग भावना के उद्दीपन की भूमिका स्वरूप है। उसमें प्रकृति की एकांत रमणीय कोड में एक नवयुवक, जो पुरुष की आत्मा का प्रतीक है, अनुभव करता है यह कि विश्व प्रकृति एक अनंत यौवना महिमामयी नारी के समान है, जिसकी शोभा ही उसके भीतर युवती की सुषमा में लिपटी हुई कामना का रूप धर कर, नवीन उषा की तरह उदित हो रही है। उसे निर्जन में कोयल का मधुर गीत सुनाई पड़ता है, जैसे उसके हृदय में सोई हुई कोई गोपन भावना जाग उठी हो और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हो। दूर से आता हुआ पपीहे का आकुल स्वर उसे आमंत्रित तथा आंदोलित करता है। उसमें एक प्रवेश है, प्रेम के लिए त्याग की वेदना है। उसकी सुप्त राग चेतना पिक तथा पपीहे के कंठों से प्रेरणा ग्रहण कर, प्रेम संबंधी विरह मिलन की व्यक्तिगत सीमाओं को अतिक्रम कर, व्यापक सामाजिक धरातल में प्रवेश करती है। इस रूपक में पिक मिलन और भोग का तथा पपीहा विरह और त्याग का प्रतीक है।
इसके बाद युवक राग भावना का आवाहन करता है, और ऐतिहासिक तथा सामाजिक धरातल पर, उसकी दृष्टि के सम्मुख, मानव राग भावना का विकास तथा परिणति, विभिन्न सांस्कृतिक युगों में विभिन्न रूप धरकर जैसे अनावृत अथवा अनवगुंठित हो उठती है। मध्ययुगीन राग भावना की प्रतिनिधि स्वरूप राम, कृष्ण, बुद्ध युग की अबलाएँ तथा आधुनिक युग की नारियाँ युवक के स्मृति पट में मूर्त होकर जैसे मानव राग चेतना के विकासक्रम की विविध झाँकियाँ प्रस्तुत करती है। इसमें यह ध्यान में रखने की बात है कि ये विविध झाँकियाँ अपने-अपने युगों के ह्रास की स्थिति का चित्रण करती हैं।
इस प्रकार विगत युगों की राग भावना का अपने मन में मूल्यांकन करता हुआ आज के नए युग का मानव राग भावना के अधिक विकसित तथा संतुलित स्वरूप का आवाहन करता है, जिससे पृथ्वी के जीवन में नर-नारियों के संबंधों की नवीन परिणति अपनी पिछली रागद्वेष, द्रोह-मोह की सीमाओं से मुक्त होकर, इस विराट् भू-जीवन का सक्रिय रचनात्मक अंग बन सके। नव युग के नर-नारी उसके कल्पना क्षितिज में अवतरित होकर देह बोध से ऊपर अपनी सृजनप्राण प्रेमभावना को जीवन मंगल तथा लोक कर्म के रूप में चरितार्थ करते हैं। गृहों की देहलियों की सीमाएँ लाँघकर राग चेतना विशाल सामाजिक प्रांगण में अपनी सार्थकता खोजती है। नवयुवतियाँ नवीन संस्कृति की संदेशवाहिका बन कर नवीन भावना के पुष्पों के रूप में नवीन सांस्कृतिक मूल्यों का वितरण करती है। भीतर से युक्त और बाहर से मुक्त नर-नारीगण नव जीवन की उल्लसित, नृत्य मुखर पदचापों से धरती के आँगन की शोभा संपन्न तथा आनंद गुंजरित करते हैं। दो शब्दों में यदि मैं कहूँ तो “मानसी” गीतिनाट्य में इसी मानव राग भावना का चिरंतन स्वरूप प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मानसी के सार्थक अंश चुन लिए गए हैं। इसका प्रारंभ वन में पपीहे की प्यासी पुकार से होता है जिसे सुनकर युवक की राग-भावना जग उठती है।
प्रेरणा
जैसा मैं प्रारंभ में कह चुका हूँ मानसी का रूपक मैंने दक्षिण भारत में लिखा था। मद्रास में जिस मकान के निचले हिस्से में मैं रहता था, वहाँ मकान-मालकिन की विदुषी लड़की का विवाहोत्सव देखने का अवसर मुझे मिला था। दक्षिण में स्त्रियों के चटकीले रेशमी वस्त्र अपनी विशेषता रखते हैं। अनेक रंगों की साड़ियों में उपस्थित अनेक संभ्रांत महिलाओं को, उस गीत-नृत्य मंत्रोच्चार से गुंजरित, फूलों से सज्जित विवाह-मंडप में देखकर यकायक मेरा ध्यान मानव राग भावना की क्रियाशीलता की ओर आकृष्ट हुआ। विवाह की संस्था को केंद्र बनाकर मेरे मन में जो भावनाएँ उठीं, उनको मैंने पीछे मानसी नामक इस रूपक में सँजोने की चेष्टा की।
मानसी नाम
मानसी नाम इस रूपक का मैंने इसलिए रखा कि मुझे प्रतीत हुआ कि राग भावना का सबसे सुंदर तथा विकसित छोर अभी जैसे मानव मन के ही भीतर अव्यक्त है। उसे जैसे बाहर समुचित परिस्थितियाँ पाकर अभी नवीन नरनारी के संबंधों के रूप में प्रस्फुटित होना है। उसी अव्यक्त राग-चेतना को मैंने मानसी नाम दिया है और अंतिम दृश्यों में उसे अवतरित कराने की चेष्टा भी की है।
गीत नाट्य रूपक
इस रूपक को मैंने गीतों में लिखना इसलिए उचित समझा कि प्रथमतः संगीत राग भावना को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त तथा हृदयस्पर्शी माध्यम है। गीत की लय वास्तव में मनोराग ही की लय है। नाट्य रूपक का रूप मैंने इसलिए देना उचित समझा कि जिससे अनेक नर-नारी अनेक प्रकार से रंगीन वस्त्रों में उपस्थित होकर अपने हाव-भाव तथा अभिनय के द्वारा राग भावना की आढ्यता तथा वैचित्र्य को दर्शकों के सामने मूर्तिमान कर सके। मानसी, भावना की दृष्टि से, सूक्ष्म होने के कारण इसे जीवंत स्थूल माध्यम द्वारा प्रकट करना आवश्यक था जिससे मेरे विचार अधिक संप्रेषणीय बन सके। इस रूपक में राम, कृष्ण और बुद्ध-युग की नारियों की रूप-सज्जा, हाव-भाव तथा आधुनिकाओं की वेश-भूषा और नवीतम नर-नारियों की आकृति प्रकृति स्वयं ही राग भावना के विकास क्रम की आँखों के सामने साकार करने में सहायता देती है। मेरा विचार है कि उपयुक्त संगीत तथा मंच सज्जा के साथ यह रूपक काफ़ी प्रभावोत्पादक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 277)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.