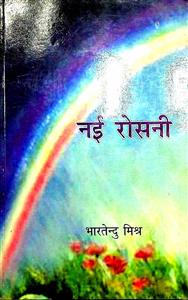पुस्तक: परिचय
भारतेंदु मिश्र ने जो एक नई रोशनी देखी है शोषितों में शोषण के ख़िलाफ़ उसे विस्तार मिलना ही चाहिए, मगर नक्सलवाद के रूप में कतई नहीं। यह बात साहित्य के विमर्श का केन्द्र होनी ही चाहिए भले ही वह अवधी का हो या हिन्दी, उर्दू, बंगला का। दलित विमर्श से कहीं कमतर तो नहीं है शोषितों का विमर्श। क्योंकि यथार्थ यह है कि धनबल बाहूबल पैदा कर ही देता है, और फिर शोषण का दौर चलता है। शोषित होने वाला कमज़ोर ही होता है। जाति या वर्ग तो गौण हो जाता है। कम से कम आज के परिवेश में तो यही हो रहा है। और जब तक यह होता रहेगा ‘नई रोसनी’ जैसी कृतियाँ भी भारतेंदु जैसे रचनाकार रचते ही रहेंगे। उनकी यह रचना निश्चित तौर पर अवधी ही नहीं किसी भी भाषा के बेहतर उपन्यासों में शुमार होने की काबिलियत रखती है। क्योंकि यह वातानुकूलित कमरों में बैठकर संगणक के संजाल या कहीं पर पढ़ी जानकारियों के आधार पर नहीं लिखा गया है। बल्कि लेखक ने उपन्यास के केन्द्र बिन्दु धांधी को लंबे समय तक बहुत करीब से देखा, जाना, जीया, अनुभव किया, फिर उससे तैयार उर्वरभूमि पर यह उपन्यास पैदा हुआ। जो यथार्थ दिखाता है। जिसमें शब्दों की बाजीगरी नहीं है, पढ़ते वक्त लगता है जैसे घटना का पुनर्नाट्यांतरण देख रहे हैं।