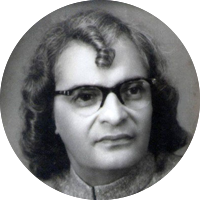पुस्तकें, जिनसे मैंने सीखा
pustken, jinse mainne sikha
मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह पुस्तकों से ही सीखें। पुस्तकों के अतिरिक्त और भी अनेकानेक साधन है, जिनसे मनुष्य शिक्षा प्राप्त कर सकता है और अपने भीतर सुरुचि, शील तथा उच्चतम संस्कारों को संचित कर सकता है। पुस्तकों की शिक्षा एक प्रकार से एकांगी शिक्षा है। हम प्रायः लोगों को कहते सुनते हैं कि अभी तुमने पढ़ा ही है, गुना नहीं। इससे यही ध्वनि निकलती है कि पुस्तकों की कोरी पढ़ाई को जीवन और स्वभाव का अंग बनाने के लिए और भी अनेक प्रकार को शिक्षाओं की आवश्यकता है, जिनमें सबसे प्रमुख स्थान शायद अनुभूति का है। वैसे भी सच्ची शिक्षा के लिए, जिससे कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास हो सके, पुस्तकों के अध्ययन मनन के साथ ही उपयुक्त वातावरण तथा संस्कृत व्यक्तियों का सहवास, जिसे सत्संग कहते हैं, अत्यंत आवश्यक है। जिनके बिना हम कोरे काग़ज़ी उपदेशों अथवा नैतिक सत्यों को अपने मन तथा स्वभाव का अंग नहीं बना सकते। महान् व्यक्तियों के उन्नत विचारों तथा महान् ग्रंथों के उत्तम आदर्शों को आत्मसात् कर उन्हें जीवन में परिणत करने के लिए यह भी नितांत आवश्यक है कि उन्हें अपने कार्यों एवं आचरणों में अभिव्यक्त करने के लिए हमें मनोनुकूल व्यापक सामाजिक क्षेत्र मिले। जिस देश या समाज में बाह्य परिस्थितियों, व्यक्तिगत राग-द्वेष तथा छोटे-मोटे स्वार्थों के कारण, मनुष्य की उन्नत आंतरिक प्रेरणाओं का विरोध करती हैं, वहाँ भी शिक्षा का परिपाक अथवा व्यक्तित्व का यथोचित विकास नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितियाँ केवल नाटे, बौने, ठिगने, कुबड़े व्यक्तियों को जन्म देकर रह जाती हैं।
स्वभाव से ही अत्यंत भाव-प्रवण तथा कवि होने के कारण मेरी रुचि पुस्तकों की ओर अधिक नहीं रही। मैंने व्यक्तियों के जीवन से, परस्पर के जनसमागम से तथा महान् पुरुषों के दर्शन एवं उनके मानसिक सत्संग से कहीं अधिक सीखा है, जिसे मैं सहज सीखना या सहज शिक्षा कहता हूँ। इससे भी अधिक मैंने प्रकृति के मौन मुखर सहवास से सीखा है। भावुक तथा संवेदनशील होने के कारण मेरे भीतर स्वभाव का अत्यधिक रहा है। स्वभाव का अंश, जिसमें अच्छा-बुरा, ऊँच-नीच, सबल तथा दुर्बल सभी कुछ रहा है और अत्यधिक रहा है। छुटपन से ही मैं सदैव अपने स्वभाव से उलझता रहा हूँ। अपने स्वभाव से संघर्ष करते रहने के कारण। मैं थोड़ा बहुत सीख सका हूँ, अपनी दुर्बलताओं तथा अपनी एकांत आकाक्षाओं का ध्यान मेरे भीतर बराबर बना रहा है। अपने को भूलकर आत्मविस्मृत होकर अपने चिंतन अथवा चिंता पुस्तकें, जिनसे मैंने सीखा के घेरे से बाहर निकलकर शायद ही मैं कभी आत्मविभोर-भाव से संसार के साथ रह सका हूँ। अगर किसी ने मुझे इस भावना से मुक्ति दी है, तो वह प्रकृति ने। प्रकृति के रूप को देखकर में अनेकानेक बार आत्म-विस्मृत हो चुका हूँ जैसे माँ-बच्चे को अपनाती है, वैसा प्रकृति ने मुझे अपनाया है। उसने मेरे चंचल मन को आकुल व्याकुलता को, जिसे मैं किसी पर प्रकट नहीं कर सका हूँ और न स्वयं ही समझ सका हूँ—अपने में ले लिया है। प्रकृति के मुख का निरीक्षण कर मेरे भीतर अनेक गहरी अनुभूतियाँ उतरी हैं। संसार के छोटे-मोटे संघर्षों तथा जीवन के कटु-तिक्त अनुभवों के परे उसने एक व्यापक पुस्तक को तरह खुलकर मेरे भीतर अनेक सहानुभूतियाँ, सांत्वनाएँ, स्नेह, ममत्व को भावनाएँ तथा अवाक् अलौकिक, अपने को भुला देने वाली, शक्तियों का स्पर्श अंकित किया है।
प्रकृति से मेरा क्या अभिप्राय है, शायद इसे मैं न समझा सकूँगा। अगर किसी वस्तु को बिना सोचे-विचारे, केवल उसका मुख देखकर, मेरे मन ने स्वीकार किया है, तो वह प्रकृति है। वह शायद मेरा ही एक अंग है, सबसे स्निग्ध, उज्ज्वल और व्यापक अंग, जिसके प्रशांत अंतस्तल में सब प्रकार के सद्-असद्, उच्च क्षुद्र, तथा सुख-दुःख अपने आप जैसे घुलमिलकर एकाकार हो जाते हैं। उसकी एकांत कोड में बैठकर मैं अपने को सबसे बड़ा अनुभव करता हूँ, जो अनुभूति मुझे और किसी के सम्मुख नहीं हुई है। छुटपन में दूसरों ने मुझे सदैव अतो विकृतियों, संकीर्णताओं, कठोरताओं, निर्दयताओं तथा ढिठाइयों से दबाने का प्रयत्न किया है। अशिष्ट, रुखाई तथा असभ्यता का सामना करने में अपने को अक्षर पाने के कारण मैं सदैव, दूसरों की अयोग्यता के सामने भी शंका विवश सिकुड़ कर रहा हूँ। किंतु प्रकृति ने अपने आँगन में मुझे सदैव खुल खेलने को उसकाया है। उसने मेरे अनेक मानसिक घावों को अपने प्रेम-स्पर्श से भर दिया है, मेरी अनेक दुर्बलताओं की प्रेरणाओं के प्रकाश से धोकर मानवीय बना दिया है। इस प्रकार जो सर्वप्रथम पुस्तक मुझे देखने को मिली, वह प्रकृति ही है।
फूल, चाँद, तारे, इंद्रधनुष और जगमगाते हुए ओसों से भरी इस रहस्यमयी प्रकृति के बाद—जिसका आनंद-संदेश मुझे साय-प्रातः पक्षी देते हैं—जिस दूसरे महान् ग्रंथ ने अपनी पवित्र मधुर छाप मेरे हृदय में अंकित की है, वह है बाइबिल का न्यू टेस्टामेट। बाइबिल भी उदार मधुर प्रकृति की तरह अनजाने ही अपने आप मेरे भीतर के जीवन का एक अन्य अंग बन गई। चिंतन और बौद्धिक व्यायाम को कठोरता से अछूती अंतरतम की सहज मर्मपूर्ण पुकार की तरह, बाइबिल, जैसे भागवत हृदय को, प्रेम-करुणा से भरी, पवित्र भावना को ज्योति प्रेरित वाणी है। वह आत्मा का शुष्क ज्ञान नहीं, आत्मा की भाव-विगलित कविता की कविता है। क्राइस्ट के अश्रुधौत, महत् त्यागपूर्ण मूर्तिमान प्रेम के व्यक्तित्व ने मेरे हृदय को मुग्ध कर दिया। दर्शन और मनोविज्ञान के नीरस तथ्यों से ऊबकर मेरा हृदय चुपचाप, शिशु के अखंड पवित्र विश्वास की तरह, सरल मधुर, वाइबिल की दिव्य लय में बँध गया। Look at the lilies of the field, how they grow कहने वाले महान् अंतर्द्रष्टा ने मेरे भीतर जीवन के स्वतः स्फूर्त सूक्ष्म अंत सौंदर्य का रहस्य खोल दिया। Resist not evil ने जैसे ईश्वरीय सत्य की अवश्यंभावी अंतिम विजय का संदेश मेरे मन में अंकित कर दिया। Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek: for they shall inherit the earth. जैसी सूक्तियों ने ईश्वर की अक्षय करुणा और प्रेम के न्याय के प्रति मेरे हृदय को अडिग विश्वास से भर दिया। इस क्षणभंगुर, रागद्वेष और कलह-कोलाहल के अंधकार के परदे को चीरकर सबसे पहले बाइबिल ने ही मेरे हृदय को ईश्वर की महिमा, स्वर्ग के राज्य तथा मानवता के भविष्य की ओर आकृष्ट किया। ‘ye are the salt of the earth, ye are the light of the world’ आदि वाक्यों ने मेरे मन की वीणा में एक अक्षय आशावादिता का स्वर जगा दिया। सब मिलाकर बाइबिल के अध्ययन ने संसार की अचिरता और ‘परिवर्तन’ के विवाद से भरे हुए मेरे अंतःकरण को एक अद्भुत नवीन विश्वास का स्वास्थ्य तथा अमरत्व प्रदान किया। अब भी बाइबिल को पढ़ने से उसी प्रकार भगवत्-प्रेम के अश्रुओं से धुला, आत्म-त्याग से पवित्र, जीवन के सात्विक सौंदर्य का जगत्, अपने मौन मधुर रूपरंगों के वैभव में मेरी मन की आँखों के सम्मुख प्रस्फुटित हो उठता है, जिसके चारो ओर एक अखंडनीय शांति का स्निग्ध वातावरण व्याप्त रहता है, जो दिव्य औषधि की तरह मन की समस्त क्लांति को मिटाकर उसे नवीन शक्ति प्रदान करता है।
बाइबिल के अतिरिक्त उपनिषदों के अध्ययन ने भी मेरे हृदय में प्रेरणाओं के अक्षय सौंदर्य को जगाया। ‘जग के उर्वर आँगन में बरसों ज्योतिर्मय जीवन का अत्यंत प्रकाशपूर्ण वैभव मेरे अंतर में उपनिषदों ने ही बरसाया है। उपनिषदों का अध्ययन मेरे लिए शाश्वत प्रकाश के असीम सिंधु में अवगाहन के समान रहा है। वे जैसे अनिर्वचनीय अलौकिक अनुभूतियों के वातायन है, जिनसे हृदय को विश्वक्षितिज के उस पार अमरत्व की अपूर्व झाँकियाँ मिलती है। अपने सत्यद्रष्टा ऋषियों के साथ चेतना के उच्च उच्चतम सोपानों में विचरण करने से अंतःकरण एक अवर्णनीय आह्लाद से ओतप्रोत हो गया। मन का कलुष और जीवन की सीमाएँ जैसे अमृत के झरनों में स्नान करने से एक बार ही धुलकर स्वच्छ एवं निर्मल हो गई। उपनिषदों का मनन करने से मन के बाह्य आधार नष्ट हो जाते हैं। उसकी सीमित कुंठित तर्क-भावना को धक्का लगता है और बुद्धि के कपाट जैसे ऊपर को खुल जाते हैं। मन एक ऐसे अतींद्रिय केंद्र में स्थित हो जाता है, जहाँ से वह साक्षी की तरह तटस्थ भाव से विश्व-जीवन के व्यापारों का निरीक्षण करने लगता है। उपनिषदों में भी ईशोषनिषद् ने नाविक के तीर की तरह मेरे मन के अंधकार को भेदने में सबसे अधिक सहायता दी है। ‘ईशावस्यमिदं सर्व यत्किच जगत्या जगत’ के मनन मात्र से ही जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और हृदय में जिज्ञासा जग उठती है कि किस प्रकार इस क्षणभंगुर संसार के दर्पण में उस शाश्वत के मुख का बिंब देखा जा सकता है। ईशोपनिषद् के विद्या और अविद्या के समन्वयात्मक दृष्टिकोण ने भी मेरे मन को अत्यंत बल तथा शांति प्रदान की।
उपनिषदों के अध्ययन के बाद जब मैंने टाल्सटाय की My Religion नामक पुस्तक पढ़ी, तो मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा और मुझे लगा कि जैसे प्रकाश से गिरकर मैं खाई मे पड़ गया हूँ। टाल्सटाय की विचारधारा पाप-भावना से ऐसी कुंठित तथा पीड़ित लगी कि उसके संपर्क में आकर मेरे भीतर गहरा विषाद जमा हो गया। उपनिषदों के उज्ज्वल, उन्मुक्त, अपापविद्ध ऊर्ध्वाकाश के वातावरण में साँस लेने वाले मन की गति जैसे श्रांति-क्लांति से शिथिल होकर निर्जीव पड़ने लगी। इससे उपनिषदों के ब्रह्मवाद का महत्त्व मेरे मन में और भी बढ़ गया। इस देशकाल नामरूप के सापेक्ष जगत् के परे जो सत्य का परात्पर शिखर है, जो द्वंद्वों में विभक्त इस जागतिक चेतना की सीमाओं से ऊपर और बुद्धि से प्रतीत है, वही परम मानवीय सत्य का आधार हो सकता है। देश, काल, परिस्थितियों के अनुरूप बदलती हुई सापेक्ष नैतिक तथा सामाजिक मान्यताओं की स्थापना का रहस्य भी वही है।
किंतु ‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो’ वाले उपनिषदों के सत्य में मन अधिक समय तक केंद्रित नहीं रह सका। मेरा स्वभाव फिर मुझसे उलझने लगा और मेरे मन में बार-बार यह जिज्ञासा उठने लगी कि यह सापेक्ष सत्य, जिसे माया कहते जो देश-काल के अनुरूप नित्य परिवर्तित होता रहता है, वह किन नियमों के अधीन है और उसे कौन-सी शक्तियाँ संचालित करती रहती हैं। मेरी इस जिज्ञासा की पूर्ति अनेक अंशों तक मार्क्सवाद कर सका। हमारी सामाजिक मान्यताओं का जगत् क्यों और कैसे बदलता है और उसमें युगीन समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है, इसका संतोषप्रद निरूपण, इसमें संदेह नहीं, केवल मार्क्सवाद ही यथेष्ट रूप से करा सकता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की तर्कप्रणाली हमारा परिचय उन नियमों से कराती है जिनके बल पर मानवीय सत्य का छिलका अथवा सामाजिक जीवन का ढाँचा संगठित होता है। वह मानव-जीवन-सिंधु के उद्वेलन-आलोड़न का, सामाजिक उत्थान-पतन तथा सभ्यता के प्रगति विकास का इतिहास है। मानव जीवन के इस समतल संचरण के वृत्त को मैंने अपनी ‘युगवाणी’ तथा ‘ग्राम्या’ में वाणी देने का प्रयत्न किया है।
किंतु पुस्तकों के अध्ययन के अतिरिक्त मानव जीवन के अध्ययन तथा मानव—स्वभाव के संघर्ष की अनुभूतियों से मैं जिन परिणामों पर पहुँचा हूँ, उनसे मुझे प्रतीत होता है कि मानव विकास की वर्तमान स्थिति में हमे मानव जीवन के सत्य को उसके आध्यात्मिक तथा भौतिक स्वरूप में पहचानने के बदले, उसे विश्वव्यापक सांस्कृतिक स्वरूप में पहचानने तथा अभिव्यक्ति देने की आवश्यकता है, जिससे उसके आध्यात्मिक तथा भौतिक जीवन के अंतर्विरोध नवीन जीवन-सौंदर्य को भावना में समन्वित हो सके। इस सांस्कृतिक सौंदर्य को भावना ही में मैं नवीन मनुष्यत्व एवं मानवता की भावना को अंतहित पाता हूँ, जो धर्म और काम के बीच, और विश्व के बीच, स्वभाव और नैतिक कर्तव्य के बीच, ऐहिक और पारलौकिक के बीच एक सुनहली पुल की तरह झूलती हुई मुझे दिखाई देती है, जिसमें मानव जाति को प्रगति तथा विकास अपने अंतरराम संगीत को लय में बँधे हुए युग-युग तक अविराम चरण धरते एवं आगे बढ़ते हुए जीवन की असीमता तथा शाश्वतता का प्रमाण देकर ईश्वर की आनंद-लीला को सार्थक करते जाएँगे। एवमस्तु।
- पुस्तक : शिल्प और दर्शन द्वितीय खंड (पृष्ठ 184)
- रचनाकार : सुमित्रा नंदन पंत
- प्रकाशन : नव साहित्य प्रेस
- संस्करण : 1961
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.