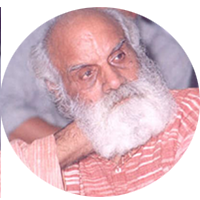निराला की नई कविता
nirala ki nai kavita
निराला जी की नई कविता से अभिप्राय उनकी उन कविताओं से है जो '39 के बाद की हैं। ये कविताएँ उनके चार संग्रहों में उपलब्ध हैं—अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते। इन्हीं चारों पुस्तकों के आधार पर यह लेख लिखा जा रहा है।
निराला जी की नई कविताएँ उनकी पुरानी कविताओं से अनेक बातों में भिन्न हैं, पुरानी कविताओं में भाव, भाषा और छंद का जैसा निर्वाचन है, नयी कविताओं में नहीं है। विषय को भी इधर उन्होंने व्यापक बनाया है। भाषा भी सामान्य बोलचाल की रखी है।
यह सब अकस्मात् नहीं घटित हुआ है। धीरे-धीरे निराला जी की शैली में परिवर्तन हुआ। यद्यपि उनके परिवर्तन-क्रम को चाणाक्ष जन नहीं लक्ष्य कर पाए तथापि उनके पूर्वरचित साहित्य में ही उनके वर्तमान साहित्य का चिह्न मिलता है। भाषा की सरलता उनकी पहली कविताओं में भी मिलती है—
रे, कुछ न हुआ तो क्या
जग धोका तो रो क्या
सब छाया से छाया
नभ नीला दिखलाया
तू घटा और बढ़ा
और गया और आया
होता क्या फिर हो क्या
चलता तू थकता तू
रुक रुक फिर बकता तू
कमज़ोरी दुनिया हो तो
कह क्या सकता तू
जो धुला उसे धो क्या
(गीतिका)
वस्तु-विषय की दृष्टि से भी निराला जी ने कोई सर्वथा नूतन समारंभ नहीं किया है—
छोड़ दो जीवन यों न मलो
ऐंठ अकड़ उसके पथ से तुम
रथ पर यों न चलो
वह भी तुम ऐसा ही सुंदर
अपने दुख-पथ का प्रवाह खर
तुम भी अपनी ही डालों पर
फूलो और फलो
मिला तुम्हें, सच है, अपार धन
पाया कृश उसने कैसा तन
क्या तुम निर्मल वही अपावन
सोचो भी सँभलो
जग के गौरव के सहस्र दल
दुर्बल तालों ही पर प्रतिपल
खिलते किरणोज्वल चल अचपल
सकल अमंगल खो
वहीं विटप शत वर्ष पुरातन
पीन प्रशाखाएँ फैला घन
अंधकार ही भरता क्षण क्षण
जन भय भावन हो
'39 से पहले की रचनाओं में भी निराला जी का दृष्टि-बिंदु सुनिश्चित और स्वच्छंद पाया जाता है। उनकी तत्कालीन रचनाओं में एक प्रकार की तटस्थ वृत्ति पाई जाती है। इसी तटस्थ वृत्ति के कारण निराला जी की रचनाओं में समाज के लिए कोई विशेष उद्बोधन नहीं पाया जाता। इसके विपरीत नयी कविताओं में वे बहुत स्पष्ट और लक्ष्योन्मुख दिखाई देते हैं।
इसमें संदेह नहीं कि निराला जी ने जब कभी कुछ कहा है एक नए सुर, एक नई शैली से कहा है। उन्होंने अपने ही निर्मित मार्ग का अनुसरण नहीं किया है। इस प्रकार वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ स्वरानुसन्धित्सु कवि हैं।
निराला जी की नई कविताओं की सर्वप्रमुख विशेषता उनका हास्य और व्यंग्य है। हास्य और व्यंग्य की प्रवृत्ति भी उनकी नई नहीं है। बहुत पहले 'सरोज स्मृति' शीर्षक शोक कविता में भी उन्होंने इसका प्रयोग किया है।
ये कान्यकुब्ज कुल कुलांगार
खाकर पत्तल में करें छेद
इनके कर कन्या, अर्थ खेद
पद फटे बिवाई के, उधार
खाए के मुख ज्यों पिए तेल
चमरौंधे जूते से सकेल
निकले जी लेते थोर गंध
उन चरणों को मैं यथा अंध
कल घ्राण-प्राण से रहित व्यक्ति
हो पूजूँ, ऐसी नहीं शक्ति
ऐसे शिव से गिरिजा विवाह
करने की मेरी नहीं चाह
निराला जी ने हास्य और व्यंग्य का पहले गद्य में ही उन्मुक्त व्यवहार किया था। पद्य में उन्होंने इसका प्रयोग '89 के बाद से ही पुष्कल मात्रा में करना प्रारंभ किया।
हिन्दी में हास्य और व्यंग्य का पद काव्य में अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। हास्य और व्यंग्य का प्रयोग अधिकतर महाकाव्यों में एकरसता को खंडित करने के लिए किया जाता रहा है। छोटी कविताओं में आंशिक या पूर्ण रूप से हास्य का प्रयोग ही पाया जाता है। हास्य और व्यंग्य लेखन की ओर लेखकों की सम्मान-दृष्टि भी कम ही रहती है।
निराला जी ने चली आती हुई रूढ़ि के प्रति थोड़ी-सी अनुरक्ति नहीं दिखाई। इसी कारण निराला जी को सबसे अधिक विरोध का सामना भी करना पड़ा। बहुत पहले निराला जी ने कहा था—
जला दे जीर्ण शीर्ण प्राचीन
क्या करूँगा तन जीवनहीन
'जीर्ण शीर्ण जीवनहीन प्राचीन' के प्रति निराला जी के मन में कोई मोह नहीं है। इसी कारण वे आज जीवन की इस ढलती बेला में भी नव-नवीन बने हुए हैं।
निराला जी की नई कविताएँ शैली के विचार से कुल तीन श्रेणियों में विभक्त की जा सकती हैं—
1. पुरानी शैली की कविताएँ
2. नई शैली की कविताएँ
3. हास्य और व्यंग्य की कविताएँ
पुरानी शैली की कविताएँ अधिकतर निराला जी की पूर्व प्रकाशित कविताओं के आदर्श की हैं। ‘परिमल’, ‘गीतिका’, ‘अनामिका’ और ‘तुलसीदास’ में जिस भाव और संस्कार-संपदा का संचय किया गया है, पुरानी शैली की नई कविताओं में उसका साधर्म्य पाया जाता है। यद्यपि निराला जी हिन्दी-काव्य में बौद्धिकतापूर्ण नई चेतना के संचारक रहे हैं तथापि उनकी रचनाओं में एक भावात्मक तरलता पाई जाती है। यह एक ऐसी विशेषता है जो केवल निराला जी में ही वर्तमान है।
पुरानी शैली की कविताएँ दो प्रकार की हैं। पहले प्रकार में तो ऐसी रचनाएँ हैं जो भाषा में काव्यप्रकृति की विशेषता से युक्त हैं। दूसरे प्रकार में ऐसी कविताएँ हैं जिनके स्वर और रूपगठन पर गद्य का प्रभाव है। इसको पुरानी शैली के अन्तर्गत रखने का यह कारण हैं कि इसमें भी कल्पना का वही वैभव है जो पुरानी शैली की रचनाओं में।
इस प्रकार की रचनाएँ वस्तुविचार की दृष्टि से पाँच प्रकार की हैं—
1. आत्मनिवेदनपरक
2. समाज समीक्षापरक
3. व्यक्ति संवर्द्धनापरक
4. वातावरणपरक
5. देशपरक
आत्मनिवदेनपरक कविताएँ अधिकतर रहस्यवाद की परंपरा में आती हैं। परोक्ष सत्ता पर निराला जी का विश्वास बना हुआ है, इसी कारण उनकी अधिकांश रचनाओं में एक प्रकार का रहस्य-संकेत वर्तमान है। कहीं-कहीं तो लोकसुलभ सत्यों को भी उन्होंने एक दुर्लभ रहस्य से आवृत करके उपस्थित किया है। भावमूलक कविताओं में निराला जी ने प्रायः रहस्य का आश्रय लिया है। यह रहस्य भी कई प्रकार का पाया जाता है। कहीं वस्तुगत, कहीं विषयगत और कहीं केवल पात्रगत।
इस प्रकार की रचनाओं के निराला जी अभ्यस्त हो गए हैं। प्रायः उनका अंतर्हृदय रहस्यवाद की तरंगों से गतिशील रहता है। जब कभी उनकी वृत्ति अन्तर्मुखी हुई और उन्होंने भावलिपि के लिए स्वरसंधान किया तब पुरानी शैली की रचनाएँ उद्गीरित हो जाया करती हैं।
नूपुर के सुर मंद रहे
जब न चरण स्वच्छंद रहे
उतरी नभ से निर्मल राका
पहले जब तुमने हँस ताका
बहुविध प्राणों को झंकृत कर
बजे छंद जो बंद रहे
नयनों के ही साथ फिरे वे
मेरे घेरे नहीं घिरे वे
तुमसे चल तुममें ही पहुँचे
जितने रस आनंद रहे
उद्धृत कविता काव्य-परंपरा का निर्वाह करती है। एक दूसरी कविता देखिए जो वर्णन और विषय-निर्देशन में तो पुरानी शैली के पास है किंतु रूप-गठन में स्वतंत्र है—
स्नेह निर्झर बह गया है
रेत ज्यों तन रह गया है
आम की यह डाल जो सूखी दिखी,
कह रही है- 'अब यहाँ पिक या शिखी
नहीं आते, पंक्ति मैं वह हूँ लिखी
नहीं जिसका अर्थ—
जीवन दह गया है।'
'दिए हैं मैंने जगत् को फूल फल
किया है अपनी प्रभा से चकित चल;
पर अनश्वर सकल पल्लवित पल—
ठाट जीवन का वही-
जो ढह गया है।'
अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा
श्याम तृण पर बैठने को, निरुपमा
बह रही है हृदय पर केवल अमा,
मैं अलक्षित हूँ, यही—
कवि कह गया है।
इस कविता में आम की सूखी डाल के सहारे कवि ने अपना प्रिय जीवनदर्शन व्यक्त किया है। अंतिम बंद में रहस्य व्यंजक शब्दों का भी प्रयोग है। वे शब्द हैं 'पुलिन', 'श्याम तृण', 'निरुपमा'।
समाज-समीक्षा संबंधी कविताएँ कहीं तो सामान्य उपदेश के रूप में मिलती हैं और कहीं जीवन की परिस्थिति विशेष का आकलन कर विशिष्ट रूप में। निराला जी एक कविता में वर्तमान सामाजिक जीवन को 'गहन अंध कारा' कहते हैं—
गहन है यह अंध कारा
स्वार्थ के अवगुंठनों से
हुआ है लुंठन हमारा
खड़ी है दीवार जड़ की घेरकर
बोलते हैं लोग ज्यों मुँह फेरकर
इस गगन में नहीं दिनकर .
नहीं शशधर नहीं तारा
इसमें कवि ने स्वार्थ को ही सामाजिक विभेदों की वस्तुस्थिति कहा है।
व्यक्ति-संवर्द्धनापरक कविताओं में निराला जी ने 'रविदास', 'शुक्ल जी', 'प्रसाद जी', 'बुद्ध', 'विजयलक्ष्मी पंडित', 'महादेवी वर्मा' के प्रति लिखा है। इन सभी कविताओं में निराला जी का जीवनदर्शन व्यक्त हुआ है। प्रसाद जी पर लिखित कविता बहुत कुछ निराला जी का स्वकीय भावचित्र हो गई है—
उठा प्रसंग प्रसंगांतर रंग-रंग से रंगकर
तुमने बना दिया है वानर को भी सुंदर
किया मूक को मुखर, लिया कुछ, दिया अधिकतर
पिया गरल पर किया जाति-साहित्य को अमर
तुम वसंत से मृदु, सरसी के सुप्त सलिल पर
मंद अनिल से उठा गए हो कंप मनोहर
कलियों में नर्तन, भौरों में उन्मद गुंजन
तरुण-तरुणियों में शतविध जीवन-व्रत-भुंजन
स्वप्न एक आँखों में, मन में लक्ष्य एक स्थिर
पार उतरने की संसृति में एक टेक चिर
बुद्ध पर लिखित उनकी कविता विज्ञान की वर्तमान विभीषिकाओं की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इसमें निराला जी की अन्तःप्रकृति का भी अंकन हो गया है, जिससे उनका अन्तःविराम प्रकट होता है।
निराला जी की कविताएँ इतनी सांग और परस्पर अविच्छेद्य भावों की होती हैं कि उनका कोई एक अंश उद्धृत करना पूरी कविता के साथ अन्याय जान पड़ता है। फिर भी आलोचक को सब कुछ प्रिय-अप्रिय करना पड़ता है।
वातावरण को निराला जी कितनी संजीवनी दे सकते हैं, देखिए—
आ रही याद
वह विजय शकों से अप्रमाद
वह महावीर विक्रमादित्य का अभिनंदन
वह प्रजाजनों का आवर्तित स्यंदन-वंदन
वे सजी हुई कलशों से अकलुष कामिनियाँ
करतीं वर्षित लाजों की अंजलि भामिनियाँ
तोरण-तोरण पर
जीवन को यौवन से भर
उठता सस्वर
मालकौंस हर
नश्वरता को नवस्वरता दे करता भास्वर
ताल-ताल पर
नागों का बृंहण, अश्वों की ह्रेषा
भर-भर
रथ का घर्घर,
घंटों की घनघन
पदातिकों का उन्मद पद पृथ्वी-मर्दन
देशपरक भावना उनकी प्रायः सभी कविता में मिल जाएगी। निराला जी अधिकतर देश को ज्ञान रूप में ही देखना पसंद करते हैं—
उठी नहीं तलवार
देश की पराजय को
वही हैं सहस्र धार
मुक्ति यहाँ से क्षय को
मृत्यु के जड़त्व के;
नहीं यहाँ थे ग़ुलाम,
देश यह वही जहाँ,
जीते गए क्रोध-काम
नई शैली की कविताएँ निराला जी की वे कविताएँ हैं जो छंद और भाषा की दृष्टि से एक नूतन भावलोक की सृष्टि करती हैं। ये कविताएँ कुछ तो फ़ारसी छंदों में हैं और कुछ उनके पूर्व प्रयुक्त मुक्त वृत्त का नवविकसित रूप हैं।
निराला जी की ये रचनाएँ कम पसंद की गई हैं। लेकिन इन नई कविताओं में भी उन्होंने अपना पूर्व काव्य-वैभव ही दिखाया है। इन कविताओं के भी वस्तु-विषय के विचार से उतने ही भेद किए जा सकते हैं जितने पुरानी शैली की कविताओं के किए गए हैं। यहाँ उन्हें दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं।
भाषा की सरलता का आरंभ लगभग 39 से हुआ। हिन्दी में '39 के पहले अधिकतर दुर्बोध्य रचनाएँ की जाती थीं। लेकिन '39 से कवियों और लेखकों की दृष्टि सरलता की ओर गई। लेखकों ने अपने को जनता और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी समझा। फलतः भाषा और साहित्य लोक जीवन के निकट आए। यद्यपि अभी साहित्य जीवन के समानांतर नहीं चल रहा है फिर भी चेष्टाशीलता स्पष्ट है। सभी बड़े कवियों ने सिंहासन छोड़कर जनपथ पर विचरण प्रारंभ किया। इसका भविष्य अधिक आशाप्रद है। जब जीवन और साहित्य एक-दूसरे के पूरक हो जाएँगे तब राष्ट्र की शक्ति का विकास होगा। निराला, पंत, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, सुमन, बच्चन और केदारनाथ अग्रवाल जैसे युगचेता भावयोगी कवि अपनी संपूर्ण प्राणशक्ति से देश की मनःशक्ति का उद्बोधन कर रहे हैं। नयी कविताओं में उनकी पूर्ववर्ती कला की छाप है। उन कविताओं की संख्या बहुत थोड़ी है जिनमें भाव और भाषा की नवीनता उपस्थापित की गई है। जीवन-उत्पल के एक उत्कल पल (वर्ष) का सांग चित्र देखिए—
उठकर छवि से आता है पल
जीवन के उत्पल का उत्कल
वर्षा की छाया की मर्मर,
गूंजी गणिका, ध्वनि, भाव सुघर
आशा की लंबी पलकों पर
पुरवाई के झोंके प्रति पल।
पंकज के ईक्षण शरद हँसी;
भू-भाल शालि की बाल फँसी;
वह चला सलिल, खुल चली नसी;
सीझे दल इधर पसीजे फल।
कुंद के दुग्ध के नयन लुब्ध;
विपरीत, शीत के भास क्षुब्ध;
व्यय के अर्जन के, अर्थ मुग्ध;
फूलों से फल, तरु से वल्कल।
नैष्पत्र गया पल्लव वसंत
आया कि मुस्कुराया दिगंत
यौवन की लाली भरी, हंत,
किसलय की कल चितवन चलदल
खेती का, खलिहानों का सुख
ग्रीष्म का खुला ज्योति से सुमुख
आकांक्षा का कुसुमित किंशुक
निर्मल मणिजल सलिला निस्तल
निराला जी की व्यंजनाओं में और अधिक सफ़ाई आ गई है। कहीं शायद ही शैथिल्य मिले। उपमाएँ प्रायः मर्मग्राही हैं—
प्रभु के नयनों से निकले कर
ज्योति के सहस्रों कोमल शर
समाज की वर्तमान दुरवस्थाओं को उन्होंने आँख ओझल नहीं होने दिया है—
भीख माँगता है अब राह पर
मुट्टी भर हड्डी का यह नर
एक जगह कवि विजय और विजयी का रहस्योद्घाटन करते हैं—
खुला भेद विजयी कहाए हुए जो
लहू दूसरों का पिए जा रहे हैं
निराला जी ने आँसुओं का मोह कभी नहीं किया। इसीलिए आज वे कहते हैं—
आँखों के आँसू न शोले बन गए तो क्या हुआ
काम के अवसर न गोले बन गए तो क्या हुआ
सामाजिक विषमताओं का निराला जी उपचार बताते हैं—
भेद कुल खुल जाए वह
सूरत हमारे दिल में है
देश को मिल जाए जो
पूँजी तुम्हारी मिल में है
निराला जी देश की दुर्दशाओं का उपचार स्पष्ट रूप से लिखते हैं—
सारी संपत्ति देश की हो
सारी उत्पत्ति देश की बने
जनता जातीय वेश की हो
वाद से विवाद यह टने
काँटा काँटे से कढ़ाओ
निराला जी बहुत पहले से मनुष्यता के कवि-गायक हैं। उसी धारा के अनुकूल वे कहते हैं—
प्रतिजन को करो सफल
जीर्ण हुए जो यौवन,
जीवन से भरो सकल
***
रँगे गगन, अंतराल,
मनुजोचित उठे भाल,
छल का छुट जाए जाल
देश मनाए मंगल
मुक्त वृत्त में इधर उन्होंने बहुत स्वच्छंद प्रयोग किए हैं। इन मुक्त वृत्तों को उन्होंने गद्य के बहुत पास ला दिया है। अधिकतर तो इनमें राग-तत्त्व का अभाव ही दिखाई देता है। हाँ, पाठ-वैशिष्ट्य अवश्य है। लेकिन केवल एक पाठ-वैशिष्ट्य क्या काव्यत्व के लिए पर्याप्त है? 'कुत्ता भौंकने लगा', 'झींगुर डटकर बोला', 'छलाँग मारता चला गया', 'डिप्टी साहब आए', 'वर्षा', 'महगू महँगा रहा', ऐसी ही कविताएँ हैं।
इन कविताओं पर सूक्ष्म विचार फिर कभी करेंगे पर अभी इतना ही कहेंगे कि इनमें पाठ-वैशिष्ट्य है। कहीं-कहीं स्वरों के सम-संचार से राग-तत्त्व का भी उद्रेक किया गया है लेकिन फिर धारा व्याहत होती है। गद्य-पद्य दोनों का सार संग्रह करके निश्चय एक नई छंद शैली की सृष्टि हो सकती है। इन कविताओं में बहुत कुछ इन्हीं बातों का प्रयत्न पाया जाता है 'कुत्ता भौंकने लगा' रेखाचित्र है। उसमें वातावरण के रंग को गहराई से आँका गया है। कविता का अंत यों होता है—
कौड़े से कुछ हटकर
लोगों के साथ कुत्ता खेतिहर का बैठा था,
चलते सिपाही को देखकर खड़ा हुआ,
और भौंकने लगा
करुणा से बंधु खेतिहर को देख-देखकर अंतिम पंक्ति में स्पष्ट ही ग्राम्योत्प्रेक्षा है। उसमें और कुछ ढूँढ़ना ठीक न होगा।
हास्य और व्यंग्य की कविताएँ इतनी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हो चुकी हैं कि उन पर कुछ कहना ठीक नहीं। 'कुकरमुत्ता', 'खजोहरा', 'रानी और कानी', 'मास्को डायलाग्स', 'गर्म पकौड़ी', 'प्रेम संगीत' ख्याति प्राप्त रचनाएँ हैं। इनका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। इनकी विशेषताओं को प्रकट करने के लिए यहाँ उचित स्थान भी नहीं है।
'स्फटिक शिला', की ताल लय बहुत मर्यादित है। इसमें हास्य और व्यंग्य की भी पुट है। गाँववालों के पारस्परिक द्वेषों का भी प्रसंग-वश निदर्शन है—
कच्चा चबूतरा मिला,
कुछ राह घेरे हुए। पत्थर एक रक्खा था,
महादेव की जगह पर। भाव मगर पक्का था—
दखल जैसे जमाना चाहता था कोई अपना
सत्य को जो बनाए हुए था वहाँ कल्पना
'ख़ुशख़बरी' और 'आँख आँख का काँटा हो गई', 'राजे ने अपनी रखवाली की' कविताएँ अर्थगांभीर्यपूर्ण हैं।
निराला जी की भाषा पर अंत में कुछ अवश्य कहूँगा।
निराला जी ने सरलता के लिए प्रचलित पारिभाषिक शब्दों तक का त्याग कर दिया है। यह कहाँ तक उचित है, विचारणीय है। एक उदाहरण दे रहे हैं। 'चरखा चला' कविता से निम्न पंक्तियाँ ली गई हैं—
वेदों का चर्खा चला,
सदियाँ गुज़रीं
लोग-बाग बसने लगे
फिर भी चलते रहे।
इसमें चलते रहे', का अर्थ 'विकास करते रहे' लेना होगा। इसी प्रकार 'बसने लगे' का अर्थ 'व्यवस्थित होने लगे' (नगरों और गाँवों में)। उक्त पदावली अपना सामान्य स्वतंत्र अर्थ रखती है, नया अर्थ उसके लिए दुर्वह है।
छंदों के विषय में भी एक बात। छंदों पर निराला जी का अधिकार असाधारण है। फिर भी 'प्रसाद जी के प्रति' कविता में छंदः प्रमाद हो गया है। पूरी कविता रोला छंदों में है। केवल छः पंक्तियाँ भिन्न हैं—
अपनी ही आँखों का तुमने खींचा प्रभात
अपनी ही नई उतारी संध्या अलस गात
तारक नयनों की अंधकार कुंतला रात
आई, सुरसरि-जल-सिक्त मंद मृदु बही वात
कितनी प्रिय बातों से वे रजनी-दिवस गए कट
अंतराल जीवन के कितने रहे, गए हट
अंत में हम कवि की पंक्तियों से ही उसकी संवर्द्धना करते हुए लेखनी को विश्राम देते हैं—
तुमने जो दिया दान, दान वह
जनता का जन-ताका ज्ञान वह
सच्चा कल्याण वह अथच है।
- पुस्तक : हंस (पृष्ठ 512)
- रचनाकार : त्रिलोचन
- संस्करण : 1946
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.